गीता के अनुसार कर्मयोग क्या है?
On

डॉ. आचार्या साध्वी देवप्रिया
महिला मुख्य केन्द्रीय प्रभारी
पतंजलि योग समिति
‘कर्म-योग’गीता का अपना ही एक स्वतन्त्र शब्द है, पूरे विश्व के चिंतन को यह गीता की अपनी ही देन है, ‘कर्म-योग’की इसी देन के कारण गीता आज भी विश्व को वैसा ही नवीन संदेश दे रही है जैसा नवीन संदेश इसने कुरुक्षेत्र की रण-भूमि में हथियार फेंक कर निराश खड़े हुए अर्जुन को दिया था। जीवन के रण-क्षेत्र में खड़े हुए अर्जुन को दिया था। जीवन के रण-क्षेत्र में खड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अर्जुन है। प्रत्येक के सम्मुख जीवन की कठोर विषम परिस्थितियाँ उठ खड़ी होती हैं। हममें से प्रत्येक इन विषम परिस्थितियों में अपने हथियार फेंक कर निराशा का करुण-क्रन्दन करने लगता है। गीता के ‘कर्म-योग’ ने गाण्डीव फेंक कर पलायन करने वाले अर्जुन को ‘कर्म-योग’का उपदेश देकर फिर से रण-भूमि में ला खड़ा किया था, वही ‘कर्म-योग’का उपदेश हमें भी निराशा से आशा के जगत् में लाकर खड़ा कर सकता है। प्रश्न है कि वह ‘कर्म-योग’,जिसने निराश हृदय में आशा का संचार किया, जिसने निर्बल को सबल, भयग्रस्त को साहसी, कर्म-संन्यासी को कर्म-योगी बना दिया, क्या है? कर्मयोगी बनने में क्या-क्या कठिनाइयाँ आती है उसका चिन्तन करते हैं।
तमोगुणी कहता है कि फल मिलेगा तो कर्म करूँगा, नहीं तो कर्म ही नहीं करूँगा, रजोगुणी कहता है कर्म तो अवश्य करूँगा, परन्तु फल पर अपना अधिकार जरूर रखूँगा। सत्त्वगुणी व्यक्ति का दृष्टिकोण ही कर्मयोग का दृष्टिकोण है, इसमें पहली दोनों दृष्टियों का समन्वय हो जाता है, इसमें तमोगुणी की तरह कर्म छोड़ा भी नहीं जाता, रजोगुणी की तरह फल पर अधिकार भी नहीं रखा जाता। कर्मयोग के इसी मार्ग को ‘निष्काम-कर्म’कहते हैं। गीता का कहना है कि बुद्धिमान् व्यक्ति को फल के प्रति आसक्ति छोडक़र ही कर्म करना चाहिये। क्या हम देखते नहीं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में है ही नहीं। हम खेती करते हैं, यह हमारे हाथ में है, परन्तु वर्षा के न होने से खेती सूख जाती है, ओले पडऩे से हरे-भरे खेत नष्ट हो जाते हैं, जानवर खेती को तबाह कर देते हैं, फल हमारे हाथ में कहाँ है? हमारे हाथ में तो है ही ‘कर्म’करना, ‘फल’हमारे हाथ में कहाँ? जब है ही नहीं, तब हम फल के प्रति आसक्ति पर अपनी शक्ति का अपव्यय क्यों करें? गीता हमें यथार्थ स्थिति को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। गीता का कहना है कि कर्म करते हुए फल पर अधिकार न रखना ही जीवन के प्रति ‘यथार्थ-दृष्टि’(Realistic Outlook) है, क्योंकि हम भले ही फल चाहते रहें, पर उस पर हमारा अधिकार नहीं है।‘कर्म-योग’ का यह अर्थ तो है कि हम फल के प्रति अनासक्त रहें, इसका यह अर्थ नहीं है कि हम फल की आशा ही न करें या यह समझने लगें कि फल होगा ही नहीं। ‘कर्म’ किया है तो उसका फल तो होगा ही। यह कैसे हो सकता है कि हम कर्म करें और फल की आशा न करें? यह तो कार्य-कारण के नियम पर कुठाराघात होगा। ‘कर्म’ करने के बाद ‘फल’ की आशा तो करनी ही होगी, परन्तु फल पर ‘अधिकार’ नहीं करना होगा, उस पर ‘आसक्ति’ नहीं रखनी होगी, उसके लिए मन में ‘लगाव’ नहीं रखना होगा। ‘कर्म-योग’ का अर्थ कर्म के फल की आशा का त्याग नहीं, अपितु कर्म के फल पर अधिकार का, आसक्ति का, लगाव का त्याग है। निष्काम-कर्मी के कर्म का फल सकाम-कर्मी के कर्म के फल से सौ गुना ज्यादा मिलता है, परन्तु वह उस पर अपना अधिकार नहीं समझता। आचार्य विनोबा भावे का कहना है कि निष्काम-कर्म स्वत: एक फल है इसलिए निष्काम-व्यक्ति किसी अन्य फल की तरफ नहीं देखता, फल पर फल क्या लगेगा? निष्काम-कर्म स्वत: फल कैसे है? चित्रकार जब चित्र बनाता है तब अगर कोई उसे कहे कि चित्र मत बनाओ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम देंगे, तो क्या वह चित्र बनाना छोड़ देगा? कवि को कहो कि कविता न करे, कविता के बदले पैसे ले लो, तो क्या वह पैसे लेकर कविता करना छोड़ देगा?
चित्रकार चित्र बनाता है, कवि कविता करता है, वे इसे अपना ‘कर्म’ समझकर करते हैं, किसी फल की आसक्ति से नहीं, इसीलिए पैसे के लिए चित्र बनाने वाले की अपेक्षा चित्र के लिए चित्र बनाने वाला, पैसे के लिए कविता करने वाले की अपेक्षा कविता के लिए कविता करने वाला ज्यादा मग्न रहता है। इनका अपने काम में मग्न रहना ऐसा ही है जैसे सूर्य का चौबीसों घण्टे संसार में प्रकाश फैलाना, चाँद का चाँदनी बिखेरना, आकाश का जल बरसाना और हवा का शीतल प्रवाहमान बहना। इस प्रकार के निष्काम-कर्म के सम्मुख सकाम-कर्म अपने-आप तुच्छ बन जाता है।
‘सर्वभूतहिते रता:’-प्राणिमात्र के साथ आत्मौपम्यभाव, अपनी तरह से बरतना, दूसरों के स्वार्थ में अपना स्वार्थ देखना, अपने हित में, अपने कल्याण में लगे रहने के स्थान में सब के कल्याण में अपने को खपा देना। जिसको भगवान् ही भगवान् सब जगह दिखाई देता है, वह जब सब जगह सम-बुद्धि से देखेगा तब उसे सब जगह एक ही तत्व दिखलाई देगा, दूसरा तत्व दिखेगा ही नहीं। वह जहाँ दु:ख देखेगा, रोग देखेगा, अकल्याण देखेगा, उसी को दूर करने में वह जुट जायेगा क्योंकि मानवमात्र का दु:ख उसका दु:ख है।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।। गीता 2.47।।
कर्त्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, कर्मत्याग में नहीं। कर्त्तव्य कर्मों के करते हुए भी उनके फलों में तेरा अधिकार नहीं है, उन्हें भी फलासक्ति रहित होकर ही करना है। ऐसा करते हुए तू कर्मफल का हेतु नहीं बनेगा, क्योंकि फलासक्ति के साथ किया गया कर्म ही बन्धनकारक कर्मफल का हेतु बनता है।
योगस्थ: कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय।
सिद्ध्यसिद्ध्यो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।। गीता 2.48।।
दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय।
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा: फलहेतव:।। गीता 2-49।।
हे धनञ्जय! पदार्थों व विषयों में आसक्ति छोडक़र योग में स्थित होकर अर्थात् समत्व में रहकर कर्म की सिद्धि या असिद्धि को समान मानकर अपना कर्म कर। कर्म की सफलता या असफलता दोनों ही अवस्थाओं में एक समान रहने वाली समत्वबुद्धि का नाम ही योग है क्योंकि समत्वबुद्धि से निष्काम कर्म करने की अपेक्षा सकाम कर्म की स्थिति बहुत ही तुच्छ है, इसलिए हे धनञ्जय! तू समत्वबुद्धि की शरण ले क्योंकि फल पर दृष्टि रखकर कर्म करने वाले लोग अत्यन्त दीनहीन हो जाते हैं।
श्रीकृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा है कि तेरा अधिकार तो अपने कर्त्तव्य कर्म करने में है जो कर्म करेगा वह फल भी पायेगा ऐसा माना जाता है। पर कर्म करने के पश्चात् फल के निर्धारण में और भी कई कारणों का योग होता है। यह निश्चित नहीं कि अभीष्ट फल उसे मिलेगा ही। अत: फल में आसक्त मत हो, तू केवल फल को लक्ष्य बनाकर कर्म करने वाला भी मत बन, क्योंकि ऐसी स्थिति में फल न मिलने पर दीनता अवश्यम्भावी है।
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कौशलम्।। गीता 2.50।।
समबुद्धियुक्त पुरुष (अन्त:करण की शुद्धि व ज्ञान प्राप्ति के द्वारा) इस लोक में पाप और पुण्य दोनों से अलिप्त रहता है। अर्थात् उनसे मुक्त हो जाता है। अत: समत्व बुद्धि रूप योग का आश्रय लें क्योंकि योग= समत्वबुद्धियोग ही कर्म करने के विषय में सबसे बड़ी कुशलता है। इसी के प्रभाव से कर्म बन्धन स्वभाव वाले होने पर भी व्यक्ति को बाँध नहीं पाते।
न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्।
स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थित:।। गीता 5.20।।
जो प्रिय वस्तु को पाकर प्रहर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिरबुद्धि, संशयरहित, ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा में एकीभाव से नित्य स्थित है।
अनाश्रित: कर्मफलं कार्यं कर्म करोति य:।
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय:।। गीता 6.1।।
जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह संन्यासी तथा योगी है और केवल अग्निहोत्र का त्याग करने वाला संन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है।
जितात्मन: प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित:।
शीतोष्णसुखदु:खेषु तथा मानापमानयो:।। गीता 6.7।।
जिसने अपनी आत्मा अर्थात् अन्त:करण (मन एवं बुद्धि) को जीत लिया हो और जिसको शान्ति प्राप्त हो गई हो, उसका परम आत्मा (निरुपाधिक आत्मा) शीत-उष्ण, सुख-दु:ख, राग-द्वेष आदि द्वन्द्वों में और मान-अपमान में भी समाहित रहता है अर्थात् विक्षुब्ध न होकर समता में रहता है।
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दु:खहा।। गीता 6.17।।
जिसका आहार-विहार नियमित है, कर्मों में चेष्टाएँ जिसकी संयमित हैं (जिसकी मन:शान्ति निश्चल है) और जिसका सोना-जागना उचित है, केवल उसी को यह योग सिद्ध होता है और उसके दु:खों का नाश करने वाला होता है।
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Oct 2024 17:59:47
ओ३म 1. सनातन की शक्ति - वेद धर्म, ऋषिधर्म, योग धर्म या यूं कहें कि सनातन धर्म के शाश्वत, वैज्ञानिक,...




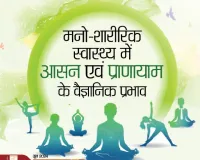













.jpg)
.jpg)
