गणतंत्र के यूरोपीय एवं भारतीय स्वरूप में अंतर
On
प्रो. रामेश्वर मिश्र पंकज
भारत के कुछ हिस्सों में ब्रिटिश प्रभाव बढऩे के साथ ही बहुत ही व्यवस्थित रीति से ईसाई मिशनरियों को आगे बढ़ाने के लिये बौद्धिक प्रयास शुरू किये गये। प्रारंभिक प्रयास आर्थिक प्रलोभन एवं राजनैतिक दबाव के थे जो विफल रहे। इस पर उन्होंने बौद्धिक प्रयास शुरू किये और योजनापूर्वक हिन्दुओं में ग्लानि भरने के लिये इतिहास तथा धर्मशास्त्र दोनों के विषय में झूठ एवं गप्प फैलाना आरंभ किया। इसमें एक तो हिन्दू समाज में काल्पनिक दोष बताने का काम किया और दूसरे भारतीय राजाओं और भारत की राज्य व्यवस्था के जो गुण थे, उन्हें ही दोष प्रचारित करने लगे। इसके पीछे मुख्य नीति यह थी कि इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों के समाजों के अपने भयावह आंतरिक दोषों, विसंगतियों एवं क्रूरताओं पर भारत के शिक्षित लोगों का ध्यान नहीं जाये। वे धुंआधार प्रचार के द्वारा इसमें सफल भी हुये।
मुख्य बात यह है कि नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम के समय तक तो संपूर्ण यूरोप में कोई भी ‘नेशन स्टेट’ (राष्ट्र राज्य) था ही नहीं। ब्रिटेन, स्वीडन, इटली, तुर्की, इजिप्त आदि कोई भी तब तक राष्ट्र नहीं थे और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस, जर्मनी एवं इटली तीनों का राजा था। वह ब्रिटेन का भी राजा होने ही वाला था। परंतु भारत के सहयोग से विकसित अंग्रेजों की नौसेना अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुई। नेपोलियन ने टीपू सुल्तान की सहायता से भारत में भी अपना प्रभाव बनाने की कोशिश की थी। रूस के जार से मैत्री टूट जाने के बाद ही नेपोलियन की शक्ति कुछ घटी। ब्रिटेन, स्पेन, स्वीडन, रूस, आस्ट्रिया और पुर्तगाल के राजाओं ने संयुक्त मोर्चा बनाकर किसी प्रकार नेपोलियन को पराजित करने में सफलता प्राप्त की। अत: स्पष्ट है कि 1821 तक तो इंग्लैंड कोई नेशन स्टेट था ही नहीं। परंतु भारत में शिक्षितों के बीच किये गये झूठे प्रचार के बल पर उसने यह भंराति फैलाई कि ‘इंग्लैंड तो एक नेशन स्टेट बन गया है और भारत कभी भी ‘नेशन स्टेट’नहीं बन सकेगा। क्योंकि यहां के राजा अपने नागरिकों के जीवन पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखते। नागरिकों के जीवन पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला राजनैतिक विचार ही भारत में नहीं है।’
इस प्रचार के दबाव से जीसस कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त कर लौटे मेधावी विद्वान श्री काशी प्रसाद जायसवाल ने ‘हिन्दू पॉलिटी’नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ रचकर यह सिद्ध किया कि भारत में प्राचीनकाल से विकसित राजनैतिक चिंतन है और साथ ही प्राचीनकाल से कई हिस्सों में गणराज्य भी रहे हैं। अन्य अनेक विद्वान भी इसी दिशा में शोध कार्य करने लगे। इसमें मुख्य बात यह है कि इस तथ्य की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया कि स्वयं यूरोप में तो गणराज्य 20वीं शताब्दी ईस्वी के तीसरे दशक के बाद ही विकसित हुये हैं और 100 वर्ष से अधिक उनका जीवन नहीं है। अभी से एक सौ वर्ष पूर्व यूरोप में कोई भी गणराज्य नहीं था। जिसे वे प्राचीन रिपब्लिक बताते हैं, वह कुछ शहरों में वहाँ के धनियों और जागीरदारों की सभायें मात्र थीं, जो शासन के विषय में संयुक्त रूप से निर्णय लेती थीं। यूनाइटेड किंगडम अधिकृत रूप से 1922 में ही ‘नेशन स्टेट’घोषित हुआ है। स्त्रियों को वोट देने का अधिकार तो वहाँ 1928 में ही मिला है। उसके पहले स्त्रियों को मताधिकार के लिये चले लंबे आंदोलनों में 1914 ईस्वी का सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जिसमें एमलीन पैंकहस्र्ट नामक प्रसिद्ध महिला नेत्री को बकिंघम पैलेस के सामने मांगपत्र प्रस्तुत करने के अपराध में गिरफ्तार किया गया।
इन तथ्यों से अनजान औसत शिक्षित भारतीय इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों को बहुत प्राचीनकाल से एक नेशन स्टेट और गणराज्य मानते हैं। सत्य यह है कि इंग्लैंड को नेशन स्टेट बने केवल 175 वर्ष हुये हैं और गणराज्य वह आज तक नहीं है। क्योंकि वहाँ संसदीय लोकतंत्र और राजतंत्र का एक मिश्रण है। आज भी वहाँ का राष्ट्रगीत है - ‘गॉड सेव द क्वीन’(भगवान महारानी की सदा रक्षा करें)। आज भी वहाँ संवैधानिक राजतंत्र ही है। संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम संवैधानिक राजतंत्र के अधीन एक ‘नेशन स्टेट’है। उसे एक बनाये रखने का आधार प्रोटेस्टेंट चर्च है। जिसकी मुख्य संरक्षक वहाँ की महारानी है। जब वहाँ गद्दी पर महाराजा बैठते हैं तो वे प्रोटेस्टेंट चर्च के मुख्य संरक्षक होते हैं। इस प्रकार यूनाइटेड किंगडम वस्तुत: एक धार्मिक राजतंत्र है। फिर भी शिक्षित भारतीयों का बड़ा हिस्सा उसे गणतंत्र ही मानता है।
गणतंत्र की जो भी यूरोपीय अवधारणायें हैं, वे वर्तमान रूप में 19वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्द्ध में ही सामने आईं हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि गणराज्य शासन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सिद्धांत रूप में सम्प्रभुता लोगों में निहित है। परंतु सर्वत्र ‘लोगों’(द पीपॅल) के अर्थ को लेकर भारी मतभेद हैं। उदाहरण के लिये 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ तक यूरोप के सभी देशों में ‘द पीपॅल’में वहाँ की स्त्रियाँ नहीं शामिल मानी जाती थीं। क्योंकि यह मान्यता थी कि स्त्रियों के भीतर आत्मा नहीं होती, केवल प्राण होते हैं। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में 200 वर्ष पूर्व तक ‘नीग्रो’या ‘अश्वेत’लोगों को द पीपॅल का अंग नहीं माना जाता था, अब माना जाता है।
नागरिक सीधे तो राज्य का नियंत्रण कर नहीं सकते और प्रत्यक्ष शासन नहीं कर सकते। अत: वे विभिन्न निकायों के लिये अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और फिर वे प्रतिनिधि शासकों को चुनते हैं। इन दिनों यूरोप में रिपब्लिक का प्रचलित अर्थ है वह राज्य जहाँ राज्य का प्रधान कोई सम्राट या राजा न होकर लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हो। संविधान के अंतर्गत यह चयन होता है। इस सामान्य अर्थ में भारत भी वैसा ही गणराज्य है। परंतु कुछ बातों में भारतीय गणराज्य विश्व के अन्य गणराज्यों से सर्वथा भिन्न है।
इसमें पहली भिन्नता यह है कि यद्यपि शासकों का चयन विधान सभाओं और संसद के द्वारा होता है और इस प्रकार वे निर्वाचित शासक होते हैं, परंतु स्थाई शासक के रूप में एक प्रशासनतंत्र है, जिसका कोई भी संबंध भारत की अपनी किसी पंरपरा से नहीं है। यह स्थिति इंग्लैंड सहित अन्य सभी राष्ट्रों से अलग है। इंग्लैंड में प्रशासनतंत्र प्रोटेस्टेंट चर्च के द्वारा प्रशिक्षित प्रशासकों द्वारा ही संचालित होता है और उसकी निष्ठा चर्च के प्रधान संरक्षक सम्राट या महारानी के प्रति ही होती है। इसीलिये प्रोटेस्टेंट चर्च ही इंग्लैंड की राष्ट्रीय एकता का मेरूदंड है। यही स्थिति अलग-अलग रूपों में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विटजरलैंड आदि में भी है।
भारत का प्रशासनतंत्र संविधान के प्रति निष्ठावान है। परंतु संविधान स्वयं में किसी एकीकृत विचार को केन्द्रीय नहीं मानता। वह भारत के सभी लोगों को उपासना, आस्था, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इस प्रकार प्रशासक भिन्न-भिन्न आस्थाओं वाले हो सकते हैं।
विश्व में सर्वमान्य है कि मनुष्य मूलत: चेतना सम्पन्न अस्तित्व हैं। अत: उनकी चेतना मुख्यत: उनकी आस्था से प्रभावित होती है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न आस्थाओं वाले प्रशासकों के बीच कोई आंतरिक एकता सम्भव नहीं होती, केवल औपचारिक तालमेल ही संभव होता है। यह स्थिति भारत के गणराज्य को अनेक मामलों में भीतरी तौर पर टकराहटों से भर देती है।
इसका समाधान भारत की ज्ञान परंपरा में तो है, परंतु आधुनिक शासन परंपरा में नहीं है। भारत की ज्ञान परंपरा यह बताती है कि सभी मनुष्यों का एक सामान्य धर्म है जो वस्तुत: सार्वभौम ब्रह्माडीय नियम ही हैं। ये हैं - सत्य, ऋत, यज्ञ एवं धर्म। धर्मशास्त्रों ने इनका वर्णन किया है और सभी मनुष्यों के द्वारा इन्हें पालनीय बताया है। यदि धर्म का यह आधार स्वीकार हो तो फिर आस्थाओं की विभिन्नता कोई समस्या नहीं बनती क्योंकि अंतत: सभी आस्थाओं को व्यापक और सार्वभौम धर्मानुशासन से अनुशासित रहना है। परंतु वर्तमान में यह स्थिति नहीं है। यद्यपि हमारा संविधान इस स्थिति का विरोधी नहीं है और उसके अंतर्गत भारत की संसद कभी भी सार्वभौम नियमों को भारत के सभी नागरिकों के लिये आधारभूत अनिवार्यता सुनिश्चित कर सकती है। परंतु ऐसा किया नहीं गया है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक आस्थाओं की टकराहट गणराज्य में अनेक समस्याओं को जन्म देती रहेगी।
ऊपर से हुआ यह है कि कांग्रेस शासकों ने संविधान की मूल भावना के विरूद्ध जाकर अनेक विधिक एवं प्रशासनिक कदम उठा लिये हैं। इनमें मुख्य यह है कि बहुसंख्यकों के धर्म के प्रति शासन की कोई भी जवाबदेही सुनिश्चित किये बिना ही, अल्पसंख्यकों के रिलीजन और मजहब के प्रति शासन की जवाबदेही सुनिश्चित कर दी गई है। यह संविधान की मूल भावना के नितांत विपरीत है। जहाँ सभी नागरिकों की उपासना और आस्था के प्रति राज्य को समभाव रखना सुनिश्चित किया गया है। परंतु बहुसंख्यकों के धर्म को संरक्षण दिये बिना अल्पसंख्यकों के मजहब को या रिलीजन को विशेष संरक्षण दे देना संविधान की मूल भावना का विरोधी है। भारतीय गणराज्य में शासकों के द्वारा उठाये गये इस कदम से कई समस्यायें उत्पन्न होती रहती हैं।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ चयनित कार्यपालिका का स्वरूप स्थायी है और वह कार्यपालिका आधारभूत रूप से किसी एक आस्था के द्वारा एकीकृत नहीं है। दूसरी ओर निर्वाचित कार्यपालिका का स्वरूप अस्थायी है और निर्वाचित कार्यपालिका शासकीय नीतियों के विषय में निर्णय की संपूर्ण अधिकारी है। परंतु उन निर्णयों के पालन को सुनिश्चित करने की कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है और निर्णयों का पालन पूरी तरह चयनित कार्यपालिका के ऊपर निर्भर है। चयनित कार्यपालिका के सदस्यों का कार्यकाल औसतन चालीस वर्ष होता है और निर्वाचित कार्यपालिका के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ऐसी स्थिति में चयनित कार्यपालिका की निर्वाचित कार्यपालिका के प्रति जिम्मेदारी रस्मी ही रह जाती है।
कई बार निर्वाचित कार्यपालिका के सदस्यों द्वारा कार्यभार संभालने की प्रक्रिया में छह माह लग जाते हैं तथा अंतिम छह माह उनके पुनर्निर्वाचन की अनिश्चित संभावनाओं वाले होते हैं और इस प्रकार चयनित कार्यपालिका पर वास्तविक नियंत्रण के लिये निर्वाचित कार्यपालिका के सदस्यों को औसतन 4 वर्ष ही मिलते हैं। ऐसे में यदि निर्वाचित कार्यपालिका के सदस्य बहुत प्रशिक्षित और कुशल नहीं हों तो वे चयनित कार्यपालिका (जिसे अफसरशाही कहा जाता है) पर सक्षम नियंत्रण में समर्थ नहीं होते।
उधर चयनित कार्यपालिका के शीर्ष अधिकारी लिखित रूप से केवल राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं और उनके लिये ही कार्य करते हैं। इस तरह निर्वाचित कार्यपालिका का उन पर वास्तविक नियंत्रण बहुत कम रह जाता है। विशेषकर यदि निर्वाचित कार्यपालिक के प्रतिनिधि प्रशिक्षित एवं कुशल न हों तो वे चयनित कार्यपालिका पर बड़ी सीमा तक निर्भर हो जाते हैं। परंतु चयनित कार्यपालिका के सदस्यों की आस्था लिखित रूप से भारतीय समाज या भारतीय परंपराओं के प्रति नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत से बाहर की शक्तियां चयनित कार्यपालिका के विविध अंगों तक अपनी पैठ बनाकर उनके निर्णयों को प्रभावित करने में समर्थ होती हैं। यह भारतीय गणराज्य की एक बड़ी समस्या है। जिस पर विचार कर निर्णय लेने की आवश्यकता है और भारत की माननीय संसद ऐसे निर्णय लेने में पूरी तरह समर्थ है।
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Oct 2024 17:59:47
ओ३म
1. सनातन की शक्ति - वेद धर्म, ऋषिधर्म, योग धर्म या यूं कहें कि सनातन धर्म के शाश्वत, वैज्ञानिक,...





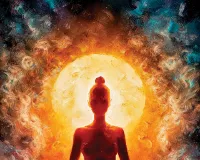


.jpg)










