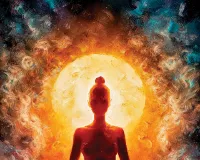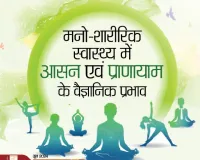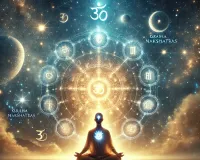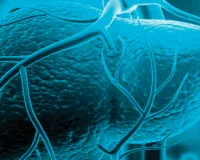शुद्धिकरण की प्रक्रिया है 'यज्ञ’
On

श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज
वेदवाणी
ऋषि- परमेष्ठी प्रजापति। देवता- सविता। छन्द- भुरिग्जगती।
वसो: पवित्रमसि शतधारं वसो: पवित्रमसि सहस्रधारम्।
देवस्त्वा सविता पुनातु वसो: पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्ष:।।1.3।।
सुरूप यज्ञ की विशेषताएँ बताने के लिए यह मन्त्र है। मन्त्र का प्रथम वाक्य है- 'वसो: पवित्रमसि शतधारम्’। यहाँ 'वसो:’ यह षष्ठ्यन्त पद प्रथमा में तथा 'असि’ क्रियापद 'अस्ति’ रूप में बदल जाएगा। यद्यपि उद्देश्य विधेय में समान लिङ्ग-वचन होते हैं तो भी 'पवित्रम्’ यहाँ सामान्य में नपुंसकलिङ्ग समझना चाहिए- जैसे व्याकरण में 'परार्थाभिधानं वृत्ति:’ प्रयोग में हुआ है या छान्दस प्रयोग भी कह सकते हैं। अत: अर्थ हुआ- जो यह वसुरूप यज्ञ है, वह बहुविध असंख्य संसार का धारण करने वाला है और पवित्र (शुद्धि) करने वाला कर्म है। पवित्र शब्द को गत मन्त्र की भाँति करणकारक में निष्पन्न 'पूयतेऽनेनेति पवित्रम् शुद्धिकारकं कर्म’ ऐसा समझना चाहिए अर्थात् यज्ञ शुद्धि करण की ही एक प्रक्रिया का नाम है।
दूसरा वाक्य है- 'वसो: पवित्रमसि सहस्रधारम्’ अर्थात् पूर्ववाक्य की भाँति ही इसका भी अर्थ होगा- यह यज्ञ अनेक प्रकार से ब्रह्माण्ड को धारण करने वाला शुद्धि का निमित्त बनकर अत्यन्त सुखप्रद है। जितना भी पृथिवी-जल-अग्नि-वायु-आकाश आदि पञ्चभूतों, वृक्ष-ओषधि-वनस्पति आदि भूमिज पदार्थों, गौ-अश्व-हस्ती आदि ग्राम्य तथा मृग आदि आरण्य पशु व मनुष्य जगत् का परस्पर सह-अस्तित्व (Co-existence) पूर्वक जो एक क्रमविशेष दिखाई देता है, वह सम्पूर्ण विस्तार यज्ञ का ही रूप है। सम्पूर्ण सृष्टि में परस्पर उपकार्य-उपकारक भाव का होना ही यज्ञ है। मनुष्येतर सृष्टि के अन्य घटक तो विधाता के नियम में बंधे हुए यज्ञ का भंग नहीं करते, किन्तु मनुष्य के पास मनरूपी साधन के विकसित होने से और साथ में मनोवाञ्छित ढंग से उसका प्रयोग करने में पूर्ण स्वाधीन होने से यह मनुष्य अज्ञान, स्वार्थ, भय, प्रलोभन, कामना व आसक्ति आदि कारणों से उस सुखप्रद यज्ञ का भंग कर देता है और परिणाम में अनन्त दु:खों को झेलता रहता है और अपने ही हाथों अपना विनाश करता हुआ अपने मन-बुद्धि व इन्द्रियों को अशुद्धि का और उसके परिणामस्वरूप दु:ख का अड्डा बना लेता है। अत: वेद-शिक्षा की आवश्यकता होती है कि व्यक्ति कर्तव्य-अकर्तव्य का ज्ञान प्राप्त करे, सृष्टि में चल रहे स्वाभाविक छन्द (Rythm) का भंग न करे। स्वयं सुख में जीए तथा अन्यों की भी सुख में जीने के लिए सहायता करे।
मन्त्र का अग्रिम वाक्य है- 'देवस्त्वा सविता पुनातु’ यहाँ 'त्वा’ शब्द व्यत्यय से 'तम्’ अर्थ को दे रहा है। अत: अर्थ होगा- वसु, अग्नि, पृथिवी आदि तैंतीस देवों की उत्पत्ति करने वाला सविता देव उस वसुरूप यज्ञ को पवित्र करे। उसमें अशुद्धि व विकार न आने दे। वह सविता देव मनुष्यों को ऐसी बुद्धि प्रदान करे कि वे इस सह-अस्तित्व रूप सृष्टियज्ञ अथवा व्यवहार यज्ञ का भंग न करे।
मन्त्र के चतुर्थ वाक्य में कहा- 'वसो: पवित्रेण शतधारेण सुप्वा’ पूर्ववत् 'वसो:’ का अर्थ हो गया 'वसु’। इससे पूर्व वाले वाक्य से 'पुनातु’ क्रिया को प्रकृत वाक्य से भी सम्बद्ध कर लेना चाहिए। यहाँ 'सुप्वा’ शब्द जो कि तृतीया एक-वचनान्त है उसका अर्थ होगा- अच्छी प्रकार जो पवित्र करने वाला है या पवित्रता का हेतु है, उस (यज्ञ) के द्वारा। इस प्रकार 'हे जगदीश्वर!’ पद का ऊपर से अध्याहार करते हुए सम्पूर्ण वाक्य का यह अर्थ हुआ, हे जगदीश्वर! आप हम लोगों द्वारा सेवित जो यह वसु रूप यज्ञ है उस शुद्धि के निमित्त वेद के विज्ञान रूप कर्म से (=पवित्रेण) तथा बहुत विद्याओं को धारण करने वाले वेद द्वारा (=शतधारेण) और अच्छी प्रकार पवित्र करने वाले यज्ञ से (=सुप्वा) हमें ('अस्मान्’ यह अध्याहृत है) पवित्र कीजिए।
मन्त्र का अन्तिम वाक्य है- 'काम् अधुक्ष:’ 'काम्’ इस पद में एकशेष निर्देश है और छान्दस एक वचन है। जिज्ञासो या विद्वन् का अध्याहार तथा वीप्सा में द्विर्वचन मानने पर अर्थ हुआ- हे विद्वन् या जिज्ञासो! तुमने किस-किस गाय का दोहन किया है। जैसा कि 'गो’ शब्द का अर्थ वेदवाणी भी होता है अत: 'काम् अधुक्ष:’ का निष्कृष्टार्थ होगा- किस-किस वेदवाणी का तुमने दोहन किया है। वेदत्रयी में से किस-किस को अपने मन में प्रपूरण करना अर्थात् जानना चाहते हो?
बिना विभक्तियों का व्यत्यय (परिवर्तन) किए भी मन्त्रार्थ को संगत किया जा सकता है- हे जिज्ञासु या हे विद्वन् पुरुष! तुम यज्ञ की पवित्रता के साधक हो और सैकड़ों प्रकार से उसे धारण करने का सामथ्र्य रखते हो। यहाँ पवित्रम् और शतधारम् पद सम्बोध्यमान विद्वत्पुरुष के साथ समानाधिकरण हैं। सामान्य अर्थ को लेकर नपुंसकलिङ्ग का प्रयोग समझना चाहिए। इसी बात को जोर देने (Emphasis) के लिए दुबारा कह दिया- 'वसो: पवित्रमसि सहस्रधारम्’। तुम यज्ञ की पवित्रता (शुद्धि) को बनाए रखने में पूर्णत: सक्षम हो, तुम में अपार सामथ्र्य है (सहस्रधारम्) अर्थात् जीव में Potential तो है किन्तु Competent होने के लिए आलस्य छोड़कर पुरुषार्थ करना पड़ता है। वसु रूप यज्ञ सह-अस्तित्व ही जिसका स्वरूप है उसको समझना और तदनुकूल जीना ही पवित्रता व अनन्त सुख साधन है। श्रीमद्भगवद् गीता में कहा है-
यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन:।
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्ग: समाचर।। (गीता- 3.9)
यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्यसमुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन! तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही भलीभाँति कर्म कर।
सहयज्ञा: प्रजा: सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति:।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्।। (गीता- 3.10)
प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञसहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होओ और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो।
सृष्टि रचना के प्रारम्भ में यज्ञ (परमार्थ पारस्परिक सहयोग) की भावना के सहित प्रजाओं की उत्पत्ति कर प्रजापति (ब्रह्मा) ने अपनी प्रजाओं से कहा- इस यज्ञ द्वारा तुम्हारी वृद्धि हो, यह यज्ञ ही तुम्हारी शुभ कामनाओं की पूर्ति करने वाला हो।
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व:।
परस्परं भावयन्त: श्रेय: परमवाप्स्यथ।। (गीता- 3.11)
तुम इस यज्ञ से देवताओं को तृप्त करो और वे देवता तुम्हें तृप्त करते रहें। इस प्रकार एक दूसरे को पुष्ट-सन्तुष्ट करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होओ। (देवता कितने हैं- देखिए बृहदारण्यकोपनिषद् (अ.3, ब्रा.9, क.1) में याज्ञवल्क्य-शाकल्य संवाद)
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता:।
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स:।।
यज्ञशिष्टाशिन: सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषै:।
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्।। (गीता- 3.12-13)
क्योंकि यज्ञ से तृप्त होकर देवता तुम्हारे इच्छित सब भोग तुम्हें प्रदान करेंगे। उन देवों द्वारा दिए हुए भोगों को उन्हें वापिस न देकर अर्थात् उनका ऋण न चुका कर जो स्वयं भोग करता है, वह सचमुच चोर है। जो यज्ञशेषभोजी (यज्ञशेष को खाने वाले) होते हैं, वे सब पापों के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं अर्थात् सब पाप यज्ञशेषभोजियों को छोड़ देते हैं, पर जो यज्ञ न करके केवल अपने लिए ही अन्न पकाते हैं, वे पापी लोग पाप का भक्षण करते हैं।
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भव:।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञ: कर्मसमुद्भव:।।
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्।। (गीता- 3.14-15)
प्राणिमात्र की उत्पत्ति एवं वृद्धि अन्न से होती है और अन्न पर्जन्य (वर्षा) से उत्पन्न होता है। पर्जन्य का उद्भव यज्ञ से होता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्नि में दी हुई आहुति सीधी सूर्य को प्राप्त होती है और सूर्य पर्जन्य को उत्पन्न कर वृष्टि करता है। कर्म को ब्रह्म=वेद से और ब्रह्म अर्थात् वेद को अक्षर (नष्ट न होने वाले परमतत्त्व) परमेश्वर से उत्पन्न हुआ जान। इस कारण सर्वगत ब्रह्म ही यज्ञ में सदा प्रतिष्ठित रहता है।
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह य:।
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति।। (गीता- 3.16)
हे पार्थ! जो इस जगत् (सृष्टि) के धारणार्थ यज्ञचक्र (कर्मचक्र) को आगे नहीं बढ़ाता, वह मानो पाप को चाह रहा है अर्थात् उसका जीवन पापरूप है। उस विषयलोलुप (जो देवताओं को न देकर स्वयं ही उपभोग करने में लगा है, ऐसे स्वार्थपरायण व्यक्ति) का जीवन व्यर्थ है, पृथ्वी पर भारस्वरूप है।
तीसरा वाक्य है- 'देवस्त्वा सविता पुनातु वसो: पवित्रेण शतधारेण सुप्वा’ वसुरूप यज्ञ की पवित्रता की साधक जो अनन्त सामथ्र्य तुम्हारे पास है, इसी को पवित्रता का साधन बनाकर (=सुप्वा) अग्नि-पृथिवी आदि समस्त अस्तित्व को प्रकट करने वाला सविता देव तुम्हें और भी पवित्र करता रहे। पवित्रता का यह क्रम निरन्तर जारी रहे, सतत बढ़ता रहे।
मन्त्र के अन्तिम वाक्य में प्रश्न है- भला! यह तो बताओ कि तुमने किन-किन गायों का दोहन किया है। अर्थात् वेदवाणी रूपी तीन गौओं में से किस-किस को अपने मन में भरने का, जानने का प्रयास किया है या कर रहे हो।
यहाँ प्रथम-द्वितीय-तृतीय मन्त्रों के अध्ययन से एक बात स्पष्ट हो रही है कि श्रेष्ठतम कर्म का नाम यज्ञ है। दो प्रकार की सृष्टि हमारे सामने है- ईश्वरसृष्टि व जीवसृष्टि। ईश्वरसृष्टि के सभी कर्म निर्विवाद रूप से यज्ञरूप हैं, किन्तु जीवसृष्टि के कर्मों को यज्ञरूप बनाने के लिए सतत पुरुषार्थ करना होता है। इसी के लिए शास्त्र रचे गए, उपदेश परम्परा शुरू हुई, तप अस्तित्व में आया। यदि ईश्वरीय सृष्टि के छन्दोगान में जीव अपना सुर, ताल, लय भंग कर देता है तो यह जीवसृष्टि बहुत ही दु:खप्रद हो जाती है। हर क्षण ईश्वर की तरह ही जीव को भी अपना यज्ञ करना होता है, किन्तु जहाँ प्रमाद हो जाता है वहीं अशुद्धि या दुर्गन्ध आने लगती है। शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या वैश्व स्तर पर जहाँ भी स्वार्थ बढ़कर दूसरे की उपेक्षा करने लगता है तो यज्ञसूत्र टूट जाता है। 'यज्ञ’ इस शब्द से स्वार्थ का विरोधी भाव परार्थ लिया जाता है। इसमें त्याग की प्रधानता रहती है। भोगी व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता, इसलिए जहाँ यज्ञ है वहाँ संयम का भाव या इन्द्रियों पर विजय का भाव स्वत: ही मध्य में आ जाता है। संयम व जितेन्द्रियता से शारीर व मानस मलों का प्रक्षालन शुरू हो जाता है। इसी प्रकार परिवार में बड़ों का आदर-सत्कार-पूजा में भी पितृयज्ञ के रूप में श्रम-शक्ति आदि का अंशदान करना होता है। समाज में भी निर्बलों के सहयोग के रूप में भूतयज्ञ या नृयज्ञ करना होता है। सृष्टि संस्था को व्यवस्थित रखने के लिए अर्थात् पञ्च महाभूतों की पवित्रता के लिए देवयज्ञ और आत्मशुद्धि के लिए ब्रह्मयज्ञ करना होता है। इस प्रकार विचार करने से यज्ञ एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया दृष्टिगोचर होती है। मन्त्र में कहा गया कि यज्ञ पवित्रता करने वाला है। यज्ञ किसे पवित्र करता है इस जिज्ञासा में कहना होगा- 'यज्ञ’ यह एक व्यापक शब्द है- श्रीमद्भगवद्गीता में श्लोक 24-33 तक अध्याय 4 में भगवान् गुरु ने 12 प्रकार के यज्ञ गिनाए हैं।
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविब्र्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना।। (गीता- 4.24)
ब्रह्म ही जिसका सर्वस्व है, अर्पण करने का साधन स्रुवा आदि भी ब्रह्म, हवि भी ब्रह्म, यजमान भी ब्रह्म, अग्नि भी ब्रह्म और आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। इस प्रकार ब्रह्माग्नि में मानो ब्रह्म ने ही हवन किया। उस ब्रह्मकर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किया जाने वाला (फल) भी ब्रह्म ही है। जिसने अहं को ब्रह्म में लीन कर दिया मानो वह स्वयं ब्रह्म हो गया।
दैवमेवापरे यज्ञं योगिन: पर्युपासते।
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति।। (गीता- 4.25)
कुछ योगी अन्य देवता आदि को उद्देश्य बनाकर दैव यज्ञ की उपासना किया करते हैं और कुछ ब्रह्माग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं। परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एकीभाव से स्थित होना ही ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। भाव यह है कि परमात्मा में आत्मा को समर्पित करना व आत्मरूप यज्ञ से परमात्मरूप का यजन करना।
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति।
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति।। (गीता- 4.26)
कोई श्रोत्र, नेत्र आदि इन्द्रियों का संयमरूप अग्नि में हवन करते हैं और कुछ लोग इन्द्रिय रूप अग्नि में शब्दादि विषयों का हवन करते हैं।
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे।
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते।।
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे।
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतय: संशितव्रता:।। (गीता- 4.27-28)
कुछ लोग इन्द्रियों तथा प्राणों के सब कर्मों को ज्ञान से प्रज्वलित आत्मसंयमरूपी योग की अग्नि में हवन करते हैं। इस प्रकार तीक्ष्ण व्रत का आचरण करने वाले अन्य जो यति अर्थात् संयमी पुरुष हैं, वे द्रव्ययज्ञ, तपरूप यज्ञ, योगरूप यज्ञ, स्वाध्यायरूप यज्ञ और ज्ञानरूप यज्ञ किया करते हैं।
अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे।
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणा:।। (गीता- 4.29)
दूसरे कुछ प्राणायाम-परायण साधक, प्राण-अपान की गति रोककर प्राण की अपान में और अपान की प्राण में आहुति दिया करते हैं। शरीर से बाहर जाने वाली वायु को 'प्राण’ तथा शरीर के भीतर प्रवेश करने वाली वायु को 'अपान’ कहते हैं। गीता के अनुसार प्राणायाम भी एक यज्ञ ही है। उपर्युक्त श्लोक के अनुसार जिस वायु का निरोध करते हैं, उसका अन्य वायु में होम होता है।
अपरे नियताहारा: प्राणान्प्राणेषु जुह्वति।
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा:।। (गीता- 4.30)
अन्य कई नियताहार अर्थात् आहार-विषयक संयम रखने वाले, समय पर हित-मित भोजन करने वाले साधक अपान में प्राण की आहुति देते हैं अर्थात् पूरक प्राणायाम (आभ्यन्तरवृत्ति) करते हैं तथा प्राण में अपान की आहुति देते हैं अर्थात् रेचक प्राणायाम (बाह्यवृत्ति) करते हैं। कुछ साधक बिना रेचन व पूरण के यथावस्थित प्राणापान की गति रोककर प्राणों की प्राणों में आहुति देते हैं अर्थात् स्तम्भवृत्ति प्राणायाम करते हैं। ये सब (जिनका वर्णन ऊपर किया गया है) यज्ञ के रहस्य के ज्ञाता (जानने वाले) हैं और उक्त यज्ञों द्वारा अपने सब पापों को क्षीण कर देते हैं। यहाँ प्राणायाम की साधना करने वालों के लिए 'नियताहारा:’ विशेषण दिया गया है, यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है; क्योंकि आहार-संयम के बिना प्राणायाम सिद्ध नहीं हो सकता है।
यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्।
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्य: कुरुसत्तम।। (गीता- 4.31)
जो व्यक्ति यज्ञशेष रूपी अमृत का भोजन करते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ (उद्योग या प्रयत्न) न करने वाले के लिए जब यह लोक ही नहीं है अर्थात् इस लोक में ही सफलता नहीं मिलती तो परलोक की तो बात ही क्या, स्वर्ग उन्हें कहाँ से मिलेगा?
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे।
कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे।। (गीता- 4.32)
इस प्रकार बहुविध (अनेक प्रकार के) यज्ञ इस ब्रह्म के मुख में (वेदवाणी में) निरन्तर विद्यमान हैं। उन सबको कर्म के द्वारा ही सम्पन्न हुआ जान। ऐसा जानकर तू मुक्त हो जाएगा।
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ: परन्तप।
सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।। (गीता- 4.33)
हे परन्तप (अर्जुन)! द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है; क्योंकि हे पार्थ! समस्त कर्मों का पर्यवसान (परिसमापन) ज्ञान में ही होता है। योगी के सब कर्म ज्ञानोपलब्धि के लिए होते हैं।
स्वामी दयानन्द ने भी कहा है कि 'निष्काम कर्म तो परमेश्वर का अनुभव करने के लिए होते हैं’। (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका वेदविषय प्रकरण) यह सारा प्रसङ्ग हमने इस सन्दर्भ में प्रस्तुत किया है कि यज्ञ शुद्धि का साधन है। कौन से यज्ञविशेष से कौन-कौन-सी शुद्धि विशेष होती है यह भी स्पष्ट है।
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Oct 2024 17:59:47
ओ३म 1. सनातन की शक्ति - वेद धर्म, ऋषिधर्म, योग धर्म या यूं कहें कि सनातन धर्म के शाश्वत, वैज्ञानिक,...