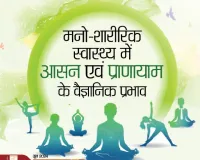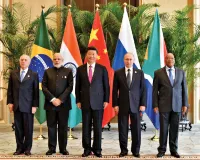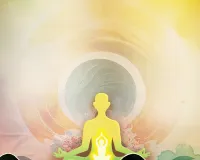महाभारत में गणराज्य का स्वरूप
On

प्रो. कुसुमलता केडिया
भारत में प्राचीनतम काल से गणराज्यों की एक विराट परंपरा है। महाभारत के शांतिपर्व में इनका उल्लेख मिलता है। यह विस्तृत गणराज्यों के विषय में विश्व में उपलब्ध प्राचीनतम लिखित साक्ष्य है। शांतिपर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में प्राचीन काल से चले आ रहे गणराज्यों का वर्णन है। सम्राट युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा कि गणतांत्रिक राज्यों के लोग किस प्रकार अपनी उन्नति करते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं तथा सुहृद्यों की प्राप्ति करते हैं एवं आपसी भेद पनपने नहीं देते, यह बताने की कृपा करें क्योंकि मैं देखता हूं कि आपसी भेदों से अनेक गणराज्य नष्ट होते रहे हैं और उनके लिये शासन की गुप्त मंत्रणायें छिपाकर रखना भी बहुत कठिन हो जाता है।
पितामह भीष्म ने कहा कि हे राजन! वस्तुत: राजाओं का राज्य हो या गणराज्य हो सभी जगह दो दोष ही सबसे अनर्थकारी होते हैं - लोभ और अमर्ष। लोभ से अन्य के धन की तीव्र कामना जब उठती है और फिर उसके कारण उस अन्य के प्रति अमर्ष पैदा होता है। लोभ और अमर्ष के कारण लोग एक-दूसरे के विनाशक बन जाते हैं। इस अमर्ष और लोभ के कारण वे एक-दूसरे के विरूद्ध गुप्तचरी कराते हैं और गुप्त मंत्रणायें करते हैं तथा बल संग्रह करते हैं। सामनीति, दाननीति और भेदनीति का प्रयोग करते हुये एक-दूसरे को दुर्बल करने के लिये अनेक उपायों का आश्रय लेते हैं और इसके लिये प्रचुर धन व्यय करते हैं:-
गणानां च कुलानां च राज्ञां भरतसत्तम।
वैरसंदीपनावेतौ लोभामर्षौ नराधिप।।
लोभमेको हि वृणुते ततोऽमर्षमनन्तरम्।
तौ क्षयव्ययसंयुक्तावन्योन्यं च विनाशिनौ।।
चारमन्त्रबलादानै: सामदानविभेदनै:।
क्षयव्ययभयोपायै: प्रकर्षन्तीतरेतरम्।
(महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय 107, श्लोक 10,11 एवं 12)
वस्तुत: यहाँ मुख्य बात यह स्पष्ट की गई है कि जहाँ बहुत से लोग शासक हों वहाँ नीति की गोपनीयता नहीं रह जाती और उससे आंतरिक कलह तथा विद्वेष उत्पन्न होता है। यह विनाश का कारण बनता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि गणराज्य आपस में फूट होने पर ही इतिहास में नष्ट होते देखे गये हैं। इसके लिये वे उपाय भी बताते हैं।
वे बताते हैं कि यदि गणराज्य में शासक न्यायशील हो और गणराज्य के सभी श्रेष्ठ पुरूष भी न्यायभावना रखें तो गणराज्य की सब प्रकार से उन्नति होती है। इसके लिये यह आवश्यक है कि संतानों को उत्तम शिक्षा दी जाये, तभी उनकी विशेष उन्नति होती है। जहाँ ऐसा होता है वहाँ गणराज्य तेजी से उन्नति करते हैं और समृद्धि बढ़ती जाती है। इसके लिये यह आवश्यक है कि गणराज्य के सभी नागरिक धनवान, शूरवीर, अस्त्र-शस्त्रों के ज्ञाता तथा शास्त्रों के ज्ञान से सम्पन्न हों:-
द्रव्यवन्तश्च शूराश्च शस्त्रज्ञा: शास्त्रपारगा:।
कृच्छ्रास्वापत्सु सम्मूढान् गणा: संतारयन्ति ते।। (107/21)
साथ ही पितामह ने सावधान किया है कि यदि गणराज्य के लोगों में क्रोध की अनावश्यक वृत्ति हो और फूट हो तथा एक-दूसरे को दंडित करने और दुर्बल बनाने या वध तक की प्रवृत्ति हो तो फिर ऐसे गणराज्य शत्रुओं के वश में हो जाते हैं। इसीलिये गणराज्य के मुख्य लोगों का सम्मान सम्पूर्ण गणराज्य में होना चाहिये। क्योंकि लोकयात्रा का विशेष भार उन मुख्य लोगों पर ही होता है -
तस्मान्मानयितव्यास्ते गणमुख्या: प्रधानत:।
लोकयात्रा समायत्ता भूयसी तेषु पार्थिव।। (107/23)
इस संदर्भ में पितामह भीष्म ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह कही है कि जाति और कुल में सभी लोग एक समान हो सकते हैं। परंतु उद्योग, बुद्धि, रूप और सम्पत्ति में सबका एक सा होना सम्भव ही नहीं है। अत: समता का सीमा से अधिक आग्रह फूट का कारण बनता है और तब शत्रु भेद को बढ़ाकर और घूस देकर गणराज्य का भेदन करने में समर्थ हो जाते हैं:-

अन्योन्यं नाभिभाषन्ते तत्पराभवलक्षणम्म्।
जात्या च सदृशा: सर्वे कुलेन सदृशास्तथा।।
न चोद्योगेन बुद्धया वा रूप द्रव्येण वा पुन:।
भेदाच्चैव प्रदानाच्च भिद्यन्ते रिपुभिर्गणा:।।
(107/30 एवं 31)
अत: विवेकशून्य समतावाद विनाश का कारण बनता है। बड़े-छोटे और उच्च पद तथा अवरपद का भेद सदा स्मरण रखना चाहिये। इसीलिये कहा गया है कि गणराज्य के मुख्य-मुख्य व्यक्तियों को सदा परस्पर मिलकर राज्य के हित का साधन करना चाहिये।
इस संदर्भ में चाणक्य ने अर्थशास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। अर्थशास्त्र के अधिकरण 11 का नाम ही संघवृत्त है। इसमें उन्होंने कहा है कि काम्बोज, सुराष्ट्र आदि देशों में क्षत्रिय लोग कृषि एवं व्यापार तथा गौरक्षा के द्वारा जीविका चलाते हुये शस्त्रजीवी रहते हैं। परन्तु लिच्छवि, व्रजि, मल्ल, कुरू, पान्चाल आदि के क्षत्रिय केवल राजशब्दोपजीवी होते हैं:-
काम्बोजसुराष्ट्रक्षत्रियश्रेण्यादयो वार्ताशस्त्रोपजीविन:।।
लिच्छिविकव्रजिकमल्लकमद्रककुकुरकुरूपान्चालादयो राजशब्दोपजीविन:।।
(अर्थशास्त्र अधिकरण 11, सूत्र 5 एवं 6)
इसका अर्थ है कि जहाँ काम्बोज अर्थात् अफगानिस्तान और ईरान के एक हिस्से में तथा सुराष्ट में क्षत्रिय गण वार्ता और शस्त्रजीवी होते हैं, वहीं बाद वाले गणराज्यों में वे केवल राजशब्दोपजीवी होते हैं। राजशब्दोपजीवी होने का अर्थ है शासन संबंधी चर्चा में ही समय लगाना और जीविका का भी वही आधार होना। इसकी तुलना वर्तमान के सभी राजनेताओं से की जा सकती है। क्योंकि वे भी राजशब्दोपजीवी ही हैं। शस्त्रजीवी अथवा उद्योग-व्यापारजीवी नहीं हैं।
गणराज्यों के विषय में महाभारत में शांतिपर्व के 81वें अध्याय में भी गंभीर चर्चा है। यह वृष्णि संघ के विषय में है जिसके अध्यक्ष थे स्वयं श्रीकृष्ण। इस अध्याय में योगेश्वर श्रीकृष्ण और महर्षि नारद का संवाद है। इसमें श्रीकृष्ण नारद से कहते हैं कि मैं आपको अपना सुहृद मानता हूँ और आप में बुद्धिबल की पूर्णता है। इसलिये आपसे कुछ जिज्ञासा है। मैंने अपने ऐश्वर्य का आधा भाग कुटुम्बीजनों के लिये छोड़ रखा है। परन्तु उन्हीं कुटुम्बीजनों के कटु वचन मेरे हृदय को सदा उसी प्रकार मथते एवं जलाते रहते हैं जैसे अग्नि को प्रकट करने की कामना से अरणी द्वारा काष्ठ का मंथन किया जाता है और तब वह लकड़ी जल उठती है। बड़े भाई अपने बल में विभोर रहते हैं और छोटा भाई अपनी सुकुमारता में। बेटा रूप-सौन्दर्य से मत्त है। इस प्रकार बहुतेरे सहायकों के होते हुये भी मैं असहाय हूँ। आहूक और अक्रूर में परस्पर वैरभाव है और इनमें से किसी एक का पक्ष लेना उचित नहीं है। परन्तु इन सदा कलहरत स्वजनों का होना तो परम दुखदायी है। ऐसे में मुझे वह उपाय बताइये जिससे कि मैं श्रेयस्कर मार्ग पर चलते हुये इन सभी ज्ञातियों का हित कर सकूं? इस पर देवर्षि उत्तर देते हैं - ‘‘हे श्रीकृष्ण!, आपत्तियां दो प्रकार की होती हैं - स्वकृत अर्थात् स्वयं के कार्यों से उत्पन्न और परकृत अर्थात् दूसरों के द्वारा उत्पन्न। आपके ज्ञातिजनों की करतूतों के द्वारा प्राप्त आपत्ति आभ्यंतर आपत्ति है। क्योंकि वह इन ज्ञातिजनों ने स्वयं ही उत्पन्न की है। आपने किसी कारण से अथवा चाहे अपने कुटुम्बियों के सम्भावित कटु वचनों से डरकर अपने ऐश्वर्य का आधा अंश स्वयं ही उन्हें दे दिया। अब वह दृढ़मूल हो चुका है। आप उस ऐश्वर्य को अब पुन: ले भी नहीं सकते क्योंकि उगला हुआ अन्न वापस नहीं लिया जाता। भले ही आप परम शक्तिशाली हैं परंतु उस ऐश्वर्य को वापस लेने से कुटुम्बी जनों में भेद की वृद्धि हो जायेगी। जो स्वयं में भय का कारण है। अत: आप समर्थ होकर भी ज्ञातिजनों के संहार की संभावना वाला कोई काम नहीं करेंगे। इसलिये हे श्रीकृष्ण परिमार्जन और अनुमार्जन नामक कोमल शस्त्रों का प्रयोग कीजिये और उनकी जिव्हा बंद कर दीजिये। अपनी शक्ति के अनुसार सदा अन्नदान करना, स्वभाव की सरलता एवं कोमलता रखना तथा सहनशील रहना और सबका यथायोग्य आदर सत्कार करना, यही वह शस्त्र हैं जो लोहे का नहीं बना है परंतु उससे अधिक प्रभावशाली है। जब ज्ञातिजन कटुवचन कहें अथवा ओछी बातें कहें, उसय समय आप उनके हृदय को शांति देने वाली वाणी बोलकर उन्हें शांत करें। क्योंकि आप ही इस वृष्णि संघ के अधिपति हैं और आप तो समस्त प्राणियों के भी गुरू हैं। आप स्वयं सब जानते हैं। परंतु आपने पूछा है, इसलिये मैं सम्यक कथन कर रहा हूँ। महापुरूष सदा अपने मन को वश में रखते हैं और सहायकों की वृद्धि करते जाते हैं। आप ही इस वृष्णि संघ के मुखिया हैं और आप ही इसमें फूट फैलने से रोक सकते हैं क्योंकि फूट से इस गणराज्य का सम्पूर्ण नाश हो जायेगा। बुद्धि, क्षमा भाव और इन्द्रिय संयम के बिना तथा धन-वैभव का अंश त्याग किये बिना गणराज्य का नेतृत्व संभव नहीं है। अपने ज्ञातिजनों के प्रति आपमें अनुराग है और उन सबका भी आप पर अनुराग है। अत: आपको इसी मार्ग का अवलंबन करना होगा’’:-
आपदो द्विविधा: कृष्ण बाह्यश्चाभ्यन्तराश्च ह।
प्रादुर्भवन्ति वाष्णेय स्वकृता यदिवान्यत:।।13।।
सेयमाभ्यन्तरा तुभ्यमापत् कृच्छ्रा स्वकर्मजा।
अक्रूरभोजप्रभवा सर्वे ह्येते त्वदन्वया:।।14।।
अर्थहेतोर्हि कामाद् वा वाचा बीभत्सयापि वा।
आत्मना प्राप्तमैश्वर्यमन्यत्र प्रतिपादितम्।।15।।
कृतमूलमिदानीं तज्ज्ञातिवृन्दं सहायवन।
न शक्यं पुनरादातुं वान्तमन्नमिव त्वया।।16।।
अनायसेन शस्त्रेण मृदुना हृदयच्छिदा।
जिह्वामुद्धर सर्वेषां परिमृज्यानुमृज्य च।।19।।
शक्त्यान्नदानं सततं तितिक्षार्जवमार्दवम्।
यथार्हप्रतिपूजा च शस्त्रमेतदनायसम्।।21।।
ज्ञातीनां वक्तुकामानां कटुकानि लघूनि च।
गिरा त्वं हृदयं वाचं शमयस्व मनांसि च।।22।।
नान्यत्र बुद्धिक्षान्तिभ्यां नान्यत्रेन्द्रियनिग्रहात्।
नान्यत्र धनसंत्यागाद् गण: प्राज्ञेऽवतिष्ठते।।26।।
त्वं गुरू: सर्वभूतानां जानीषे त्वं गतागतम्।
त्वामासाद्य यदुश्रेष्ठमेधन्ते यादवा: सुखम्।।30।।
इस प्रकार महाभारत में तथा अन्यत्र भी प्राचीन काल से चले आये भारतीय गणराज्यों के विषय में विस्तार से लिखा है। बौद्ध ग्रंथों में भी और यवन यात्रियों के संस्मरणों में भी इनका विस्तृत उल्लेख है।
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Oct 2024 17:59:47
ओ३म 1. सनातन की शक्ति - वेद धर्म, ऋषिधर्म, योग धर्म या यूं कहें कि सनातन धर्म के शाश्वत, वैज्ञानिक,...