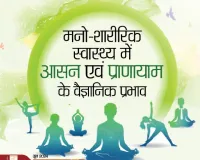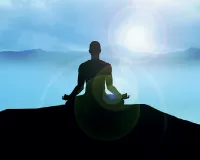प्राचीन भारत में आर्थिक चिन्तन
On

महामहोपाध्याय डॉ. महावीर अग्रवाल
प्रति-कुलपति, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार
हमारे प्रात: स्मरणीय आचार्यों ने मानव जीवन का उदेद्श्य निर्धारित किया है ‘पुरुषार्थ चतुष्टय’अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना ही मानव जीवन में प्राप्तव्य है। हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त ज्ञान, कर्म और उपासना का जो अनुष्ठान करें, वह सब इन पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिये करना चाहिए।
विश्व के प्राचीनतम ज्ञान के महासागर ऋग्वेद से लेकर समग्र वैदिक साहित्य में तथा वेदानुकूल लौकिक संस्कृत साहित्य में इन चारों के विषय में प्रचुर मात्रा में चिन्तन उपलब्ध होता है।
यद्यपि मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष, कैवल्य अथवा अमृतत्व की प्राप्ति है, पुनरपि जीवन यात्रा में पदे-पदे धर्म, अर्थ और काम भी मानव व्यवहार में विद्यमान रहते हैं। इन तीनों में भी अर्थ सर्वाधिक प्रबल पक्ष है। बिना अर्थ के कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए कहा गया- ‘अर्थस्य पुरूषो दास:’।
आज सारा संसार धनं, धनं की पुकार करता हुआ, येन केन प्रकारेण धन प्राप्ति की दौड़ में लगा हुआ है। संस्कृत कवियों ने कहा- ‘सर्वे गुणा: काञ्चनमाश्रयन्ते’’।
भारतीय प्रज्ञा वेदों को परम प्रामाणिक मानती है। ‘सर्वज्ञानमयो हि स:’ ‘वेदोऽखिलो धर्ममूलम्’‘सर्वं वेदात् प्रसिध्यति’आदि अमृतवचनों का यही अभिप्राय है कि मानव के लिये जो-जो अभिप्रेत है, वह सब वेदों में विद्यमान है। धर्म के साथ-साथ अर्थ पर भी वहां विशुद्ध विवेचन हुआ है।
संस्कृत साहित्य मे धन के पर्यायवाची अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है। यथा- अर्थ, धन, द्रविण, रयि, वित्त, रेक्ण, राध, द्युम्न, वसु, श्रव:, गय:, रिक्थ आदि। । ये सभी शब्द धन के पर्यायवाची होते हुए भी उसकी विभिन्न अवस्थाओं के प्रतिपादक है।
अर्थ- ‘अर्थ्यते प्रार्थ्यते इति अर्थ:’। यह शब्द व्यापक अर्थवाला है। धनैश्वर्य सम्बन्धी जिन-जिन पदार्थों की कामना हम करते हैं, और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय, श्रम अथवा वस्तुओं के आदान-प्रदान से जो प्राप्त करते हैं, वह अर्थ है।
धन- यह बहुत व्यापक शब्द है। इसके अन्तर्गत सुवर्ण आदि धातुएं, भूसम्पत्ति, पशु, अन्नादि चल-अचल सम्पत्ति परिगणित होती हैं, जो कि पृथिवी पर सर्वत्र विद्यमान हैं, परन्तु जब इस पर अपना, पराया, स्वामित्व, स्थायित्व, गतित्व का प्रभाव पढ़ता है तो उसकी विविध संज्ञाएं हो जाती हैं। ‘मा गृध: कस्य स्विद् धनम् (यजु- 40/1) में धन शब्द का यही अभिप्राय है।
द्रविण- उपार्जित राशि में से जो राशि हमारे व्यक्त्तिगत कार्य के लिए है उसे द्रविण कहते हैं। द्रविण प्राप्ति की प्रार्थना वेद के अनेक मन्त्रें में की गई है। यथा- ‘इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणनि देहि।’
रयि- गतिशील धन को रयि कहते हैं। दानार्थक ‘रा’ धातु से रयि शब्द निष्पन्न होता है। वेद के एक मन्त्र में प्रार्थना की गई- ‘अग्ने नय सुपथा राये’। हे अग्निस्वरूप प्रभो! हमें ‘रै’ अर्थात् धनश्वर्यों की प्राप्ति के लिये सुपथ से ले चलो।
वित्त- ब्रह्मराशि में से जो भाग चुकाने के लिए है उसे वित्त कहते हैं। ‘वित्यते त्यज्यते अनेनेति वित्त:’ अर्थात् जो भाग दिया जाता है उसे वित्त कहा जाता है। उपनिषद् में आया- ‘न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य:।’
रेक्ण- किसी की ओर शेष राशि जो कि संशयित है, अर्थात् जिसकी प्राप्ति की आशा कम रह जाती है, उसे ‘रेक्ण’ कहा गया है। रिच् धातु से अगुन् प्रत्यय करने पर यह सिद्ध होता है।
राध:- द्रविण में से बचकर जो भाग अपनी निधि को बढ़ाता है, उसे राध: कहते हैं। महर्षि दयानन्द सरस्वती यजुर्वेद भाष्य में राध: का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखते हैं- ‘राध्नुवन्ति सम्यङ् निर्वर्तयन्ति सुखानि येभ्य: साधनेभ्यस्तानि। यजु- 3/13
द्युम्न- राध संज्ञक धन-राशि से हम जिन स्वर्ण, हीरा, मोती आदि पदार्थों को क्रय करते हैं, भवन आदि बनवाते हैं, वह द्युम्न है। महर्षि दयानन्द ने वेद भाष्य में द्युम्न का अर्थ धन ही किया है।
वसु:- भू-सम्पत्ति एवं भवन आदि की निवास योग्य सम्पत्ति वसु कहलाती है। वेद में परमात्मा को ‘वसोष्पति’ कहा गया है। ‘वसोष्पते नि रमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्।’
श्रव: - जिस धन का दानादि में विनियोग हो या यज्ञादि कार्यों का जिस धन से विस्तार हो वह श्रव: कहलाता है। श्रव:, यश अथवा कीर्ति को भी कहते हैं। जो धन कीर्ति प्रदान करे, वह श्रव: है।
गय:- जिस धन या सम्पत्ति को हम अपनी सन्तानों के लिए, प्रजा के कल्याणार्थ अथवा राज्य के विस्तार में लगाते हैं, वह गय: है। गय: का अर्थ सन्तान भी कहा गया है।
रिक्थ- जिस सम्पत्ति को हम दाय भाग के रूप में प्राप्त करते हैं- या दाय भाग के लिए रखते हैं, वह ‘रिक्थ’ संज्ञक है।
इनके अतिरिक्त भी अनेक धन के पर्यायवाची शब्द प्राचीन वैदिक साहित्य में उपलब्ध है।
प्राचीन साहित्य में अर्थ प्राप्ति के कृषि, वाणिज्य, उद्योग, शिल्पकला, पशुपालन, कुटीर-उद्योग, सेवा कार्य आदि अनेक उपाय बताये हैं। कर व्यवस्था, परिवहन, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का भी अनेक स्थानों पर उल्लेख है किन्तु इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण चिन्तन है- अर्थ के प्रयोग का। पञ्चतन्त्र आदि नीतिग्रन्थों में धन की तीन गतियां प्रतिपादित की हैं।
दानं भोगो नाशश्चेति तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य।
यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गति र्भवन्ति।।
जो मानव न दान करता है और न अर्जित धन का ठीक प्रकार से उपभोग करता है, उसके धन की तीसरी गति अर्थात् विनाश ही होता है।
यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं-
ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध: कस्यस्विद्धनम्।। यजु- 40.1
इस गतिशील संसार में जो कुछ है, वह परमात्मा से व्याप्त है। वह ईश्वर सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है। संसार का समस्त ऐश्वर्य उसी का है इसलिए हमारे पास जो धन-वैभव है, उसका हम त्यागभाव से उपभोग करें। गिद्ध दृष्टि न रखें, यह धन किसका है? क: अर्थात् उसी प्रजापति का है। संस्कृत के एक मनीषि ने कितना सुन्दर लिखा है-
यावद् भ्रियेत जठरं तावत् सत्वं हि देहिनाम्।
अधिकं योऽभिमन्यते स स्तेनो दण्डमर्हति।।
जितने धन से हमारी जीवन यात्रा सुखपूर्वक चल सकती है, हमारा अधिकार उतने पर ही है। जो इससे अधिक को अपना समझता है उसे हमारी चिन्तन धारा स्तेन (चोर) मानती है, और वह दण्डनीय है। हमारे पूर्वज सदैव सुमार्ग और परिश्रम से प्राप्त लक्ष्मी को ही वरेण्य मानते थे, जो जीवन की सुख, शान्ति को नष्ट न करने वाली हो-
या मा लक्ष्मी: पतयालुर जुष्टा अभिचस्कन्द बंदनेव वृक्षम्।
अन्यत्रास्मद् सवितस्तामितो धा: हिरण्यस्तो वसु वो रराण:।।
अथर्व 7.115.2
प्रभु हिरण्य हस्त है। ऐश्वर्य, स्वर्ण हितकर और रमणीय रूप में उसके हाथों में चमक रहे हैं। वे ही इसका वितरण और विभाजन प्राणियों में कर रहे हैं। समग्र ऐश्वर्य प्रभु का है, हम तो मात्र उसके न्यासी (ट्रस्टी) हैं, यह भाव रखते हुए परिश्रम और ईमानदारी से अधिकाधिक धन अर्जित करना और मानवमात्र के तथा राष्ट्रहित में उसे वितरित करना, यही वेद का सन्देश है- शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर।
हमारा प्राचीन साहित्य कहता है- ‘सहभक्षा: स्याम’हम साथ भोजन करें। हमारे भारतीय समाज का यह पावन गीत है-
‘सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
भारतीय जन प्रतिदिन वेद की इस पावन ऋचा का उच्चारण करते हैं
‘मोघमन्नं विन्दते अप्रचेता: सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य।
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी।। ऋग- 10.117.6
जो अकेले भोजन करते हैं वे अन्न भक्षण न करते हुए केवल पाप भक्षण ही कर रहे होते हैं। ऐसा भोग उन्हें किसी भी तरह पुष्ट नहीं करता।
वेदों में कहीं भी धन की निन्दा नहीं की गई है, अपितु उपासक सन्ध्या, यज्ञादि करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता है- ‘वयं स्याम पतयो रयीणाम्’
हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बनें। संस्कृत साहित्य में दरिद्रता की निन्दा करते हुए कहा गया- ‘दारिद्रंय षष्ठं महापातकम्’।
संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक ‘मृच्छकटिकम्’ में महाकवि शूद्रक निर्धनता की दयनीय दशा का चित्रण करते हुए लिखते हैं-
दारिद्रयात् पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न सन्तिष्ठते,
सुस्निग्धा विमुखी भवन्ति सुहृद: स्फारी भवन्त्यापद:।
सत्वं हृासमुपैति, शीलशशिन: कान्ति: परिम्लायते,
पापं कर्म च यत् परैरपि कृतं तत्तस्य सम्भाव्यते।। मृच्छ 1.14
अर्थात्- दरिद्रता के कारण मनुष्य के मित्रगण उसकी बात नहीं सुनते। प्रिय मित्र भी विमुख हो जाते हैं। आपत्तियां बढ़ जाती हैं शक्ति क्षीण हो जाती है, शीलरूपी चन्द्रमा की कान्ति भी मलिन पड़ जाती है तथा दूसरे का किया हुआ पाप कर्म भी उसी पर आरोपित कर दिया जाता है।
एक अन्य पद्य में कहा-
शून्यमपुत्रस्य गृहं, चिरशून्यं नास्ति यस्य सन्मित्रम्।
मूर्खस्य दिश: शून्या:, सर्वं शून्यं दरिद्रस्य।। मृच्छ, 1.8
पुत्रहीन व्यक्ति का घर सूना होता है, जिसका कोई अच्छा मित्र नहीं उसका जीवन चिरशून्य होता है, मूर्ख व्यक्ति के लिए समस्त दिशाएं शून्य होती हैं, जबकि निर्धन व्यक्ति के लिए तो घर, समय और दिशाएं सभी कुछ सूना होता है।
वे पुन: लिखते हैं-
एतत्तु मां दहति यद्गृहमस्मदीयं,
क्षीणार्थमित्यतिथय: परिवर्जयन्ति।। मृच्छा 1.12
यह बात मुझे अत्यन्त सन्ताप्त करती है जो कि अतिथियों ने धनहीन मानकर मेरे घर पर आना ही छोड़ दिया है।
इस प्रकार निर्धनता कदापि उपयुक्त नहीं है। यह भारत देश पुराकाल में धन-धान्य से संपन्न परमैश्वर्यवान देश था। इसीलिये इसे सोने की चिडिय़ा ‘स्वर्ण चटका’कहा जाता था।
महर्षि दयानन्द सरस्वती अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास के प्रारम्भ में लिखते हैं-
‘‘यह आर्यावर्त देश ऐसा देश है, जिसके सदृश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है। इसलिये इस भूमि का नाम सुवर्णभूमि है, क्योंकि यही सुवर्णादि रत्नों को उत्पन्न करती है। इसीलिए सृष्टि की आदि में आर्य लोग इसी देश में आकर बसे। जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते और आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है, वह बात तो झूठी है परन्तु आर्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिसको लोहे रूप दरिद्र विदेशी छूते के साथ ही सुवर्ण अर्थात् धनाढ्य हो जाते हैं।’’
प्राचीन भारतीय धर्म का पूर्णत: परिपालन करते थे। राजधर्म, गुरुधर्म, शिष्यधर्म, पुत्रधर्म, पतिधर्म, मातृ-पितृ धर्म का पालन करते हुए सभी मर्यादित जीवन जीते थे। अर्थ का अर्जन और उसका उपभोग भी धर्म पूर्वक ही करते थे। ‘अक्षैर्मा दिव्य: कृषिमित् कृषस्व।’ ऋ . 10.34.7
आदि वचन कृषि की महत्ता को दर्शाते हैं तो ‘अन्नं वै ब्रह्म’कहकर हमने अन्न को ईश्वर के समान गौरव प्रदान किया है।
‘शंनो द्विपदे शं चतुष्पदे।’अथर्व- 12.2.40 से पशुपालन का सन्देश प्राप्त होता है। शिल्पियों, वास्तुविदों, अभियन्तागणों, व्यापारियों, उद्यमशीलों की प्रशंसा से तत्कालीन अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में इन सबका योगदान हमारे नेत्रों के समक्ष उपस्थित हो जाता है। कर व्यवस्था अत्यन्त सुदृढ़ थी। राजकोष में एकत्रित होने वाला धन प्रजा के कल्याण में व्यय होता था। महाकवि कालिदास के अमर नाटक अभिज्ञान शाकुन्तल एवं रघुवंश महाकाव्य में इसका सुन्दर चित्रण प्राप्त होता है। महाकवि दुष्यन्त के मुख से कहलवाते हैं-
‘तप: षड्भागमक्षय्यं ददत्यारण्यका हि न:’। अर्थात् समस्त प्रजा अपनी आय का छठा भाग आयकर के रूपमें राजकोष में जमा करती थी। इस अर्थ के सुदपयोग का वर्णन करते हुए वे रघुवंश में कहते हैं-
‘‘प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्।
सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रवि:।।’’रघुवंश प्रथम सर्ग।
रघुवंशीय राजा अपनी प्रजा से कर के रूप में जो लेते थे, उसे प्रजा के कल्याण के लिये ही व्यय कर देते थे, जैसे- सूर्य, पृथिवी से जल ग्रहण कर, उसे हजारों गुणा करके पुन: भूमि को ही प्रदान कर देते हैं।
कैसी उत्तम अर्थ व्यवस्था थी। यही रामराज्य था, यही वैदिक संस्कृति थी, यही प्राचीन ज्ञानधारा थी। आज पुन: उसी परम पावनी अर्थव्यवस्था की देश को आवश्यकता है।
लेखक
Latest News
01 Nov 2024 17:59:04
जीवन सूत्र (1) जीवन का निचोड़/निष्कर्ष- जब भी बड़ों के पास बैठते हैं तो जीवन के सार तत्त्व की बात...