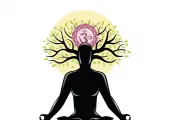भाव-विचारों में मतभेद व मनभेद
On

श्रद्धेय गुरुदेव
आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज
मनुष्य के व्यक्तित्व में बुद्धि व मन की विशेष भूमिका है। विचार व भाव इन दोनों के साथ सम्बद्ध रहते हैं। विचार का सम्बन्ध बुद्धि के साथ होता है और भावों का मन के साथ। विचार प्रकाश-रूप होते हैं और भाव शक्ति-रूप। प्राय: ऐसा होता है कि जैसे विचार होते हैं, उसी के अनुरूप भाव बन जाते हैं और फिर यह नियम उलट भी जाता है, जैसे भाव होते हैं वैसे ही विचार उत्पन्न होने लगते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति को स्वार्थी, अहङ्कारी, लोभी, ईष्र्यालु, द्वेषी, क्रोधी, प्रतिशोध लेने वाला समझते हैं अर्थात् यदि किसी व्यक्ति का इन्हीं रूपों वाला चित्र हमारे समक्ष उपस्थित होता है तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कभी भी सद्भाव (प्रेम, विश्वास, सम्मान, स्नेह, पूजा, श्रद्धा इत्यादि) उत्पन्न नहीं होंगे। साथ में किसी के प्रति हमारे भाव उत्तम नहीं हैं, घृणापूर्ण तुच्छ भाव हैं तो उसके प्रति विचार भी उत्तम नहीं होंगे, फिर यदि किसी के प्रति भाव उत्तम हैं तो विचार भी उसके प्रति उत्तम ही होंगे और यदि विचार उत्तम हैं तो भाव भी उसके प्रति उत्तम ही होंगे। अर्थात् भाव व विचार विसंवादी नहीं होते बल्कि सुसंवादी ही रहते हैं। भाव व विचार के विषय में यह भी एक बात रहती है कि सद्भाव आगे फिर सद्भावों को जन्म देते हैं और सद्विचार सद्विचारों को तथा असद्भाव असद्भावों को और असद्विचार असद्विचारों को जन्म देते रहते हैं। |
भाव व विचार में किसके अनुसार चलने से व्यक्ति या समाज का अधिक भला हो सकता है। भला या बुरा तो शुद्धि-अशुद्धि के आधार पर होता है। यदि भाव व विचार दोनों ही शुद्ध हैं अर्थात् बुद्धि व मन दोनों ही निर्मल हैं तो किसी के भी अनुसार चलें, भला ही होगा। और दोनों अशुद्ध हैं तो किसी के भी अनुसार चलेंगे, बुरा ही होगा। भावों की शुद्धि होती है तप व त्याग से, सबके प्रति उदार होने से, किसी का नाममात्र भी अहित न करने से, सदा ही भलाई करने से, किसी भी अच्छाई का या भलाई का अभिमान न करने से, किसी भी प्रकार के त्याग का अभिमान छोड़ देने से या भागवत प्रेम से, अपनी मान्यता के अनुसार आचरण करने से, काम-क्रोध-लोभादि विकारों से मुक्त होकर जीवन जीने से, अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रह तथा शौच-सन्तोष-तप-स्वाध्याय-ईश्वरप्रणिधान से। उपर्युक्त ये सभी उपाय भावशुद्धि के साधन हैं तथा विचार अर्थात् बुद्धि की शुद्धि के साधन हैं- शास्त्र व अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन, संसार के पदार्थों के प्रति आसक्ति का त्याग, ध्यान व एकाग्रता के द्वारा भगवान् के 'भर्ग’ नामक तेज का धारण करना अर्थात् ईश्वर स्तुति-प्रार्थना-उपासना, जीवन के प्रत्येक पहलू पर गहराई के साथ किया गया विचार भी बुद्धि को शुद्ध करने का साधन है इत्यादि। भावों की शुद्धि से विचारों की शुद्धि और विचारों की शुद्धि से भावों की शुद्धि-यह प्रक्रिया भी साथ-साथ चलती रहती है।
मानव व्यक्तित्व में उच्च और निम्र को श्रेणीबद्ध (hierarchy) करके देखा जाए तो आत्मा सर्वोच्च पद पर है, जो भी आत्मा के निकट होगा वह उच्च और जितना आत्मा से दूर होगा वह उतना ही निम्र होता जायेगा। आत्मा के निकटतम बुद्धि तत्त्व है, मन बुद्धि से अवर है। अत: विचार का स्थान ऊँचा हुआ और भाव उसके अधीनस्थ। इच्छा की जन्मभूमि मन है किन्तु इच्छा तो सदा ज्ञान के अनुसार होती है। कभी भी ज्ञान के उच्च धरातल पर ठहरे हुए व्यक्ति में अवर या निम्र इच्छा पैदा नहीं हो सकती। निम्र धरातल पर खड़े व्यक्ति में उच्च इच्छा उत्पन्न हो सकती है पर वह तभी जब उसे कोई उच्च सत्सङ्ग या कोई वैसा शास्त्र का आलम्बन मिल जाए, उसकी बुद्धि उस ज्ञान को अपने लिए उपयोगी स्वीकार कर ले। अत: कहा जाता है यदि किसी भी उपाय से व्यक्ति का ज्ञान शुद्ध हो जाता है तो इच्छाएँ भी बदल जाती हैं। यह हम स्पष्ट कर चुके हैं कि भावशुद्धि का ज्ञानशुद्धि पर बहुत ही कारगर प्रभाव पड़ता रहता है। ज्ञानशुद्धि कहें या विचारशुद्धि, एक ही बात है।
यदि विचार असमान हैं तो उससे भाव भी प्रभावित होते हैं और जब दो व्यक्तियों के पृथक् विचारों के द्वारा भाव प्रभावित हो गए तो जीवन नीरस हो जाता है। क्योंकि जीवन में सरसता का आगमन तो भावों के द्वारा ही होता है। ऐसी समस्या आने पर महापुरुष यह उत्तर देते हैं कि ‘बेशक तुम्हारा विचार-भेद (मतभेद) हो जाए पर मन-भेद नहीं होना चाहिए। |
परिवार में, समाज में या किसी संस्था में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब काम करते हैं तो उनके विचार (उनकी दृष्टि) और उनके भाव (प्रेम, सम्मान, विश्वास इत्यादि) यदि समान हों तब तो कोई समस्या ही नहीं होती। किन्तु यदि विचार असमान हैं तो उससे भाव भी प्रभावित होते हैं और जब दो व्यक्तियों के पृथक् विचारों के द्वारा भाव प्रभावित हो गए तो जीवन नीरस हो जाता है। क्योंकि जीवन में सरसता का आगमन तो भावों के द्वारा ही होता है। ऐसी समस्या आने पर महापुरुष यह उत्तर देते हैं कि 'बेशक तुम्हारा विचार-भेद (मतभेद) हो जाए पर मन-भेद नहीं होना चाहिए। किन्तु व्यवहार में दो व्यक्तियों के बीच का यह प्रसङ्ग तो ऐसा है कि यहाँ यह आवश्यक नहीं कि किन्हीं दो व्यक्तियों की दृष्टि, सिद्धान्त आदि मिलते हों तो वे अवश्य ही एक-दूसरे से प्रेम करेंगे। उनके अपने-अपने अहङ्कार, अपने स्वार्थ भी तो बीच में आ जाते हैं। अत: व्यक्तियों के बीच में भावपूर्ण स्थिति में जीने की जो बात है उसके लिए कुछ अलग ही प्रयत्न करना पड़ता है। दो व्यक्ति सर्वथा विरुद्ध दृष्टि व स्वभाव वाले हों, जैसे गीता के शब्दों में एक दैवी सम्पत् को महत्त्व देता है और दूसरा आसुरी सम्पत् को, तब तो एक ही जगह रहना और रसमय होकर काम करना कठिन हो जाता है। अन्यथा अपने अहङ्कार व स्वार्थ को हटाकर मिलकर काम किया जा सकता है। कई परिवारों के ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि पत्नी देवता के साकार विग्रह की पूजा में विश्वास करती है और पति निराकार का उपासक है फिर भी बड़े प्रेम से रहते हैं। यहाँ दोनों की उन्नत समझ के कारण ऐसा हो रहा है। दोनों में कोई भी एक यदि आग्रह करने लगे कि आपको ऐसा ही करना है तो अवश्य ही समस्या बन जायेगी, किन्तु आग्रहरहित होने पर कोई समस्या नहीं। अर्थात् वहाँ मतभेद तो है पर मनभेद नहीं।
ब्रह्मसूत्र में अनेकत्र बादरायण ने कई ऋषियों के अपने से अलग मत दर्शाए हैं, इसी प्रकार चरक में पुनर्वसु आत्रेय का कई विषयों में अन्य ऋषियों के साथ मतभेद देखने को मिलता है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि बादरायण या पुनर्वसु उन ऋषियों से प्रेम नहीं कर रहे जिनके साथ उनका मत वैविध्य है। श्री अरविन्द ने बुद्ध के दु:खवाद और आचार्य शङ्कर के मायावाद का खण्डन करते हुए भी इन दोनों महापुरुषों की बड़ी महिमा भी गाई है क्योंकि श्री अरविन्द का उन महापुरुषों से आंशिक रूप में मतभेद होते हुए भी मनभेद नहीं है। महर्षि दयानन्द ने भगवान् शङ्कराचार्य की अद्वैत दृष्टि का खण्डन भी किया और उनकी प्रशंसा भी ढ़ेर सारी की। अत: मतभेद होने पर भी मनभेद नहीं है। उनको आदरणीय, प्रशंसनीय मानते हैं तभी तो उनके द्वारा किए गए 'शास्त्रयोनित्वात्’ सूत्र के भाष्य को अपनी 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका’ में किसी प्रसङ्ग में उदाहरण व प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। जिसका जिससे मनभेद हो तो वह उसके भाष्य को इस प्रकार प्रमाण के रूप में उपस्थापित नहीं करेगा। जैसा कि महर्षि दयानन्द वाम मार्गियों के ग्रन्थ से कोई कितनी ही अच्छी बात हो उसका उदाहरण नहीं देंगे। स्वामी दयानन्द के विचार से श्रीमद्भागवत के लेखक वेदव्यास न होकर उत्तरकालिक कोई विद्वान् हैं और उन्होंने उस ग्रन्थ की और उस लेखक की कटु आलोचना भी की है। अब मैं कहना यह चाहता हूँ- श्रीमद्भागवत में हजारों बातें बहुत उत्कृष्ट होने पर भी स्वामी दयानन्द ने उसका एक भी उदाहरण अपने ग्रन्थों में प्रमाण के रूप में या एक सुन्दर उक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि उनका उस ग्रन्थ के लेखक के साथ मतभेद ही नहीं है गहरा मनभेद भी है। भगवत्पाद शंकराचार्य जी को तो उद्घृत कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ आंशिक मतभेद होते हुए भी उनका मनभेद नहीं है।
व्यवहार में भी देखने में आया कि कोई व्यक्ति क, ख के समक्ष ग की किसी दार्शनिक विषय में प्रशंसा कर रहा है किन्तु ख को ग के द्वारा स्वीकृत सिद्धान्त मान्य नहीं है अत: जैसे ही क, ग की चर्चा चलाना आरम्भ करता है तो ख, क को रोकते हुए कहता है- अरे! इस व्यक्ति की मेरे सामने कोई बात मत करो। क्योंकि ख ने ग को अपने सिद्धान्त का विरोधी मान लिया है और वह विरोध मतभेद के साथ-साथ मनभेद तक पहुँच गया। मतभेद से मनभेद को दर्शाने वाले ऐसे अनेक उदाहरण मिल जायेंगे। अत: प्रकृत में सार बात यही है कि विचार भेद से इतनी बड़ी हानि नहीं है जितनी कि मनभेद से। अत: मनभेद से अपने को बचाने के लिए किसी भी सच्चे साधक को ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है।
अब यह बात सामने आती है कि उस ध्यान देने का क्या स्वरूप होगा जो हमें मनभेद होने से बचा सके। पहली बात तो यही है कि व्यक्ति अपनी गहरी आँखों से यह देख सके कि अमुक व्यक्ति के साथ मेरा मतभेद के साथ मनभेद होता जा रहा है जो कि मेरे जीवन को अनावश्यक दु:ख के बोझ से बोझिल बना देगा। दु:खमुक्त जीवन की माँग ही एक ऐसा सशक्त उपाय है कि अपने आप आगे से आगे चलने के लिए बाधा रहित पथ प्राप्त होता रहता है। यदि हम देख सकें कि अहङ्कार-ईष्र्या-द्वेष-घृणा ये सभी दुर्भाव असंस्कृत मन में ही पैदा होते हैं तो हम अपने मन को असंस्कृत रखना नहीं चाहेंगे। स्वाभाविक रूप से मनुष्य में दिव्यता का बीज है। विधाता ने मानव की रचना ही ऐसी की है कि उसे असत्य के प्रति घृणा (अश्रद्धा) और सत्य के प्रति लगाव (श्रद्धा) जन्मजात प्राप्त है। केवल इतनी बात है कि उसे असत्य असत्य के रूप में और सत्य सत्य के रूप में दिखना चाहिए। बस आगे का काम तो अपने आप हो जाता है। Seeing the false as the false and the true as the true is transformation, because when you see something very clearly as the truth, that truth librates. When you see that something is false that false thing drops away.
क्योंकि कौन ऐसी समझदार माँ होगी कि घर के बीच में किसी छोटे बच्चे ने मल-मूत्र कर दिया और वह उसे अनदेखा करके उस स्थान की सफाई न करे और अपने किसी दूसरे काम में व्यस्त रहे। ऐसे प्रसङ्गों में यही देखा गया है कि वह माता अपने सब आवश्यक कार्यों को छोड़कर पहले गन्दगी की सफाई करती है, फिर किसी और काम को हाथ लगाती है। इसी प्रकार यदि हमें अपना मन अशुद्ध दिखाई दे जाए तो हम भी उसे शुद्ध करने के लिए व्यग्र हो उठेंगे। इससे तो यह बात सामने आई कि हमारी बुद्धि हमारे मन की अशुद्धि को दिखाती है और फिर मन में वह शक्ति आती है कि वह अपनी अशुद्धि को साफ करे। हाँ! इसीलिए तो हमने प्रारम्भ में ही कहा कि विचार और भाव या बुद्धि व मन Reciprocal होते हुए एक दूसरे पर काम करते हैं। भावशुद्धि से बुद्धि शुद्ध होती है और शुद्ध बुद्धि पुन: भावों को शुद्ध करती है। बुद्धि का गहरा हिस्सा भावों की शुद्धि-अशुद्धि को देख पाता है और बुद्धि का सतही रूप तो तात्कालिक प्रतिक्रियाओं से प्रभावित रहता है। अत: भावों को शुद्ध करने के लिए व्यक्ति को गम्भीर होना पड़ता है। स्वयं में रसमय जीवन की प्यास जगानी पड़ती है। रस को भङ्ग करने वाली या रस में बाधा डालने वाली चीजों को देखना पड़ता है।
यदि व्यक्ति ऐसे प्रसङ्गों में सचेत होकर एक कदम पीछे हट जाए तो समाधान निकल आता है। इसके लिए Step Back इस सूत्र को अपने समक्ष रख सकते हैं। सुनने में यह सामान्य समाधान लगता है किन्तु यह आचार-शास्त्र का हीरा (Gem) है।
इसी से मिलता-जुलता एक दूसरा सूत्र है व्यक्ति को हमेशा ध्यान रहे कि 'मम सत्यम्’ का अर्थ होता है युद्ध। युद्ध विरोधी-शक्तियों के साथ किया जाता है। अपनों के साथ ही युद्ध करने का कोई औचित्य नहीं। परिवार, समाज, संस्था के सभी घटक परस्पर विरोधी नहीं होते बल्कि एक-दूसरे के पूरक (Complimentary) होते हैं। हमें सदा अपने भीतर यह भाव जगाना चाहिए कि मुझे पूरक बनकर अपनी भूमिका का निर्वाह करना है। एक ग्रामीण स्थूल कहावत है कि 'हार मानी, झगड़ा टूटा’। अपने ही लोगों के साथ कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो भी जाए तो हार मानने में ही विजय है।
अहङ्कार, ईष्र्या, घृणा ये सब प्रेम के विरोधी भाव हैं। जैसे अन्धकार को प्रकाश से हटाया जाता है वैसे ही प्रेम से इन दुर्भावों को हटाने में पूर्ण स्वाभाविकता है। जैसे प्रकाश के अभाव या अवरोध का नाम अन्धकार है, इसी प्रकार प्रेम के अभाव या अवरुद्ध होने पर ये सब दुर्भाव प्रकट हो जाते हैं, प्रकट होने लगते हैं। अत: मनभेद करने वाले अहङ्कार-ईष्र्या-द्वेष आदि भावों को मुझे किञ्चित् भी स्थान नहीं देना- ऐसे संकल्प को सदा जागरित रखना चाहिए।
जैसा कि हमने कहा कहीं विचार भेद होने पर भी मन भेद को विचार के द्वारा या प्रेम के द्वारा हटाया जा सकता है, किन्तु जहाँ संस्कृति का ही अन्तर हो जाता है जैसे एक को हिंसा, भोग व अनावश्यक संघर्ष में बड़ा मजा आता है, अहङ्कार का पोषण ही जिसकी खुराक है, दूसरा स्वभाव से ही अहिंसक है, योग जीवन का पक्षपाती है, शान्तिप्रिय है, ऐसी स्थिति में तो मन भेद को समाप्त कर पाना कठिनतम कार्य बन जाता है। अर्थात् विरुद्ध संस्कृतियों वालो में ऐसा प्रेम हो पाना मुश्किल है कि एक ही घर में रहते हुए बिना बाधा के प्रेम से रह सकें। इसलिए वैवाहिक जीवन पर विचार करने वाले लोग विवाह करने के इच्छुक लोगों को यह सलाह देते हैं कि आपके गुण-कर्म-स्वभाव परस्पर जितने अधिक समान होंगे उतना ही जीवन में सुख बढ़ेगा।
ऋग्वेद के अन्तिम संज्ञान सूक्त में भी समान मानसिकता का संदेश देते हुए कहा गया-
संगच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते।। (ऋ० १०.१९१.२)
हे मनुष्यों! मिलकर चलो, एकमत होकर बोलो। तुम्हारे मन एकमत हो जाएँ। जिस प्रकार दान, दिव्यता आदि गुणों से युक्त हमारे पूर्वजों ने परस्पर मिलकर निर्लोभ भाव से अपने-अपने भाग का सेवन किया है, दूसरे के भाग को लेने का लालच नहीं किया, उसी प्रकार तुम भी परस्पर मिलकर खाते-खिलाते हुए अपने भाग को ग्रहण करो। अर्थात् परस्परता में तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार जो तुम्हें भोग, साधन या सम्मान मिलता है उसी में संतुष्ट व प्रसन्न रहो, दूसरों को प्राप्त साधन, सम्मान व प्रभुता से ईष्र्या मत करो। अपने अहङ्कार को बीच में मत लाओ, ऐसा मत सोचो कि मेरी तो कुछ चलती ही नहीं, सब जगह इसी की चलती है या उसकी ही चलती है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, इत्यादि।
समानो मन्त्र: समिति: समानी समानं-मन: सहचित्तम् एषाम्।
समानं मन्त्रम् अभि मन्त्रये व: समानेन वो हविषा जुहोमि।। (ऋ० १०.१९१.३)
अर्थात् तुम्हारा चिन्तन, मनन और विचार एक हो। विभिन्न विषयों और समस्याओं पर विचार करने के लिए सबका संगठन, सबकी संगोष्ठी अथवा सभा एक हो। मैं (राजा अथवा उपदेशक) तुम सबको एक ही मन्त्र, एक ही विचार, एक ही सलाह दे रहा हँू कि जिस प्रकार सब देवता एक ही अग्नि अथवा यज्ञकुण्ड से अपनी हवि ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार तुम भी एक ही स्थान पर एक साथ मिलकर अन्न ग्रहण करो। इसी के लिए मैं तुम्हारा आह्वान कर रहा हूँ।
समानी व आकूति: समाना हृदयानि व:।
समानम् अस्तु वो मनो यथा व: सुसहासति।।
(ऋ० १०.१९१.४)
हे मनुष्यों! तुम्हारा सङ्कल्प, तुम्हारा निश्चय एक हो, तुम्हारा हृदय एक हो, तुम्हारा मन एक हो, जिस प्रकार से तुम्हारा सुसङ्गठन, उत्तम साथ, उत्तम संगठन हो जाये।
इस प्रकार यह समग्र अध्ययन हमें यह दिशा देता है कि आदर्श स्थिति तो यही है कि हमारे ऊपर प्रेम का शासन हो। एकत्व, भाईचारा (Unity, Brotherhood) आदि शब्दों से भी इसी आदर्श को अभिव्यक्त किया है। अन्य-अन्य देशों के भी सभी दार्शनिकों, विचारकों, चिन्तकों का यही निष्कर्ष है कि प्रेम में ही समाधान है व्यापक स्तर पर भी और सीमित स्तर पर भी, अर्थात् एक शरीर, परिवार, संस्था, समाज, देश और विश्व तक। वह व्यक्ति सबसे सुखी होगा जिसकी सत्ता के सभी अङ्ग, सभी घटक सुसंवादी हों। जिसके मन, बुद्धि, प्राण, भाव सब अलग-अलग दिशा में जा रहे हैं वह कैसे सुखी हो सकता है।
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Nov 2024 17:59:04
जीवन सूत्र (1) जीवन का निचोड़/निष्कर्ष- जब भी बड़ों के पास बैठते हैं तो जीवन के सार तत्त्व की बात...