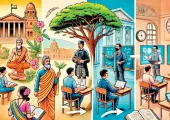शारीरिक व मानसिक स्वास्थ हेतु आहार चिकित्सा
On

डॉ. रश्मि अतुल जोशी
साइंटिस्ट-सी, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, हरिद्वार
भारतवर्ष में सदियों से ऋषि-मुनियों ने प्राकृतिक संसाधनों से स्वस्थ शरीर की अवधारणा पर जोर दिया है। विभिन्न प्राकृतिक तत्व जैसे मिट्टी, जल, हवा, धूप, जड़ी-बूटियों द्वारा विभिन्न रोगों की उपचार पद्धति को ही हम आज के परिपेक्ष्य में प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में समझते हैं जो कि वास्तव में जीवन जीने की अद्भुत कला है। मनुष्य पंचतत्वों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) से बना हुआ, प्रकृति का हिस्सा है। इन तत्त्वों का विभिन्न कारणों से मनुष्य में असंतुलन ही विभिन्न प्रकार के रोगों का कारक होता है, जिसके फलस्वरूप विजातीय द्रव्यों का समावेश होता है। आज के परिपेक्ष्य में हमारी विकृत जीवन शैली के कारण यह विजातीय द्रव्य शरीर से निकल नही पाते हैं और मनुष्य शारीरिक रोग से ग्रस्त हो जाता है। यह विजातीय द्रव्य शरीर में घटते बढ़ते रहते हैं एवं अपना स्थान बदलते रहते हैं जिसके फलस्वरूप रोग भी बढ़ते घटते व रूपान्तरित होते रहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में आहार (पृथ्वी) एक मुख्य स्तंभ है, इसके साथ पंचमहाभूतों के अन्य तत्व (जल, वायु, आकश व अग्नि) के द्वारा भी उपचार किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा हमें आहार, निद्रा, पेयजल, सूर्य का प्रकाश, विशुद्ध हवा, सकारात्मकता एवं योग विज्ञान का समुचित ज्ञान कराती है, जिसके द्वारा न केवल रोग ठीक होते हैं अपितु मनुष्य आगे रोगयुक्त भी नही होता है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार ‘आहार ही औषधि’ है ऐसा माना जाता है एवं उसे प्राकृतिक औषधी के रूप में भी समझा जाता है। भोजन को उसके प्राकृतिक स्वरूप में ही ग्रहण करना चाहिये यही आहार चिकित्सा का मुख्य सिद्धांत है। उसमें उपलब्ध खनिज, लवण व अन्य जरूरी पोषक तत्व मनुष्य के शरीर में लाभ प्रदान करते हैं व बीमारियों से लडऩे की क्षमता प्रदान करते हैं।
‘‘पृथ्वी न चाहारसम किंचिद् भैषज्य मुकलभ्यते।
शक्यतेऽयन्नं मात्रेण नर: कुर्त निरामय:।।
भेषजो नोपन्नोऽसि निराहारो न शक्यते।
तस्याद् भिषग्भिराहारो महा भैषन्यनुच्यते।।
अर्थात्! भोजन से बढक़र दूसरी दवा नहीं है, केवल भोजन में सुधार से मनुष्य के सारे रोग दूर हो जाते हैं। दवा कितनी भी दी जाए यदि रोगी के भोजन में उचित सुधार न किया जाए तो कुछ लाभ नहीं होगा। मनुष्य जो खाता है, वह भैषज्य नहीं महाभैषज्य (प्राणिनामप्राण, महाभैषज्य या ब्रह्म आयुर्वेद में कहा गया है) है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का मनुष्य के शरीर और मन दोनों पर प्रभाव पड़ता है। मन की शुद्धता सात्विक आहार पर निर्भर रहती है और ईश्वर स्तुति शुद्ध मन पर निर्भर रहती है। आहार-विहार एवं रहन-सहन की अनियमितता तथा असंयमता के कारण ही रोगों का प्रादुर्भाव होता है। अगर इस अनियमितता से मनुष्य अपने को दूर कर ले तो वह निरोगी व सुखी जीवन व्यतीत करने में समर्थ हो जाएगा। अतैव प्राचीनकाल से ही उपवास रखना, सादा भोजन खाना नियमित समय पर भोजन ग्रहण करना इत्यादि का वर्णन हमें प्रमुख ग्रंथों में मिलता है।
‘‘अधतेडीप च भूतनित्यन्नत्व मुच्यते
तैत्तिरीयक वेदान्ते तस्य भावोऽनुचिन्तयताम्
अध्यते विधिवद मुक्तमति भोकतरमन्यथा (तैतरीय उपनिषद)
अर्थात् भोजन जो ग्रहण किया जाता है तथा जिसके द्वारा किया जाता है वह दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। गलत विधि के द्वारा जो भोजन ग्रहण करता है, उसको वो भोजन ही खा जाता है- वह मनुष्य में विपरीत प्रभाव डालता है। सही विधि से पकाया भोजन व उचित ढंग से ग्रहण किया गया भोजन मनुष्य को आयुष व स्वास्थ्य प्रदान करता है। वैदिक सभ्यता व पुराण काल में आहार चिकित्सा प्रचलित थी, जिसके अनुसार राजा दिलीप ने दुग्ध, कल्प, फल जल सेवन से लाभ प्राप्त किया। उपवास सभी रोगों से मुक्त होने का सहज उपचार माना जाता है। त्रेतायुग में रावण के समय जड़ी-बूटियों का प्रयोग होने लगा क्योंकि उसने बिना उपवास (लंघन) के बिना चिकित्सा की विधि के लिए वैद्यों को आदेश दिया जिसके फलस्वरूप पेड़-पौधों का उपयोग चिकित्सीय लाभ के लिए किया जाने लगा। आयुर्वेद व धार्मिक ग्रंथ गीता में सात्विक, राजसिक एवं तामसिक आहार का वर्णन प्राप्त होता है। आयुर्वेदनुसार -
‘‘विनापि भैषजैव्र्याधि पथयादेव विर्वतते।
नतुंपथ्य विहीनस्य भेषजानां शतैरपि।।
अर्थात् बिना किसी औषधि के सभी रोग पथ्य पूर्वक आहार-विहार, सोच-विचार से ठीक हो जाते है। यदि इन्हीं का अपथ्य रखा जाए तो किसी भी औषधि से ये ठीक नहीं किए जा सकते हैं। आहार शुद्ध होने पर मन की शुद्धि होती है व्यक्ति को अपनी इंद्रीयों पर नियंत्रण रहता है तथा एकाग्रता आती है। शरीर के लिए हितकर भोजन वह है जो सुपाच्य हो, अनुत्तेजक हो तथा आयु, स्मरण शक्ति, सत्तव, साहस, दया, सहयोग आदि बढ़ाने वाला हो। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित ‘भक्ति रहस्य’ में ईश्वर की भक्ति प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम सात्विक या प्राकृतिक खाद्य का सेवन ही सर्वप्रथम बताया गया है, क्योंकि वह शक्ति जो देह और मन का निर्माण करती है वह खाद्य पदार्थों में ही विद्यमान है। महात्मा गाँधी ने भी आहार पर विशेष महत्व दिया। उनके अनुसार तीन प्रकार के आहार बताए गए- शाकाहार, मांसाहार एवं मिश्राहार। उनके अनुसार असंख्य लोग मिश्राहारी है। आहार प्रत्येक प्राणी का जीवन है क्योंकि उसमें विद्यमान पोषक तत्त्व जैसे- कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन खनिज विटामिन उपस्थित होते हैं, जो मनुष्य के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं। प्रत्येक पोषक तत्व शरीर में अलग-अलग रूप से कार्य करता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति कुछ पोषक तत्वों को कम या अधिक करता है तो आयुर्वेदानुसार उसके शरीर में वात-पित्त, कफ (त्रिदोष) उत्पन्न हो जाएगा जिसके फलस्परूप व्यक्ति धीरे-धीरे रोगी बन जाएगा। अतैव सभी पोषण तत्वों को उचित मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण करना पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। इसी सिद्धांत को हम संपूर्ण पोषण (complete nutrition) अथवा संतुलित भोजन (balanced diet) की संज्ञा देते हैं।
सात्विक, राजसिक व तामसिक भोजन
भारतीय शास्त्रों में भोजन को तीन श्रेणी में रखा गया है- सात्विक, राजसिक व तामसिक। जो मनुष्य शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं उन्हे सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिये। सात्विक आहार आयु, उत्साह, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति बढ़ाने वाले रसदार पदार्थ होते हैं। इसमें प्रमुखत: कच्चे फल, सब्जियाँ, भाप में पकाया भोजन, अंकुरित अनाज, फलों का रस इत्यादि आते हैं। राजसिक भोजन द्वारा मनुष्य को शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार का स्वास्थ्य मिलता है। राजसिक आहार की श्रेणी में कड़वे, खट्टे, नमकीन, अति गर्म, तीक्ष्ण, रूखे रजोगुणी पदार्थ आते हैं। इसमें अंकुरित दालें, प्याज, लहसुन, मांसाहार इत्यादि प्रमुख हैं। तामसिक आहार के अंतर्गत बासी, नीरस, अति गर्म, तीक्ष्ण, तमोगुणी पदार्थ आते हैं जिसमें प्रमुखत: मैदे से बनी चीजें, चाय, कॉफी, चाकलेट, गरिष्ठ व तला हुआ भोजन हैं। भोजन का उद्देश्य भूख को शांत करना या जिह्वा की परितृप्ति नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य शारीरिक पोषण के साथ-साथ मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य में भी वृद्धि करना है क्योंकि शरीर, मन और आत्मा तीनों ही स्वास्थ्य के प्रमुख स्तंभ है। जब तक तीनों स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक पूर्ण स्वास्थ्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है।
ऋतु अनुसार करें पथ्य-अपथ्य का निर्धारण
ऋतुओं के अनुसार भी पथ्य-अपथ्य आहार का निर्धारण किया गया है। हेमंत ऋतु में ठण्ड होने के कारण पाचन अधिक होता है अतैव दूध से बने चिकने पदार्थ, गुड़, चीनी, मिश्री युक्त पदार्थों का सेवन करें तथा वात प्रधान भोजन एवं सत्तू का प्रयोग नहीं करना चाहिये। शिशिर ऋतु में कटु-तिक्त-कसाय, वात वर्धक व शीतल भोजन (काली मिर्च, लाल मिर्च, पिपली, करेला इत्यादि) त्याग देना चाहिये। ग्रीष्म ऋतु में मधुर, घी, दूध, चावल का सेवन करना चाहिये। अम्ल, कटु, ऊष्ण व लवण आदि का सेवन नहीं करना चाहिये। शीतल पानी पीने की मात्रा बढ़ा देनी चाहिये। वर्षा ऋतु में जठराग्नि कमजोर हो जाती है, वात कुपित हो जाता है। अम्ल, लवण व चिकने पदार्थों का सेवन करना चाहिये। पानी उबालकर, ठण्डा करके पीना चाहिये। शरद ऋतु में पित्त कुपित हो जाता है इसलिए पित्त को शांत करने वाले शीतल, तिक्त, रसयुक्त आहार अधिक लेने चाहिये। शिशिर के बाद बसंत ऋतु में शारीरिक बल मध्यम होता है। सूर्य द्वारा कफ कुपित होकर कष्ट कारक बनता है इसलिए गर्म, मीठे व चिकने आहार नहीं लेने चाहिये। गेहूँ का सेवन, मधु तथा ताजे भोजन का सेवन करना चाहिये। इस प्रकार आज के इस भौतिक युग में थोड़ा पथ्य-अपथ्य आहार का ध्यान रखकर हम बहुत सी बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं।
क्षारीय व अम्लीय आहार
आहार चिकित्सा के अंतर्गत मुख्यत: दो प्रकार के आहारों का वर्णन है- क्षारीय आहार एवं अम्लीय आहार। यह दोनों वर्गीकरण रक्त में pH की मात्रा अनुसार किया गया है। अम्लीय आहार में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन अधिकत्या आता है जो कि विघटन (Catabolism) के दौरान अम्लीय पदार्थ शरीर में बनाते हैं। आज के परिपेक्ष में साधारण रूप से अगर इसको समझें तो दालें, गेहूँ, चावल, अंडा, मांस, मछली इत्यादि, आलू, शकरकंद प्रमुख्यत: प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं।
भोजन में फल व सब्जियाँ क्षारीय आहार के रूप में वर्णित हैं, जैसे- लौकी, तुरई, सेम इत्यादि। एक संपूर्ण संतुलित भोजन में प्राकृतिक चिकित्सानुसार 20 प्रतिशत अम्लीय व 80 प्रतिशत क्षारीय आहार होना चाहिये। हालांकि इस पद्धति में भोजन के आयुर्वेद सिद्धांत एक यौगिक गुणों का भी समावेश रहता है। पंचमहाभूत का सिद्धांत भी इस पद्धतिनुसार उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है।
उचित प्राकृतिक आहार चिकित्सा के अंतर्गत अनुशासित आहार तालिका, रोगी व ऋतु के अनुसार तैयार की जाती है। आहार चिकित्सा में विभिन्न प्रकार के फल व सब्जी को प्राकृतिक रूप से ग्रहण करने का विधान है। इनमें खनिज, लवण विटामिन बहुतायत में होते हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होते है। इस श्रेणी में अंकुरित अनाज व सूखे मेवों को भी शामिल किया जाता है। आहार तालिका में कच्चे आहार (सलाद व अंकुरित पदार्थों) फल, सब्जियों का भरपूर समावेश होता है। लघु उपवास, अथवा दीर्घ उपवास भी आहार चिकित्सा के महत्वपूर्ण अंग है।
रोगों के लक्षणों को अनदेखा न करें
उच्च रक्तचाप की समस्या आजकल प्राय: लगभग सभी मनुष्यों में पाई जाती है। इस बीमारी का बहुत से लोगों को पता भी नहीं चल पाता है, क्योंकि प्राय: इसके लक्षण बहुत ही आम समझे जाते हैं जैसे- सिर दर्द रहना, नींद न आना, शिथिलता, चक्कर आना। प्राय: रोगी इन लक्षणों की अनदेखी कर देता है। इस रोग में असंयम, नमक का अधिक सेवन, चिन्ता, क्रोध, गुर्दे के रोग, कब्ज एवं आँव का होना घातक सिद्ध होता है।
विविध रोगों में आहार चिकत्सा का महत्व
इसकी चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण आहार है। उपवास रखना, पानी का अधिक सेवन, अंकुरित व कच्चा भोजन, शांत चित्त व एकान्त में करना इत्यादि पर ध्यान देना चाहिये। नियमानुसार उचित मात्रा में उचित समय पर भोजन ग्रहण करना चाहिये। बेलपत्र, केले के तने का रस व त्रिफला का सेवन भी इसमें लाभदायक है। इस रोग का उपचार कर लेने से अन्य जीवन शैली से जुड़े रोग जैसे- मोटापा, एसीडिटी, गैस, कब्ज इत्यादि अपने आप ही दूर हो जाते हैं। क्षय रोग की आरम्भिक अवस्था में बकरी के दूध अधिक सेवन करना चाहिये, नींबू, शहद व पानी को भी अधिक से अधिक ग्रहण करना चाहिये। संधिशोध या संधिवात में खट्टे अंगूर, चीनी, बैगन, मटर, भिंडी, राजमा, हरी मिर्च, क्रीम, दूध, केल, डिब्बाबंद पदार्थों का सेवन बंद कर देना चाहिये। हर मनुष्य अपनी शारीरिक व मानसिक अवस्था की जरूरत के अनुसार अपने आहार का विशेष ध्यान रखकर असंख्य बीमारीयों से निजात पा सकता है।
आहार चिकित्सा के तीन चरण
रोगग्रस्त मनुष्य के लिए आहार चिकित्सा लाभदायक है। इसके प्रमुखत: तीन चरण होते है। आहार चिकित्सा के प्रथम चरण में रोगी के आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को निषेध कर दिया जाता है इस प्रकार की आहार प्रणाली को eliminative diet कहा जाता है। इसमें शरीर में उपस्थित विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थ (toxins) का निष्कासन जल्दी हो पाता है और शरीर detox हो जाता है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ महसूस कर पाता है। यह उपचार विधि लगभग उपवास रखने जैसी है। इस प्रकार के आहार को शुद्धिकारक आहार कहा जाता है जिसमें नारियल का पानी, सब्जियों का सूप (लौकी, टमाटर), गेहूँ के ज्वारे का ताजा रस, एलोवेरा व ऑवले का रस, विभिन्न प्रकार के खट्टे फल जैसे- मौसमी, कीनू, नींबू इत्यादि का रस शामिल है।
जब शरीर सब प्रकार के विजातीय द्रव्यों से मुक्त हो जाता है एवं शरीर लगभग रोगमुक्त हो जाता है, तब इसके पश्चात रोगी को शांतकारक आहार प्रदान किया जाता है। इस आहार की श्रेणी में मौसम के अनुसार फल, सब्जियाँ, उबली हुई, भाप में पकी सब्जियाँ, अंकुरित मूंग, मोठ, मेथी, धनिये, पुदीने की चटनी, कढ़ी पत्ता आते हैं। मौसम अनुसार फल सब्जी का सलाद, सूप इत्यादि का प्रयोग करके शरीर में प्रतिरोधक (एंटीऑक्सीडेंट) तत्व की बढ़ोत्तरी होती है, व शरीर स्वस्थ रहता है। प्राय: देखा गया है कि लोग हरी पत्तियों वाली सब्जी, गोभी, बंदगोभी इत्यादि, वर्षाऋतु में भी खाते हैं।
इस ऋतु में इसमें कीड़े लगने की संभावना अधिक हो जाती है जिसके बचाव हेतु विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग किसान के द्वारा किया जाता है, जो अंतत: हमारे शरीर को हानि पहुँचा सकता है। अतैव ऋतु के अनुरूप ही फल सब्जियों व अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिये। तीसरे चरण में रोगी को पुष्टीकारक आहार दिया जाता है। पुष्टिकारक आहार में सभी प्रकार के अन्न का आटा, दालें, दही, दलिया इत्यादि आते है।अत: आहार चिकित्सा द्वारा विभिन्न प्रकार के आहार का समयनुसार सेवन करने से स्वास्थ्य का संवर्धन होने केसाथ विजातीय द्रव्यों का शरीर से निष्कासन भी हो पाता है जिसके फलस्वरूप पाचन संस्थान का शुद्धिकरण होता है जिससे रोगमुक्त शरीर का निमार्ण होता है। इसके अलावा आहार चिकित्सा में प्रमुखत: निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये-
भोजन ग्रहण का समय निर्धारित करें। भोजन ग्रहण करते समय, शोक, क्रोध, जल्दबाजी न करें। भोजन के चयन में विशेष ध्यान देना चाहिये। भोजन सुपाच्य हो, अधिक गरिष्ठ व रसायन युक्त नही होना चाहिये। ज्यादा गर्म एवं ज्यादा ठण्डे अथवा बासी भोजन को ग्रहण न करें।
भोजन देर रात्री में न करें। सोने से दो घण्टे पूर्व अवश्य करें। खाने के आधे घण्टे बाद व सोने से पहले एक या दो बार पानी का सेवन करने से पाचन ठीक होता है। खाने से पहले, बीच में व बाद में अत्याधिक पानी न पिएँ।
भोजन में 20 प्रतिशत अम्लीय व 80 प्रतिशत क्षारीय भोजन करना चाहिये। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आँवला संतरा, नींबू, टमाटर, ताजे फल व सब्जियाँ, अंकुरित अनाज का अत्याधिक सेवन करना चाहिये। इन सभी पदार्थों में भरपूर मात्रा में विटामिन, खनिज व लवण होते हैं, जिससे शरीर में एंटीबॉडीज के निर्माण की प्रक्रिया बढ़ जाती है खून का निर्माण होता रहता है। छिल्के वाली दाल, चना, लौकी, गेहूँ, मूँगफली, दूध, दही, छाछ, तिल, आलू, प्याज, चुकंदर, लहसुन, हरी पत्तों वाली सब्जीयों का सेवन अधिक करना चाहिये।
प्रत्येक माह में एक दो दिन का उपवास तथा 3-4 माह में 2-4 दिन का उपवास फलों पर करना चाहिये।
आहार चिकित्सा में कुछ खाद्य वस्तुएँ हैं जिनका प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते, इसी प्रकार का वर्णन हमें आयुर्वेदानुसार पथ्य-अपथ्य आहार विवेचन में भी प्राप्त होता है। दूध के साथ दही, प्याज, अचार, सिरका, मूली व माँसाहार न करें। शहद व घी का बराबर की मात्रा में सेवन करना भी निषेध है क्योंकि सम-मात्रा में यह विष समान हो जाता है। भोजन ग्रहण करने से ठीक पहले, बीच में व एकदम बाद में ज्यादा मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिये।
आज के इस व्यस्त जीवन में अगर हमें रोग मुक्त रहना है तो हमें प्रकृति के निकट जाना होगा, चाहे वो वृक्षारोपण के द्वारा हो, प्रदूषण युक्त वातावरण का निर्माण करना हो या फिर स्वयं अपने आहार पर ध्यान रखना हो। आहार चिकित्सा कोई कठिन चिकित्सा पद्धति नहीं है, वस्तुत: यह एक विज्ञान है जिसके द्वारा हम पंचमहाभूत के सिद्धांतो को समझते हुए, पथ्य-अपथ्य, आहार-विहार का पालन करते हुए अपने स्वास्थ का ध्यान रखते हुए अपने आप को निरोगी रखते हैं। स्वस्थ तन से ही स्वस्थ मन का निर्माण होता है, मनुष्य विवेकशील बनता है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन की जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए प्रगतिशील समाज का निर्माण करता है।
‘ऊँ सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:’
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Dec 2024 18:59:48
योग प्रज्ञा योग - योग जीवन का प्रयोजन, उपयोगिता, उपलब्धि, साधन-साधना-साध्य, सिद्धान्त, कत्र्तव्य, मंतव्य, गंतव्य, लक्ष्य, संकल्प, सिद्धि, कर्म धर्म,...








.jpg)