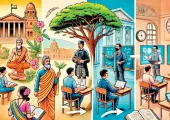गीतानुशासन
On

प्रो. रामेश्वर मिश्र पंकज
भारतीय परंपरा में किसी भी विमर्श के संदर्भ में यह नियम है कि जो विमर्श प्रारंभ करें उसके विषय में सबसे पहले चार बातों का विचार आवश्यक है। इसे अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, इसके अधिकारी कौन हैं और जो प्रतिपादन किया जा रहा है या जो कृति प्रस्तुत की जा रही है या जो शास्त्र अथवा व्याख्यान प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका विषय से, अधिकारी से और प्रयोजन से संबंध क्या है। यह चार बातें पहले बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए।
इस विमर्श का विषय है- ‘अथ गीतानुशासनं’। गीता का एक शासन है जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने, स्वयं परम सत्ता ने सनातन काल से इस सृष्टि को संचालित रखने के लिए रच रखा है। जो उस शासन को मानते हैं और जो नहीं मानते, सभी उसी शासन से संचालित हैं। यह संपूर्ण सृष्टि उसी शासन से चल रही है जिसका प्रतिपादन श्रीमद्भगवद्गीता में है। जब हम उस पर चर्चा करते हैं तो उस शासन का अनुस्मरण करते हैं। उसे गुरु के मार्गदर्शन में हृदयंगम करने की कोशिश करते हैं। ताकि हम एक तो उस ज्ञान को जान सकें जो गीता में दिया है। वह बल प्राप्त कर सकें जो गीता के ज्ञान से प्राप्त होता है। उस बल के अनुरूप और उस ज्ञान के अनुरूप स्वधर्म का निर्धारण कर सकें और स्वधर्म निर्धारण का बल प्राप्त करके हम स्वधर्म पालन कर सकें। क्यों? क्योंकि गीता में अध्याय 18, श्लोक 46 में कहा है -
यत: प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्।
स्वकर्मणा तमभ्यच्र्य सिद्धिं विन्दति मानव:।।
(स्वकर्म द्वारा ही परमेश्वर की अर्चना होती है। उस अर्चना द्वारा ही मनुष्य सिद्धि प्राप्त करते हैं।) उससे पूर्व श्लोक 45 में भगवान ने कहा है -
स्वे स्वे कर्मण्यभिरत: संसिद्धिं लभते नर:।
स्वकर्मनिरत: सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु।।
(अर्थात अपने-अपने लिये नियत या निर्धारित कर्म (स्वधर्म) का पालन करते हुये मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। यह सिद्धि किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो।)
यह जो सृष्टि चक्र प्रवर्तित है इसमें अपने स्वधर्म का बोध करके जब हम कर्म करते हैं, तो प्राणियों की प्रवृत्ति जिस कारण से हुई है, भगवान ने इस सृष्टि को जैसे प्रवर्तित कर रखा है और उसमें प्रत्येक जीवात्मा जिन कारणों से प्रवर्तित है, उन कारणों के अनुशासन में उस जीवात्मा की सार्थकता है, उसके जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह स्वधर्म का पालन करे। तो अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से, स्वधर्म पालन से, वह जो परम सत्ता है, जो संचालन कर रही है इस संसार का, उसकी अर्चना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। ऐसा भगवान ने कहा है। तो इसलिए स्वधर्म पालन के लिए आवश्यक ज्ञान को जानना। गीता के शासन को जानना। यही गीता का अनुशासन है। यह इसका विषय है।
त्रिविध ज्ञान
गीता में तीन प्रकार के ज्ञान प्रतिपादित हैं। एक तो जगत संबंधी ज्ञान। जगत का स्वरूप क्या है? जगत का मूल क्या है? जगत चलता कैसे है? इसके विषय में जो आधारभूत ज्ञान है, वह गीता में दिया हुआ है।
इसके अतिरिक्त जीव के रूप में जो आत्म सत्ता है, जो इस जगत में वर्तती है, व्यवहार करती है, कोई काम करती है और साथ ही स्वधर्म का पालन करते हुए सिद्धियां और पुरुषार्थ प्राप्त करती है, सिद्धियां प्राप्त करती है, उस आत्म सत्ता का स्वरूप क्या है? यानी विश्व का ज्ञान और आत्म ज्ञान और उसके अतिरिक्त जो इस संपूर्ण विश्व को संचालित करने वाली परम सत्ता है, जिसे ब्रह्म कहा है उस ब्रह्म का ज्ञान।
तो गीता तीन प्रकार के ज्ञान देती है: एक जगत ज्ञान या विश्व ज्ञान। यानी विश्व के सार का ज्ञान। विस्तार का नहीं। उसके मूल तत्वों का ज्ञान। दूसरा आत्मा के स्वरूप का ज्ञान और तीसरा ब्रह्म सत्ता के स्वरूप का ज्ञान। तो जगत ज्ञान या विश्व ज्ञान, आत्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, इन तीनों ही प्रकार के ज्ञान के लिए गीता का अध्ययन और मनन नितांत आवश्यक है। यह है गीता का महात्म्य और यह हमारा विषय है।
प्रयोजन
प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यही है कि इसके द्वारा जो जिज्ञासु हैं, वे विश्व ज्ञान प्राप्त करें, आत्म ज्ञान प्राप्त करें और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें। प्रारंभ में उसके विषय में सूत्र ज्ञात करें। फिर इसके बाद गुरु के मार्गदर्शन में साधना के द्वारा जब पुरुषार्थ करेंगे तो उनके जीवन की धन्यता या सार्थकता सिद्ध होगी। केवल सुनने से कुछ नहीं हो जाता।
शास्त्र-श्रवण से संस्कार बनते हैं
सनातन धर्म में यह नहीं कहा है कि आपने कोई शास्त्र सुन लिया तो इससे आप उस शास्त्र के ज्ञाता हो गए या उस धर्म के अनुष्ठाता हो गए। कई ऐसे पंथ हैं दुनिया में जैसे ईसाइयत है, इस्लाम है, इसमें माना जाता है कि किसी परम सत्ता का जो मैसेज आया है या कोई भी सत्ता जो उनके यहाँ वर्णित है, उसका मैसेज आपने ईमान के साथ सुन लिया, इतना पर्याप्त है। सनातन धर्म में यह नहीं है। शास्त्र श्रवण बहुत पुण्य कर्म है लेकिन श्रवण से आपके भीतर एक तरह का संस्कार बनता है। यही बस। इतना ही पुण्य इससे है। मनन से संस्कार दृढ़ होते हैं।
इसके बाद शेष काम यानी उसका मनन करना, उसको चित्त में अच्छी तरह अवधारण करना, उसको चित्त में बैठाना, उसका गुरु से, मार्गदर्शक से, शास्त्रों से विविध प्रकार से बारंबार अवगाहन करना, उसे दृढ़ करना। फिर तद्नुरूप स्वधर्म का निर्धारण करके स्वधर्म का पालन करना। जीवन में तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त करना, पुरुषार्थ प्राप्त करना, ऐश्वर्य प्राप्त करना और उसके द्वारा जीवन को सार्थक बनाना। तब माना जाता है कि आपने धर्माचरण किया है, आप धर्मनिष्ठ हैं।
शास्त्र कंठस्थ होना धर्मनिष्ठ होने का प्रमाण नहीं, उसकी सम्भावना मात्र है आपने किसी शास्त्र को पढ़ लिया है इससे ये नहीं पता चलता कि आप धर्मनिष्ठ है। आपको कोई शास्त्र कंठस्थ है तो भी यह नहीं पता चलता कि आप धर्मनिष्ठ हैं। हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं कहा है। क्योंकि पाठ से, पढऩे से, सुनने से आपमें एक संस्कार आ गए लेकिन साथ ही अन्य संस्कार भी बने रह सकते हैं। इसी के लिए पुराणों में बड़े विस्तार से बताया है कि बड़े-बड़े ऋषि हैं, तपस्वी योगी हैं, उनमें ज्ञान भी है, तप का ऐश्वर्य भी है, प्रकाश है, सब प्रकार से और फिर भी कोई पुरानी पिछले जन्मों की या इसी जन्म की वासना अचानक तीव्र होती है और क्या होता है? वह उस वासना के वश में थोड़ी देर आ जाते हैं। जिसे कहते हैं स्खलित हो जाना। तो केवल ‘मैसेज’ को सुनना पर्याप्त नहीं है।
सच यह है कि उसका बारंबार आपने ठीक से पारायण भी कर लिया, कुछ साधना भी कर ली, कुछ सिद्धि भी प्राप्त कर ली तो भी यह आशंका बनी रहती है कि कोई अन्य वासना आपके भीतर जो पिछले जन्मों के कारण या वर्तमान जन्म के कारण रह गई है, वह अचानक जागृत होकर आपको स्खलित कर सकती हैं, धर्मभ्रष्ट कर सकती हैं, धर्मच्युत कर सकती हैं। तो अपने यहां धर्मपालन इतना सरल नहीं कहा है। इसीलिए बारम्बार कहा है - ‘क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति’। तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन है धर्ममय जीवन। यह दुर्गम पथ है। इसे गुरू अपने मार्गदर्शन में सुगम बनाने का प्रयास करते हैं। किसी सत्ता का संदेश, किसी महापुरुष का संदेश या कोई परम दिव्य सत्ता, रहस्यमय सत्ता का संदेश, कोई इलहाम जो प्राप्त हुआ हो किसी को, वह सुन लेने से, किसी ‘द बुक’ को, किसी किताब को, किसी आसमानी किताब को सुन लेने से या उसमें ‘फेथ’, ईमान जता देने से आप धर्मनिष्ठ नहीं हो जाते।
उसको विवेक पूर्वक सनातन धर्म के अनुशासन में जांचना होता है कि आपने जो सुना है, क्या वह सनातन धर्म के अनुरूप है? इसलिए हमारे यहां नए को, जैसा नया आजकल फैशन चला है कि यह नया है, हम नया करेंगे इस अर्थ में, सर्वथा अपूर्व के अर्थ में, नए को कोई अच्छा नहीं मानते। वस्तुत: नया कुछ होता भी नहीं है। सृष्टि चक्र है। सभी प्रकार के लोग, सभी प्रकार की वृतियाँ, सभी प्रकार के उद्योग, सभी प्रकार के पुरुषार्थ अनेक बार हो चुके हैं, अनेक बार भविष्य में होंगे। सभी प्रकार के जीव अच्छे और बुरे, दुष्ट और सज्जन सब प्रकार के लोग। वीर और कायर, धर्मात्मा और धर्म विरोधी, पुण्यात्मा और पापी, सब प्रकार के लोग सदा से होते रहे हैं। सब प्रकार के कर्म होते रहे हैं। तो उस अर्थ में पूर्णत: नया कुछ होता नहीं है। सत्य यही है। लेकिन उससे भी महत्त्वपूर्ण यह है कि नया संदिग्ध है, नया सही नहीं है जब तक वह सनातन के अनुशासन में ना हो। यही कहा गया है। क्योंकि नए के अच्छे होने का प्रमाण क्या है? जब तक वह शास्त्र वचन से, आप्त पुरुषों के कथन से प्रमाणित नहीं हो। शाश्वत जो नियम हैं, इस सृष्टि के संचालन के, उनके अनुरूप नहीं हो। उनसे सुसंगत नहीं हो। उनके विरोध में पड़ता हो, तब तक नया तो अनर्थकारी भी हो सकता है अथवा यूं ही मनमानी भी हो सकता है। इसलिए किसी चीज का नया होना कि मुझे तो बड़ी नई जानकारी मिली है, नई जानकारी मिली है तो वो किसी काम की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नया होना स्वयं में कोई गुणवाचक नहीं है। वह एक स्थिति वाचक है कि यह नया है। वह गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आपको नया ज्ञान मिला है इससे नहीं पता चलता कि वो कोई अच्छा, सम्यक, सत्य ज्ञान है। उसको जांचना पड़ता है। शास्त्रों से। सार्वभौम नियमों से।
सनातन धर्म का ज्ञानार्जन ही गीता का प्रयोजन है
तो प्रयोजन क्या है? सनातन धर्म के अनुरूप ज्ञान का अर्जन। उसमें गीता में जो प्रतिपादित है विश्व का ज्ञान, आत्मसत्ता का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। उसको जानना ताकि स्वधर्माचरण में हमको उससे सहायता मिले। हमारे भीतर वह अनुशासन आए जिसके द्वारा हम ऐसे पुरुषार्थ कर सकें कि हम भविष्य में धर्मनिष्ठ ही रहें, स्खलित नहीं हों। स्खलित हों तो उसके अनुसार प्रायश्चित को जानें। यह भी नहीं कहा है कि यदि कभी कोई स्खलित हुए, एक बार हुए तो सदा के लिए नरक में चले जाओगे। नहीं। मनुष्य में स्खलन होता ही रहता है। तो उसके लिए आवश्यक प्रायश्चित की व्यवस्था है। शास्त्र के अनुरूप प्रायश्चित कीजिए। पुन: सन्मार्ग पर प्रवृत होइए। आगे बढि़ए। निरंतर गतिशील रहिए। निरंतर आगे बढ़ते रहिए यही कहा है। तो यह है प्रयोजन कि यह जानना कि हमें क्या करना है, हमारे भगवद्गीता में सृष्टि के विषय में, आत्म सत्ता के विषय में और ब्रह्म के विषय में क्या कहा गया है।
गीता ज्ञान का अधिकारी कौन
तो इसका अधिकारी कौन है? अनुबंध चतुष्टय में चार चीज जाननी चाहिए। विषय क्या है, प्रयोजन क्या है। प्रयोजन क्या है ज्ञान प्राप्त करना ताकि पुरुषार्थ संपादन में स्वधर्म पालन हेतु बल प्राप्त हो, सहयोग प्राप्त हो। और अधिकारी कौन है इसका? इसका अधिकारी वह है, जिसे सनातन धर्म में श्रद्धा हो। गीता में श्रद्धा हो। जो मानता हो कि गीता में ऐसा ज्ञान है कि जिसके द्वारा हमारा जीवन संपन्न हो सकता है, भरपूर हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है, समृद्ध हो सकता है। हम में धर्म ज्ञान आएगा, हमारे भीतर आत्म ज्ञान आएगा, हमारे भीतर ब्रह्म ज्ञान आएगा, अगर हम गीता के ज्ञान को जान लेंगे और आवश्यक साधना करेंगे।
तो जो सनातन धर्म के प्रति जिज्ञासु और श्रद्धालु हैं, वही इसके अधिकारी हैं। 18 वें अध्याय में ही स्पष्ट कहा है ‘इदं ते नातपस्काय’। जो किसी तरह का तप करने, ज्ञान साधना के लिये किसी तरह का कष्ट सहने के लिए नहीं तैयार है, उसके लिये यह नहीं है। बस, जो कुछ सुन रखा है जो कुछ मान रखा है, जो कहता है, जी हम तो यह मानते हैं, हम तो मानते हैं कि भगवान नहीं है, हम तो मानते हैं कि हिंदू धर्म में दोष ही दोष है, हम तो मानते हैं कि यह देश तो दुनिया में सबसे गया गुजरा है, जो भी तरह तरह के लोग मिलते हैं एक से एक नमूने, कार्टून तो जो वह सब मानते हैं, वह इसके अधिकारी नहीं हैं।
Tags: गीतानुशासन
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Dec 2024 18:59:48
योग प्रज्ञा योग - योग जीवन का प्रयोजन, उपयोगिता, उपलब्धि, साधन-साधना-साध्य, सिद्धान्त, कत्र्तव्य, मंतव्य, गंतव्य, लक्ष्य, संकल्प, सिद्धि, कर्म धर्म,...








.jpg)