मेरे सभी कर्म हैं योग
On

पूज्या साध्वी देवप्रिया,
संकायाध्यक्षा (DEAN) एवं कुलानुशासिका
पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार
सृष्टि के आदिकाल से लेकर आज तक, वेद से लेकर ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद, दर्शन, रामायण, गीता आदि तक सभी आध्यात्मिक, धार्मिक ग्रन्थों में सर्वाधिक प्रचलित, स्थाई एवं नित्य कोई शब्द है तो वह है- योग। लौकिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत, दोनों में ही योगी को अति गौरव की दृष्टि से देखा जाता है। जीवन के किसी भी वर्णाश्रम में रहते हुए अथवा पृथिवि के किसी भी भू-भाग पर रहते हुए व्यक्ति योगी बन सकता है इसलिए हमारे यहाँ योग के लिए विभिन्न शब्द प्रचलित हैं- राजयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, अष्टाङ्गयोग, ध्यानयोग, समाधियोग, कैवल्य योग, प्रतिप्रसव योग आदि-आदि। लेकिन इन तमाम योग मार्गों में जो कॉमन चीज है जिसके बिना कोई भी योग सिद्ध नहीं होता, वह है- तप।
महर्षि व्यास कहते हैं- ‘नातपस्विनो योगसिध्यति’। अर्थात् अतपस्वी को किसी भी योग की सिद्धी नहीं हो सकती, अत: तप को अवश्य करना पड़ेगा। जिस प्रकार की सिद्धि है उसी का तप भी अपेक्षित है। यदि विद्या की सिद्धि चाहिए तो विद्यार्थी का तप अलग प्रकार है और यदि अन्न चाहिए तो किसान का तप अलग है और यदि धन चाहिए तो धनवान का तप अलग है यदि कोई सामाजिक पद-प्रतिष्ठा चाहिए तो राजनेता व सामाजिक कार्यकर्ता का तप अलग है, यदि गृहिणी आदर्श बहू, आदर्श सास या आदर्श महिला बनना चाहती है तो अलग प्रकार का तप है और यदि किसी को आत्मिक, मानसिक शान्ति चाहिए तो अलग तप है। अत: अलग-अलग उपलब्धियों के लिए अलग-अलग तप किए जाते हैं और जो तपस्वी है वह कोई भी कर्म करते हुए योगी बन सकता है। अब प्रश्न यह है कि हम योगी या तपस्वी क्यों बनें? इसका उत्तर यह है कि जन्म से तो सभी मनुष्य समान ही होते हैं, सभी का जन्म माँ के गर्भ से तो समान रीति से ही होता है लेकिन अपने-अपने कर्म से लोग महान्, सामान्य या बदनाम हो जाते हैं। योगी बनना जीवन की चरम उपलब्धि है जो एक बार मिलने पर कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तक कि सब कुछ का हरण करने वाली मृत्यु भी इसे छीन नहीं सकती। यह मनुष्य पूर्ण सुख या शाश्वत सुख का अधिकारी बन जाता है। तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं-
1. | सामान्य मनुष्य | सामान्य शरीर इन्द्रियाँ | सामान्य आचरण व व्यवहार |
2. | विशेष मनुष्य | विशेष शरीर इन्द्रियाँ | विशेष आचरण व व्यवहार |
3. | दिव्य मनुष्य | दिव्य शरीर इन्द्रियाँ | दिव्य आचरण व व्यवहार |
प्रथम श्रेणी में सभी मनुष्य आ जाते हैं। मध्यम श्रेणी अपने-अपने क्षेत्र के महापुरुष आ जाते हैं और उत्तम श्रेणी में केवल योगीजन ही आते हैं। इनका जन्म लेना धन्य हो जाता है, ये सदा के लिए कृतकृत्य हो जाते हैं। यह पढक़र आपको भी जरूर लालच आया होगा कि तब तो हम भी योगी बनें और यह हम सब आत्माओं का जन्मसिद्ध अधिकार है, यही हम सबका लक्ष्य और कभी न कभी हम सबको यह करना ही पड़ेगा। तो अब मन में प्रश्न आएगा कि तप करें कैसे, योगी बनें कैसे, हमारे ऊपर तो बहुत सारी सांसारिक जिम्मेदारियाँ हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान् कृष्ण कहते हैं कि डरने की या चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान् ने हम सबको शरीर, इन्द्रिय, मन और समय ये चार बड़े साधन देकर भेजा है, और ये चारों सबके पास समान ही हैं, बस प्रयोग कैसे करना है, वह आपको मैं बता देता हूँ। जिस प्रकार चाबी एक ही होती है और उसके एक दिशा में घुमाने पर ताला बन्द हो जाता है और दूसरी दिशा में घुमाने पर ताला खुलकर पूरा खजाना, बंगला हमारे हाथ में आ जाता है, इसी प्रकार जीवन में एक खास रीति से शरीर, इन्द्रिय व मन का प्रयोग करने से व्यक्ति कर्मबन्धन में बँध जाता है और विशेष रीति से इनका प्रयोग किये जाने पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसी का उपाय बताते हुए भगवान् कृष्ण गीता के सत्रहवें अध्याय के श्लोक नं. 14,15,16 में तीन प्रकार के तप वर्णन करते हुए कहते हैं-
देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम्।
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते।। (गीता- 17.14)
अर्थात् देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवनमुक्त योगीजनों का यथायोग्य पूजन करना, शरीर से शुचिता का पालन करना, सरल बनना अर्थात् अकड़, टेढ़ापन या अभियान का व्यवहार छोडक़र निरभिमान बनना, अपनी सभी इन्द्रियों पर संयम रखना किसी की हिंसा न करना, किसी को कष्ट न देना- यह शरीर का तप है। इस शारीरिक तप में त्याग की मुख्यता है जैसे- पूजन में अपने बड़प्पन का त्याग है, शुचिता रखने में अपने आलस्य, प्रमाद का त्याग है, सरलता रखने में अभिमान का त्याग है, ब्रह्मचर्य में इन्द्रियों के विषय सुख का त्याग है और अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग है। इस प्रकार जीवन में त्याग की मुख्यता शारीरिक तप है इसी प्रकार वाणी से तप बताया। यहाँ वाणी सभी इन्द्रियों की प्रतिनिधि है-
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्।
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते।। (गीता-17.15)
अर्थात् जो कि उद्विग्न न करने वाला, सत्य, प्रिय और हितकारक भाषण है, तथा जैसा स्वाध्याय किया वैसा ही अभ्यास भी करना यह वाणी का तप है। यदि हम योगदर्शन की भाषा में कहे तो शारीरिक तप में वैराग्य की प्रधानता है और वाणी के तप में अर्थात् सभी इन्द्रियों से किये जाने वाले कर्मों से सद्अभ्यास की प्रधानता है, और इस प्रकार तीसरा साधन है मन। मन का प्रयोग कैसे करें कि वह तप बन जायें, क्योंकि हम कर्म भले ही शरीर से करें या वाणी से पर मन का सहयोग अनिवार्य रूप से अपेक्षित है और कभी-कभी हम केवल मन से भी कर्म करते हैं। सृष्टि का नियम है कि स्थूल से भी सूक्ष्म शक्तिशाली होता है। शरीर और इन्द्रियाँ तो स्थूल हैं बाह्य हैं पर मन एक सूक्ष्म साधन है, आन्तरिक साधन है, अत्यन्त शक्तिशाली है जिसको मन का सही प्रयोग करना आ गया वह व्यक्ति महान् है, योगी है। अत: गीता में कहा है कि तप करने के लिए हिमालय जाने की या संन्यासी बनने की जरुरत नहीं है अपितु आप जो भी कर्म करते हैं उसे करते हुए या जीवन में अच्छी-बुरी जो भी परिस्थितियाँ आती हैं उन सबके बीच में मन की प्रसन्नता को न बिगडऩे दें उसकी मधुरता, प्रसन्नता, सौम्यता को प्रयासपूर्वक यदि बनाये रखते हैं तो आप धीरे-धीरे तपस्वी योगी बन ही जायेंगे।
मन: प्रसाद: सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह:।
भावसंश्रुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते।। (गीता- 17.16)
अर्थात् मन की प्रसन्नता प्रयासपूर्वक हर परिस्थिति में बनाये रखें, स्वभाव में कठोरता, क्रूरता नहीं अपितु, प्रयासपूर्वक सौम्यता लेकर आयें, मन मे अनावश्यक विचारों की भीड़ व उथल-पुथल को हटाकर मन को अधिक से अधिक मौन रखने का प्रयास करें, आत्म विनिग्रह का अभिप्राय है कि हमारा मन हमारे इतने कन्ट्रोल में होना चाहिए कि हम मन को जहाँ लगाना चाहें वहाँ लग जाये और जहाँ से हटाना चाहें वहाँ से हट जाये। व्यक्ति की सबसे बड़ी परेशानी यही रहती है कि जिसको याद करने से कष्ट होता है वह व्यक्ति या परिस्थिति बार-बार याद आते हैं भुलाये नहीं जाते और जो भजन-सुमिरन सतत करना चाहते हैं उसमें मन नहीं टिकता। विचारो के अतिरिक्त हृदय के पवित्र भाव, प्रेम, करुणा, मुदिता के भाव भी मानस तप के अन्तर्गत ही आते हैं। अब आप ही बतायें क्या ये तीनों प्रकार के तप हम कहीं भी रहते हुए नहीं कर सकते है? क्या हमने किसी दूसरे की अपेक्षा है? नहीं। ये तीनों प्रकार के तप हम सभी, हर स्थान पर, हर परिस्थिति में कर सकते हैं और समय एक साधन है जिसके अन्तर्गत सभी को रात-दिन में 24 घण्टे का ही समय दिया। उस समय का जो सदुपयोग करता है, वह योगी बन जाता है और जो दुरुपयोग करता है, वह भोगी बन जाता है। गीता के अगले तीन श्लोकों में (अध्याय 17 के- 17.18.19) बताया कि यह शरीर, वाणी और मन का तप भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद से तीन प्रकार का होता हैं।
श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरै:।
अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तै: सात्विकं परिचक्षते।। (गीता-17.17)
अर्थात् शरीर, वाणी और मन से परम श्रद्धा से युक्त होकर फल की इच्छा का त्याग करते हुए अर्थात् फल की कामना का त्याग करके कर्त्तव्य भाव से किया जाने वाला तप सात्विक तप कहलाता है और-
सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्।
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्।। (गीता- 17.18)
जो सत्कार, मान और अपनी पूजा करवाने के लिए दूसरों की दृष्टि में मैं तपस्वी दिखूं इस दिखावे के भाव से जो तप किया जाता है वह राजसिक तप कहलाता है। और-
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तप:।
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्।। (गीता- 17.19)
मूढ़तापूर्वक हठ से, अपने को पीड़ा देकर या दूसरों को कष्ट देने के लिए या प्रतिशोध अथवा बदला लेने की भावना से जो तप किया जाता है उसे तामसिक तप कहते हैं।
अत: योगेश्वर कृष्ण ने हम सबको योगी तपस्वी बनाने के लिए कितना सरल उपाय गीता में बताया है- जिसकी सहायता से हम अपने प्रत्येक कर्म को सेवा और पूजा बनाते हुए, दिव्य कर्म बनाते हुए परम सन्तोष और परम शान्ति को प्राप्त करके, मानव जन्म को सार्थक बना सकते हैं।
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Dec 2024 18:59:48
योग प्रज्ञा योग - योग जीवन का प्रयोजन, उपयोगिता, उपलब्धि, साधन-साधना-साध्य, सिद्धान्त, कत्र्तव्य, मंतव्य, गंतव्य, लक्ष्य, संकल्प, सिद्धि, कर्म धर्म,...








.jpg)
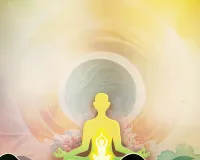





.jpg)


1.jpg)
.jpg)
