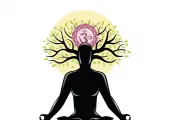हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति
On

वंदना बरनवाल
राज्य प्रभारी, महिला पतंजलि योग समिति
उ.प्र. (मध्य)
किसी भी भाषा का और वो भी मातृभाषा का अलग से कोई दिन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि भाषा तो चौबीसों घंटे हमारी अस्मिता और अस्तित्व दोनों का अनिवार्य अंग है। भाषा का कार्य संस्कृति को जीवित रखना है और इसे अगली पीढ़ी तक ले जाना है। |
लोगों को जोडऩे का सबसे सरल और सबसे जरुरी माध्यम भाषा ही तो है, जिसका उपयोग कर हम अपनी भावनाओं को संप्रेषित कर पाते हैं और जब यह भाषा हमारी स्वयं की मातृभाषा हो तो उसमें स्वत: ही एक रस और अपनापन होने के साथ ही आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी मददगार साबित होने का गुण मौजूद होता है।
मेरी अस्मिता भी तुम हो, अस्तित्व भी तुम हो
मेरा मान भी तुम हो, मेरा स्वाभिमान तुम हो
कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वाणी, ये कहावत भारत जैसे बहुरंगी और विविध संस्कृति वाले देश के लिए शब्दश: सटीक बैठती है। भारत और इसकी संस्कृति जहाँ हर थोड़ी दूर पर बोली बदल जाती है, रहन-सहन और खान-पान से लेकर पहनावा-ओढ़ावा भी बदल जाता है, रंग रूप में अंतर आ जाता हो और यहाँ तक कि भाषा और बोली सब कुछ बदल जाती हो, ऐसी विविधताओं वाले देश में निश्चित रूप से चुनौतियाँ भी विविध प्रकार की होती हैं। सैकड़ों बोलियों और भाषा वाले इस देश में हिंदी का स्थान अद्वितीय है पर एक ऐसा देश जिसका नाम वर्षों से हिंदी में अलग और अंग्रेजी में अलग हो और वहां के लोगों को इससे कोई फर्क न पड़े कि वे भारतीय हैं या इंडियन तो निश्चित रूप से ऐसे में हिंदी भाषा के लिए चुनौतियाँ कितनी अधिक हैं इसे समझ पाना मुश्किल नहीं है।
2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की कुल आबादी में से 41.03 प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है और अगर हिन्दी को दूसरी भाषा के तौर पर इस्तेमाल करने वाले अन्य भारतीयों को भी इसमें मिला लिया जाए तो देश के लगभग 75 प्रतिशत लोग हिन्दी बोल सकते हैं। भारत के इन 75 प्रतिशत हिंदी भाषियों सहित पूरी दुनिया में तकरीबन 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोल या समझ सकते हैं। निश्चित रूप से यह आंकड़ा हिंदी भाषा की ताकत को बताता है।
हिंदी की इसी ताकत से मौजूदा समय में विश्व के लगभग डेढ़ सौ विश्वविद्यालयों में इसका पठन-पाठन हो रहा है और जनसंख्या की दृष्टि से यदि पूरी दुनिया में चीनी भाषा मंदारिन बोलने वालों का स्थान पहला है तो हिंदी भाषा बोलने वाले दूसरे नंबर पर पहुँच चुके हैं जबकि अंग्रेजी भाषी तीसरे स्थान पर है। यानि हिंदी में संभावनाएँ तो अथाह हैं बस शर्त यही है कि अन्य मुद्दों की तरह ही इसे भी मजबूत इरादों के साथ ‘एक देश एक विधान’, ‘एक देश एक चुनाव’, ‘वन नेशन वन टैक्स’, ‘वन नेशन वन ग्रिड’के तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर ‘एक देश एक भाषा’जैसे नारे के साथ खड़ा कर दिया जाये और साथ ही लोगों को यह समझाया जाये कि ‘आत्मनिर्भर भारत’के लिए हिंदी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाना कितना आवश्यक है। ‘आत्मनिर्भर भारत’ही नहीं बल्कि ‘वोकल फॉर लोकल’की मुहीम के लिए भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर राह आसान तभी होगी जब हम हिंदी को राजभाषा के साथ ही राष्ट्रभाषा का दर्जा भी दे पायें। वैसे राजभाषा और राष्ट्रभाषा को लेकर बहुत से लोग भ्रमित रहते हैं और कई लोगों को लगता है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है जबकि ऐसा नहीं है। फिलहाल यह एक कटु सत्य है कि भारत की अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भाषा को तीन प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं- पहला वो जिसे हमारे समाज में और हमारे आसपास में बोला जाता है, इसे हम मातृभाषा कहते हैं। दूसरा वो जिसे विभिन्न राज्यों में सरकारी उपयोग में भी लाया जाता है, इसको राजभाषा कहते हैं। और तीसरा वो जिसे पूरे राष्ट्र में उपयोग में लाया जाये, सभी सरकारी विभागों द्वारा उपयोग किया जाये और जिसकी मान्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो यानि की राष्ट्रभाषा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की ‘राजभाषा’यानी राजकाज की भाषा है न कि राष्ट्रभाषा और भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। निश्चित रूप से विभिन्न भाषाओं और बोलियों की सम्पन्नता के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर आज तक हम किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं कर सके जो की दुखद होने के साथ ही अफसोसजनक भी है।
भारतीय संविधान में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में राजकीय कार्यों में प्रयोग के लिए हिन्दी के अतिरिक्त 21 अन्य भारतीय भाषाओं यानि कुल 22 भारतीय भाषाओं को स्वीकार किया है। इन 22 भाषाओं में हिंदी, असमिया, ओडिय़ा, डोगरी, उर्दू, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, मणिपुरी, संस्कृत, सिन्धी, कन्नड़, कोंकणी, बंगाली, पंजाबी, बोड़ो, नेपाली, मराठी, मलयालम, मैथिलि, संथाली और तेलुगु भाषा शामिल हैं तथा राज्यों की विधानसभाएं बहुमत के आधार पर इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा अथवा एक से अधिक भाषा को अपने राज्य की राजभाषा घोषित कर सकती हैं।
दरअसल वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके सामने भाषा को लेकर बड़ा सवाल मुँह बाए खड़ा था, क्योंकि एक तो वर्षों तक अंग्रेज और अंग्रेजियत की गुलामी उस पर से देश के भीतर बोली जाने वाली अनेकों भाषाएं। ऐसे में कौन सी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा चुनी जाये यह मुद्दा काफी महत्वपूर्ण था। हिंदी चूँकि देश के अधिकांश हिस्सों में बोली व समझी जाती थी, इसलिए हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में स्थापित की गई क्योंकि उस समय सभी को यही लगा कि हिंदी एक मात्र ऐसी भाषा है जो पूरे देश को जोड़ सकेगी। पर काफी सोच विचार के बाद हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ही नए राष्ट्र की भाषा चुन लिया गया और फिर संविधान सभा ने देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। बाद में फिर 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। किन्तु कुछ राज्यों में हिंदी भाषा में कार्य करने में असुविधा महसूस की जाने लगी और साथ ही अंग्रेजी भाषा को हटाए जाने की खबर जब देश के दक्षिण भारतीय हिस्सों में पहुंची तो वहाँ हिंसक विरोध प्रर्दशन भी हुए।
बहरहाल हिंदी भाषा के उपयोग की प्रगति का जायजा लेने के लिए वर्ष 1955 में संविधान की धारा 344 के अनुसार एक राजभाषा आयोग बनाया गया तथा इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 1957 में एक संसदीय समिति बनाई गई। इन दोनों की राय यह थी कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग चलते रहना चाहिए, तद्नुसार 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया, जिसका 1976 में संशोधन किया गया। और फिर सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए। राजभाषा नियम बन जाने से हिन्दी के प्रयोग में काफी सहायता मिली अत: यह एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हुआ पर फिर भी हिंदी की बिंदी को राष्ट्र के माथे पर तिलक के सामान नहीं लगाया जा सका।
|
हिंदी में संभावनाएँ तो अथाह हैं बस शर्त यही है कि अन्य मुद्दों की तरह ही इसे भी मजबूत इरादों के साथ ‘एक देश एक विधान’, ‘एक देश एक चुनाव’, ‘वन नेशन वन टैक्स’, ‘वन नेशन वन ग्रिड’ के तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर ‘एक देश एक भाषा’जैसे नारे के साथ खड़ा कर दिया जाये और साथ ही लोगों को यह समझाया जाये कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए हिंदी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाना कितना आवश्यक है। |
पर यदि देश में हिंदी का राजनीतिक विरोध करने वाले लोग हैं तो दुनिया भर में हिंदी को चाहने वालों की भी कोई कमी नहीं है। अपने इसी हिंदी प्रेम के कारण हिंदी भाषा के प्रेमियों ने भारत के अलावा दुनिया भर में हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए अपना प्रयास जारी रखा और सभी ने मिलकर 10 जनवरी 1975 को नागपुर में एक विश्वज हिन्दीे सम्मेेलन आयोजित किया। इस सम्मलेन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए और फिर वर्ष 2006 से हर साल 10 जनवरी को विश्वभर में विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाने लगा।
वैसे संभवत: विश्व में किसी और भाषा के लिए कोई दिवस नहीं मनाया जाता है इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हिंदी को हिंदी दिवस की बैसाखी थमा दी गई हो। जबकि वर्तमान में हिंदी की लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व भर में हर पांच में से एक व्यक्ति हिंदी में इंटरनेट प्रयोग करता है और इन्टरनेट पर हिंदी सामग्री की खपत करीब 94 प्रतिशत बढ़ गई है और बड़ी बड़ी दिग्गज कम्पनियाँ हिंदी भाषियों को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रही हैं अर्थात् यदि हम चाहें तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म अर्थात् फेसबुक, ट्विटर और वाट्स एप आदि में हिंदी में लिख सकते हैं जिसके लिए गूगल हिंदी इनपुट, लिपिक डॉट इन जैसे अनेक सॉफ्टवेयर और स्मार्टफोन एप्लीकेशन दिग्गज कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराये गए हैं। यही नहीं हिंदी सहित भारतीय भाषाओं में इंटरनेट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने वॉइस सर्च इन हिंदी, सर्च रिजल्ट पेज पर हिंदी टैब, क्रोम में न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन इन क्रोम तथा गूगल असिस्टेंट आदि सुविधाएँ भी उपलब्ध करवाई हैं और भारतीय भाषा विशेष रूप से हिंदी के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के विकास पर प्रकाश डालते हुए केपीएमजी के साथ मिलकर एक रिपोर्ट भी पेश की है। रिपोर्ट का सार है कि वर्ष 2021 के अंत तक इन्टरनेट पर अंग्रेजी से ज्यादा प्रचलित भाषा हिंदी होगी यानि इसमें कोई संशय शेष नहीं कि हिंदी की ताकत को दुनिया मान रही है।
पहले हिंदी या किसी अन्य भारतीय भाषा में कंप्यूटर या मोबाइल पर कार्य करने में बहुत मुश्किलें आती थीं पर यूनिकोड आने के बाद इस समस्या का हल भी निकल गया है। एक समान कोडिंग होने के कारण अब अंग्रेजी के समान ही किसी भी भारतीय भाषा में कंप्यूटर पर ज्ञान-विज्ञान का आदान प्रदान आसानी से किया जा सकता है। ये अलग बात है कि आने वाले समय में शायद एक नई तरह की चुनौती का सामना भी हमें करना पड़ सकता है। क्योंकि हिंदी लिखने के लिए अधिकांश लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर के की-बोर्ड पर क्वाटरी की-पैड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यानि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित इंडिक टूल या फिर गूगल हिंदी इनपुट का इस्तेमाल कर उन्हें ऐसा लगता है कि उनको हिंदी टाइपिंग आ गया। इसलिए इस बार के हिंदी दिवस पर एक बार हमें क्वाटरी ‘की-बोर्ड’ या ‘की-पैड’ के उपयोग के आदतों पर भी ध्यान देना होगा।
आने वाले समय में नई शिक्षा नीति से भी अच्छे संकेतों के मिलने की उम्मीदें हैं क्योंकि इसमें देश की विविधता और स्थानीय संदर्भों को उचित और समान स्थान देने के लिए त्रिभाषा को स्थान दिया गया है यानि एक तरफ मातृ भाषा तथा अन्य भाषाओं को सीखने पर जोर दिया गया है तो दूसरी तरफ भारत की प्राचीन भाषाओं के महत्व को भी स्वीकार किया गया है।
चलते-चलते इस बार के राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर हम सभी स्वयं से एक प्रश्न जरुर पूछें कि यदि हमारे सामने कोई फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा कोई शख्स हो तो क्या उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, उससे हिंदी में वार्तालाप करने में स्वयं को असहज पाते हैं, अंग्रेजी में उत्तर देने में ही अपनी शान समझते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ में है तो मेरी सलाह है कि हिंदी दिवस पर किसी को शुभकामना देने की औपचारिकता छोडक़र पहले आप अपनी भाषा पर गर्व करना सीखिए क्योंकि उसके बगैर हिंदी दिवस का आयोजन व्यर्थ है।
आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले महान् साहित्यकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की दो पंक्तियों से मैं इस लेख का समापन करती हूँ-
निज भाषा उन्नति रहे, सब उन्नति के मूल
बिनु निज भाषा ज्ञान के, रहत मूढ़-के-मूढ़।
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Nov 2024 17:59:04
जीवन सूत्र (1) जीवन का निचोड़/निष्कर्ष- जब भी बड़ों के पास बैठते हैं तो जीवन के सार तत्त्व की बात...





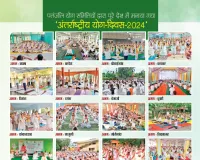
.jpg)