कैसे होता है प्राणायाम से पाप का नाश
On

आचार्य विजयपाल प्रचेता
पतञ्जलि योगपीठ, हरिद्वार
स्मृतियों (धर्मशात्रों) में पापनाश के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है। वहाँ एक बात सामान्यरूप से पाई जाती है कि प्राय: सभी पापों के विविध प्रायश्चित्तों के साथ एक प्रायश्चित्त प्राणायाम करना भी बताया जाता है। प्रायश्चित्त का अभिप्राय है कि पाप हो जाने पर पछतावा करते हुए तप करने का निश्चय करते हुए कोई विशिष्ट तप करे। ऐसा करने से व्यक्ति पाप से दूर हो जाता है। जैसा कि मनुस्मृति में कहा है-
प्रायो नाम तप: प्रोत्तं चित्तं निश्चय उच्यते।
तपोनिश्चयसंयुत्तं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्।।
(मनुस्मृति-11-5)
प्राय का अर्थ तप है और चित्त का अर्थ- निश्चय। पाप हो जाने पर पाप की वासना को तथा उसके संस्कार को नष्ट करना आवश्यक है, जिससे पाप की पुनरावृत्ति न हो। इस प्रकार के निश्चय के साथ तप करना ही प्रायश्चित्त है। विविध पापों के प्रायश्चित्त के प्रसंग में धर्मशास्त्रकारों ने प्राणायाम को एक मुख्य प्रायश्चित्त बताया है-
प्राणायामशतं कार्यं सर्वपापापनुत्तये। (याज्ञवल्क्यस्मृति-3.305)
इसका भाव है कि सभी पापों को दूर करने के लिए 100 प्राणायाम करने चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि धर्मशास्त्रकारों की दृष्टि में प्राणायाम एक पापनाशक साधन है तथा यह सभी पापों को दूर करने के लिए एक सामान्य प्रायश्चित्त है। इसके पीछे कारण यह है कि पाप मन की विकृति से होता है और प्राणायाम मन की विकृति को दूर करता है। न केवल धर्मशास्त्रकारों की दृष्टि में, योगशास्त्रियों की दृष्टि में भी प्राणायाम को पाप, कल्मष व अशुद्धि का नाशक माना जाता है। जैसा कि योगसूत्र के व्यासभाष्य में उद्धृत पञ्चशिखाचार्य के इस वचन से स्पष्ट है-
तपो न परं प्राणायामात्, ततो विशुद्धिर्मलानां, दीप्तिश्च ज्ञानस्य।
(योगसूत्र, व्यासभाष्य- 2.52)
इसका अर्थ है- प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है, इससे मलों की शुद्धि व ज्ञान (विवेक) की वृद्धि होती है। प्राणायाम एक शारीरिक क्रिया है। इससे पापनाश कैसे होता है; यह विचार का विषय है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस विषय में गहन चिन्तन व अनुभव किया है। उनके अनुभूत वचन इस विषय में हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि प्राणायाम एक तप है। इसके करने से शरीर, इन्द्रियाँ व मन तपते हैं तथा उनके विकार, चञ्चलता व कल्मष नष्ट हो जाते हैं। यह तथ्य मनुस्मृति में निम्न शब्दों में कहा गया है-
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मला:।
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा: प्राणस्य निग्रहात्।। (मनु.-6.70)
जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्ण आदि धातुओं के मल जल जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम से मन व इन्द्रियों के दोष जल जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्राणायाम से मन के विकार काम, क्रोध, लोभ आदि व विषयासक्ति क्षीण हो जाती है तथा प्राणायाम का अभ्यासी व्यक्ति जितेन्द्रिय होकर पापमुक्त जीवन जीता है।
श्रीमद्भगवद्गीता में हम इस तथ्य का और भी अधिक व विशद विवेचन पाते हैं कि प्राणायाम से पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन श्रीकृष्ण से पूछते हैं-
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुष:।
अनिच्छन्नपि वाष्र्णेय बलादिव नियोजित:।। (गीता-3-36)
हे भगवन्! किससे प्रेरित होकर यह पुरुष पाप करता है। व्यक्ति न चाहता हुआ भी किसके द्वारा हठपूर्वक पाप में प्रवृत्त कर दिया जाता है; भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि-
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भव:।
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्।। (गीता-3.37)
हे अर्जुन! रजोगुण से उत्पन्न होने वाला यह जो काम और क्रोध है, यही वह वैरी है, जो अनिच्छुक पुरुष को भी पाप में प्रवृत्त कर देता है। यह काम महाशन अर्थात् कभी न तृप्त होने वाला है। यह असीम है। कामनाओं की बाधा होते ही तुरन्त उत्पन्न होने वाला जो क्रोध है, वह साक्षात् महापाप रूप है। क्रोध को महापाप कहने का अभिप्राय यह है कि क्रुद्धावस्था में विवेकहीन व्यक्ति बड़े से बड़ा पाप कर गुजरता है। उसका कारण क्रोध ही है। इसलिए महापाप का कारण होने से इसे प्रस्तुत श्लोक में साक्षात् महापाप ही कहा है।
इससे स्पष्ट हुआ कि न चाहते हुए भी मनुष्य को पाप में लगाने वाला रजोगुणजन्य काम व क्रोध है। जब तक रजोगुण प्रबल रहता है तब तक काम व क्रोध भी मनुष्य को वशीभूत किये रहते हैं। इनसे मुक्त होने के लिए, पाप से बचने के लिए रजोगुणी प्रवृत्ति को क्षीण करना आवश्यक है। गीता में इसके लिए अन्य आध्यात्मिक उपायों के साथ प्राणायाम को एक महत्त्वपूर्ण उपाय के रूप में बताया है। वहाँ प्राणायाम को यज्ञ के रूप में प्रस्तुत करते हुए उक्त कल्मषों (मलों व पापों) का नाशक कहा गया है-
अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे।
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणा:।।
अपरे नियताहारा: प्राणान् प्राणेषु जुह्वति।
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा:।। (गीता-4.29-30)
अर्थात् नियताहार (आहार-विषयक संयम रखने वाले, समय पर हित-मित भोजन करने वाले) साधक अपान में प्राण की आहुति देते हैं अर्थात् पूरक प्राणायाम (आभ्यन्तर वृत्ति) करते हैं तथा प्राण में अपान की आहुति देते हैं अर्थात् रेचक प्राणायाम (बाह्यवृत्ति) करते हैं। कुछ साधक बिना रेचन व पूरण के यथावस्थित प्राणापान की गति को रोक कर प्राणों की प्राणों में आहुति देते हैं अर्थात् स्तम्भवृत्ति प्राणायाम करते हैं। इस गीतावचन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राणायाम एक ऐसा यज्ञ है जो कल्मषों, मन व इन्द्रियों के विकारों को क्षीण कर देता है। इसका भाव यही है कि प्राणायाम से जब शरीर, मन व इन्द्रियों को तपाया जाता है तो इनके कल्मष जल जाते हैं। व्यक्ति रजोगुण के वश में न रहकर सत्त्वगुण प्रधान हो जाता है। इससे उसकी प्रवृत्ति पाप में न होकर पुण्यकर्मों में होती है। रजोगुण के क्षीण होने व सत्त्वगुण के बढऩे से उसके मन में एकाग्रता आ जाती है। एकाग्रता से ज्ञान प्रकट होता है और व्यक्ति उचित अनुचित का विवेक कर अनुचित को छोड़ देता है तथा उचित कार्यों में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार प्राणायाम से बनी सात्त्विक वृत्ति मनुष्य को पापमुक्त, सच्चरित्र व सन्मार्गगामी बना देती है। ऐसा व्यक्ति परिवार, समाज व राष्ट्र का परम हितकारी बन जाता है। इस प्रकार प्राणायाम व्यक्तिगत जीवन में शुचिता लाकर हमारे सामाजिक जीवन को भी उज्ज्वल करने का अमोघ साधन है।
प्राणायाम से पापनाश की इस प्रक्रिया का समर्थन महर्षि पतञ्जलि द्वारा रचित योगसूत्र में भी किया गया है। वहाँ प्राणायाम का स्वरूप बताने के उपरान्त इसका लाभ बताते हुए महर्षि कहते हैं कि-
तत: क्षीयते प्रकाशावरणम्। धारणासु च योग्यता मनस:।
(योगसूत्र-2.52-53)
इसका भाव है कि प्राणायाम करने से प्रकाश (ज्ञान) का आवरण (पर्दा) तमोगुण क्षीण हो जाता है अर्थात् जब प्राणायाम का अभ्यासी व्यक्ति अपने शरीर, मन व इन्द्रियों को प्राणायाम रूपी तप से तपाता है तो उसके मन का वह तमोगुण क्षीण हो जाता है, जिसने ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल रखा था तथा मनुष्य को मूढता की स्थिति में रखा था। प्राणायाम का दूसरा लाभ बताते हुए महर्षि कहते हैं कि इससे धारणा में, टिकाव में, एकाग्रता साधने में मन की योग्यता बनती है। इसका भाव है कि प्राणायामरूपी तप से शरीर, मन व इन्द्रियों को तपाने से वह रजोगुण रूपी दोष क्षीण हो जाता है, जो मन को चञ्चल बनाए रहता है। रजोगुण का लक्षण चञ्चलता एवं राग-द्वेष है- चलञ्च रज: (सांख्यकारिका- 13), रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् (श्रीमद्भगवद्गीता-14.7), रागद्वेषात्मकं रज:। रागद्वेषौ रज: स्मृतम् (मनुस्मृति-12.27)। यह रजोगुण ही मन की धारणा (स्थिरता) नहीं बनने देता है। महर्षि पतञ्जलि कहते हैं कि प्राणायाम से मन की धारणा (टिकाव) में योग्यता बन जाती है।
इसका सीधा सा अर्थ यही है कि प्राणायामरूपी तप से मन का रजोगुण क्षीण हो जाता है व मन में स्थिरता (एकाग्रता) की योग्यता आ जाती है। इससे पहले गीता के प्रमाण से कहा जा चुका है कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम व क्रोध मनुष्य को पाप में लगा देता है। उस रजोगुण का प्राणायाम से क्षीण होना महर्षि पतञ्जलि के वचन से भी प्रमाणित है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि मनुष्य को पाप में लगाने वाला रजोगुण प्राणायाम से क्षीण होता है। रजोगुण के क्षीण होने से, इससे उत्पन्न होने वाले काम व क्रोध शिथिल पड़ जाते हैं। रजोगुण से होने वाली विषयासक्ति प्राणायाम के अभ्यास से दुर्बल होने लगती है और मनुष्य की प्रवृत्ति पाप से हटकर पुण्य में होने लगती है। अत: योगदर्शन के उक्त वचन भी गीताप्रोक्त उस तथ्य को पुष्ट करते हैं कि प्राणायाम द्वारा रजोगुण नष्ट होता है, ऐसा होने पर रजोगुणजन्य काम, क्रोध नष्ट होते हैं। ये ही पाप के मूल हैं। इनके नष्ट होने से पाप नष्ट होता है।
योगदर्शन की साधनापद्धति के अनुसार प्राणायाम द्वारा तमोगुण व रजोगुण के क्षीण होने पर साधक की साधना में प्रगति होती है। उसका निर्मल ज्ञान बढ़ता है व मन का टिकाव होने लगता है। मन का यह टिकाव (एकाग्रता) ही आगे साधना में उन्नति का मूल आधार है। इसी से साधक आगे समाधि की उच्च स्थिति तक पहुँचता है। इस प्रकार यह एकाग्रता आध्यात्मिक पथ के पथिक के लिए आगे की उन्नति का मूल आधार है। प्राणायाम के अभ्यास से प्राप्त यह एकाग्रता व मन की निर्मलता लौकिक व्यक्ति के लिए भी बड़े काम की है। मनुष्य का इहलौकिक व पारलौकिक कल्याण मन की इसी एकाग्रता व निर्मलता पर निर्भर है, जिसे सिद्ध करने के लिए प्राणायाम एक अमोघ उपाय है। चरकसंहिता में मन की इस एकाग्रता व निर्मलता को मन:समाधि नाम से बतलाते हुए इसे ही सारे कल्याणों का मूल कहा है-
प्रेत्य चेह च यच्छ्रेय: श्रेयो मोक्षे च यत्परम्।
मन:समाधौ तत्सर्वमायत्तं सर्वदेहिनाम्।।
(चरकसंहिता, चिकित्सास्थान-24.52)
इसका भाव यह है कि इस जन्म में तथा मरने के उपरान्त अगले जन्म में जो शुभ है एवं मोक्षरूपी जो शुभ है, वह सब मन की एकाग्रता पर ही निर्भर है। जिसका मन रजोगुणजन्य काम, क्रोध आदि से व्याकुल न होकर एकाग्र व निष्कल्मष हो गया है, वह व्यक्ति ही इस जन्म में व अगले जन्म में शुभ व कल्याण को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अन्तत: मोक्ष (मुक्ति) भी प्राप्त कर लेता है।
उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो गया है कि यद्यपि प्राणायाम एक शारीरिक प्रक्रिया है, परन्तु तपरूपी यह प्रक्रिया शास्त्रकारों के द्वारा बताई पूर्वोक्त रीति से पाप को नष्ट कर देती है। मन को निर्मल, निष्पाप व एकाग्र बना देती है। प्राणायाम की इसी क्षमता के कारण धर्मशास्त्रकारों ने इसे पापों को दूर करने वाला एक उत्तम प्रायश्चित्त बताया है। हम यहाँ धर्मशास्त्रकारों के इस आशय के कुछ वचन प्रस्तुत कर रहे हैं-
अह्ना रात्र्या च यान् जन्तून् निहन्त्यज्ञानतो यति:।
तेषां स्नात्वा विशुद्ध्यर्थं प्राणायामान् षडाचरेत्।। (मनुस्मृति:- 6.69)
भ्रमणादि के समय अनजाने में रात-दिन में जो जन्तुओं की हिंसा हो जाती है, उसके प्रायश्चित्त के लिए यति को स्नान करके छ: प्राणायाम करने चाहिए।
अथवा मुच्यते पापात् प्राणायामपरायण:।
प्राणायामैर्दहेत्सर्वं शरीरे यच्च पातकम्।। (अरुणस्मृति:- 121)
प्राणायाम करने वाला व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। प्राणायाम से मन का पाप और शरीर का मल जल जाता है।
यथा हि वेगतो वह्नि: शुष्काद्र्रं दहतीन्धनम्।
प्राणायामैस्तथा पापं शुष्काद्र्रं नात्र संशय:।।
जैसे तीव्र प्रज्ज्वलित अग्नि सूखे व गीले इन्धन को जला देती है, उसी प्रकार प्राणायाम नये व पुराने पाप को नष्ट कर देता है।
प्राणायामशतं कार्यं सर्वपापप्रणाशनम्।
उपपातकजातानामनादिष्टस्य चैव हि।।
पापनाश के लिए 100 प्राणायाम करने चाहिए, ऐसा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। धर्मशास्त्रों में बताए उपपातक व अनिर्दिष्ट पातकों के लिए भी यही प्रायश्चित्त समझना चाहिए।
गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च।
नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च।। (गीतामाहात्म्यम्)
गीताध्ययनशील व प्राणायामपरायण व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वे इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों।
प्राणायाम की इस पापनाशक क्षमता का वर्णन मूलत: हमें वेदों में मिलता है। उसी के आधार पर शास्त्रकारों ने उपर्युक्त रीति से इसका विस्तार किया है। ऋग्वेद में कहा है-
वृत्रस्य त्वा श्वसथादीषमाणा विश्वे देवा अजहुर्ये सखाय:।
मरुद्भिरिन्द्र सख्यं ते अस्त्वथेमा विश्वा: पृतना जयासि।। (ऋग्वेद-8.96.7)
हे आत्मन्! वृत्र (पाप) की हुंकार से भयभीत होते हुए जिन सब देवों (दिव्यगुणों, अच्छी प्रवृत्तियों) ने तुझे छोड़ दिया था, ऐसे समय में यदि तेरी मित्रता मरुद्गणों (प्राणों) से हो जाय, तो तू वृत्र (पाप) की इस सारी सेना को जीत सकता है। इस मन्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पाप के प्रबल होने पर सद्गुण मनुष्य को छोड़ जाते हैं। यदि मनुष्य प्राणों के साथ मित्रता कर ले अर्थात् प्राणायाम की साधना करे तो वह पाप की इस सारी सेना को जीत सकता है। इस प्रकार इस वेदमन्त्र में यह तथ्य स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि प्राणायाम पापनाशक साधन है। एक दूसरे वेदमन्त्र में भी यह तथ्य प्रतिपादित किया गया है-
यदा गच्छात्यसुनीतिमेतामथा देवानां वशनीर्भवाति। (ऋग्वेद-10.16.2)
अर्थात् जब मनुष्य असुनीति (प्राणायाम) को साधता है, तो वह देवों (इन्द्रियों) का वशकत्र्ता स्वामी बन जाता है। उनका दास नहीं रहता। इससे भी यह सर्वथा स्पष्ट है कि प्राणायाम से इन्द्रियों की विषयासक्ति नष्ट हो जाती है तथा व्यक्ति जितेन्द्रिय एवं पापरहित हो जाता है।
भारतीय ऋषियों ने इस तथ्य को अति प्राचीनकाल में ही बहुत अच्छी तरह से जान लिया था, अत: उन्होंने प्राणायाम की क्रिया को प्रत्येक व्यक्ति के लिये अनिवार्यतया की जाने वाली सन्ध्याविधि में ही जोड़ दिया था। संसार में अन्य किसी भी धर्म की उपासना-पद्धति ऐसी नहीं है, जिसमें प्राणायाम किया जाता हो। वैदिक-सन्ध्या ही एक ऐसी उपासना-पद्धति है, जिसमें प्राणायाम मन्त्र है तथा प्राणायाम उसका अपरिहार्य अंग है।
मन की व्यग्रता, व्याकुलता, बेचैनी को दूर करने का भी यह सुपरीक्षित उपाय है। जब ऐसी अवस्था अनुभव करें तो धैयर्पूर्वक गहरे श्वास लेना शुरु कर दें। बाह्य व आभ्यन्तर प्राणायाम की 10-15 आवृत्ति करें। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि मन की अशान्ति दूर हो रही है तथा मन शान्त व स्थिर होने लगा है। हमारे मन की चञ्चलता, अशान्ति, विकृति व पाप को दूर करने वाला यह अचूक उपाय बहुत पहले ऋषि-मुनियों ने खोज लिया था, यह आज भी उतना ही कारगर व प्रासंगिक है।
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Dec 2024 18:59:48
योग प्रज्ञा योग - योग जीवन का प्रयोजन, उपयोगिता, उपलब्धि, साधन-साधना-साध्य, सिद्धान्त, कत्र्तव्य, मंतव्य, गंतव्य, लक्ष्य, संकल्प, सिद्धि, कर्म धर्म,...



.jpg)
.jpg)



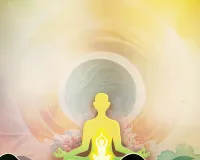







.jpg)


1.jpg)
.jpg)
