मन को दिशा दें और बनें समृद्धिवान
On

आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज
बृहदारण्यक उपनिषद् का ऋषि मन के स्वरूप को इस रूप में प्रकट करता है कि काम, संकल्प, विचिकित्सा,श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति:, अधृति:, ह्री:, धी: ये सब मन के ही विविध रूप हैं। मन के बिना काम, संकल्पादि का मानो कोई अस्तित्व ही नहीं है। वे कहते हैं प्रगाढ़ निद्रा में या समाधि में मन नहीं होता, इसलिए वहाँ काम (कामना), संकल्पादि भी नहीं होते। जबकि शुभ या अशुभ इच्छा के उत्पन्न होने पर व्यक्ति उस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ करने की इच्छा करता है, यही 'संकल्प’ है। मन के सम्बन्ध में श्री महाराज सदा मन को मित्र बनाकर रखने की सलाह दिया करते हैं। महाराज का कहना है- जैसे एक सच्चा मित्र कभी भी अपने मित्र का अनिष्ट नहीं करता, इसी प्रकार मन यदि हमारा मित्र हो जाता है तो वह सदा हमारा कल्याण करने में भी जुट जाता है।
इसके लिए मन से नित्य प्रार्थना की जाए कि तू एक ही साथ जहाँ ध्यान मग्न योगी की तरह पूर्ण शान्त है, वहाँ वीर योद्धा के समान प्रचण्ड वेग से भी भरा हुआ है। जिस काम को तू करना ठान लेता है- त्रिलोकी में भी उसे रोकने का किसी में सामर्थ्य नहीं है। तू मेरा अक्षयपात्र है; मेरे हृदय का पूज्य देव है; सच्चा सुहृद् है; सेनापति इन्द्र है; महान् धन कुबेर है; कठिनाइयाँ व बाधाएँ तेरे गले का हार हैं। हे मेरे मन! तू मेरा सच्चा हितैषी है। तू एक ही साथ माँ के समान प्रेम का अवतार है और गुरु के समान अनन्त धैर्य का सागर है। मैं कहाँ तक तेरा गुणगान करूँ? बस! तुझसे मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि तू सदा मुझे अपना प्यारा मित्र समझता रहे और मैं भी तेरे प्रति सदा निश्चल प्रेम से भरा रहूँ। जीवन-यात्रा में आगे बढ़ने के लिए मुझे तेरे सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि इस प्रार्थना से मन संकल्पनानुसार जगे बिना नहीं रहेगा।
केवल मन की शक्ति से त्वचा इन्द्रिय में ही नहीं, बल्कि सभी ज्ञानेन्द्रियों में भी वही अनुभूति (Sensation) उत्पन्न हो जाती है। जैसे कोई गन्ध नहीं है, फिर भी नासिका उस विशिष्ट गन्ध को ग्रहण करने लगती है। कान शब्द सुनने लगते हैं। आँखें तो रूप देखती ही हैं। रसना बिना किसी पदार्थ के ही विशिष्ट रस को ग्रहण करने में सक्षम हो जाती है। यों तो हम सब को यह एक सामान्य घटना लगती है; किन्तु ध्यान दिया जाए तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे मन ही उस इन्द्रिय के अन्दर वह संवेदना उत्पन्न कर देता है जो कि जागृत अवस्था में बाह्य विषय के साथ संयोग से ही सम्भव है। यह मन की एकाग्रता की शक्ति के कारण ही हो पाता है।
इसी प्रकार मन जब किसी विषय में पूर्ण विश्वासी हो जाता है, तो उस विशेष अवस्था में वह अपरिमित बल से भरा हुआ होता है। और तब सारा शरीर-तन्त्र मन का आज्ञानुवर्ती हो जाता है। दूसरे शब्दों में जो कुछ भी शुभ या अशुभ जैसा भी मन को सिखा दिया या समझा दिया जाता है, मन की ओर से उसी के अनुसार प्रतिक्रिया होती है। यदि मन को सिखा दिया कि विषयों में सुख है तो ठीक उसी के अनुसार प्रत्युत्तर (Response) मिलता है और विषयों मेंं दु:ख देखना सिखा दिया जाता है तो फिर उसे सदा दु:ख ही दिखायी देता है।
इसी प्रकार 'मैं शान्त हूँ’ मन के द्वारा यह सोचते ही सब कुछ शान्त हो जाता है। 'मैं आज बड़ा अशान्त हू’ तो अशान्ति की ही श्रंखला चालू हो जाती है। किसी भी उपाय से यदि हमारे आन्तरिक विश्वास में यह बात अच्छे से बिठा दी जाती है कि मन तो हमारा महाशत्रु है तो वह सदा शत्रु रूप में ही दिखता है। मन को एक घनिष्ठ मित्र के रूप में देखने की दृष्टि विकसित हो जाती है, तो फिर वह मित्र ही दिखायी देता है। मन के संदर्भ में यह दो दृष्टियां हैं। आगे जिसको जो पसन्द हो, उसे स्वयं ही चुनाव करना होता है।
आचार्य शंकर कहते हैं- ''मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो:।‘’ अर्थात सांसारिक विषयसुख (सत्ता-सम्पत्ति-सम्मान) की इच्छा भी मन से ही होती है और अमृतत्व की इच्छा भी मन से ही।
अथर्ववेद में ये मन्त्र हैं, जो मन के महत्व को दर्शाते हैं-
अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तर:। अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शन:।।6।।
हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाच: पुरोगवी।
अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभि मृशामसि।।7।। (अथर्व 4/13/6-7)
पाठकों के समक्ष मन की अपरिमित शक्ति का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य उदयवीर शास्त्री ने प्राचीन साङ्खय सन्दर्भ नामक अपने ग्रन्थ में लिखते हैं कि पंजाब प्रान्तीय 'मुकेरियाँ’ नगर के निवासी प्रोफेसर जगदीश मित्र जो सन् 1917 से 1921 तक प्रत्येक वर्ष गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर के वार्षिक महोत्सव पर पधारते रहे। उनके द्वारा मन को लेकर बीसों प्रदर्शन देखने का मुझे अवसर मिला।
प्रो0 जगदीश मित्र मन: शक्ति का उपयोग जीवनपर्यन्त मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए करते रहे।
एक दिन कॉलेज से वापसी पर मैं प्रोफेसर के साथ बैठा बातें कर रहा था। उससे पहले दिन प्रोफेसर ने एफ0सी0 कॉलेज (फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज) में प्रदर्शन किया था। मुझे वहाँ बैठे दस-बारह मिनट ही हुए होंगे, इतने में आवाज सुनाई पड़ी कि प्रोफेसर कहाँ है? यह बड़ा मक्कार आदमी है, कल इसने सबको बेवकूफ बनाया। कहाँ है ? हम इसे समझेंगे! स्वर बड़ा ऊँचा व तीव्र था।
हम दोनों यह सुन ही रहे थे कि कुछ सेकण्ड में बराण्डे को लाँघते हुए दो नवयुवक धड़धड़ाते हुए तीव्रता के साथ कमरे के दरवाजे तक पहुँच गए। प्रोफेसर ने उनकी ओर देखा और सरलता पूर्वक पर आदेश की मुद्रा में कहा- आप अन्दर नहीं आ सकते। युवकों का जवाब था- हम जरूर अन्दर आएँगे, अन्दर आएँगे। प्रोफेसर के द्वारा दुबारा यह कहते ही कि- आप हर्गिज अन्दर नहीं आ सकते, दोनों युवक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। जोर से चिल्लाये- पेन! शूटिंग पेन! मैंने सामने देखा- वे दोनों पानी के बाहर मछली की तरह तड़प रहे हैं।
उनकी इस तड़पन की आवाज पर प्रोफेसर ने पूछा- पेन कहाँ है? स्टमक में प्रोफेसर! शूटिंग पेन! तत्काल प्रोफेसर ने युवकों के कन्धों को स्पर्श किया, क्षण भी नहीं लगा, दोनों युवक ऐसे शान्त हो गए जैसे भयंकर कष्ट के बाद आशातीत राहत पाई हो। कुछ ही सेकण्ड में दोनों युवक उठे और प्रोफेसर के पैरों में पड़कर बड़ी विनम्रता के साथ क्षमा-प्रार्थना करने लगे। प्रोफेसर ने हर प्रकार सान्त्वना देकर उन्हें विदा किया। उनकी बेजा हरकत पर उलाहना आदि के रूप में एक भी शब्द प्रोफेसर ने अपने मुँह से नहीं निकाला।
इस संदर्भ में श्री महाराज जी की अपनी दृष्टि है कि 'मन-इन्द्रियाँ-शरीर-हृदय सबको एक हँसते-खेलते परिवार के रूप में देखना चाहिए।‘ वे कहते हैं अपने मन को सतत सुझाव (Auto Suggestions) देते रहने से मन निश्चित रूप से हमारा मित्र बनकर रहना स्वीकार कर लेता है और वह कभी भी ऐसी बात नहीं सोचता, ऐसा संकल्प नहीं करता जिससे हमारा अहित होता हो। मन की मित्रता ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है, उसी अनुपात में साधक को अनुभव होता जाता है कि बाधाएँ सहज ही निवृत्त होती जा रही हैं ।
मन के सम्बन्ध में यहाँ तक कहा गया है कि जिसने कण को जान लिया वह धनवान् है। जिसने क्षण को पकड़ लिया वह विद्वान् है। जिसने मन को समझ लिया वह भाग्यवान् है । श्री महाराज कहते हैं कि मन को समझने का भाव है- इसकी प्रकृति (Nature), इसकी अनन्त शक्तियों, इसके अप्रतिहत ओज व तेज, शान्त व उग्ररूप, साहस, धैर्य, शौर्य, बल-वीर्य-पराक्रम, सरल व सौम्यरूप, दृढ़-इच्छा शक्ति को समझना, साथ ही सदा ही सजग व सावधान चेष्टा से उत्साह के साथ अजित अवस्था में समस्त आपत्तियों-विपत्तियों की या फिर उसकी स्वेच्छाचारिता के समय प्रलयंकारी दृश्यों की कुरूप झाँकियों को देखना-समझना। जो ऐसा कर लेता है, वह सफल दिशा पा जाता है और उसके समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं।
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Dec 2024 18:59:48
योग प्रज्ञा योग - योग जीवन का प्रयोजन, उपयोगिता, उपलब्धि, साधन-साधना-साध्य, सिद्धान्त, कत्र्तव्य, मंतव्य, गंतव्य, लक्ष्य, संकल्प, सिद्धि, कर्म धर्म,...









.jpg)
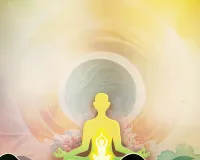





.jpg)


1.jpg)
.jpg)
