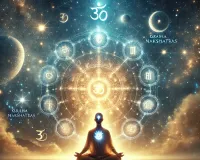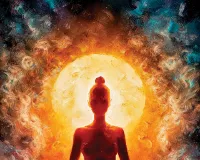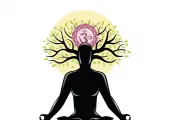‘आदि युग से पूज्य स्वामी जी के युग तक’ ‘योग का शंखनाद’
On

डॉ. रुपेश शर्मा
योग संदेश विभाग
शिव पुराण में लिखा है कि स्वयं देव आदि देव भगवान् शिव ही परम योगी कहलाये गए हैं। भगवान् शिव का नृत्य, ध्यान, समाधि के कारण वह आदि योगी नाम से पुकारे जाते हैं। शिव पुराण में यह भी लिखा है कि योग की पहली शिक्षा माता पार्वती जी ने ही ली थी। तद्उपरांत दूसरी शिक्षा में उन्होंने पृथ्वीलोक में स्थित केदारनाथ धाम के पास कांति सरोवर के तट पर अपने सात शिष्यों को योग के स्वरूप से परिचय करवाया था। इन्ही सातों ऋषियों को आगे चलकर सप्तऋषि के नाम से जाना गया। सातों ऋषियों के माध्यम से पृथ्वी पर योग के अलग-अलग आयाम बतायें गये और यह सभी आयाम योगशास्त्र में सात मूल स्वरूप में स्थापित हो गये। आज के योग में भी यह सातों विशिष्ट स्वरूप में मौजूद हैं। इन सप्त ऋषियों को आदि देव के निर्देशानुसार विश्व की अलग-अलग दिशाओं में भेजकर योग और उसकी शिक्षा से मानव कल्याण के कार्य आरम्भ किये गये। भारत में प्राचीनकाल से ही साधु-संतो एवं योगियों के मठो में यौगिक क्रियाओं को विधिवता कराये जाने की परम्परा रही है। आस्था और अंधविश्वास से अलग हटकर योग एक शारीरिक विज्ञान है, जोकि प्रायौगिक सिद्धान्त पर आधरित है तथा पूर्ण रूप से शारीरिक चिकित्सा पद्धति है। वास्तव में धार्मिक कट्टरता लोगों को एक खूंटे से बाँधती है, वहीं पर योग सभी तरह के बंधनों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है।
योग का परिचय
योग आपकी आत्मा को अनुसंधान में रखने की एक क्रिया है। इससे व्यक्ति स्वयं संयमित कर मन को निर्मलता व तन को स्वस्थ रखता है तथा समाज एवं राष्ट्र के लिए हितकारी बन जाता हैं। सह-अस्तित्व एवं एकतत्व के साथ दिव्य जीवन जीना योग का मुख्य लक्ष्य है। योग एक ऐसा विशुद्ध विज्ञान है, जिसके माध्यम से व्यक्ति की स्व-चेतना का जागरण होता है। उसकी सम्पूर्ण शक्ति जाग्रत होती है वह अपरिचित शक्तियों का स्वामी बन जाता है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि योग स्वचेतना, स्वशक्ति , स्वबल अर्थात् आत्मबल इत्यादि को पूर्णत: जाग्रत करने का विज्ञान है। योग मूलत: पूर्णतया सत्यबोध कराने वाली अध्यात्म विद्या है। योग ही अपराविद्या व पराविद्या का मूल हैं। योग ही धर्म है, योग ही हमारे अभ्युदय व नि:श्रेयस का आधार है। दरिद्रता तथा पलायन धर्म और अध्यात्म नहीं है।
वेदों में योग
पौराणिक परम्पराओं के अनुसार भगवान् शिव को योग का संस्थापक (आदि योगी) कहा जाता है और पार्वती योग की उनकी पहली शिष्या थी। योग के जानकारों के अनुसार योग का उल्लेख सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मौजूद है। इसके माध्यम से ऋषि-मुनि सत्य एवं तप के अनुष्ठान से ब्रह्माण्ड के अनेक रहस्यों से साक्षात्कार करते आये हैं। आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार योग करने से व्यक्ति की चेतना, ब्रह्माण्ड की चेतना से जुड़ जाती है। इसके प्रभाव से मन एवं शरीर और मानव एवं प्रकृति के बीच पूर्ण समंजस्य की अनुभूति होने लगती है।
वह चिंतन, सोच एवं कार्य के बीच एकीकरण एवं तालमेल स्थापित करता है। सदियों से योग की कई शाखाएं विकसित हुई है, लेकिन इस बात पर आम सहमति है कि इसका विकास पूर्ण रूप से भारत में मानव सभ्यता के शुरु में, पूर्व वैदिक काल में हुआ।
अनादिकाल से अक्षुण्ण प्रवाहमान योग से सम्बद्ध विविध परम्पराओं के अंदर ‘योग’ शब्द का प्रयोग ‘साधन’ व ‘साध्य’ दोनों अर्थों में होता आ रहा है। दुनियां के अन्दर विद्यमान प्राय: सभी मत, पंथ, धर्म, दर्शन, संस्कृति, सम्प्रदाय व परम्परा आदि मनुष्य जीवन के ‘परम लक्ष्य’ की बात करते है। वस्तुत: उस ‘परम लक्ष्य’ को ही योग-परम्परा में ‘योग’ शब्द से (साध्य अर्थ में) अभिहित किया जाता है। उस ‘योग’ की प्राप्ति के लिए विविध योग परम्पराओं ने कुछ समान तथा कुछ असमान संख्या वालों अंगों (साधनों) से युक्त ‘योग’ (साधन अर्थ में) का प्रतिपादन किया है वस्तुत: उन अंगों में से जो सार्वभौमिक, सार्वकालिक व सार्वजनिक है, केवल उसे ही हम ‘योगाङ्ग’ कह सकते है अन्यों की नहीं। अन्य अंगों के उन-उन मत, पन्थ धर्म, दर्शन, संस्कृति, सम्प्रदाय व परम्परा आदि की दृष्टि से कुछ विशिष्ट लाभ हो सकते है परन्तु वे सार्वभौमिक, सार्वकालिक व सार्वजनिक न होने के कारण योग ‘योगाङ्ग’ नहीं कहे जा सकते। जहाँ एक और ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति का नाम योग है, वहीं उस स्थिति तक आरोहण कराने के साधन का नाम भी योग है। उदाहरणार्थ जहाँ महर्षि पतंजलि प्रदत्त योग की परिभाषा, चित्त की वृत्तियों के निरोध का योग कहते हैं। इस प्रकार के सभी योगाङ्गों का पालन मुख्य रूप से साधक की समाधि-यात्रा में किसी न किसी रूप में सहयोगी बन सके, इसलिए इन्हें करने का ऋषियों, योगियों ,आचार्य व सन्तों आदि का निर्देश मिलता है। प्रत्येक योगाङ्ग से साधक के तीनों शरीर (स्थूल, सूक्ष्म व कारण) के विविध घटक यथा-पंचकोश (अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय व आनन्दमय) अष्टचक्र (मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, मनस व सहस्रार) विविध नाडिय़ा (ईड़ा, पिगंला सुषम्णा आदि 72 करोड़ 72 लाख 10 हजार 201 नाडिय़ां) अन्त:करण (मन, बुद्धि, चित्त, व अहंकार) आदि समग्र रूप में या आंशिक रूप में प्रभावित हो जाते है। इसी के आधार पर अलग-अलग योगाङ्ग के पालन के पीछे योग (साध्य/लक्ष्य) की प्राप्ति के लिए साधक का क्या उद्देश्य होना चाहिए? इसका भी पूर्वाचार्यो ने निर्धारण किया है, प्राय: सभी योगाङ्गों के उद्देश्य की पूर्ण प्राप्ति ‘असम्प्रज्ञात-समाधि’ में स्थित होने पर हो जाती है। तथापि आंशिक लाभ तो साधक जिस क्षण लक्ष्य को ध्यान में रखकर निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ‘अभ्यास’ प्रारम्भ कर देता है उसी क्षण से मिलना प्रारम्भ हो जाता है। ‘अभ्यास’ हेतु इतिहास के विविध कालखण्ड में विविध ऋषियों-योगियों आदि के द्वारा अनुसन्धित कुछ विधियां ग्रन्थों तथा परम्पराओं में सुरक्षित हैं।
आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक योग ने व उसके प्रकार ने कई करवटें ली हैं, मगर आज भी योग को आदिकाल के स्वरूप में ही स्वीकार किया गया है। यहाँ पर मंत्र के प्रकार को समझते है।
योग की उच्चावस्था समाधि, मोक्ष, कैवल्य आदि तक पहुँचने के लिए अनेकों साधको ने जो साधन अपनायें उन्ही साधनों का वर्णन योग ग्रन्थों में समय-समय पर किया गया है। योग की जो प्रमाणिक संग्रहालय है, उसमें शिव संहिता तथा गोरक्षशतक में योग के चार प्रकारों का वर्णन किया गया हैं। इन्हे समझे बगैर योग को समझना कठिन हो जाता है।
मंत्र योग
‘मंत्र’ का सामान्य अर्थ है ‘मननात् त्रायते इति मन्त्र:’ मनन करने पर जो त्राण दे या रक्षा करे, वही मंत्र है।। मंत्र योग का सम्बंध मन से है, मन को इस प्रकार परिभाषित किया है- मनन् इति मन:। जो मनन्, चिन्तन करता है वही मन है। मन की चंचलता का निरोध मंत्र के द्वारा करना मंत्र योग है।
हठयोग
हठ का शब्दिक अर्थ हठपूर्वक किसी कार्य को करने के लिए किया जाता है। हठ प्रदीपिका पुस्तक में इसका विस्तृत रूप में बताया गया है।
हकारेणोच्यते सूर्यष्ठकार चन्द्र उच्यते।
सूर्या चन्द्रमसो योगाद्धयोगोऽभिधीयते।।
अर्थात् ‘ह’ का अर्थ सूर्य तथा ‘ठ’ का अर्थ चन्द्र बताया गया हैं। सूर्य और चन्द्र की समान अवस्था हठयोग है। शरीर में कई हजार नाडिय़ां है, उनमें तीन प्रमुख नाडिय़ां का वर्णन हैं। वे इस प्रकार है- सूर्य नाड़ी अर्थात् पिंगला जो दाहिने स्वर का प्रतीक है। चन्द्र नाड़ी अर्थात् ईड़ा जो बायें स्वर का प्रतीक है। इन दोनों के बीच तीसरी नाड़ी सुषुम्ना है। इस प्रकार हठयोग वह क्रिया है, जिसमें पिंगला और ईड़ा नाड़ी के सहारे प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराकर ब्रह्मरन्ध्र में समाधिस्थ किया जाता हैं। हठ प्रदीपिका में हठयोग के चार अंगों का वर्णन है-आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बन्ध तथा नादानुसंधान घेरण्ड संहिता में सात अंगों- षट्कर्म, आसन, मुद्राबन्ध, प्राणायाम, ध्यान समाधि जबकि योग तत्वोपनिषद् में आठ अंगों का वर्णन है- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि।
लययोग
चित्त का स्वरूप में विलीन होन या चित्त की निरुद्ध अवस्था लय योग के अन्तर्गत आता है। साधक के चित्त में जब चलते, बैठते, सोते और भोजन करते समय, हर समय ब्रह्म का ध्यान रहें, इसी को लय योग कहते है। योग तत्त्वोपनिषद् में इस प्रकार वर्णन है।
गच्छस्तिष्ठन स्वपन भुंजन् ध्यायेन्त्रिष्कलमीश्वरम् स एव लययोग: स्यात (योगत्वोपनिषद, 22-23)
राजयोग
राजयोग जैसा की नाम से ही अपना परिचय देता है। यह भोगों का राजा कहलाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ-न-कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती हैं। राजयोग महर्षि पतंजलि द्वारा रचित अष्टांग योग का वर्णन आता है। राजयोग का विषय चित्तवृत्तियां का निरोध करना है। महर्षि पतंजलि के अनुसार समाहित चित्त वालों के लिए अभ्यास और वैराग्य तथा विक्षिप्त चित्त वालों के लिए क्रियाओं का सहारा लेकर आगे बढऩे का रास्ता सुझाया हैं। इन साधनों का उपयोग करके साधक के क्लेशों का नाश होता है। चित्त प्रसन्न होकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है और विवेक ख्याति प्राप्त होती है। महर्षि पतंजलि ने राजयोग के अन्तर्गत अष्टांग को इस प्रकार बताया है-
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान
समाधयोऽष्टावंगानि।। (योगदर्शन पा0 2 सूत्र 9)
योग के आठ अंगों में प्रथम पांच बहिरंग तथा अन्य तीन अन्तरंग में आते है। उपर्युक्त चार प्रकार के अतिरिक्त गीता में दो प्रकार के योगों का भी वर्णन मिलता है।
1) ज्ञान योग
2) कर्मयोग
ज्ञानयोग, सांख्ययोग से सम्बंध रखता हैं। पुरुष प्रकृति के बन्धनों से मुक्त होना ही ज्ञानयोग है। सांख्य दर्शन में 25 तत्त्वों का वर्णन मिलता है।
पुराणों में योग
पौराणिक परम्पराओं के अनुसार भगवान् शिव को योग का संस्थापक आदियोगी कहा जाता है और पार्वती माता को योग की पहली शिष्या। इसके माध्यम से ऋषि-मुनि सत्य एवं तप के अनुष्ठानसे ब्रह्माण्ड के अनेक रहस्यों से साक्षात्कार करते आए हैं। आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार योग करने से व्यक्ति की चेतना, ब्रह्माण्ड की चेतना से जुड़ जाती है। इसके असर से मन एवं शरीर और मानव एवं प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य की अनुभूति होने लगती हैं। इस चिंतन सोच एवं कर्म के बीच एकीकरण एवं तालमेल स्थापित करता है। सदियों से योग की कई शाखाएं विकसित हुई है, लेकिन इस बात पर आम सहमति है कि इसका विकास पूर्ण रूप से भारत में मानव सभ्यता के शुरू में पूर्व वैदिक काल में हुआ है।
सिन्धु-सभ्यता में योग
वेदों और पुराणों में हमने योग और आसनों पर विस्तार से बात की, लेकिन यहाँ पर यह समझाना अत्यन्त आवश्यक है कि हड़प्पा और मोहन जोदड़ों में इनके साक्ष्य अति-विकसित सभ्यताओं में भी मौजूद रहे है। इन सभ्यताओं में कई ऐसी मुहरे पाई गई है, साथ ही इसी प्रकार से मिलती-जुलती कई चीजें मिली है। जो साक्ष्य के तौर पर यह सब अपने अंदर समाये हुए है। इन सभी चीजों से प्रमाणित होता है कि भारतीय संस्कृति कितनी विकसित और उन्नत रही है। उस काल के मुहरों पर योग की विभिन्न तरह की मुद्राओं का उभार नज़र आता है। जिसको देखकर कहा जा सकता है कि ये आसन और प्राणायाम की मुद्राएं है्र। सिन्धु-सभ्यता से मिलें इन सिक्कों को भगवान् पशुपति की आकृति बताते है, जो योग मुद्रा में विराजमान है, कुल मिलाकर यह सभी चिन्ह हमारी प्राचीन विद्या योग की उन्नत और व्यापक संस्कृति की पुष्टि करता है।
विभिन्न काल खण्डो में योग को जीवित रखने का श्रेय कुछ ही महान् विभूतियों को जाता हैं। जिनमें से तिरुमिलाई कृष्णमाचार्य को महान् योग गुरु माना जाता है। उन्होंने विन्यास योग शैली का इस्तेमाल किया और हठयोग का पुन:उद्धार किया, उन्हे योग व आयुर्वेद दोनों की अच्छी जानकारी थी। तिरुमिलाई को योग के माध्यम से रोगी के दिल की धडक़न पर नियंत्रण की महारत हासिल थी। कृष्णमाचार्य का जन्म कर्नाटक के चित्रदुर्ग में 18 नवम्बर 1888 को हुआ थ। कृष्णमाचार्य के पिता वेद-उपनिषद् के शिक्षक थे। कृष्णमाचार्य ने हिमालय की गुफाओं में रहने वाले योगाचार्य राममोहन ब्रह्मचारी से पतंजलि योगसूत्र की बारीकियां सीखी थी।
कृष्णमाचार्य जी के साथ-साथ एक बड़ा दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है। उस समय हिमालय की गुफाओं में जाने के लिए व हिमालय पर रहने के लिए वॉयसराय स्तर के अधिकारी की परमिशन का होना आवश्यक होता था। उस समय कृष्णमाचार्य जी ने उस वक्त शिमला के वॉयसराय रहें लार्ड इरविन से हिमालय में जाने की परमिशन ली थी। तब कहीं जाकर कृष्णमाचार्य जी हिमालय की गुफाओं मे योग विद्या को ग्रहण कर पाये थे।
एक बार लार्ड इरविन बीमार पड़ गये तब कृष्णमाचार्य ने योग थेरेपी के माध्यम से उनका उपचार किया था। इसके बाद से इरविन उनके मुरीद हो गये थे। कहा जाता है कि बाद में वह चेन्नई के विवेकानन्द कॉलेज में लेक्चरार की पोस्ट ऑफर की गई थी। 28 फरवरी 1989 को चेन्नई में उन्होंने 101 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली थी।
स्वामी शिवानंद सरस्वती
स्वामी शिवानंद सरस्वती जी पेशे से एक डाक्टर थे, उन्होंने एक योगी की 18 खासियतों के बारे में वर्णन किया हुआ है। उनके मुताबिक एक योगी का मजाकिया स्वभाव का होना अत्यन्त आवश्यक है। हठयोग, कर्मयोग और मास्टर योग को मिलाकर उन्होंने त्रिमूर्ति योग का सूत्र तैयार किया था। स्वामी शिवानंद सरस्वती का योग, वेदांत और कई अन्य विषयों से काफी लगाव था। जिन पर उन्होने कर्म और भक्ति के साथ योग का भी पूरी दुनियां में प्रचार-प्रसार किया है।
स्वामी शिवानंद सरस्वती का जन्म 8 सितम्बर 1887 को हुआ था। उनका बचपन से ही वेदांत की अध्ययन का अभ्यास करने लगे थे। उसके बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया तत्पश्चात् उन्होंने मलेशिया में जाकर डाक्टर के रूप में अपनी सेवा दी। सन् 1924 में चिकित्सा सेवा से मन उठने के कारण वह ध्यान व अध्यात्मिक साधना के लिए ऋषिकेश को अपना स्थान बनाया।
स्वामी शिवानंद सरस्वती यौगिक साधनाओं की बदौलत चमत्कार दिखाने के विरुद्ध थे, पर पीडि़त मानवता की सेवा करने और अपने शिष्यों को आध्यात्मिक मार्ग पर बनाएं रखने के लिए कई बार ऐसा काम कर देते थे, जिन्हें आम आदमी चमत्कार मान बैठता था।
स्वामी औंकारानंद जी ने अपनी पुस्तकों में शिवानंद सरस्वती जी से जुड़ी ऐसी कई घटनाओं को वर्णन किया हुआ हैं। वह लिखते है एक बार दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहर के अस्पताल में उनका एक शिष्य गंभीर बीमारी से पीडि़त था। उसकी हालत खराब थी। दूसरी तरफ कुआलालमपुर में ऐसी ही स्थिति में एक अन्य शिष्य था। इन दोनों शिष्यों द्वारा बतलायें गए समय और तिथि के मुताबिक स्वामी शिवानंद ने एक ही समय में दोनों को दर्शन दिये थे और दोनों ही स्वस्थ होकर घर लौट आये थे। जिस दौरान यह घटनायें जन्म ले रही थी तब स्वामी औंकारनंद, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी की छत्र-छाया के साधनरत् थे। सन् 14 जुलाई 1963 को स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने महासमाधि ले ली थी।
परमहंस योगानंद
पश्चिम जगत को योग से रू-ब-रू करवाने का श्रेय परमहंस योगानंद को जाता है। क्रिया योग का विज्ञान योगानंद जी की शिक्षा का मूल है। 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर (उत्तरप्रदेश) में हुआ था। परमहंस योगानंद जी को बीसवीं सदी के एक आध्यात्मिक गुरु, योगी और संत के रूप में देखा जाता है। परमहंस जी मानते है कि योग क्रिया ईश्वर से साक्षात्कार की एक प्रभावी विधि व विद्या हैं। जिसके पालन से आप अपने जीवन को संवार सकते है और ईश्वर की ओर अग्रसर हो सकते है। पश्चिम देशों में योग की अलख जगाने वाले परमहंस प्रथम योगी थे। जिन्होंने पश्चिम देशों में अपना स्थायी निवास बनाया। योगानंद जी का नाम मुकुन्दा लाल घोष था। वह एक धनी बंगाली परिवार में जन्मे थे। बचपन से ही उनका स्वभाव आध्यात्मिकता की ओर था। उनका मनपंसद कार्य संतों से मिलना, आध्यात्मिकता को तलाशना और उनकी यही चाहत उन्हे उनके गुरु से रामपुर के स्वामी श्री मुक्तेश्वर जी तक लें गयी। अपने गुरु के अन्तर्गत प्रशिक्षण की बदौलत मात्र 6 महीनों में समाधी अर्थात् ईश्वर के साथ अप्रतिबांधित एकता को प्राप्त करने का हुनर सीख लिया था।
योगानंद जी के साथ भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है। एक दोपहर वह विद्यालय में ध्यान करते हुए उन्हें दिव्य दृष्टि से बुलावा महसूस हुआ कि उनके गुरु द्वारा यह कहा गया कि योग की पवित्र शिक्षाओं को अब भारत के साथ-साथ पश्चिमी देशों में ले जाने का समय आ गया है। वह तुरन्त बॉस्टन के लिये निकल गये थे और पश्चिमी देशों में योग की पताका को फहराया।
पूज्य स्वामी जी के योग युग का शंखनाद
आज 21वीं सदी में योग की बात परम पूज्य स्वामी जी महाराज के बिना अधूरी हैं। आजादी के बाद योग, आयुर्वेद की जिस प्रकार से उपेक्षा हुई, वह जग जाहिर है। परम पूज्य स्वामी जी ने योग को घर-घर तक पहुँचाने में व योग को पुन: जीवित करने के लिए उच्च स्तर पर जाकर कार्य किया। आज विश्व पटल पर योग को लेकर जो भी जागरुकता आयी है, उसके पीछे परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बड़ा योगदान हैं।
वर्तमान काल खण्ड में विश्व जो योग दिवस का आयोजन करता है, उसके पीछे योगऋषि स्वामी जी का कठोर तप व पुरुषार्थ हैं। जिस कारण विश्व 21जून 2015 को योग दिवस मनाने के लिए प्रेरित हो गया। 21 जून यही वह दिन है जब सारी दुनियां योग के ज्ञान को आत्मसात् करने का मौका मिला। जिसके लिए योग व भारतीय संस्कृति से प्रेम करने वाले सदियों से लालायित थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आग्रह पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल पर इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पहचान मिली। हजारों-हजार साल की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसका डंका एक साथ विश्व के 192 देशों में बज उठा। भारत को इस प्राचीन विरासता ने एक बार फिर हिन्दूस्तान का मस्तक गौरव से ऊँचा कर दिया। आज़ादी के बाद से योग व उससे जुड़ी सभी विद्या सिमटने की कगार पर खड़े थी। आसन, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद जैसी पवित्र ज्ञान को नष्ट करने का काम सुनियोजित रूप से किया जा रहा था, धीरे-धीरे मनुष्य जाति अपनी प्राचीन संस्कृति से दूर जा रही थी। तभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग के आसनों को, प्रणायाम को, आसनों के तरीकों से विश्व समुदाय के बीच रखा। योगऋषि स्वामी जी द्वारा बताये गये तरीकों से योग करने व उनसे दूर होने वाली बीमारियों को मनुष्य समझ चुका था। साथ ही सम्पूर्ण विश्व समुदाय योग क्रियाओं के करने से अपने तन-मन को भी पवित्र कर रहा था। जिस भी व्यक्ति ने इस अद्भूत क्षणों को अपने जीवन में जगह दी, उसका मानों सारा जीवन सहज हो गया। आज सारी दुनियां भारतीय संस्कृति के इस ज्ञान को पाकर गौरवमय महसूस कर रही हैं। इस सुखद आभास को जीने वाला हर मानव शरीर, हृदय से परम पूज्य स्वामी जी महाराज को कोटि-कोटि नमन कर रहा हैं।
आज यह तो देश के प्रधानमंत्री जी भी मानते है कि योग, आयुर्वेद, प्राणायाम, अनुलोम-विलोम जिस प्रकार घर-घर किया जा रहा है उसके पीछे योगऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का कठिन तप समाहित है। लोग पुन: योग की ओर आकृषित हुए समय निकालकर योग प्राणायाम करके अपने को व मानव जाति को स्वस्थ रखने की राह दिखा रहें हैं। इसके पीछे स्वामी जी महाराज द्वारा कठिन योग आसनों को सहजता से करने का अभ्यास करवाना, साथ ही मानव शरीर मे होने वाली व्याधियों को किस प्रकार के आसनों से दूर किया जा सकता है। उस ज्ञान को नि:स्वार्थ भाव से मानव समाज के बीच रख साथ ही सम्पूर्ण मानव देह को स्वस्थ रखने का संकल्प भी लिया।
योग की राह
आज परम पूज्य स्वामी जी योग व आयुर्वेद के पर्याय माने जाते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज का जन्म 26 दिसम्बर 1965 को महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) में हुआ था। स्वामी जी का बचपन का नाम रामकृष्ण था। स्वामी जी महाराज ने अपने गुरुकुलम् के कठिन नियमों के बीच विद्या को ग्रहण किया। बाद में श्री आचार्य प्रद्युम्मन व योगाचार्य श्री बलदेव जी से पूज्य स्वामी जी प्राचीन वेदों की व पवित्र योग विद्या की शिक्षा ली। यही वह समय था जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपनी युवावस्था में संन्यास लेने का संकल्प कर लिया था। योगऋषि स्वामी जी महाराज ने कहा है कि जब मैं 9 वर्ष का था तब उनके मन में ऐसा विचार आया कि उन्हें भारतीय संस्कृति को पुन: स्थापित करना है, ऐसा उनके जीवन में पुर्नजन्म के संस्कारों के कारण हुआ। जिस कारण वह योग की राह पर आगे चल पड़े।
वह उदाहरण देकर बताते है कि यह विज्ञान का युग है सब लोग वैज्ञानिक तथ्यों को स्वीकार करते है इसलिए विज्ञान का भी सिद्धान्त है कि कभी कोई चीज समाप्त नहीं होती, परिवर्तित जरुर हो जाती है, इसलिए पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण मैं संन्यासी बन गया। 9 अप्रैल 1995 को रामनवमी वाले दिन मैंने संन्यास की दीक्षा ले ली।
पूज्य स्वामी जी गुरुकुल की यादों को याद करते हुए कहते है कि गुरुकुल में हम योगाभ्यास और व्यायाम तो बहुत करा करते थे, मगर हमेशा से कुछ अलग करने में ध्यान लगा रहता था। तब हमें बिजनौर के एक संत महात्मा ने मुझे पहली बार कपालभाति, अनुलोम-विलोम करना सिखाया। उस दिन के बाद से मैंने कपालभाति एवं अनुलोम-विलोम पर कई वर्षों तक अभ्यास किया फिर लोगों पर कपालभाति और अनुलोम-विलोम के माध्यम से रोगियों के रोग दूर किये। जब इस क्रिया से लोगों की व्याधि दूर होने लगी तो मुझे पहली बार आशा की किरण दिखाई दी और बस हम यहीं से व्याधि से समाधि की ओर लौटे।
योगऋाषि स्वामी जी महाराज ध्यान व समाधि लगाने के लिए हिमालय की गुफाओं की ओर चल दिये जहाँ पर वर्षों तक पूज्य स्वामी जी महाराज ने ध्यान धारण कर कठोर तप किया, वहाँ से कई प्रकार की सिद्धियों को अपने अन्दर धारण करने के उपरान्त वह योग सेवा को विस्तार देने के लिए हरिद्वार कृपालु बाग आश्रम में रहने लगे, यही वह पुण्य स्थान है जहाँ से पूज्य स्वामी जी महाराज के जीवन ने निर्णायक मोड़ का सफर प्रारम्भ किया। इसी स्थान से पूज्य स्वामी जी विश्व योग गुरु के रूप में अपनी पहचान को स्थापित कर पाये।
परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि विश्व योग गुरु बनने का सफर इतना आसान नहीं था। वह बताते है उन्होंने पहला योग शिविर गुजरात के सूरत में लगाया था जहाँ योग सिखने वालों की संख्या उतनी नहीं थी मगर धीरे-२ कई जगह पर योग शिविरों का आयोजन किया जिसमें जनता की संख्या लाखों में शामिल होने लगी। इस जनता में आम और खास दोनों तरह के लोगों ने हिस्सा लिया। योगऋषि स्वामी जी के साथ लाखों लोग योग, आसन, प्राणायाम व अनुलोम-विलोम, कपालभाति करते थे, जिससे हजारों की संख्या में लोग रोगमुक्त होने लगे। मोटे लोगों का वजन कम होने लगा, यह वह समय था जब पूज्य स्वामी जी भारतीय संस्कृति के योग को नया मुकाम दे रहे थे। हर घर में स्वामी जी के योग को टी.वी. पर देखकर योग अभ्यास कर रहे थे, कठिन परिश्रम, कठोर पुरुषार्थ से पूज्य स्वामी जी ने योग को भारत ही नहीं विश्व के सभी देशों में अपने योग शिविरों के माध्यम से इस प्राचीन धरोहर को सबके साथ साझा किया। साथ ही सरल भाषा में योग के महत्त्व को समझाया भी है।
पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग का परचम तो फहराया ही, साथ ही ऋषियों-मुनियों की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को जिसे ऐलोपैथिक दवाई माफियाओं ने आम जन-मानस के जेहन से उतार दिया था। उसी ऋषि परम्परा व प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को पुन: स्थापित करने का श्रेय यदि किसी का जाता है तो वह परम पूज्य स्वामी जी महाराज ही हैं। जिन्हें बहुर्राष्ट्रीय कम्पनी वाले चूर्ण बेचने वाला तक बोलते थे। ऐसे तिरस्कारों के बीच आयुर्वेद की विद्या को घर-घर तक ले जाने के संकल्प के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज आगे बढ़ते चले गये।
योगऋषि स्वामी जी ने अपने योग शिविर के माध्यमों से यह साबित कर दिया था कि ऐलोपैथिक दवाई किसी रोग को कुछ समय के लिए रोक तो सकती है, मगर कभी उस रोग को खत्म नहीं कर सकती। आयुर्वेद ही वह पद्धति जिससे रोगमुक्त हुआ जा सकता है प्राकृतिक जड़ी-बूटियों से बनी दवाईयों के सेवन से न तो किसी प्रकार का कोई साईड इफेक्ट होता है और जिस रोग के लिए आप जो दवाई खा रहे है वह आप को रोगमुक्त भी कर देगी।
आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का उल्लेख आदिकाल से होता चला आ रहा है। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी, तब प्रभु राम भी स्वयं आयुर्वेद की शरण में आये थे, तब सुषेण वैद्य जी ने श्री हनुमान जी को संजीवनी लाने को भेजा था। उसी संजीवनी के सेवन से लक्ष्मण जी के प्राण को बचाया जा सका।
प्रभु श्रीराम जी के काल से परम पूज्य रामदेव जी के काल तक आयुर्वेद ही संजीवनी का कार्य कर रही हैं।
विश्वव्यापी महामारी कोरोना की बहुप्रतिष्ठित दवा बनाने की चुनौतिपूर्ण कार्य को सर्वप्रथम पतंजलि ने पूर्ण किया, अर्थात् आयुर्वेद पद्धति ने।
परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने कहा कि आयुर्वेद पर आधारित पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अथक पुरुषार्थ करके पहले क्लीनिकल बेस स्टडी तथा बाद में कंट्रोल्ड क्लीनिकल ट्रायल करके, औषधि अनुसंधान के सभी प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए कोरोना के सम्पूर्ण मैनेजमेंट के लिए सफल औषधि ‘कोरोनिल’ तथा ‘श्वासारि वटी’ की खोज की हैं। उन्होंने कहा कि जिस कोरोना की औषधि पूरा विश्व खोज रहा है वह हमारे आस-पास मौजूद आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों में अकूत मात्रा में पाया जाता है, अंतर केवल इसके ज्ञान का है। आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा निर्मित इस दवाई ने आज हजारों नहीं लाखों मरीजों को काल का ग्रास बनने से बचाया है, साथ में रोगी के शरीर में अन्य कोई व्याधि उत्पन्न किये बगैर।
कोरोना की दूसरी लहर में एलोपैथिक डॉक्टरों ने योग की महत्ता को खुद समझा एम्स के जाने माने डॉक्टरों ने जब मरीजों का ऑक्सीजन लेबल कम होता देखा तो प्राणायाम करवाकर उनके ऑक्सीजन स्तर को स्थिर किया।
जिस योग व आयुर्वेद से दूरी बनाकर रखने वाले एलोपैथिक के डॉक्टर आखिर में योग व आयुर्वेद की शरण में आकर नतमस्तक हुए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमेशा से कहते चले आये हैं कि लम्बी-लम्बी श्वास लेने से कभी भी ऑक्सीजन लेबल नहीं कम होगा। भांप लेने से कोरोना वायरस नाक में ही नष्ट हो जायेगा। आखिर में इस पद्धति को अंग्रेजी दवाईयों के डॉक्टर भी अपने मरीजों पर इस क्रिया को अपनाने लगे। योगऋषि स्वामी जी महाराज ने कोरोना के पहले दिन से रोगी की इम्यूनिटी बढ़ाने पर बल दिया जिसे बाद में एलोपैथिक चिकित्सकों ने भी स्वीकार्यता दी। अन्त में परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते है कि यदि योग से मानव अपने शरीर को मजबूत करके रखेगा तो उसे किसी प्रकर की बीमारी का खतरा नहीं रह जाता। यही सभी बातें महर्षि चरक ने आपने ज्ञानकोश में भी लिखी हैं। इस महामारी ने मानव सभ्यता को यह एहसास करवा दिया कि चाहे कैसी भी बीमारी क्यूं न हो। उसका ईलाज योग और हमारी प्रकृति में है। बस बात इतनी सी ही है, उसे समझता और स्वीकार कौन करता है।
इसी सदी के विश्व गुरु परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज अपने संकल्प को दोहराते हुए कहते है कि वह अपनी आखिरी सांस तक योग की महिमा, वेदों-ऋषियों की महिमा गायेंगे, साथ ही देश को स्वदेशी की राह पर लेकर जायेंगे। वह योग और आयुर्वेद से रोगियों का उपचार करेंगे और भारत को पुन: विश्व गुरु बनायेंगे।
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Nov 2024 17:59:04
जीवन सूत्र (1) जीवन का निचोड़/निष्कर्ष- जब भी बड़ों के पास बैठते हैं तो जीवन के सार तत्त्व की बात...