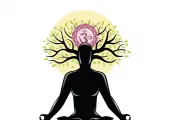महाराज शांतनु और भीष्म के धर्मपूर्ण शासन का पुण्यप्रताप
On

प्रो. कुसुमलता केडिय़ा
महाभारत में महाराज शान्तनु और देवव्रत भीष्म के धर्मपूर्ण शासन का गौरवशाली वर्णन है। जो कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देता है। सम्राट शान्तनु के सदाचार, शील और ज्ञान तथा वीरता के कारण पृथ्वी के सब राजाओं ने मिलकर उन्हें राजराजेश्वर के पद पर अभिषिक्त किया-
वर्तमानं हि धर्मेषु सर्वधर्मभृतां वरम्।
तं महीपा महीपालं राजराज्येऽभ्यषेचयन्।।
(आदिपर्व, अध्याय 100, श्लोक 7)
शान्तनुप्रमुखैर्गुप्ते लोके नृपतिभिस्तदा।
नियमात् सर्ववर्णानां धार्मोत्तरमवर्तत।। (श्लोक 10)
स हास्तिनपुरे रम्ये कुरूणां पुटभेदने।
वसन् सागरपर्यन्तामन्वशासद् वसुन्धराम्।। (श्लोक 12)
स देवराजसदृशो धर्मज्ञ: सत्यवागृजु:।
दानधर्मतपोयोगाच्छ्रिया परमया युत:।। (श्लोक 13)
(सभी राजाओं द्वारा राजराजेश्वर के पद पर अभिषिक्त सम्राट शान्तनु के अधीन सभी राजाओं द्वारा सुरक्षित जगत में सभी वर्णों के लोग नियमपूर्वक धर्ममय आचरण करते रहे। महाराज शान्तनु हस्तिनापुर को राजधानी बनाकर समुद्र पर्यन्त समस्त पृथ्वी का अपने अधीनस्थ राजाओं के साथ शासन और पालन करते रहे। वे देवराज इन्द्र के सदृश पराक्रमी, धर्मज्ञ, सत्यवादी और सरल थे तथा दान, धर्म और तपस्या इन तीनों के योग से वे परम ऐश्वर्यसम्पन्न हुये।)
इस विवरण में भारत की चक्रवर्ती सम्राट परंपरा का महत्वपूर्ण सूत्र व्याप्त होता है। यहां चक्रवर्ती सम्राट कोई यूरोपीय लोगों जैसा उपनिवेशवादी या एकाधिकारवादी शासक नहीं है। अपनी प्रभुता और श्रेष्ठता के कारण वे सर्वसमादृत हैं और उनकी सर्वोच्चता को सभी राजा मान देते हैं। शेष अपने-अपने क्षेत्र में प्रत्येक राजा संपूर्ण स्वतंत्र है और वे राजधर्म के अनुसार शासन का संचालन करते रहते हैं। राजाओं और सम्राटों को न तो राज्य संचालन के मनमाने नियम बनाने का अधिकार है और न ही प्रजा के कल्याण के विषय में कोई मनमानी कल्पना करने का अधिकार है तथा न ही न्याय के आधारों में अपनी कोई मान्यता घुसेडऩे का अधिकार है। परंपरा से धर्मशास्त्रों में वर्णित विभिन्न कुलसमूहों, जातियों, वर्णों, गणों और श्रेणियों के विषय में जो परंपरायें और लोकाचार तथा लोकव्यवहार प्रतिष्ठित हैं, जिनके आधार पर अधिकांश व्यवहार संबंधी वाद पंचायतों, खापों और श्रेणिपरिषदों तथा शिष्ट परिषदों के स्तर पर सुलझा लिये जाते हैं, उन्हीं आधारों पर उन वादों के विषय में प्रकरण अपने सामने आने की स्थिति में धर्मज्ञ विद्वानों की सम्मति से सम्राट न्यायिक निर्णय करते हैं। व्यवहार और वाद निर्णय की यह पद्धति और प्रक्रिया शास्त्रों में इतने विस्तार से वर्णित है, जितनी उस समय के विश्व के किसी भी अन्य समाज या सभ्यता के पास उपलब्ध नहीं है। वस्तुत: न्यायिक निर्णयों की भारतीय प्रक्रिया का ही अनुसरण 19वीं शताब्दी ईस्वी में सर्वप्रथम इंग्लैंड में तथा बाद में यूरोप के अन्य देशों में अपनी परंपरा के अनुसार थोड़े हेर-फेर के साथ अपनाया गया, इसके प्रचुर प्रमाण हैं। इस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट आधुनिक पदावली में अत्यंत उदार और लोकतांत्रिक प्रधान ही कहे जा सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक स्तर पर राजाओं और सम्राटों को राजधर्म का ही पालन करना होता था और राजधर्म धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित था। अपनी ओर से कोई मनमाना कानून बनाने का अधिकार भारत में राजाओं और महाराजाओं को कभी भी नहीं था। ऐसा लगता है कि इस विराट अनुशासन से घबरा कर ही 19वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में कई भारतीय हिन्दू राजाओं ने अंग्रेजों का अनुसरण करने का निर्णय किया। क्योंकि उसमें उन्हें मनमानी की भरपूर गुंजाइश दिखी और निरंकुश प्रभुत्व की लालसा ने उन्हें स्वधर्म से विचलित कर दिया। अस्तु ;
भगवती गंगा के जाने के बाद 36 वर्षों तक सम्राट शान्तनु अकेले ही रहे और शासन का संचालन करते रहे। एक दिन वे किसी हिंसक पशु का पीछा करते हुये गंगा तट पहुंचे तो देखा वहां एक युवक दिव्य अस्त्र-शस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और अपने बाणों से समूची गंगा जी की धारा को रोककर खड़ा है। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और वे उसके पास पहुंचे। वहाँ उन्होंने गंगाजी का ध्यान किया। तब भगवती गंगा प्रगट हुईं और उन्होंने बताया कि यह वही आठवां पुत्र है जिसे आपने मुझसे प्राप्त किया था। मैंने इसका पोषण किया है। अब आप इस पुत्र को ग्रहण कीजिये और घर ले जाइये। यह महान धनुर्धर है और शुक्रनीति का भी विशारद है तथा बृहस्पति शास्त्र का भी ज्ञाता है। इसने वेद-वेदांग सबका अध्ययन किया है और राजधर्म तथा अर्थशास्त्र का भी महान पंडित है।
सम्राट शान्तनु पुत्र को राजधानी ले गये और वहां उसे युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। युवराज देवव्रत का शासन इतना श्रेष्ठ तथा धर्ममय था कि उसके कारण कुरूदेश की सर्वांगीण उन्नति हुई। महाभारत में कहा है-
ऊधर्वसस्याभवद् भूमि: सस्यानि रसवन्ति च।
यथर्तुवर्षी पर्जन्यो बहुपुप्फला द्रुमा:।।
वाहनानि प्रहृष्टानि मुदिता मृगपक्षिण:।
गन्धवन्ति च माल्यानि रसवन्ति $फलानि च।।
वाणिग्भिश्चान्वकीर्यन्त नगराण्यथ शिल्पिभि:।
शूराश्च कृतविद्याश्च सन्तश्च सुखिनोऽभवन्।।
नाभवन् दस्यव: केचिन्नाधर्मरूचयो जना:।
प्रदेशेष्वपि राष्ट्राणां कृतं युगमवर्तत।।
(महाभारत, आदिपर्व, अध्याय 108, श्लोक 2 से 5)
(युवराज देवव्रत के शासन से पृथ्वी पर खेती की उपज बहुत बढ़ गई और सभी अन्न सरस होने लगे। वर्षा समय पर होती थी और वृक्षों में पुष्पों और फलों की बहुलता हो गई। घोड़े, हाथी आदि वाहन हष्ट-पुष्ट रखे जाते थे और मृग तथा पक्षी चारों ओर आनंद से विहार करते थे। पुष्पों और पुष्पमालाओं में अनुपम सुगंध होती और फलों का रस भी विशिष्ट होता। व्यापार कुशल वैश्य और शिल्पकला में निपुण शिल्पी सभी नगरों में भरे रहते थे। विद्वान, शूरवीर और संत सुखपूर्वक स्वधर्म पालन करते थे। कोई भी मनुष्य किसी अन्य का धान छीनने की इच्छा भी नहीं करता था और पाप में किसी की रूचि नहीं देखी जाती थी। राष्ट्र के सभी प्रातों में सत्य युग छा गया था।)
महाभारत में ऐसे वर्णन बारम्बार आये हैं। जिनमें कहा गया है कि धर्मनिष्ठ और वीर तथा सदाचारी शासक के शासन में सत्य युग छा जाता है, भले ही उसी समय पृथ्वी के अन्य भागों में द्वापर या कोई अन्य युग हो। इस प्रकार राजा को ही काल का कारण कहा गया है। इसीलिये युवराज देवव्रत के सुशासन से उनके सम्पूर्ण राज्य में सत्य युग छा गया।
36 वर्षों तक एकान्त और संयमित जीवन जीने के बाद सहसा एक दिन शान्तनु जब नदी तट पर घूम रहे थे तो वहां उन्हें एक अवर्णनीय सुगंधा का अनुभव हुआ। जब उन्होंने आगे बढक़र उस सुगंध के स्रोत को जानना चाहा तो मल्लाहों की एक परमसुन्दरी कन्या दिखी। जो नाव चला रही थी। सम्राट के पूछने पर उसने बताया कि मैं केवल धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। राजा ने कन्या के पिता से उस कन्या को मांगा। पिता ने कहा कि इस कन्या का विवाह उसी राजा से करने की मेरी प्रतिज्ञा है जो इसके पुत्र को ही राजपद देने की प्रतिज्ञा करे। क्योंकि यह कन्या मेरी नहीं अपितु एक श्रेष्ठ आर्य की सन्तान है और हमने इसके लिये राज्यशुल्क निर्धारित किया है।
सम्राट शान्तनु यह सुनते ही वापस चले गये क्योंकि उन्हें तत्काल अपने परम प्रिय पुत्र देवव्रत का ध्यान आया। परन्तु राजभवन में जाकर भी राजा उस परमसुन्दरी युवती को कभी भुला नहीं पाये और इसका उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पडऩे लगा। तब सुयोग्य युवराज ने महाराज के सारथी से यह पता किया और तब वे सत्यवती के पिता से मिलने पहुंचे जिन्होंने वही बात दुहराई। देवव्रत ने राजपद त्यागने की घोषणा की तब भी वह मल्लाह संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कहा कि आपके पुत्र भविष्य में मेरी पुत्री के पुत्रों का राज्य छीन सकते हैं। इस पर परम पितृभक्त देवव्रत ने वह प्रतिज्ञा की जिसे भीषम प्रतिज्ञा कहा जाता है। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की घोषणा की। इसी प्रतिज्ञा के कारण वे भीष्म कहलाये। उन्होंने आग्रहपूर्वक सत्यवती का विवाह शान्तनु से कर दिया। सत्यवती से शान्तनु के दो पुत्र पैदा हुये चित्रंगद और विचित्रवीर्य। कुछ समय बाद सम्राट शान्तनु का निधन हो गया और फिर एक गन्धर्व से युद्ध में चित्रंगद भी मारे गये तब विचित्रवीर्य को राज्य पद पर अभिषिक्त किया गया।
महाबली भीष्म ने काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर स्थल से हरण किया और अम्बिका तथा अम्बालिका के साथ विचित्रवीर्य का विवाह किया। परन्तु विचित्रवीर्य का निधन हो जाने से माता सत्यवती की आज्ञा से (उनसे कुमारी अवस्था में ऋषि पाराशर से उत्पन्न पुत्र) व्यास जी ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर इन तीन पुत्रों को क्रमश: अम्बिका और अम्बालिका से तथा तीसरे पुत्र को अम्बिका की दासी से जन्म दिया। यह कथा विश्व प्रसिद्ध है।
यहाँ विदुर की कथा का स्मरण आवश्यक है। क्योंकि महात्मा माण्डव्य के शाप से साक्षात धर्मराज ही विदुर रूप में उत्पन्न हुये थे। वे जन्म से ही काम और क्रोध से रहित थे तथा अर्थतत्व के ज्ञाता थे। महाभारत में आदिपर्व में अध्याय 105 का 29वां श्लोक है-
धर्मो विदुररूपेण शापात् तस्य महात्मन:।
माण्डव्यस्यार्थतत्त्वज्ञ: कामक्रोधविवर्जित:।।
106वें एवं 107वें अध्याय में माण्डव्य की कथा है। माण्डव्य एक विख्यात धर्मज्ञ ब्राह्मण थे। वे सत्यनिष्ठ तथा तपस्वी थे। वे आश्रम के द्वार पर एक वृक्ष के नीचे मौन व्रत धारण कर बहुत बड़ी तपस्या कर रहे थे। एक दिन उनके आश्रम में चोरों ने पीछा कर रहे सैनिकों से डर कर चोरी का माल छिपा दिया। सैनिकों ने आकर पूछा परन्तु मौन तपस्वी चुप रहे। अंत में चोरी का माल और चोर दोनों ही आश्रम में छिपे मिल गये। तब सैनिकों ने जाकर चोरी का माल और चोरों को राजसभा में उपस्थित करते हुये उस आश्रम की बात भी बताई। इस पर राजा ने ऋषि माण्डव्य को भी शूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। रक्षकों ने माण्डव्य मुनि को शूली पर चढ़ा तो दिया परंतु योगबल के कारण मुनि के प्राण नहीं गये। जब कई दिनों तक वे शूली पर ही बैठे रहे तो रक्षकों ने जाकर यह आश्चर्यजनक बात राजा को बताई। इस पर राजा ने आकर क्षमा मांगी और उन्हें शूली से उतारा तथा सत्कार किया। मुनि ने समाधि में जाकर धर्मराज से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे यह दण्ड मिला। जब धर्मराज ने बताया कि आपने बाल्यावस्था में फतिंगों के पुच्छभाग में सींक घुसेड़ दी थी। उसी कर्म का यह फल आपको मिला है। तब माण्डव्य मुनि ने सर्वप्रथम तो यह स्मरण दिलाया कि धर्मशास्त्रों के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की अवस्था तक बालक जो कुछ करेगा, उसमें उसे अधर्म नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने धर्मराज को शाप दिया कि आपने बहुत थोड़े से अपराध के लिये मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है। इसलिये मेरा शाप है कि आप शूद्र योनि में मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे। माण्डव्य ऋषि के उसी शाप से धर्मराज दासी के गर्भ से विदुर रूप में उत्पन्न हुये।

108वें अध्याय में बताया गया है कि भीष्म के धर्मपूर्ण शासन से कुरू देश की सर्वांगीण उन्नति हुई अैर राष्ट्र के सभी प्रदेशों में सतयुग छा गया। भीष्म ने धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुर तीनों ही भाइयों का पुत्र की भांति पालन किया और सभी संस्कार कराये तथा वेदों की शिक्षा के साथ ही धनुर्वेद, अश्वविद्या, गदायुद्ध, ढाल-तलवार के युद्ध, गज विद्या और नीतिशास्त्र में सबको निपुण बनाया। साथ ही इतिहास और पुराण का ज्ञान कराया और विविध प्रकार के शिष्टाचारों का भी ज्ञान कराया।
इसके उपरांत महावीर भीष्म जी ने सर्वप्रथम धृतराष्ट्र का विवाह गांधार नरेश सुबल की कन्या गांधारी से कराया और फिर यदुवंशी शूरसेन की कन्या प्रथा का विवाह पाण्डु से कराया तदुपरान्त मद्र नरेश की कन्या से पाण्डु का दूसरा विवाह कराया। इसकी रोचक चर्चा अगले लेख में।
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Nov 2024 17:59:04
जीवन सूत्र (1) जीवन का निचोड़/निष्कर्ष- जब भी बड़ों के पास बैठते हैं तो जीवन के सार तत्त्व की बात...



.jpg)





.jpg)