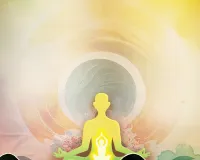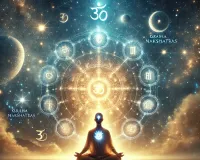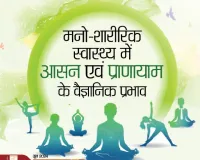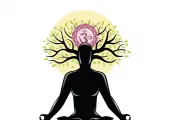कुटिलता का त्याग
On

श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज
वेदवाणी
ऋषि-परमेष्ठी प्रजापति:। देवता- यज्ञ।
छन्द:- स्वराडार्षी त्रिष्टुप्।
वसो: पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो घर्मोसि विश्वधा असि। परमेण धाम्ना दृ ँ्हस्व मा ह्वार्मा ते यज्ञपतिह्र्वार्षीत् ।। यजु. 1.2 ।।
दों में कहा है कि श्रेष्ठतम कर्म ही यज्ञ है। वह यज्ञ कैसा होता है, उसका स्वरूप बताने के लिए यह मन्त्र है। 'यज्ञो वै वसु:’ (श0- 1.7.1.9.14) इस वचन से 'वसु’ यह शब्द 'यज्ञ’ इस अर्थ का वाचक है। वासयतीति वसु:, अथवा वसन्त्यस्मिन्निति वसु: या वस्यत आच्छाद्यतेऽनेनेति वसु:। 'बसाना’ अर्थ को मूल में लेकर यह शब्द प्रवृत्त हुआ है। बसाने में सहायभूत होने से वसु शब्द यज्ञ अर्थ को प्रदान कर रहा है। यज्ञ का काम बसाना है। यज्ञ शब्द धात्वर्थ के अनुसार तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है- एक तो इस लोक और परलोक के सुख के लिए विद्या, ज्ञान और धर्म के सेवन से जो वृद्ध हैं अर्थात् बड़े-बड़े विद्वान् हैं उनका सत्कार करना। दूसरा अच्छी प्रकार पदार्थों के गुणों के मेल और विरोध के ज्ञान से शिल्पविद्या का प्रत्यक्ष करना और तीसरा विद्वानों का नित्य समागम करना अथवा विद्या सुख धर्म और सत्यादि शुभ गुणों का नित्य दान करना। ये तीनों ही कर्म सृष्टि को चालू रखने के लिए उपयोगी हैं।
मन्त्रगत पवित्र शब्द का अर्थ है पुनातीति पवित्रम् अथवा पूयतेऽनेनेति पवित्रम्। पुञ् धातु से कर्ता या करण कारक में यह शब्द सिद्ध होता है। वेद में एक सिद्धान्त मान्य हुआ है- 'अर्थवशाद् विभक्तिविपरिणाम:’ इसी को व्याकरण में व्यत्यय (Interchange of rule) भी कह देते हैं। अत: पहला वाक्य बना- वसु: पवित्रमस्ति। अर्थात् यज्ञ पवित्रता करने वाला है अथवा यज्ञ पवित्रता का साधन है। 'पवित्रम्’ यहाँ 'सामान्ये नपुंसकम्’ इस नियम से नपुंसक लिङ्ग है। यज्ञ शब्द के हमने जो ऊपर अर्थ दिए हैं, उनके अनुसार यज्ञ का काम है शुद्धि करना। 'धृत-सामग्री-समिधा-यजमान-पुरोहित-मन्त्र’ इन सब के मेल से जो अग्निहोत्र रूप यज्ञ होता है, वह शुद्धिकारक है, शुद्धि का साधन है यह सर्वविदित तथ्य है। विद्वान् आचार्य जो अध्ययन-अध्यापन रूप यज्ञ करते हैं, वे अज्ञानियों के अज्ञान को हटाकर पवित्रता (शुद्धि) का हेतु बनते हैं। वृद्धों के सत्कार रूप यज्ञ से जो उनकी ओर से आशीर्वाद मिलता है, उससे व्यक्ति में इन्द्रियजय का मूल जो विनय (इन्द्रियों का विनयन=अनुशासन) है वह प्राप्त होता है। चाणक्य ने भी कहा है- इन्द्रियजयस्य मूलं विनय:। विनयस्य मूलं वृद्धोपसेवा। वृद्धोपसेवयाऽऽत्मानं सम्पादयेत्। सम्पादितात्मा जितात्मा भवति। अत: यह वृद्धोपसेवारूप यज्ञ भी शुद्धि में सहायक होता है।
मन्त्र का दूसरा वाक्य है- द्यौरसि अर्थात् द्यौरस्ति पूर्व वाक्य से 'वसु:’ पद की अनुवृत्ति या अन्वय अग्रिम सभी वाक्यों से होता जाएगा। अर्थ हुआ- यज्ञ विज्ञान के प्रकाश का हेतु है। 'द्यौ:’ शब्द का अर्थ सूर्यकि रण भी होता है, अत: यज्ञ सूर्य किरणों में स्थिर होने वाला है।
तीसरा वाक्य है- पृथिव्यसि अर्थात् पृथिव्यस्ति। यज्ञ वायु के साथ देश-देशान्तर में फैलने वाला है। यहाँ एक विशेष बात यह समझनी है कि संस्कृत भाषा का एक नियम है कि संस्कृत शब्द आख्यातज (जिसके मूल में क्रिया हो) माने जाते हैं (All nouns derived from verbs) अत: कभी तो वे शब्द उस मात्र क्रियायोग को कह देते हैं और कभी क्रियासम्बद्ध द्रव्य को। प्रकृत में पृथिवी शब्द भूमि (Land) इस पदार्थ का वाचक न होकर प्रथित, विस्तृत इस अर्थ को कह रहा है, अत पृथिवी शब्द का अर्थ हो गया- यज्ञ देश-देशान्तर में फैलने वाला है।
चतुर्थ वाक्य है- मातरिश्वनो घर्मोऽसि अर्थात् मातरिश्वन: घर्मोऽस्ति। मातरिश्वन् शब्द वायु का वाचक है क्योंकि 'माता’ कहते हैं अन्तरिक्ष को, अन्तरिक्ष में जो श्वसन=प्राणन क्रिया करता है। अत: वाक्य का अर्थ हुआ- अग्निताप से युक्त हुआ यह यज्ञ वायु का शोधक है। घर्म का अर्थ है शोधक (शुद्ध करने वाला)।
पाँचवाँ वाक्य है- (अयं वसु:) विश्वधाऽसि अर्थात् विश्वधाऽस्ति। यह यज्ञ समस्त अस्तित्व को धारण करने वाला है। व्यापक अर्थ में या संकुचित (केवल अग्निहोत्र) दोनों ही दृष्टियों से यज्ञ विश्वधारक सर्वधारक है। यजुर्वेद में ही दूसरी जगह प्रश्नोत्तरशैली में बताया- अयं यज्ञो भुवनस्य नाभि:। इस यज्ञ ने ही समस्त विश्व को बांधा हुआ है (णह बन्धने धातु से नाभि शब्द बनता है)।
छठा वाक्य है- परमेण धाम्ना दृ्हस्व अर्थात् परमेण धाम्ना दृंहते (वर्धते)। यह यज्ञ परम धाम=उत्तम सुख स्थान के साथ सुख को बढ़ाने वाला है। वद्र्धते क्रिया 'वद्र्धयते’ णिजन्त के अर्थ को दे रही है। 'परम धाम’ का अर्थ है तृतीय धाम, सुख धाम, आनन्द धाम अर्थात् यह यज्ञ उस परम सुख के साथ अर्थात् उस परम सुख का त्याग न करते हुए सुख को बढ़ाता है। ईश्वरीय आनन्द को अपने साथ रखते हुए संसार सुखों को बढ़ाता है।
सातवाँ वाक्य है- 'मा ह्वार्मा ते यज्ञपतिह्र्वार्षीत्’। यहाँ ह्वृ धातु त्याग करने अर्थ में है। विद्वत् पुरुष जो दूसरों के लिए आदर्श है दूसरों के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है, उसे मन्त्र ने आदेश दिया कि हे विद्वत् पुरुष! मन्त्रोक्त छ: विशेषताओं से युक्त जो यज्ञ है उसे मत छोड़ और साथ में यह भी कह दिया कि तुम्हारा यज्ञ का रक्षा करने वाला यजमान भी उस यज्ञ को न छोड़े।
यह मन्त्र का यज्ञपरक अर्थ हुआ। यदि यहाँ वसु शब्द जगदीश्वर अर्थ का वाचक माना जाए तो अर्थ बनेगा- वह वसु जगदीश्वर पवित्रताकारक है, विज्ञानप्रकाश का करने वाला है, पृथिवी की तरह विस्तृत सब जगह फैला हुआ, वायु आदि का चालक है, विश्व माने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का धारक है। सबको परम करुणा से धारण करता हुआ उन्नति पथ पर ले जाता है। हे विद्वन् मनुष्य! ऐसे उस जगदीश्वर को तुम कभी मत छोड़ो और तुम्हारे कहे में चलने वाला तुम्हारा अनुगामी या सहयोगी यजमान भी उस परमेश्वर को न छोड़े। वसु शब्द वेद में परमेश्वर का वाचक प्रसिद्ध ही है- 'त्वं हि न: पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ’।
यहाँ हमने देखा 'ह्वर’ क्रिया का कर्ता 'हे विद्वन् मनुष्य’ इस सम्बोधनान्त पद का अध्याहार किया गया है। एक अर्थ मन्त्र का यह भी हो सकता है कि सीधा जीव को सम्बोधन करके कहा जा रहा है कि हे जीव! तू यज्ञ का पवित्र करने वाला है। यज्ञ तो अपने आप में पवित्र है, पर तेरी महिमा तो इससे भी बढ़कर है, उस पवित्र यज्ञ का भी तू पवित्रकर्ता है। तू न हो तो यज्ञ की पवित्रता को कौन जाने? कौन सिद्ध करके दिखाए कि यज्ञ पवित्र है? द्युलोक के समान तेरी ऊँचाई है, पृथिवी के समान तेरा विस्तार है, तू वायु के शोधक तेज (घर्म) के समान है, तू इतना महान् है कि सबका धारक है। परम धाम के साथ, ईश्वरीय सुख के साथ तू वृद्धि को प्राप्त होता रह। अपनी महिमा को देखते हुए तू कभी कुटिल चाल मत चल और जहाँ भी तू कार्य करे, जो तुम्हारे संगठन का मुखिया (यज्ञपति) हो, वह भी कुटिलता न करे। तुम और तुम्हारे नेता अन्दर-बाहर से एक रूप हों, सदा शिशुवत् सरल होकर जीएँ।
अब हम यह जानना चाहते हैं- यह कुटिलता है क्या? कुटिलता का अर्थ है- मन में कुछ और, वाणी में कुछ और ही, तथा कर्म में कुछ और- यही कुटिलता है (मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यद् दुरात्मनाम्)। कुटिलता के रहते व्यक्ति अन्तर्मुख नहीं हो सकता, उसके मन की गति या प्रवृत्ति आत्मा की ओर नहीं हो सकती। आत्मा में प्रवेश पाने के लिए अपनी इन्द्रियों को पार करके मन को शान्त करना होता है और फिर उससे भी परे अपनी बुद्धि को स्थिर करना होता है, यह काम वह व्यक्ति नहीं कर सकता जो कि कुटिल है। कुटिल व्यक्ति पुरुषार्थ चतुष्टय में से धर्म की साधना भी नहीं कर सकता बल्कि यह कहना चाहिए कि किसी भी पुरुषार्थ को सिद्ध नहीं कर सकता। क्योंकि धर्म से कटते ही अर्थ व काम से तो व्यक्ति का सम्बन्ध स्वत: ही विच्छिन्न हो जाता है। धर्म से अलग होते ही अर्थ अर्थ न रहकर अनर्थ हो जाता है, इसी प्रकार काम काम न रहकर दुष्काम या कुकाम बन जाता है। धर्म से संयुक्त अवस्था में ही अर्थ को अर्थ व काम को काम नाम से कहा जाता है। अत: धर्म से जुदा होते ही मोक्ष की साधना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। अज्ञान की अवस्था में व्यक्ति अपनी भूल से यह सोचता रहता है कि ऐसा करने से यह लाभ हो जाएगा, वह लाभ हो जाएगा, किन्तु टेढ़े व्यवहार से हानि के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता।
दूसरी शिक्षा है- 'तेरा यज्ञपति भी कुटिल न हो’। यहाँ यज्ञपति से अभिप्राय है 'यज्ञ का स्वामी’। जिस कार्य में व्यक्ति अपनी समस्त ऊर्जा लगाना चाहता है, वह यदि सार्वजनिक महत्त्व का कार्य हो, तो उस संघ का जो प्रमुख संचालक हो, वह भी कुटिल न हो, क्योंकि वह यदि कुटिल मार्ग पर चलेगा तो उसके सभी अनुयायी भ्रान्त हो जायेंगे और सरल सत्यपूर्ण व्यवहार छोड़ देंगे, जिसके भयंकर परिणाम सभी को भोगने पड़ेंगे। राष्ट्राध्यक्ष, किसी संस्था का प्रमुख, किसी संगठन का नेता, परिवार का मुखिया, ग्राम का प्रधान- ये सभी यज्ञपति ही हैं। इसीलिए यजुर्वेद में जिन कर्मों को करने के लिए आदेश दिये हैं, वे सभी 'अध्वर’, अकुटिल कर्म, अहिंसापूर्ण कर्म कहलाते हैं, इन कर्मों की यज्ञ संज्ञा है। भाव यह है कि समुदाय का हर घटक समूचा संघ और संघ का नेता सभी सरल व्यवहार करने के अभ्यस्त बने। कोई भी कुटिलता का आश्रय न ले। अन्यत्र भी कहा है- 'युयोध्यस्मद्-जुहुराणमेन:’। 'दुरितानि परासुव’ इत्यादि। मन्त्र का एक अर्थ यह भी सम्भावित है कि उस परमेश्वर को ही सम्बोधन करके मन्त्र कह रहा है- हे सविता देव परमात्मन् तुम इस विष्णुरूप यज्ञ के (=वसो:) पवित्रता के हेतु हैं (=पवित्रमसि) तुम विज्ञान के प्रकाशक हो (=द्यौरसि) सर्वत्र प्रथनशील होकर विद्यमान हो (=पृथिवी असि) वायु के चालक हो (=मातरिश्वनो घर्मोऽसि) सबके धारक हैं (=विश्वधाऽसि) अपने परम तेज से (=परमेण धाम्ना) हमको बढ़ाओ (=दृंहस्व=वर्धयस्व) आप हमारे लिए इस यज्ञ को कभी न छोड़ें, आपके द्वारा प्रवृत्त यह यज्ञ सतत् चलता रहे (=मा ह्व:) और आपका यह यजमान जो कि प्रार्थी बना हुआ है, यह भी आप द्वारा प्रवृत्त इस यज्ञ को अपना आदर्श मानता हुआ इसे कभी भी न छोड़े (=मा ह्वार्षीत्)।
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Nov 2024 17:59:04
जीवन सूत्र (1) जीवन का निचोड़/निष्कर्ष- जब भी बड़ों के पास बैठते हैं तो जीवन के सार तत्त्व की बात...