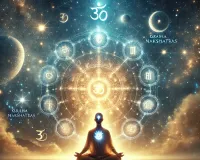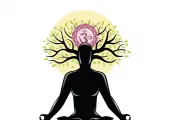विद्वान् पुरुष सांसारिक लोगों में बुद्धिभेद उत्पन्न न करें
On

डॉ. साध्वी देवप्रिया,
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्षा- दर्शन विभाग पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार
अध्यात्म के नाम से कु छ भ्रान्तियां समाज में बहुत ही व्यापक रूप से फैली हुई हैं। इसमें सबसे बड़ी भ्रान्ति है ‘कर्म बंधन का कारण है’, जबकि सत्य तो यह है कि अशुभ कर्म दु:ख व बंधन का कारण हैं। कर्म का त्याग, ऐश्वर्य को मोह-माया व मिथ्या कहकर धन, ऐश्वर्य व वैभव का त्याग कर दरिद्रता को महिमामंडित करना तथा मैं केवल आत्मा हूँ, ये शरीरादि सब नाशवान हैं और शरीर से रोगी आदि होकर दु:ख भोगना आदि व्यापक भ्रान्तियों को दूर करने का कार्य पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज एक महान् विरक्त सन्त थे, उन्होंने भी ‘कर्म बंधन का कारण है’ आदि भ्रान्तियों को दूर करने के लिए अत्यन्त गम्भीरता से ‘साधक संजीवनी’ नामक गीता की हिन्दी टीका में जो लिखा है, उसे हम सबके उपयोग एवं सम्यक् बोध हेतु यहाँ कृतज्ञतापूर्वक प्रकाशित कर रहे हैं। |
संसार की हानि सामान्य लोगों केसकाम कर्म करने से नहीं अपितु विद्वान् लोगों केगलत दिशा-निर्देश व गलत आचरण से अधिक होती है, क्योंकि सामान्य लोग उन्हीं को आदर्श मानकर उन्हीं के उपदेशानुसार आचरण व व्यवहार किया करते हैं। अत: इस श्लोक में विद्वानों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए भगवान् ने निर्देश दिया है-
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्।
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्त: समाचरन्।। (गीता 3/26)
अर्थात् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां विद्वान् बुद्धिभेदं न जनयेत्=सकाम कार्य करने वाले अज्ञानियों में विद्वान् बुद्धिभेद=कन्फ्यूजन पैदा न करे अपितु युक्त: समाचरन् सर्वकर्माणि जोषयेत् अर्थात् स्वयं निष्कामकर्म, दिव्यकर्म करता हुआ, अपने जीवन से आदर्श प्रस्तुत करता हुआ सब मनुष्यों को स्वधर्म व स्वकर्म में लगाये, न कि कोरे उपदेश देकर उन्हें निठल्ला व निकम्मा बनाये। गीता में भगवान् विद्वान् को आज्ञा देते हैं कि उसे ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिये और ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिये, जिससे अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से विचलित हो जाए। जिसके अन्त:करण में स्वाभाविक समता है, जिसकी स्थिति निर्विकार है, जिसकी समस्त इन्द्रियाँ अच्छी तरह जीती हुई हैं और जिसके लिये मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान हैं, ऐसा तत्त्वज्ञ महापुरुष 'युक्त’ या 'विद्वान्’ कहलाता है। उस श्रेष्ठ पुरुष पर विशेष जिम्मेदारी होती है। क्योंकि दूसरे लोग स्वाभाविक ही उसका अनुसरण करते हैं। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति से उन्हें विचलित करना (नीचे गिराना) ही उनमें 'बुद्धिभेद’ उत्पन्न करना है। अत: विद्वान् को सबके हित का भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्रविहित शुभ-कर्मों का आचरण करते रहना चाहिये, जिससे दूसरे पुरुषों को भी निष्काम भाव से कत्र्तव्य-कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। समाज एवं परिवार के मुख्य व्यक्तियों पर भी यही बात लागू होती है। उनको भी सावधानी पूर्वक अपने कत्र्तव्य-कर्मों का अच्छी तरह आचरण करते रहना चाहिये, जिससे समाज और परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़े।
बुद्धिभेद पैदा करने के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-
1. कर्मों में क्या रखा है? कर्मों से तो जीव बंधता है, कर्म निकृष्ट हैं, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिये आदि उपदेश देना अथवा इस प्रकार के अपने आचरणों और वचनों से दूसरों में कत्र्तव्य-कर्मों के प्रति अश्रद्धा-अविश्वास उत्पन्न करना।
2. जहाँ देखो, वहीं स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना कोई रह नहीं सकता, सभी स्वार्थ के लिये कर्म करते हैं, मनुष्य कोई कर्म करे तो फल की इच्छा लिये कर्म करते हैं, फल की इच्छा न रहे तो वह कर्म करेगा ही क्यों आदि उपदेश देना।
3. फल की इच्छा रखकर (अपने लिये) कर्म करने से (फल भोगने के लिये) बार-बार जन्म लेना पड़ता है आदि उपदेश देना।
इस प्रकार के उपदेशों से कामना वाले पुरुषों का कर्मफल पर विश्वास नहीं रहता। फलस्वरूप उनकी (फल में) आसक्ति तो छूटती नहीं, शुभ कर्म जरूर छूट जाते हैं। बन्धन का कारण आसक्ति ही है, कर्म नहीं।
इस प्रकार लोगों में बुद्धिभेद उत्पन्न न करके तत्त्वज्ञ पुरुष को चाहिये कि वह अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार स्वयं कत्र्तव्य-कर्म करें और दूसरों से भी वैसे ही करवायें। उसे चाहिये कि वह अपने आचरण और वचनों के द्वारा अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करते हुए उन्हें वर्तमान स्थिति से क्रमश: ऊँचा उठायें। जिन शास्त्रविहित शुभ-कर्मों को अज्ञानी पुरुष अभी कर रहे हैं, उनकी वह विशेष रूप से प्रशंसा करें और उनके कर्मों में होने वाली त्रुटियों से उन्हें अवगत करायें, जिससे वे उन त्रुटियों को दूर करके साङ्गोपाङ्ग विधि से कर्म कर सके। इसके साथ ही ज्ञानी पुरुष उन्हें यह उपदेश दें कि यज्ञ, दान, पूजा, पाठ आदि शुभकर्म करना तो बहुत अच्छा है, पर उन कर्मों में फल की इच्छा रखना उचित नहीं; क्योंकि हीरे को कंकड़-पत्थरों के बदले बेचना बुद्धिमत्ता नहीं है। अत: सकाम भाव त्याग करके शुभ-कर्म करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। इस प्रकार सकाम भाव से निष्काम भाव की ओर जाना बुद्धिभेद नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। इस तरह उपासना के विषय में भी तत्त्वज्ञ पुरुष को बुद्धिभेद पैदा नहीं करना चाहिये। जैसे प्राय: लोग कह दिया करते हैं कि नाम-जप करते समय भगवान् में मन नहीं लगा तो नाम जप करना व्यर्थ है। परन्तु तत्त्वज्ञ पुरुष को ऐसे नकारात्मक भाव से बचते हुए सकारात्मक उपदेश देना चाहिये कि नामजप कभी व्यर्थ हो नहीं सकता क्योंकि भगवान् के प्रति कुछ न कुछ भाव रहने से ही नामजप होता है। भाव के बिना नामजप में प्रवृत्ति संभव नहीं होती। अत: किसी भी अवस्था में नामजप का त्याग नहीं करना चाहिये। जो यह कहा गया है कि 'मनुवाँ तो चहू दिसि फिरै, यह तो सुमिरन नाहिं’ इसका भी यही अर्थ है कि मन न लगने से यह 'सुमिरन’ (स्मरण) नहीं है, 'जप’ तो है ही। हाँ! मन लगाकर ध्यानपूर्वक नाम-जप करने से बहुत जल्दी लाभ होता है।
कोई भी मनुष्य सर्वथा गुणरहित नहीं होता। उसमें कुछ-न-कुछ गुण रहते ही हैं। इसलिये तत्त्वज्ञ महापुरुष को चाहिये कि अगर किसी व्यक्ति को कोई शिक्षा देनी हो, कोई बात समझानी हो, तो उस व्यक्ति की निन्दा या अपमान न करके उसके गुणों की प्रशंसा करे। गुणों की प्रशंसा करते हुए आदरपूर्वक उसे जो शिक्षा दी जायेगी, उस शिक्षा का उस पर विशेष असर पड़ेगा। समाज और परिवार के मुख्य व्यक्तियों को भी इसी रीति से दूसरों को शिक्षा देनी चाहिये।
उक्त श्लोक (गीता-३/२६) में 'जोषयेत्’ और 'समाचरन्’ पदों से भगवान् विद्वान् को दो आज्ञाएं देते हैं- (1) स्वयं निष्काम भाव से सावधानीपूर्वक शास्त्रविहित कत्र्तव्य-कर्मों को अच्छी तरह करें और (2) कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही निष्काम भाव से कर्म करवायें। मात्र लोगों को दिखाने के लिये कर्म करना 'दम्भ’ नामक आसुरी-सम्पत्ति का लक्षण है (गीता-१६/४)। भगवान् लोगों को दिखाने के लिये नहीं, प्रत्युत लोकसंग्रह के लिये आज्ञा देते हैं।
तत्त्वज्ञ पुरुष को चाहिये कि कर्म करने से अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी वह समस्त कत्र्तव्य-कर्मों को सुचारु रूप से करता रहे, जिससे कर्मों में आसक्त पुरुष में भी निष्काम कर्मों के प्रति महत्त्वबुद्धि जाग्रत् हो और वे भी निष्काम भाव से कर्म करने लगे। क्योंकि-
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन:। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।। (गीता 3/21)
तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष के आसक्तिरहित आचरणों को देखकर अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने की चेष्टा करने लगेंगे। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष को चाहिये कि वह कर्मों में पुरुषों को आदरपूर्वक समझाकर उनसे निषिद्ध कर्मों का स्वरूप से (सर्वथा) त्याग करवायें और विहित कर्मों में से सकामभाव त्याग करने की प्रेरणा करें।
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Nov 2024 17:59:04
जीवन सूत्र (1) जीवन का निचोड़/निष्कर्ष- जब भी बड़ों के पास बैठते हैं तो जीवन के सार तत्त्व की बात...