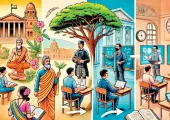प्रज्ञापराध
On

योगऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज
आयुर्वेद के एक महान् ग्रन्थ चरक संहिता में हमें शिक्षा के रूप में एक सुन्दर वाक्य सुनने को मिलता है- 'प्रज्ञापराधो मूलं सर्वरोगाणाम्’। शरीर व मन में विकारों के रूप में पैदा होकर जो कष्ट देते हैं, व्यक्ति को तोड़ डालते हैं वे रोग कहलाते हैं (रुजन्ति ते रोगा:)। जैसे शरीर-सम्बन्धी सैकड़ों प्रकार के रोग होते हैं- ज्वर, खाँसी, जुकाम, पेट दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, वात विकार, कफ विकार, पित्त विकार इत्यादि। उसी प्रकार काम-क्रोध-लोभ-मोह-मान-मद-ईर्ष्या-असूया इत्यादि अनेकानेक मानस रोग भी होते हैं। आचार्य चरक यह देख रहे हैं- रोग चाहे शारीरिक हों या मानस वे अकारण नहीं आते, उनका कोई न कोई कारण होता है। यद्यपि कारण दो प्रकार के हो सकते हैं- नित्य या आगन्तु। पर रोगों का कारण नित्य होता, तो न तो उसे हटाया जा सकता और न ही उससे बचा जा सकता। कारण यदि आगन्तु है तो उसे हटाया भी जा सकता है और सावधानी रखी जाए तो बचा भी। आगन्तु कारण के भी दो रूप हो सकते हैं- सामान्य और विशेष। सामान्य वह होता है जो सब जगह मिले और विशेष वह जो कहीं मिले कहीं न मिले। महामति आचार्य चरक ने सभी शारीरिक व मानस रोगों का एक सामान्य-साझा कारण खोजकर बतलाया। वह है 'प्रज्ञापराध’। आचार्य ने यह बात यथाप्रसंग सम्पूर्ण शास्त्र में बार-बार दोहराई है।
प्रज्ञापराध क्या होता है? आचार्य ने स्वयं ही अपने महान् कण्ठ से यह बतलाने की भी कृपा की है। वे कहते हैं-
धीघृतिस्मृतिविभ्रष्ट: कर्म यत् कुरुतेऽशुभम्।
प्रज्ञापराधं तं विद्यात् सर्वदोषप्रकोपणम्।। (शा. १.१०२)
धी, धृति और स्मृति से च्युत हुआ व्यक्ति जब कोई अशुभ कर्म करता है, तो वात-पित्तादि सभी शारीरिक दोष और रजस्-तमस् आदि मानस दोष प्रकुपित हो जाते हैं यही 'प्रज्ञापराध’ है।
बुद्ध्या विषमविज्ञानं विषमं च प्रवर्तनम्।
प्रज्ञापराधं जानीयान्मनसो गोचरं हि तत्।। (शा. १०.१०९)
बुद्धि से विषम देखना, जो चीज जैसी है उसे वैसा न देखना और फिर गलत समझ के कारण गलत प्रवृत्ति का होना, गलत आचरण करना ही 'प्रज्ञापराध’ है। यह 'प्रज्ञापराध’ मन के क्षेत्र में आता है अर्थात् मन के द्वारा ही इसे देखा जा सकता है।
धी, धृति और स्मृति ये तीनों ही प्रज्ञा के भेद हैं। प्रज्ञा की तीनों शक्तियाँ जब ठीक-ठीक काम करती हैं, तो ही व्यक्ति प्रज्ञावान् कहा जाता है। तीनों में से कोई एक, दो या तीनों ही भ्रष्ट हो जाती हैं तो इसे ही 'प्रज्ञापराध’ कहते हैं। आचार्य ने इन तीनों का ही पृथक्-पृथक् लक्षण व पृथक्-पृथक् स्वरूप दर्शाया है।
'धीविभ्रंश क्या है?’ इस बारे में आचार्य कहते हैं-
विषमाभिनिवेशो यो नित्यानित्ये हिताहिते।
ज्ञेय: स बुद्धिविभ्रंश: समं बुद्धिर्हि पश्यति।। (शा. १.९९)
नित्य में अनित्य और अनित्य में नित्य, हित में अहित और अहित में हित देखना ही विषमाभिनिवेश (अयथाभूतत्वेन निश्चय) है। यदि कोई यह पूछे कि यह बुद्धिविभ्रंश कैसे है? तो इसके उत्तर में यही कहना होगा कि बुद्धि सर्वदा सम (यथाभूत) ही देखती है। बुद्धि की यह योग्यता है कि जो चीज जैसी है, उसको वैसा देखे, किन्तु बुद्धि यदि अपनी इस योग्यता का निर्वाह ठीक से नहीं कर पा रही, तो इस असमदर्शन को बुद्धिविभ्रंश कहना उचित ही है। योगशास्त्र ने बुद्धिविभ्रंश को 'अविद्या = अविवेक = विपरीत ज्ञान’ इन नामों से स्मरण किया है। न्यायदर्शन में इस स्थिति को 'मोह या मिथ्याज्ञान’ कहा गया है। अर्थात् 'वह बुद्धि जो अपने हित-अहित, नित्य-अनित्य को ठीक-ठीक नहीं देख पा रही है, जो हितकारक खान-पान, आहार-विहार, व्यवहार आदि को अहितकारक समझ रही है और जो अहितकारक है उसे हितकारक।‘ इसी प्रकार जो बुद्धि आत्मादि नित्य तत्त्वों को नित्य और शरीरादि अनित्य पदार्थों को अनित्य नहीं समझ पा रही है, इसे भी प्रज्ञापराध का एक महत्त्वपूर्ण घटक धीविभंश कहा जायेगा। श्रीमद्भगवद्गीता १८ अध्याय के ३१, ३२वें श्लोक में राजसी-तामसी बुद्धि के नाम से धीविभ्रंश का वर्णन है-
यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च।
अयथावत् प्रजानाति बुद्धि: सा पार्थ राजसी।।३१।।
जिस बुद्धि से मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कार्य तथा अकार्य को यथार्थ नहीं जानता है, हे पार्थ! वह बुद्धि राजसी है। जबकि-
अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता।
सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी।।३२।।
अर्थात् तामसी बुद्धि तमोगुण (अन्धकार) से आवृत्त होने के कारण सब कार्यों, बातों को विपरीत ही मानती है। अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म, अच्छी वस्तु को बुरी वस्तु और बुरी को अच्छी, परम तत्त्व को तुच्छ और तुच्छ को परम- इस प्रकार सब कुछ विपरीत मानती है।
प्रज्ञापराध का दूसरा घटक है धृतिभ्रंश। धृतिभ्रंश का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं-
विषयप्रवणं सत्त्वं धृतिभ्रंशान्न शक्यते।
नियन्तुमहितादर्थाद् धृतिर्हि नियमात्मिका।। (शा. १.१००)
यदि धृतिभ्रंश हो रहा है, तो विषयों में डूबे हुए मन को अहित अर्थ से कभी रोका नहीं जा सकता, क्योंकि धृति ही तो नियन्त्रण करने वाली शक्ति है। मन व इन्द्रियों का नियंत्रण करने में अशक्त धृति अपने कर्म से भ्रष्ट हुई 'धृतिभ्रंश’ नाम से कही जाती है। जब कभी व्यक्ति का मन अशुभ में, अधर्म में या अपने संकल्पित पथ से अन्य पथ पर जाने लगता है, इन्द्रियाँ अपने विषयों में दौड़ने लगती हैं तो धृति उन्हें रोककर रखती है। भाव यह है- मनुष्य के पास यह एक अद्भुत सामर्थ्य वाली शक्ति है, जिसके द्वारा वह अपने को अकार्य से रोक कर रखता है। मनु ने भी 'धृति: क्षमा दमोऽस्तेयं.’ धर्म के दस लक्षण बताते समय धृति को सबसे प्रथम स्थान पर रखा है, क्योंकि उसके बिना धर्ममार्ग में प्रवेश ही नहीं है। संस्कृत में धृ धातु 'पकड़ कर रखना’ इस अर्थ में प्रयुक्त होती है जैसे 'हस्ते धृत्वा गच्छति’ हाथ में पकड़ कर जा रहा है।
श्रीमद्भगवद्गीता में धृति के तीन भेद बताए गये हैं-
धृत्या यया धारयते मन: प्राणेन्द्रियक्रिया:।
योगेनाव्यभिचारिण्या धृति: सा पार्थ सात्त्विकी।।३३।।
जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मोक्ष के साधनभूत भगवद् उपासना रूप योग से मन, प्राण और इन्द्रियों की सब क्रियाएँ धारण की जाती हैं अर्थात् मन, प्राण और इन्द्रियों की सब चेष्टाएँ जिसके द्वारा शास्त्रविरुद्ध प्रवृत्ति से रोकी जाती हैं, वह धृति सात्त्विकी है। सात्त्विकी धृति द्वारा धारण की हुई इन्द्रियाँ ही शास्त्र विरुद्ध विषय में प्रवृत्त नहीं होती।
कहने का तात्पर्य यह है कि अपने को नियन्त्रण में रखने वाला मनुष्य, जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा एकाग्रता रूप योग से मन, प्राण व इन्द्रियों की चेष्टाओं को धारण किया करता है, रोके रहता है। इस प्रकार की धृति सात्त्विकी है।
यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन।
प्रसङ्गेन फलाकाङक्षी धृति: सा पार्थ राजसी।।३४।।
योगेश्वर स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन! फलाकाङ् क्षी पुरुष जिस धृति से अत्यन्त आसक्ति पूर्वक धर्म, काम और अर्थ को धारण करता है, वह धृति राजसी है।
यया स्वप्रं भयं शोकं विषादं मदमेव च।
न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति: सा तामसी मता।।३५।।
जिस धृति के द्वारा दुर्बुद्धिग्रस्त मनुष्य स्वप्र (निद्रा), भय (त्रास), शोक, विषाद और मद को नहीं छोड़ता। अर्थात् विषय सेवन को ही अपने लिये बहुत बड़ा पुरुषार्थ मानकर उन्मत्त की भाँति मद को मन में सदा कर्तव्य रूप समझता है, इन सबको नहीं छोड़ता। अर्थात् धारण ही किये रहता है। उसकी धृति, तामसी मानी गयी है।
जबकि स्मृतिभ्रंश का निरूपण इस प्रकार है-
तत्त्वज्ञाने स्मृतिर्यस्य रजोमोहावृतात्मन:।
भ्रश्यते स स्मृतिभ्रंश: स्मर्तव्यं हि स्मृतौ स्थितम्।।
(शा. स्थान १.१०१)
रजोगुण-तमोगुण से आवृत आत्मा वाले जिस व्यक्ति की तत्त्व ज्ञान में स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, वह स्मृतिभ्रंश का लक्षण है, क्योंकि स्मर्तव्य विषय स्मृति में स्थित रहता है, स्मृति के अपराध से स्मर्तव्य विषय का विस्मरण हो जाता है। योगशास्त्र में भी स्मृति साधन को ज्ञान प्राप्ति का अन्यतम साधन बताया गया है- अर्थापत्ति से वहाँ यह बात ध्वनित होती है कि स्मृति नहीं तो ज्ञान भी नहीं (श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञा.)। यो.सू. १.२०
चरक में सूत्रस्थान के उपसंहार के रूप में एक बड़ा ही सारगर्भित र्मार्मक संदेश उपलब्ध है-
समग्रं दु:खमायत्तमविज्ञाने द्वयाश्रयम्।
सुखं समग्रं विज्ञाने विमले संप्रतिष्ठितम्।।
श्लोक में पठित 'अविज्ञाने’ शब्द शब्दान्तर से प्रज्ञापराध की ओर ही इङ्गित कर रहा है। भाव यह है- शरीर व मन का समग्र दु:ख अविज्ञान=मिथ्याज्ञान या प्रज्ञापराध पर ही टिका हुआ है। इसी प्रकार शरीर व मन का सम्पूर्ण सुख-शुद्ध ज्ञान में प्रतिष्ठित है। श्रीमद्भगद्गीता में प्रज्ञा (शुद्धबुद्धि/सात्त्विकबुद्धि) की महिमा इस प्रकार वर्णित है कि-
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये।
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्त्विकी।।
अर्थात् प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय तथा बन्ध और मोक्ष- इन सब को जो बुद्धि ठीक-ठीक जानती है, हे पार्थ! वह बुद्धि सात्त्विकी है। जैसा कि पहले ही कहा गया कि 'धी, धृति, स्मृति’ प्रज्ञा की ये तीन अवस्था विशेष हैं। प्रज्ञावान् व्यक्ति इन तीनों को स्वस्थ रखता हुआ पूर्ण सुखमय जीवन व्यतीत करता है।
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Dec 2024 18:59:48
योग प्रज्ञा योग - योग जीवन का प्रयोजन, उपयोगिता, उपलब्धि, साधन-साधना-साध्य, सिद्धान्त, कत्र्तव्य, मंतव्य, गंतव्य, लक्ष्य, संकल्प, सिद्धि, कर्म धर्म,...







.jpg)
.jpg)
.jpg)






.jpg)