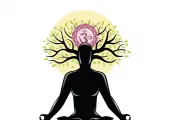मनोरोगों के निवारण में योगनिद्रा की भूमिका
On

डॉ. सचिन त्यागी, विभागाध्यक्ष-षट्कर्म चिकित्सा
एवं अनुसंधान केन्द्र, पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल, हरिद्वार
संसार में प्राणी मात्र की इच्छा सुख की चाह या प्राप्ति होती है। कोई भी प्राणी दु:ख की कामना नहीं करता है। सभी प्राणियों में विकसित प्राणी मनुष्य ही है। मनुष्य मात्र चाहता है कि वह स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सम्पन्न रहें और विश्व के समस्त ऐश्वर्य उसे प्राप्त हो, किन्तु इन समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए सबसे प्रमुख आवश्यकता ‘सु-मन' अर्थात् स्वस्थ मन की है। किन्तु आज विश्व में धन-धान्य सम्पादन एवं संवर्धन की होड़ लगी है। आज की तनावभरी जिंदगी में साधन उपलब्ध होते हुए भी व्यक्ति सुख एवं खुशी की चाह में भटक ही रहा है। इस अंधी दौड़ में व्यक्ति स्वार्थी हो गया हैं।
उसका जीवन मूल्य और जीवन पद्धति इस प्रकार की हो गयी है। गये है कि उसका मन विकृत हो गया है। जहाँ स्वस्थ मन व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखता है, जिसके द्वारा मनुष्य संसार के समस्त ऐश्वर्यों का भोग करता है, वही अस्वस्थ मन विभिन्न प्रकार की शारीरिक व्याधियों के साथ-साथ सामाजिक विकृतियों का कारण बनता हैं। मन ही मनुष्य के सुख एवं दु:ख कारण है। इसलिए ब्रह्मबिंदुपनिषद् में कहा गया है कि - "मन एवं मनुष्यनां कारण बन्ध मोक्ष्यो" अर्थात् विकारग्रस्त मन मनुष्य के बन्धनो (दु:खों) का कारण है और स्वस्थ मन मनुष्य के सुख का कारण है।
मानसिक रोग क्या है?
मानसिक रोग क्या है? इसको सूक्ष्मता से समझने की आवश्कता है। मन और मन के रोग, इन दोनों बातों को पृथक-पृथक समझना पड़ेगा। विचार कर देखा जाये तो मन अपने आप में एक रोग है, किन्तु उस रोग का चिकित्सक भी मन ही है। जिन रोगों का सम्बन्ध बाह्य पदार्थों से न होकर केवल मन से होता है, वे रोग मानसिक कहलाते हैं। विशुद्ध रूप से जो रोग मन के अन्दर ही जन्म लेते हैं, मन को ही पीडि़त करते हैं और जिनका निवारण भी केवल मन के ही अधीन होता है। वे रोग मनोरोग या मानसिक रोग कहलाते हैं। आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि- काम की अधिकता, पागलपन, स्मृतिभ्रंश, चिंता, अपस्मार, शंका, क्रोध, विकृत अहंभाव, विकृत स्वप्न दर्शन, विस्मरण, दु:ख स्मृति आदि रोग मानस रोग कहलाते हैं क्योंकि इनका जन्म मानसिक विकृतियों से होता है।
सामान्य दृष्टि से देखा जाये तो प्रत्येक मनुष्य पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता जीवन की कठिनाइयाँ जीवन की यात्रा में उतार-चढ़ाव एवं वातावरण के कारण सभी मनुष्यों को कभी न कभी निराशा, चिंता, भय, बेचैनी, घबराहट, अनिद्रा, तनाव अनिश्चतता, उत्साह, हताशा आदि विभिन्न मानसिक स्थितियों से गुजरना ही पड़ता हैं, लेकिन इन स्थितियों से ग्रसित मनुष्यों को मानसिक रोगी नहीं कहा जा सकता। बल्कि इसके विपरीत मन पर ऐसी प्रतिक्रियाओं का न होना असमान्यता का लक्षण होता है। मानसिक रोगो की श्रेणी में वही प्रतिक्रियायें आती है जो सामान्य से भिन्न दिखाई देती है।
आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार मानसिक रोगों के कारण
आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार मनोरोगों का मुख्य कारण मनुष्य की मन:- स्थिति, दोषपूर्ण जीवनशैली, दोषपूर्ण विकास सिद्धांत तथा पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में स्वयं को उचित रूप में समायोजित न कर पाना है। बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक सभी किसी न किसी मानसिक समस्या से ग्रस्त है। बाल्यावस्था में यदि किसी शिशु को प्रेम न मिले, अच्छे संस्कार न मिले तो उसमे भय, असुरक्षा, विरोध तथा अपराध आदि के भाव उपस्थित हो जाते है। फ्रायड के अनुसार मनोरोग तब उत्पन्न होते हैं जब समाज द्वारा दमित और अस्वीकृत वासनायें अचेतन से निकलकर मन पर नियन्त्रण कर लेती है।
भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार मानसिक रोगों के कारण
भारतीय मनोविज्ञान में मनोविकार के ऊपर स्वतंत्र ग्रन्थ प्राप्त नहीं होता, अपितु वेद, उपनिषद्, पुराण, योग, आयुर्वेदशास्त्र और दर्शनशास्त्र आदि में मन के स्वरूप और उसके विकारों की चर्चा की गई है। योग के अनुसार महर्षि पतंजलि द्वारा संकलित योगसूत्र में मन के विकार एवं उसके कारको तथा लक्षणों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है, क्योंकि योग परम स्वास्थ्य का विज्ञान है। जिसका उद्देश्य स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन के साथ समाधि की पूर्ण अवस्था को प्राप्त करते हुए अपने स्वरूप में स्थित होना है। यही पूर्ण स्वास्थ्य है तथा यही पूर्ण मानसिक आरोग्य है। इस पूर्ण आरोग्य को प्राप्त किये बिना आध्यात्मिक साधना भी संभव नहीं है। योग में मनोरोगों के स्वरूप तथा लक्षणों को योगमार्ग में आने वाले विघ्नों के रूप में वर्णित करते हुए इन्हे चित्तविक्षेप की संज्ञा दी गई है। यथा- व्याधि (शारीरिक व मानसिक विकार), स्तयान (अर्कमण्यता), संशय (संदेहात्मक ज्ञान), प्रमाद (योग्यता होते हुए भी कर्तव्य कर्म को न करना), आलस्य (तमोगुण की वृद्धि), अविरति (इन्द्रियों की विषयो में आसक्ति), भ्रान्तिदर्शन (विषयो का मिथ्याज्ञान), अलब्धभूमिकत्व (साधना में किसी स्थान को प्राप्त न करना) तथा अनवस्थितत्व (किसी स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी उसमे स्थिर न रहना) योग की दृष्टि से यही प्रमुख मनोरोग एवं उनके लक्षणों का स्वरूप हैं। उपर्युक्त नौ अन्तरायों या चित्त विक्षेपो के साथ पाँच अन्य लक्षण भी उपस्थित हो जाते हैं। जिन्हें विक्षेप सहभुव कहा जाता है।
यथा-दु:ख (विघ्नो के द्वारा प्राप्त प्रतिकुल भाव या पीड़ा)। दु:खो को आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक रूप से तीन प्रकार का बताया गया हैं। दौर्मनस्य (क्षोभ), अंगमेजयत्व (शारीरिक अंगो में कम्पन्न होना), श्वास और प्रश्वास (श्वास लेने और छोडऩे पर नियन्त्रण न रहना)। ये पाँचो लक्षण भी मानसिक अस्थिरता की श्रेणी में आते हैं।
मानसिक रोगो के कारणो में महर्षि पतंजलि पंच क्लेशों का वर्णन करते है- अविद्या (भ्रमपूर्व चिंतन), अस्मिता (आत्मा और चित्त की अभिन्नता का ज्ञान), राग (सुखों को भोगने की तृष्णा), द्वेष (अनुकुल विषयों की प्राप्ति में जो वस्तुयें बाधा उत्पन्न करती है उनके प्रति चित्त में उत्पन्न होने वाली वृत्तियाँ) तथा अभिनिवेश (नश्वर शरीर की मृत्यु का भय)।
भगवान् कृष्ण गीता में मनोरोगों के मूल में अज्ञान को मानते है तथा सम्पूर्ण मनोविकारों का कारण अविद्या को मानते है, यहाँ वे कहते है कि विवेकशील को मानसिक कष्ट हो सकता है तत्वज्ञानी को नहीं क्योंकि विवेकशील मनुष्य अभी कच्चे घड़े के समान है और तत्व ज्ञानी पके हुए घड़े के समान। जिस पर मौसम की अनुकुलता या प्रतिकुलता का प्रभाव नही होता।
आयुर्वेद के अनुसार मानसिक रोगों के कारण
भारतीय विद्याओं की गौरवमयी परम्परा में आयुर्वेद का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आयुर्वेद मनोविकारो के मूल में तीन प्रमुख कारको को मानता हैं। (1) प्रज्ञापराध (अषानता) (2) असात्मेन्द्रियार्थ संयोग (इन्द्रियों का अपने विषयों के साथ अनुचित संयोग), (३) परिणाम (वातावरण की प्रतिकुलता) इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में अधर्म और दुराचार, विषाद का अतिरेक भी मनोरोगों के मूल में प्रमुख माना है।
योगनिद्रा और मानसिक स्वास्थ्य, योगनिद्रा का अर्थ
योगनिद्रा का अर्थ है- आध्यात्मिक नींद या अतीन्द्रिय निद्रा। योग निद्रा के अभ्यास के दौरान व्यक्ति सोता हुआ प्रतीत होता है परन्तु उस समय चेतना जागरूकता के गहरे स्तर पर कार्य कर रही होती है। इस कारण योग निद्रा को मानसिक नींद या आंतरिक जागरूकता के साथ गहन विश्राम के रूप में माना जाता है। नींद और जागने के बीच के इस मध्यवर्ती चरण में, अवचेतन और अचेतन आयाम के साथ संपर्क अनायास होता है। योगनिद्रा में बाहरी अनुभवों से हटकर आन्तरिक विश्राम की स्थिति प्राप्त की जाती है। योगनिद्रा के अभ्यास में शारीरिक केन्द्रो की स्थिति अंतर्मुखी हो जाती है। जब मन किसी केन्द्र पर एकाग्र हो जाता है, तब प्राण शक्ति तथा रक्त आदि उसी स्थान पर केन्द्रित हो जाते हैं।

योगनिद्रा के अभ्यास से अच्छा मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है और इसके साथ ही व्यक्ति को अपनी क्षमता के बारे में, वर्तमान जीवनशैली से सम्बन्धित तनावों का सामना करने में और एक संतोषजनक जीवनशैली को जीने में मदद मिलती है।
मानसिक समस्याएँ व्यक्ति की भावनाओं, विचारो और कार्यों को प्रभावित करती है, जिससे व्यक्ति की दैनिक जीवनशैली पर सीधा प्रभाव पड़ता है। निराशा, तनाव, क्रोध एवं चिंता आदि सभी भावनाएं हैं, लेकिन जब यही भावनाएं लम्बे समय तक रहती है तो मानसिक विकारो के रूप में जन्म ले लेती है। योगनिद्रा के अभ्यास से बहुत ही अच्छे एवं प्रभावाशाली तरीकों से इन विकारों को दूर किया जा सकता है। जब व्यक्ति किसी एक नकारात्मक विचार का बहुत गहरे मन से चिंतन करता है तब वह विचार हमारे अवचेतन मन में बीज रूप में अव्यवस्थित हो जाता है। यह बीज रूपी विचार समय के साथ पौधा फिर वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसी नकारात्मक वृक्ष के ऊपर नकारात्मकता, निराशा, हताशा, क्रोध, ईष्र्या, अनिद्रा आदि फल लगने लगते हैं। इसलिए मन ही हमारे सुख एवं दु:ख का कारण है। अच्छे, पवित्र सकारात्मक विचारों का चिंतन बंधनों एव विकारों से मुक्त करने वाला होता है तथा अपवित्र, नकारात्मक एवं असात्विक विचारों का चिंतन, बन्धन एवं विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं को जन्म देता हैं।
योगनिद्रा की अवस्था में चेतना की परिस्कृत एवं सूक्ष्म शक्ति के द्वारा अवचेतन मन से इसी नकारात्मकता के वृक्ष को जड़ से उखाड़ा जा सकता है तथा मन के संयम के द्वारा पुन: अवचेतन मन की भूमि में पवित्र एवं सकारात्मकता के बीज को बोया जा सकता है। इसका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। योगनिद्रा तनाव को दूर करने का एक प्रभावशाली साधन है। तनाव चाहे मानसिक हो, भावनात्मक हो या मांसपेशियात्मक, आधुनिक युग में सबसे बड़ी समस्या यह तनाव है, चूंकि हम मशीनी युग में जीवन जी रहे हैं जहाँ आध्यात्मिकता की रोशनी का नितांत अभाव है इसलिए लोगों के जीवन में बहुत अधिक निराशा और हताशा रहती है।
योगनिद्रा में लिया गया संकल्प मन को शान्त और स्थिर करने की प्रभावशाली तकनीक है। जीवन में कुछ भी आपको विफल कर सकता है लेकिन योगनिद्रा के दौरान लिए गए संकल्प को नहीं। योगनिद्रा में लिया गया संकल्प अवचेतन मन में बोया जाता है तब वह शिथिल एवं ग्रहणशील होता है। योगनिद्रा के आरम्भ में लिया गया संकल्प बीज बोने जैसा है और अन्त में उसी संकल्प को दोहराना उसे सींचने जैसा है। अत: योगनिद्रा में लिया गया संकल्प अवश्य ही फलीभूत होता है बस आवश्यकता है संकल्प में दृढ़ता की अर्थात् दृढ़ भावना से संकल्प लिया हो।
योगनिद्रा मन को शांत करती है, मन, मस्तिष्क, शरीर और भावनाओं को जोडऩे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शरीर में सजगता, जागरूकता को तेज करने से मस्तिष्क उत्तेजित होता है, जब सजगता से अपनी चेतना या मन को शरीर के विभिन्न अंगों पर घुमाया जाता है तो यह शारीरिक विश्राम को प्रेरित करती है। साथ ही मस्तिष्क के तंत्रिका मार्गों को भी साफ करती है। एक अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि योगनिद्रा के अभ्यास से मस्तिष्क में अल्फा तरंगों की प्रधानता पायी जाती है। जो मानसिक विश्राम की विशेषता है। वास्तव में योगनिद्रा के अभ्यास का आधा घण्टा भी सामान्य नींद के 8-10 घण्टे के बराबर बल्कि उससे भी ज्यादा तन और मन को शांत एवं ऊर्जावान करने वाला होता है।
आधुनिक जीवनशैली, असात्विक आहार, अपवित्र विचार एवं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाओं के कारण शरीर की साम्यावस्था असन्तुलित होने लगती है। इस कारण तंत्रिका तन्त्र पर नकारात्मक प्रभाव होने से न्यूरोरेसेस्टर तथा न्यूरॉन के बीच आपसी सामंजस्य गड़बड़ा जाता है। यही वह स्थिति है जब बाँयें और दाँयें मस्तिष्क का समन्वय तथा मस्तिष्क एवं शरीर का समन्वय असंतुलित हो जाता है तथा विभिन्न मानसिक विकृतियाँ या असमान्यातायें प्रकट होने लगती हैं। इस स्थिति के मूल में केवल एक विचार ही होता है। योगनिद्रा में शरीर एवं मस्तिष्क की इसी असंतुलित अवस्था को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है जिससे धीरे-धीरे पूर्ण शारीरिक, शवनात्मक और मानसिक विश्राम एवं स्वस्थ्ता की अवस्था उत्पन्न हो जाती है।
इस तरह योगनिद्रा का अभ्यास तनाव का प्रतिकार करता है, साथ ही तनाव से सम्बंधित बीमारियों को रोकने में भी मदद करता है। योगनिद्रा के अभ्यास से डोपामिन, ऐन्डोरफिन, सेरेटोनिन तथा ऑक्सीटोसिन नाम के अच्छे हॉर्मोन्स रक्त में बढऩे लगते हैं तथा अभ्यासी की चिंता, तनाव और श्य आदि का स्तर कम हो जाता है, जिससे योगनिद्रा अनिद्रा के लिए एक सफल उपचार है। योगनिद्रा के विभिन्न चरणों का अभ्यास जैसे- संकल्प, शिथिलीकरण सजगता (सांसो पर ध्यान) और मानसिक आदि द्वन्द्वों के साथ-साथ अस्थमा, हृदय रोग, उच्चरक्तचाप एवं हाई-कालेस्ट्रॉल के रोगियों के लिए चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। योगनिद्रा में संकल्प अभ्यासी की इच्छाशक्ति में सुधार करके उसे मजबूत बनाता है और आशावाद के निर्माण में मदद करता है। इसी आशावादी तथा सकारात्मक इच्छा शक्ति के द्वारा खोया हुआ मनोबल पुन: प्राप्त किया जा सकता है।
योगनिद्रा की विधि
तैयारी- योगनिद्रा के अभ्यास के लिए आँखे बंद कर शवासन में लेट जाइए। दोनों हाथ शरीर के बराबर में रहें। दोनों पैर एक-दूसरे से थोड़ी दूर पर हों। शारीरिक हलचल बंद कर दें। आपका शरीर शांत है और आपके नियंत्रण में है।
शिथिलीकरण- अपनी चेतना को अपने शरीर के ऊपर ले जाइए तथा सम्पूर्ण भौतिक शरीर का अनुसंधान कीजिए। सम्पूर्ण शरीर को शिथिल बनाइए, स्वयं को मानसिक रूप से देखें शरीर में किसी प्रकार का तनाव न हो। यदि हो तो उसे दूर कीजिए।
सजगता- सजगता से यहाँ तात्पर्य साक्षी भाव से है। अपने शरीर के आन्तरिक अंगों एवं श्वासों को साक्षी भाव से देखना तथा अपनी चेतना (मन) को सम्पूर्ण शरीर के ऊपर घुमाना अर्थात् देखना।
संकल्प- योगनिद्रा को आरंभ करने से पूर्व एक संकल्प लेंगे। संकल्प भौतिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक हो सकते हैं। आप यह निश्चय करें कि आपको किस प्रकार का संकल्प लेना है। संकल्प की भाषा स्पष्ट हो। संकल्प योगा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है इसलिए कभी भी बीमारी या आदतों से सम्बंधित संकल्प न लें। जैसे- बुरी आदतों से छुटकारा या बीमारी को दूर करना या किसी प्रकार की जनसेवा, सिद्धि या शक्तियों को पाना। व्यक्ति का संकल्प दिव्य गुणों से युक्त तथा आध्यात्मिक पथ पर आगे बढऩे के लिए अग्रसर करने वाला होना चाहिए। योगनिद्रा में लिया संकल्प अवश्य पूर्ण होता है।
चेतना को घुमाना- शरीर के 76 अंगो में चेतना को घुमाया जाता है। मन को एक अंग से दूसरे अंग की ओर तेजी से घुमाना चाहिए। चेतना को शरीर के विभिन्न अंगो में घुमाते समय क्रम को बदलना नहीं चाहिए।
शरीर और जमीन का स्पर्श- अपने सम्पूर्ण भौतिक आकार (शरीर) को जमीन पर लेटा हुए देखिए। अपने शरीर और जमीन के मिलन बिंदुओ के प्रति सजग बनिये। अपने पूरे शरीर में उन अंगों के प्रति सजग बनिये जो जमीन से ऊर्जा का आत्मसात कर रहे हैं तथा जो वायु से प्राण ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं।
संवेदनाओ के प्रति सजग- संवेदनाओ से यहाँ तात्पर्य भारीपन, हल्कापन, गर्मी, ठण्डक, दर्द, तथा आनन्द की अनुभुति का चिंतन करने से है। संवेदनाओं की अनुभुतियों का स्मरण कर उसे अपने मन पर आरोपित करना चाहिए।
चक्रों का मानस दर्शन- इस प्रक्रिया में शरीर में स्थित ऊर्जा केन्द्रों जिनको चक्र या अतीन्द्रिय केन्द्र कहते हैं को ऊपर अपनी चेतना को घुमाना है। प्रत्येक ऊर्जा केन्द्र की अपनी विशेषता होती है उसी विशेषता को अपने अन्दर अनुभव करना होता है।
समाप्ति- आँखो को खोले बिना शांतिपूर्वक उठकर बैठ जाइए। शरीर को धीरे-धीरे शान्तिपूर्वक हिलाइए, शरीर को तानना नहीं है। एक साथ 3 बार ओम् का उच्चारण उच्च स्वर में कीजिए। अब धीरे-धीरे आँखे खोल लीजिए और योगनिद्रा के प्रभाव का अनुभव कीजिए।
उपसंहार- इस प्रकार योगनिन्द्रा के द्वारा न केवल नींद अपितु शरीर से सम्बंधित समस्त प्रकार की व्याधियों को दूर करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है। पूज्य स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य जी के मार्गदर्शन में अनुभवी योगाचार्यों द्वारा इस क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन षट्कर्म चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र में सम्पन्न कराया जा रहा है।
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Nov 2024 17:59:04
जीवन सूत्र (1) जीवन का निचोड़/निष्कर्ष- जब भी बड़ों के पास बैठते हैं तो जीवन के सार तत्त्व की बात...