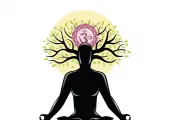योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा है मानसिक रोगों का सर्वोत्तम उपचार
On

डॉ. नागेन्द्र नीरज, निदेशक - योगग्राम
आज अधिकांशत: बीमारियाँ मानसजन्य हैं। तनाव, प्रतिस्पद्र्धा, कुण्ठा, द्वन्द्व और दबाव, सामाजिक बीमारी, बलात्कार, हिंसा, हत्या, आत्महत्या, चोरी एवं अन्य अपराध भी मानसिक विक्षिप्तता का ही स्वरूप हैं। ऐसे मानसिक रोगियों के साथ अक्सर उपचार के नाम पर पशुओं से भी बदतर सलूक किया जाता है। कुछ मानसिक चिकित्सालय भी खुले हैं, लेकिन वहाँ भी मानवीय-दृष्टिकोण के अभाव के कारण रोगियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। सहानुभूति के स्थान पर उनके साथ बदसलूकी की जाती है। पैसे के लालच में ऐसे रोगियों की आँखें निकालने जैसे जघन्य कृत्य भी मानवीय इतिहास में मिले हैं जिन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। मानसिक रोगियों का तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में मित्रवत् व्यवहार के साथ उपचार करना चाहिए। योगग्राम में इस प्रकार के मानसिक रोगियों का उपचार योग व प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से किया जाता है। |
मानसिक रोग-असामान्य मनोविज्ञान व मनश्चिकित्सा की भाषा में यह दो प्रकार का होता है-
मनस्तन्त्रिका ताप (साइकोन्यूरोसिस)
यह रोग एक प्रकार के संवेगात्मक दबाव, कुण्ठा तथा अंतःद्वंद के कारण होता है। इसका उपचार प्राकृतिक योग चिकित्सा से संभव है। ऐसे रोगी भ्रान्ति, विभ्रम तथा मानसिक संभ्रम से ग्रस्त नहीं होते हैं। चिन्तन तथा बातचीत में तारतम्यता तथा तर्कसंगतता होती है। ऐसे रोगी समाजविरोधी व्यवहार नहीं करते हैं। इनमें हत्या की प्रवृत्ति नहीं होती है। ये अपनी देखभाल स्वयं कर सकते हैं। स्वयं निर्णय लेने में ऐसे रोगी सक्षम होते हैं। इनका व्यक्तित्व परिवर्तित नहीं होता है तथा ऐसे रोगियों की मृत्यु दर भी कम है। साइकोन्यूरोसिस वर्ग में मन:श्रान्ति, दु:श्चिन्ता-मनस्ताप, क्षोभोन्माद, मनोग्रस्ति बाध्यता आदि मानसिक रोग होते हैं।
मनोविक्षिप्ति या साइकोसिस
यह जटिल मानसिक रोग है। यह रोग आनुवांशिक तथा नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन से होता है। इस रोग के रोगी उग्र और विक्षिप्त होते हैं। इनमें बोलने तथा चिन्तन की प्रक्रिया में कोई तारतम्यता न होकर यह खंडित तथा विक्षुब्ध होती है। इनमें सभी प्रकार के भ्रम पाये जाते हैं। ये असामाजिक व्यवहार करते हैं। इनमें आत्मानुशासन का अभाव होता है तथा हत्या की प्रवृत्ति प्रबल होती है। स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हैं। इनका व्यक्तित्व छिन्न-भिन्न हो जाता है। इनके उपचार में शामक रसायनों का सहारा लेना आवश्यक होता है। उपचार के बाद भी कुछ साइकोसिस बीमारियाँ उग्र रूप से उभर सकती हैं। इनके रोग लक्षण स्थिर होते हैं तथा इन्हें देखभाल की अतिआवश्यकता होती है। साइकोसिस ग्रस्त रोगियों की मृत्यु दर अधिक होती है।

मंस्तान्त्रिका ताप के भेद
मनस्तंत्रिका ताप के भेद मन:श्रान्ति (Neurosthania): यह रोग अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक श्रम, स्नायुदौर्बल्य, अल्प श्रम, कठिनाइयों तथा समस्याओं से पलायन करने के कारण, मानसिक विक्षोभ, सामाजिक असुरक्षा, संवेगात्मक तनाव व दबाव, हीन भावना आदि कारणों से होता है। यह रोग आनुवांशिक (पैतृक) भी होता है। कब्ज़ के कारण भी यह रोग होता है। शरीर एवं मन में निरन्तर थकान, काम के प्रति अनिच्छा, विश्राम एवं निद्रा के बाद भी थकान, विषाद, खेल, भोजन, मनोरंजन, पोशाक अथवा किसी भी चीज में अभिरुचि नहीं होना, बाह्य पर्यावरण के प्रति उदासीनता, हमेशा अपने दु:ख एवं रोग के सम्बंध में सोचनीय, आत्मकेन्द्रित तथा स्वार्थी होना, सोने पर बार-बार निद्रा भंग होना, अनिद्रा, हमेशा सिर, पेट, कमर, पिण्डली, पैर, हृदय, आँख, कान में दर्द महसूस करना, कई दिनों तक बिना स्नान, बिना दाड़ी बनाए, बिना खाना खाये, आलसियों जैसा जीवन आदि अनेक लक्षण इस रोग में दिखते हैं। ऐसे रोगियों को हर कार्य एक बोझ-सा प्रतीत होता है।
दुश्चिन्ता-मनस्ताप (Anxiety-neurosis): इस रोग में रोगी अकारण भय की आशंका से चिन्तित रहता है। अपने सगे-सम्बन्धी के कहीं जाने पर उसकी दुर्घटना में मृत्यु न हो जाय या कहीं और कोई दुर्घटना न हो जाए, इसकी चिन्ता निरंतर रोगी को बनी रहती है। निरंतर भयभीत तथा चिन्तित रहने के कारण श्वास गति, हृदय गति तथा रक्तचाप बढ़ा हुआ रहता है। पुरुषों में नपुंसकता तथा स्त्रियों में कामशैथिल्य के लक्षण दिखते हैं। पाचन-क्रिया अव्यवस्थित हो जाती है। आँख, सिर, कर्ण तथा उदरशूल की शिकायत बनी रहती है।
कामेच्छा की अतृप्ति तथा उसका दमन, मानसिक अंतर्द्वंद, कुंठा, हीनभावना, तनाव तथा दबाव दुश्चिन्ता-मनस्ताप के मुख्य कारण हैं।
क्षोभोन्माद (Hysteria): क्षोभोन्माद प्राय: स्त्रियों का रोग है। स्त्रियों में मनोलैंगिक (Psycho-sexual) विकास जटिल होता है। कुछ स्त्रियों में लैंगिक तुष्टि में अप्रिय अनुभव, बलात्कार के कारण पुरुषों के प्रति घृणा या किसी प्रकार के मानसिक अंतर्द्वंद के कारण हिस्टीरिया होता है। प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व तक यह सिर्फ स्त्रियों का रोग समझा जाता था। लेकिन कुछ सैनिको में भय और भागने की निन्दा के कारण मानसिक अंतर्द्वंद से हिस्टीरिया रोग पाया गया। वास्तव में समस्याओं से जूझने की जिम्मेदारी को न निभा पाने के कारण असामर्थ्य की ओर पलायन कर जाना ही हिस्टीरिया रोग है। दूसरों से सहायता, सहानुभूति तथा प्यार पाने के लिए हिस्टीरिया रोग के लक्षण दिखते हैं। प्रियजनों की मृत्यु, आर्थिक हानि, प्रेम तथा वैवाहिक असफलता, सामाजिक अप्रतिष्ठा एवं अन्य मानसिक आघात, मंद बुद्धि, प्रेम सम्बन्ध, व्यापार-नौकरी आदि से सम्बन्धित समस्याओं के कारण, किशोरावस्था में बहुमुखी व्यक्तित्व व आत्मविश्लेषण की कमी, स्वयं से अपरिचय, असंतुष्ट एवं दमित कामेच्छा, हीनग्रंथि, सामाजिक जीवन को निर्वाह नहीं कर पाना आदि अनेक कारण हैं जिससे हिस्टीरिया रोग होता है। इस रोग में अंगों में काल्पनिक संवेदनहीनता, दृष्टि एवं श्रवण-दोष, लकवा, बैठने, खड़ा होने तथा चलने में असामर्थ्य, वाणी-दोष (तुतलाहट एवं गूँगापन) अधिक पसीना आना, चेहरे एवं त्वचा का रंग बदलना, भूख की कमी, उदरशूल, वमन आदि अनेक शारीरिक रोग-लक्षण दिखते हैं। निद्राभ्रमण, विस्मृति, संवेगात्मक अस्थिरता, रोते-रोते हँसना, या हँसते-हँसते रोना, नोचना-काटना, तोडफ़ोड़ करना, दूसरों की उपस्थिति में बेहोश हो जाना, द्वैध व्यक्तित्व, कभी नैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक आचरण करना, तो कभी असामाजिक, उद्दण्ड, उच्छृंखल, अशुभ, स्वार्थ एवं निर्लज्जतापूर्ण जीना, अस्थिर, अहम्-केन्द्रित संसूचनग्राही मन:स्थिति के साथ जीना आदि अनेक मानसिक-भावनात्मक लक्षण दिखते हैं।
दुश्चिन्ता-क्षोभोन्माद (Anxiety-hsyteria): दमित एवं असंतुष्ट कामेच्छा व वासनाएँ भय के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। भय अकारण होते हैं। बच्चों का डरना स्वाभाविक है लेकिन बड़ों को बच्चों की तरह डरना असामान्य है। अस्तित्वहीन वस्तुओं, व्यक्तियों तथा जानवरों से डरना तथा भयोत्पादक कारण के दूर हो जाने के बाद भी निरंतर भय बना रहना आदि दुश्चिन्ता-क्षोभोन्माद के कुछ प्रमुख कारण हैं।
मनोग्रस्ति बाध्यता: मनोग्रस्ति बाध्यता में विशेष विचार या कल्पना की बारम्बार पुनरावृत्ति होती रहती है। चाहकर भी उसे रोका नहीं जा सकता। आवेग आते ही रहते हैं। अवश एवं लाचार रोगी एक ही विचार या कर्मकाण्ड में फँसा रहता है। लगातार रुपये गिनना, दिनभर स्नान करना, उठ-उठकर दरवाजा बन्द करना, बार-बार हाथ धोना, किसी वस्तु के प्रति अनावश्यक चिन्तन तथा भय इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
मनोविक्षिप्ति (Psychosis) के भेद:
मनोविक्षिप्ति दो प्रकार की होती है-
शारीरिक या जैविक विषजन्य मनोविक्षिप्ति (Organic toxic Psychosis): आँत्र ज्वर, र्यूमेटिक, टाइफस, मलेरिया, इन्फ्लुऐंजा बुखार, विसर्प कंठशोथीय न्यूमोनिया आदि संक्रामक रोग, शराब, भोजन औद्योगिक एवं औषधियों से सम्बन्धित विषजन्य प्रभाव तथा लकवा, कैंसर, गुर्दे, हृदय, यकृत, मस्तिष्क और उदर सम्बन्धी जीर्ण रोगों के कारण उत्पन्न विषमयता के फलस्वरूप मनोविक्षिप्त होती है। गर्भावस्था तथा प्रसवोत्तर काल में भय एवं अनियंत्रित उत्कंठा व आशंका के कारण मनोविक्षिप्ति के लक्षण दिखायी देते हैं। फंक्शनल साइकोसिस- यह आनुवांशिक तथा अप्रिय अनुभवों के दमन से उत्पन्न होता है। ये निम्नलिखित हैं-
विखंडित मनस्कता या मनोविदग्धता (Scizophrenea): शीजोफ्रेनिया काफी जटिल रोग है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है। यह रोग प्राय: 15 से 50 वर्ष की उम्र में विकसित होता है। दोषयुक्त लालन-पालन, पौरुष ग्रंथियों में विक्षोभ, आपराधिक वातावरण, आघात, आनुवांशिक, अंतर्द्वंद के कारण दमित तीव्र काम-वासना का पलायन, मनोग्रन्थियों के दमन तथा कामेच्छा का प्रतिगमन, हीन ग्रंथि, विकृत अन्तर्मुखी व्यक्तित्व, स्त्रैण तथा पुरुष प्रवृत्ति के मध्य का द्वंद्व आदि अनेक कारण हैं जिससे शीजोफे्रनिया रोग होता है। शीजोफ्रेनिया के रोगी दु:ख-सुख के प्रति उदासीन होते हैं। आत्मीय स्वजनों की मृत्यु सफलता, दुर्घटना पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। एकान्तप्रिय होते हैं। हँसते-हँसते रोने लगते हैं। स्मृति दुर्बल हो जाती है, चिन्तन अव्यवस्थित हो जाता है। कभी इन्हें अप्रिय तो कभी प्रिय वस्तु, ईश्वर या प्रेतात्माओं को देखने तथा उनकी आवाज सुनने का भ्रम होता है। इन्हें हर समय दूसरों द्वारा अपने प्रति षड्यंत्र, मारने-काटने की शङ्का बनी रहती है। कभी-कभी ये लम्बे-लम्बे वाक्य तेजी के साथ काफी देर तक बोलते चले जाते हैं तो कभी पूर्णत: शान्त व शून्य हो जाते हैं। इनके शब्द निरर्थक तथा बहुत शब्दों को मिलाकर स्व-सृजित नये शब्द होते हैं।
उन्माद या अवसाद: उन्माद तथा अवसाद एक ही रोग के लक्षण हैं, जो कभी एक साथ, तो कभी अलग-अलग परिलक्षित होते हैं। उन्माद तथा अवसाद के मध्य रोगी की सामान्य स्थिति भी आ जाती है। रोग की स्थिति में ध्यान को स्थिर नहीं रख पाना, अपरिचित को मित्र तथा मित्र को शत्रु समझना, भ्रम, बिना आवाज के आवाज सुनाई पडऩा, कभी खुशबू तो कभी बदबू आदि अनेक विभ्रम, चिड़चिड़ापन, क्रोध, तीव्र कामुकता, निर्णय न कर पाना, संवेदनहीनता, बहुत खुशी या उदासी में बेहोश हो जाना आदि अनेक रोग लक्षण दिखते हैं।
संभ्रान्ति (Paranoia): संभ्रान्ति के रोगी प्राय: सामान्य बुद्धि के होते हैं। उनका चिन्तन तथा व्यवहार संतुलित होता है। ये रोगी अहंकेन्द्रित होते हैं। उत्तरदायित्व का भार वहन किये बिना ही अपने को महान् सिद्ध करना चाहते हैं। जब इच्छा पूर्ति नहीं होती है तब भ्रान्तिग्रस्त हो जाते हैं। रोगी की चिन्तन व सोचने की प्रक्रिया अस्त-व्यस्त, गड्डमड्ड होती है। अत: समझा कर संभ्रान्ति को दूर किया जा सकता है।
संभ्रान्ति के कारण: विभिन्न संभ्रान्तियों का मुख्य कारण अतिरंजित संवेग, हीन तथा अपराध भाव, कुंठा, अंतर्द्वंद तथा मनोग्रंथि है। इसके कारण मस्तिष्क में तनाव तथा अशांति पैदा होती है। उससे बचने के लिए व्यक्ति धार्मिक, सुधारात्मक या अन्य संभ्रान्ति में फँस जाता है। शराब तथा अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से उत्पन्न उन्माद के रोगियों में ईष्र्या, चिड़चिड़ापन, दोषोन्वेशी, अश्लील विनोद, अस्पष्टता के लक्षण दिखते हैं। डरावने दु:स्वप्र आना, सायंकालीन भय, भयावह दृष्टि एवं श्रवण भ्रम होता है। उसे हमेशा विकराल जन्तु के आक्रमण का भय होता है। उसे डरावनी धमकियाँ सुनाई पड़ती हैं। इन भयों से मुक्ति के लिए रोगी आक्रमण कर सकता है, खिडक़ी से कूद सकता है। रात में भय और बेचैनी बढ़ जाती है। रोगी की अँगुलियाँ, जिह्वा, आँख की पलकें तथा पूरा शरीर हिलने लगता है। इसे संकल्प प्रवाह कहते हैं। चेहरा अतिरक्तिम, होंठ नीले, अत्यधिक पसीना, नाड़ी कमजोर तथा तीव्र, हृदय की आवाज मंद, तापमान वृद्धि के लक्षण परिलक्षित होते हैं। नपुंसकता, यकृत तथा पेट का शोथ हो जाता है। शीघ्र बुढ़ापा आ जाता है।
विविध मानसिक रोगों के कारण: मानसिक रोगों के विविध कारणों में द्वन्द्व, कामेच्छा काम दमन, अन्त:स्रावी ग्रंथियों का अनियंत्रित स्राव तथा आनुवांशिकता प्रमुख हैं। इन कारणों को दूर करने के लिए प्राकृतिक योग चिकित्सा प्रमुख भूमिका निभाती है। प्राकृतिक चिकित्सा का आधार भी मनश्चिकित्सा के अनुकूल है। अचेतन मन में दमित विविध वासनाएँ, कुंठाएँ, द्वन्द्व, कामेच्छा के विभिन्न मानसिक रोग होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का आधार भी यही है कि रोग का कारण एक है- टॉक्सिक आर्गेनिज्म विजातीय पदार्थ का विभिन्न संस्थानों तथा स्नायुओं में एकत्रित होना। दमित तथा एकत्रित द्वन्द्व, वासनाओं तथा विजातीय पदार्थों के निष्कासन से हम स्वस्थ होने लगते हैं। सदैव ध्यान रखें कि शरीर तथा मन एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। मन का स्वास्थ्य शरीर का स्वास्थ्य है; तथा शरीर का स्वास्थ्य मन का स्वास्थ्य है। शरीर की स्नायु संचार तथा रक्तसंचार व्यवस्था एवं अन्य संस्थान सुव्यवस्थित कार्य कर रहे हैं तो आप पूर्णरूपेण स्वस्थ हैं।
मनोरोगों की अचूक प्राकृतिक चिकित्सा
प्राकृतिक-चिकित्सिा की निम्रलिखित विधियाँ उपर्युक्त मानसिक रोगों के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन प्रविधियों का सभी प्रकार के मानसिक रोगियों में विवेक के अनुसार प्रयोग करने से लाभ अवश्य मिलता है। ब्रह्मचर्य को बलपूर्वक थोपें नहीं, जागरण से ब्रह्मचर्य उतरने दें। मानसिक रोगियों में कोष्ठबद्धता की शिकायत मिलती है। अभी हाल ही के प्रयोगों से यह बात स्पष्ट हो गयी है कि कोष्ठबद्धता के कारण आँतों में पैथोजेनिक रोगाणुओं का अरबों की संख्या में ओवर-ग्रोथ होता है जो कुछ एमिनो एसिड (प्रोटीन) से प्रतिक्रिया कर हानिकारक तत्त्व ‘‘बायोजेनिक एमाइंस’’बनाते हैं। ट्रेप्टोफिन ट्रिप्टैमाइन में, हिस्टीडाइन हिस्टेमाइन में, टाइरोसाइन टाइरोमाइन में एवं अन्य घातक तत्त्वों में बदल जाता है। ये बायोजेनिक एमाइंस यकृत को क्षतिग्रस्त कर सीधे रक्तप्रवाह द्वारा स्नायु-संस्थान में पहुँच जाते हैं। फलत: रोगी में शीजोफ्रेनिया, मानसिक अवसाद, संभ्रान्ति आदि के लक्षण दिखने लगते हैं। अत: मानसिक रोगी को लगातार कुछ दिनों तक सिर, रीढ़ एवं पेडू पर मिट्टी की पट्टी; तत्पश्चात् रीढ़ व पेट का गरम-ठण्डा सेंक देकर पेट व रीढ़ की मालिश करने के बाद एनिमा दें। पुन: रोग की स्थिति के अनुसार पूर्ण टब इमर्शन स्नान, गरम पाद स्नान, गरम-ठण्डा कटि स्नान, गीली चादर लपेट, वाष्प स्नान, ठण्डा कटि स्नान, सूखा घर्षण स्नान, सर्वांग मिट्टी का लेप आदि बदल-बदल कर देना चाहिए। उग्र रोगियों को पूर्ण टब स्नान (पानी का तापक्रम 1030 FU) 45 मिनट तक दें। कुछ मानसिक रोगी शौच तथा पेशाब की हाजत को दबा लेते हैं, आँतों की संकुचनहीनता के कारण जीर्ण कब्ज़ हो जाता है। अत: आँतों की सफाई के लिए परिस्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के एनिमा का प्रयोग करना चाहिए। मानसिक रोगियों का उपचार कठिनसाध्य होता है। रात्रि को इन रोगियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
मनोरोगों में अत्यन्त प्रभावी यौगिक चिकित्सा
यौगिक चिकित्सा में आसन, प्राणायाम, ध्यान, षट्कर्म तथा सूक्ष्म व्यायाम विशेष लाभदायक होते हैं। सर्वप्रथम मानसिक रोगी को कुञ्जर व जलनेति क्रिया 15 दिन तक लगातार करानी चाहिए। पुन: कुञ्जर क्रिया सप्ताह में एक दिन तथा जलनेति 6 महीने तक लगातार कराएँ। 15 दिन में एक बार शंख प्रक्षालन क्रिया अवश्य कराएँ।
सूक्ष्म व्यायाम: सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास मानसिक रोगियों के लिए विशेष उपयोगी पाया गया है क्योंकि इससे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तथा विविध क्रियाओं से मानसिक द्वन्द्व तथा दमित वासनाएँ मुक्त होती हैं। सूक्ष्म व्यायाम की दृष्टि से उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि, बुद्धि तथा धृतशक्ति, स्मरणशक्ति, मेधाशक्ति, कपोलशक्ति, कर्णशक्ति वद्र्धन, ग्रीवा, स्कन्ध तथा बाहुमूल, भुजबंध कोहनी, भुजवल्ली, पूर्ण भुजा, मणिबन्ध, करपृष्ठ, करतल, अँगुलीमूल, अँगुली, वक्षस्थल, उदर, कटि, कुण्डलिनी, जंघा, जानु, पिण्डली, पादमूल, गुल्फ, पाद पृष्ठपादतल तथा पादांगुली शक्ति विकास क्रियाएँ लाभदायी हैं।
आसन: आसनों में पद्मासन, सिद्धासन, जानुशिरासन, अद्र्धमत्सयेन्द्रासन, पश्चिमोत्तानासन, वज्रासन, बद्धपद्मासन, योग मुद्रा, सुप्तवज्रासन, गोमुखासन, पक्षी आसन, उत्तानपादासन, धनुरासन, चक्रासन, भुजंगासन, शलभासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, कर्णपीड़ासन तथा मत्स्यासन उपयोगी है। इन आसनों से अन्त:स्रावी ग्रंथियों का स्राव नियंत्रित होता है। स्नायु-संस्थान (सिम्पेथेटिक व पैरासिम्पेथेटिक) पर नियंत्रक प्रभाव होता है। प्राणायाम में अनुलोम-विलोम प्राणयाम विशेष लाभदायक है।
ध्यान: ध्यान के विविध प्रयोगों में आनापान शक्ति प्रयोग, विपश्यना, साक्षी भाव, वृत्तियों का निरीक्षण, ॐ प्राणायाम अत्यधिक लाभदायक है। मानसिक रोगों में पैरासिम्पेथेटिक तथा सिम्पेथेटिक-ये दोनों ही स्नायु-संस्थान अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं। पैरासिम्पेथेटिक स्नायु-संस्थान के अधिक उत्तेजित होने से रोगी उद्दण्डता, आक्रमण तथा अपराध वृत्ति की ओर प्रवृत्त होता है। संवेदी स्नायु-संस्थान अत्यधिक उत्तेजना के कारण रोगी भय तथा हीन भावना से ग्रस्त होता जाता है। मानसिक रोगियों के उक्त दोनों संस्थान उपर्युक्त यौगिक क्रियाओं से नियंत्रित होते हैं, फलत: रोगी स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होता है। उक्त आसनों, ध्यान, प्राणायाम का विशेष प्रभाव रीढ़ तथा मस्तिष्क पर होता है फलत: संवेग नियंत्रित होता है। द्वन्द्व निष्कासित होता है। उपर्युक्त सभी क्रियाओं का प्रयोग किसी योग्य प्राकृतिक-योग चिकित्सा विशेषज्ञ के निर्देशन में ही करना चाहिए।
आनुवांशिक तथा साइकोसिस मनोव्याधियों का निवारण कठिन होता है। मनोव्याधियों की चिकित्सा के लिए आधुनिक विज्ञान में सम्मोहन, संसूचन, समूह-मनश्चिकित्सालय मनोनाटक, मनोविश्लेषण, स्वप्रविश्लेषण, शिक्षा चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, आघात चिकित्सा में विद्युत तथा इंसुलिन आघात चिकित्सा (E.S.T. तथा I.C.T), मनोशल्य तथा साइको सोमेटिक औषधियाँ काम में ली जाती हैं। इनका उपयोगी रोगी की स्थिति के अनुसार किया जाता है। इ.एस.टी. तथा आई.सी.टी., प्रशामक औषधियाँ तथा साइको सर्जरी का प्रयोग उग्रतम रोगियों में किया जाता है। उग्र विक्षिप्त मनोव्याधि के रोगियों में औषधियों का प्रयोग करते हुए पूर्ण टब इमर्शन बाथ अत्यधिक उपयोगी पाया गया है।
प्राकृतिक योग चिकित्सकों को मनोव्याधियों का उपचार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि रोगी की संवेगात्मक अस्थिरता, अंतर्द्वंद तथा अचेतन मन को समझ कर विध्वंसक दमित इच्छाओं, ग्रंथियों, अनुभूतियों तथा भावों को मुक्तकर रोगी में आत्मविश्वास जगाया जाए जिससे अंतर्द्वंद दूर होकर मानसिक संतुलन आ जाये।
मानसिक रोगियों की चिकित्सा में रोगी तथा चिकित्सक के बीच विश्वास तथा सहयोग अतिआवश्यक है। रोगी अपनी संवेगात्मक समस्या, दमित, दु:खद तथा अप्रिय बातों पर खुलकर चर्चा कर सके, इसके लिए चिकित्सक को काफी धैर्यवान् तथा समझदार होना चाहिए। यहाँ चिकित्सक का अनुभव तथा ज्ञान काम में आता है। चिकित्सक एवं रोगी के बीच संवेगात्मक सम्बन्ध विकसित न हो, इसका भी ध्यान रहे, अन्यथा चिकित्सक भी रोगी बन सकता है। चिकित्सक रोगी के अन्दर निषेधात्मक विचारों को दूर कर उसे विधायक एवं स्वस्थ्य विचार तथा सुकर्म के लिए प्रेरित करे। रोगी को प्रोत्साहन देकर उसके अन्दर विवेक तथा अन्तर्दृष्टि पैदा करें ताकि वह भला-बुरा समझने लगे।
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Nov 2024 17:59:04
जीवन सूत्र (1) जीवन का निचोड़/निष्कर्ष- जब भी बड़ों के पास बैठते हैं तो जीवन के सार तत्त्व की बात...





.jpg)
.jpg)
.jpg)