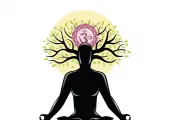जो शेष है वही 'शिष्य' है
On

वंदना बरनवाल
महिला पतंजलि योग समिति - उ.प्र.(मध्य)
हम भारत के लोग बड़े खुशनसीब हैं क्योंकि हमारे वहां सदियों से गुरु-शिष्य की अनूठी और अद्भुत सांस्कृतिक परंपरा चली आ रही है। गुरु-शिष्य की इस परंपरा की सबसे ख़ास बात यह है कि इसका निर्वहन सिर्फ आध्यात्मिक गलियारों में ही नहीं होता अपितु पारिवारिक और सामाजिक गलियारों में भी इसकी उतनी ही अहमियत है, इसीलिए तो हम अपने माता-पिता को प्रथम गुरु कहते हैं, गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने गुरु-शिष्य परम्परा को ‘परम्पराप्राप्तम योग’ भी बताया है। गुरु-शिष्य की ऐसी ही परंपराओं से भारत में ना सिर्फ साधना और ज्ञान की पद्धतियाँ सफल हुई बल्कि परिवार और समाज के मूल्य भी गढ़े जाते रहे, जिज्ञासु शिष्य की जिज्ञासा का समाधान भी इसी परंपरा के माध्यम से ऐसी गुरूसत्ता द्वारा किया जाता रहा जिसने स्वयं उसका साक्षात्कार किया हो। इन विशेषताओं के कारण ही सदियों से चली आ रही ज्ञानसंपदा का संरक्षण आज भारत कर सका है अन्यथा समय के साथ ना जाने कितनी सभ्यताएं आई और विलुप्त भी हो गई परन्तु भारतीय सभ्यता आज भी कायम है, सिर्फ कायम ही नहीं बल्कि आज पूरी दुनिया को राह भी दिखा रही है। इस परंपरा की अनेकों विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि एक तरफ गुरु अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए शिष्य पर पड़े अज्ञान के पर्दे को हटाते हैं और तो वहीं दूसरी तरफ शिष्य भी पूर्ण समर्पण भाव के साथ अपने अहंकार को दूर कर ज्ञान अर्जन करते हैं, इसलिए गुरु-शिष्य परंपरा में गुरु की श्रेष्ठता के साथ शिष्य के भीतर गुरु के प्रति श्रद्धा भी अपार होनी चाहिए।
श्रद्धा क्या है
श्रद्धा का अर्थ है सत्य को धारण करना, ‘श्रत’अर्थात ‘सत्य’, ‘धा’ अर्थात् ‘धारण करना’ श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है ‘सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, यो यच्छृद्व: स एव स:’ अर्थात् सभी की श्रद्धा उसके अन्त:करण के अनुरूप होती है। व्यक्ति श्रद्धामय है और जिसकी जो श्रद्धा है, वह वास्तव में वही है। इसलिए कहा जाता है कि हम गुरुनिष्ठ बने रहें और गुरुनिष्ठ बनने के लिए गुरु के हर वाक्य में निष्ठा तो रखनी ही होगी। जब हम गुरुनिष्ठ बनते हैं तभी गुरु द्वारा उपदेशित ज्ञान का संचार हमारे भीतर होता है क्योंकि श्रद्धा की कोख में ही तो ज्ञान पनपता है। श्रीमद्भगवत गीता में श्रद्धा को ज्ञान की जननी भी बताया गया है। ज्ञान की प्राप्ति होते ही हमारे भीतर से श्रेष्ठता का भाव समाप्त हो जाता है और हमारा व्यक्तित्व समाधान का रूप ले लेता है और फिर जब शिष्य श्रद्धापूर्वक गुरुनिष्ठ होता है तो गुरु-शिष्य में स्वत: ही एक आध्यात्मिक और उच्चस्तरीय विचारों का आदान-प्रदान होने लगता है, ऐसी स्थिति में पहुँचने के बाद शिष्य अपनी सत्ता को, अपने अहंकार को, गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है और गुरु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उसे ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बनाकर देश और समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर देता है। इसलिए श्रद्धा वह प्रकाश है जो गुरु की प्राप्ति के लिए बनाए गए मार्ग को दिखाती है।
गुरु कौन है
गुरु कौन है इसको समझाने के लिए तो हमारे वेदों और शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपाधि तो दी ही गई है साथ ही गुरु और गोविन्द दोनों की उपस्थिति में गुरु को पहले प्रणाम करने की वजह भी बताई गई हैं। गुरु के लिए जब इतना सब कुछ कहा जा चुका हो तो फिर इसके आगे कुछ भी कहना शेष नहीं रह जाता। इसलिए गुरु कौन है के उत्तर को जानने के लिए अपने गुरु को अपने में महसूस कीजिये, अपने कार्यों में अपनी दिनचर्या में उनको शामिल कर लीजिये। जिस प्रकार हम प्रकाश को देख नहीं सकते पर उसकी अनुपस्थिति में कुछ और देख भी नहीं सकते उसी प्रकार गुरु तत्व की उपस्थिति भी हमारे लिए होती है। गुरु ब्रह्मा हैं अर्थात वे रचनात्मक और उत्पादक बने रहने की प्रेरणा देते हैं। ताउम्र क्या किया, हमारी उत्पादकता और उपलब्धि क्या रही, इसका ध्यान दिलाते रहते हैं। उनकी इसी प्रेरणा से ही तो वे एक ऐसे तत्व के रूप में हमारे भीतर प्रवेश करते हैं और उनकी उपस्थिति मात्र से हमारी रचनाधर्मिता और सृजनशीलता में वृद्धि होती है। गुरु विष्णु भी हैं, विष्णु यानि विराट के साथ ही विस्तारक भी और पालनकर्ता भी गुरु के विष्णु रूप का अर्थ हमारे भीतर दूसरों को कुछ देने की भावना का बने रहना और साथ ही सबकी स्वीकृति भी बने रहना है। दूसरों को कुछ देने की यही भावना और उसकी स्वीकृति सामथ्र्यवान बनाती है और इस सामथ्र्य को संभालना भी एक बहुत बड़ी साधना है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के पश्चात कहा गया ‘गुरु देवो महेश्वर:’ यानि जो सही नहीं है उसका निस्तारण करना भी तो आना चाहिए। गंदगी भीतर की हो या फिर बाहर की यदि हम उसको समाप्त करना नहीं सीख सके तो कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें व्यर्थ है। इसके साथ ही गुरु को माता-पिता, परिजन, बन्धु, सखा एवं परिवेश आदि भी बताया गया क्योंकि ये सब कहीं न कहीं जीवन में सीख देते हैं। इसीलिए हमारे वहां शिक्षा नहीं बल्कि दीक्षा को महत्व दिया गया और विश्वविद्यालयों में शिक्षा पूरी होने के पश्चात शिक्षांत नहीं बल्कि दीक्षांत समारोह मनाने की परंपरा है। शिक्षा के लिए तो इन्टरनेट पर, बाजार में हर जगह ढेरों पाठ्य सामग्री मिल जायेंगे। आपकी जिस विषय में रूचि हो उसकी पुस्तकें पढ़ डालिए, वीडियो लेकर सुन लीजिये, कुछ ही समय में आप भी उस विषय के अच्छे विद्वान् बन जायेंगे। इसलिए शिक्षा के लिए नहीं बल्कि दीक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की व्याख्या करते हुए कहा भी गया है - गुकारस्त्वन्धकारस्तु रुकार स्तेज उच्यते, अन्धकार निरोधत्वात् गुरुरित्यभिधीयते।
एक मानक के तौर पर गुरु
मानव मन की प्रकृति है कि वो बहुत कुछ ले लेना चाहता है पर लेते समय इसका ध्यान नहीं रख पाता कि वो किस श्रोत या गलियारे से आ रहा है, इसलिए जो कुछ हम ग्रहण कर रहे हैं उसका श्रोत सही हो इसका ध्यान तो रखना ही होगा। गुरु हमारे रोल मॉडल होते हैं, एक ऐसे आदर्श एक ऐसे मानक जिनका जिसका अनुसरण जीवन के हर क्षेत्र में हम करने की इच्छा रखते हैं। उनका आचरण, उनका चरित्र, उनकी प्रकृति हमारे लिए एक मानक तय कर देती है, यही मानक हमें यह अहसास कराती है कि हमारी दिशा सही है या नहीं और कहीं हम भटक तो नहीं रहे। गुरु कौन हो और कैसे हों इस पर भारतीय दर्शन कहता है- विशारदं ब्रह्मनिष्ठं श्रोत्रियं गुरुकाश्रयेत विशारदश् अर्थात् जो अपने आश्रय में शिष्य को लेकर उस पर शक्तिपात करने की सामथ्र्य रखता हो ‘ब्रह्मनिष्ठ’ अर्थात् आचरण की दृष्टि से श्रेष्ठ व ब्राह्मण जैसा ब्रह्म में निवास कर परोक्ष साक्षात्कार कर चुका हो तथा ‘श्रोत्रिय’ अर्थात् जो श्रुतियों से शब्द ब्रह्म को जान सके, तत्वदर्शी हो यानि उनका तत्व समझ सके। सच पूछा जाये तो गुरु के लिए कोई पैमाना तय नहीं किया जा सकता पर गुरु का वरण करते समय इसका ध्यान तो रखना ही चाहिए कि जिनका वरण हम अपने गुरु के रूप में कर रहे हैं उनके भीतर वह तेजस्विता, उच्चता, श्रेष्ठता, उत्तमता है या नहीं जो हमारे जीवनपथ को प्रकाशमान कर सके, क्योंकि दूसरों को प्रकाश भी तो वही दे सकता है जो स्वयं प्रकाशित हो।
जो शेष बचा वही शिष्य है
शिष्य कौन है इसके बारे में जानने के लिए इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई यह जानना आवश्यक है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़े आजकल के लोग हिंदी में प्रयुक्त शब्दों को ठीक से समझने के लिए उसके अंग्रेजी अनुवाद का सहारा लेते हैं इसलिए उनको शिष्य का सही अर्थ नहीं पता होता। दरअसल शिष्य शब्द की उत्पत्ति शेष शब्द से हुई है इसलिए छात्र और शिष्य शब्द की तुलना नहीं की जा सकती। वास्तव में शिष्य शब्द शेष का ही विशेषण है यानि संज्ञा के तौर पर गुरु और विशेषण के तौर पर शिष्य एक खुबसूरत उदाहरण है। पश्चिम की संकल्पना कहती है कि शिक्षा देनी है तो हमें ज्ञान प्रदान करना है। कुछ निश्चित ज्ञान बुद्धि के स्तर पर छात्र के मस्तिष्क में लाना है जबकि भारतीय संकल्पना यह कहती है कि शिष्य का स्वरुप तो ज्ञान का ही है बस उसके ऊपर अज्ञानता का जो आवरण आ चुका है उसे हटा देना है और उसके बाद जो शेष बचा वही तो शिष्य है। हम सब ‘ओम् पूर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते’ श्लोक का उच्चारण अक्सर करते भी हैं पर बहुत कम ही लोग इसके अर्थ पर ध्यान देते हैं। इस श्लोक में गुरु-शिष्य से कहते हैं कि हर व्यक्ति पूर्ण है और पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है। यानि अनंतता में से अनंतता निकाल देने के बाद भी जो शेष बचा वह अनंत ही रहेगा और वही शेष अनंत शिष्य है।
शिष्य की पात्रता
गुरु तत्व की प्रशंसा तो सभी शास्त्रों ने की है पर शिष्यत्व पर चर्चा कम ही हुई है, इसलिए जब गुरु तत्व की चर्चा हो तो शिष्यत्व की चर्चा करनी भी जरुरी है अन्यथा चर्चा अधूरी प्रतीत होती है। शिष्य का एक अर्थ तो शेष होता ही है साथ शिष्य का अर्थ होता है जो सीखने के लिए तत्पर हो और सीखने को तत्पर वही होगा जिसे अपनी जानकारियों का कोई आग्रह या घमण्ड नहीं होगा। ऐसा शिष्य ही साधना में अग्रणी होता है और गुरु के सानिंध्य में आते ही एक के बाद एक पड़ाव पार करता चला जाता है। शिष्यत्व व्यक्ति को उसकी योग्यता के साथ ही साथ पात्रता भी प्रदान करती है। पात्रता की योग्यता के बिना शिष्य का कोई मूल्य भी नहीं है। शिष्यत्व का अर्थ ही होता है शीश को झुकाना, जब गुरु के समक्ष शिष्य अपना शीश झुका देता है तब उसमें गुरु कृपा पाने की पात्रता विकसित होती है और फिर उसके भीतर गुरु की मूल प्रकृति को आत्मसात करने की क्षमता भी जागती है। पात्रता और श्रद्धा, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। जैसे-जैसे पात्रता बढ़ती जाती है। श्रद्धा की गहराई भी बढ़ती जाती है और इसी के साथ गुरु अपने ज्ञान से शिष्य को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। वास्तव में श्रद्धा सर्वप्रथम शिष्यत्व ही जगाती है, तत्पश्चात सामने वाले में अर्थात् जिसके प्रति श्रद्धा है, उसमें गुरुत्व प्रकट हो उठता है। श्रद्धा से ही शिष्यत्व का जन्म होता। जिस स्तर का हमारा शिष्य भाव होगा, उसी स्तर के गहरे गुरुत्व की हमें प्राप्ति होगी।
श्रद्धा की अखंड ज्योति
शास्त्र कहते हैं कि श्रद्धा की सम्पत्ति की रक्षा करना हर शिष्य का काम है और शिष्य की अगाध श्रद्धा में फल-फूल लगाना गुरु का काम है। अत: श्रद्धा की अग्नि को गुरु सेवा के हर अवसर का उपयोग करते हुए कभी भी बुझने ना दें। गुरु के प्रति हमारी जितनी गहरी श्रद्धा होगी गुरु इच्छा पूर्ण करने की भूख हमारे भीतर उतनी ही तीव्रता से उठेगी। भगवान राम के प्रति हनुमान की श्रद्धा इसी की मिसाल है। उनकी वानर सेना में अनेकों लोग थे पर हनुमान को राम से अधिक ‘राम का काज’प्रिय इसलिए लगा क्योंकि उनमें राम के प्रति गहरी श्रद्धा थी। प्रभु नाम का स्मरण एवं प्रभु समर्पण ही उनके जीवन का सार था, इसी श्रद्धामय समर्पण के बल पर उन्होंने अपनी भावना को राम के प्रति गुरुत्वमय पराकाष्ठा पर पहुंचाया सदैव राम के काज को करने के लिए आतुर रहे ‘राम का काज करिबे को आतुर’ इसलिए भारतीय संस्कृति के अनुसार सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखे। गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो, गुरु के प्रति गहरी आस्था रखता हो और गुरु की सच्चे तन-मन भाव से सेवा करता हो। गुरु के प्रति यह श्रद्धा ही शिष्य को उच्च आध्यात्मिकता तक पहुंचाती है और अंतत: अनेकों परीक्षाओं से गुजरता हुआ पूर्ण श्रद्धावान शिष्य ही वास्तविक गुरुकृपा का अधिकारी बनता है, इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा की अपनी अखंड ज्योति को कभी बुझने ना दें।
गुरु शिष्य का सम्बन्ध
गुरु और शिष्य का सम्बन्ध बस वैसा ही है जैसे कि मशाल और उसकी रोशनी, मशाल के बुझते ही रोशनी भी खत्म। प्राचीन समय से ही गुरु-शिष्य का सम्बन्ध अटूट रहा है। गुरु-शिष्य का प्रेम माता-पिता की तरह ही निस्वार्थ होता है। गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा शिष्य सफलता के द्वार तक पहुँच पाता है। संत कबीर ने गुरु और शिष्य का सम्बन्ध कुम्हार और मिट्टी जैसा बताया है। वो कहते हैं- ‘गुरु कुम्हार शिष कुंभ है गढि़-गढि़ काढ़ै खोट, अन्तर हाथ सहार दै बाहर बाहै चोट’ उन्होंने गुरु को कुम्हार की संज्ञा दी है और शिष्य को कच्ची मिटटी से निर्मित घड़ा बताया है। कबीर के अनुसार एक शिष्य कच्ची मिट्टी के सामान होता है और गुरु रूपी कुम्हार उसे बराबर चोट करके उसे घड़े की आकृति देता है। आकृति देने के पश्चात उसे तपाकर सुन्दर पात्रता प्रदान करता है क्योंकि तीव्र आंच पर तपने के बाद ही तो वह घड़ा लोगों की प्यास बुझाने के योग्य बन पाता है अन्यथा वो तो मिट्टी था।
गुरु के सानिंध्य का महत्व
गुरू-शिष्य परंपरा में सानिध्य का बड़ा महत्त्व है। गुरु के सानिध्य में शिष्य अपनी साधना करता है। शिष्य की साधना के सारे प्रयोग व्यवहारिक होते हैं जो कि गुरु की देखरेख और मार्गदर्शन में ही किये जाते हैं अन्यथा उन प्रयोगों का कोई महत्व नहीं, एक सुभाषित है। गुरु एक अक्षर का ज्ञान भी शिष्य को दे दे, तो पृथ्वी पर ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसे देकर शिष्य ऋण मुक्त हो जाए। गुरु हमें अकेले भले ही दिखें किन्तु वे कभी अकेले नहीं होते। उनके साथ देवता से लेकर ग्रह-नक्षत्र ईश्वर तथा ऋषि एवं गुरु परंपराओं की शक्ति सब समाहित होती है। तभी तो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में वह घड़ी बड़ी सुखद होती है, जब उसके जीवन में गुरु प्रकट होते हैं, इसलिए जब कभी भी आपके भीतर शिष्यत्व की जिज्ञासाएं जागें और उस समय समाधान के लिए गुरु का सानिध्य मिल जाये तो उस समय को अपने जीवन का सबसे सौभाग्यशाली पल मानिए। जीवन में गुरु के आगमन का अर्थ ही यही हुआ कि हमारा जीवन सौभाग्य से भर उठे, क्योंकि गुरु अपने आगमन के साथ ही हमें एक पात्र बना देते हैं जिससे हमारी अपात्रता दूर हो जाती है। वे हमें समर्थ बनाते हैं और हमें ‘मैं’ की बेडिय़ों से मुक्तकर ‘जगत’ को सौंप देते हैं।
गुरु शरण का अर्थ
गुरु का सानिंध्य और गुरु की शरणागति दोनों एक दूसरे के पूरक के तौर पर देखे जा सकते हैं। गुरु के सानिध्य में हम साधना करते हैं और शरणागति की स्थिति में पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, कुछ लोगों में यह भय होता है कि गुरु की शरण में जाने का अर्थ है कि अपनी वैचारिक स्वतंत्रता को खो देना, पर यह धारणा गलत है। गुरु की शरणागति का अर्थ परतंत्रता नहीं होती, गुरु तो बस मां के सामान होते हैं। जब बच्चा चलना सीख रहा होता है तो आरंभ में मां उसका हाथ पकडक़र चलाती है और बाद में जैसे ही वह देखती है कि बच्चा कुछ कदम बिना सहारे चल रहा है, वह उसका हाथ छोड़ देती है ताकि वह स्वयं आत्मनिर्भर हो और बिना सहारे के चल सके। इसे ही आप गुरु की शरणागति में जाना कह सकते हैं। इस दौरान मां की भूमिका के साथ ही गुरु अपने शिष्य के लिए एक माली की भूमिका भी निभाता है। माली जब बीज रोपता है तो शुरू-शुरू में उनकी बहुत देखभाल करनी होती है। मिट्टी में खाद डालने के साथ ही, उसको सींचना, थोड़ा बढऩे पर पशु-पक्षियों से बचाना, उसके चारों ओर बाड़ बनाना आदि करता है। धीरे- धीरे पौधे जब जड़ पकडक़र बड़े हो जाते हैं तब उस पौधे को माली के देखभाल की आवश्यकता नहीं रहती तब माली निश्चिन्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब उसके द्वारा तैयार हुआ पौधा स्वयं अपनी देखभाल तो कर ही सकता है साथ ही फलदार वृक्ष बनकर जन कल्याण का कार्य भी कर सकता है। गुरु की शरणागति से बस यही घटना गुरु-शिष्य संबंध में भी घटित होती है।
गोस्वामी तुलसीदास जी तो हनुमान चालीसा की शुरुआत ही गुरु का नाम लेकर करते हैं ‘श्री गुरु चरन सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि’ अर्थात् मैं उस गुरु की चरण रज को धारण करती हूँ जो मेरे मन रूपी दर्पण को साफ कर दे, तब मैं प्रभु के निर्मल यश का गायन करुँगी जो मुझे चार फल प्रदान कर देगा। मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने उस युग में जन्म लिया है जब परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने स्वयं अवतार लिया है और गुरु के रूप में मुझ पर उनकी असीम कृपा सदैव बनी रहती है। तुलसीदास जी ने भी संभवत: जब हनुमान चालीसा में आगे की चौपाई में ‘जै जै जै हनुमान गोसाईं, कृपा करहु गुरुदेव की नाईं’ लिखा होगा तो शायद उनकी कल्पना में भी परम पूज्य गुरुवर जैसी क्षमता वाला ही कोई गुरु रहा होगा। ऐसे में क्या अपने गुरु के बारे में कुछ भी लिखना मेरे लिए शेष रह जाता है क्योंकि मैं तो स्वयं शेष होने के प्रयास में हूँ।
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Nov 2024 17:59:04
जीवन सूत्र (1) जीवन का निचोड़/निष्कर्ष- जब भी बड़ों के पास बैठते हैं तो जीवन के सार तत्त्व की बात...




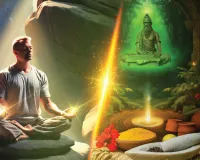





.jpg)