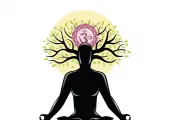शिक्षा क्या है? हमारी शिक्षा पद्धति- भूत, वर्तमान व भविष्य
On

न्यायाधिपति एस.एस. कोठारी
पूर्व लोकायुक्त, राजस्थान
हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी।
आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएँ सभी।। -भारत भारती
स्वराज्य के प्रथम मंत्रदृष्टा, राष्ट्रीय पुनर्जागरण के पुरोधा, सामाजिक क्रान्ति के अग्रदूत व आर्यसमाज के संस्थापक युगपुरुष महर्षि दयानन्द सरस्वती एक सर्वतोमुखी प्रतिभा वाले महापुरुष थे। वे एक विद्वान् शिक्षाविद् भी थे और शिक्षा के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने अपने अमर क्रान्तिकारी ग्रन्थ 'सत्यार्थ प्रकाश’ के तृत्तीय समुल्लास में शिक्षा-अध्ययन-अध्यापन विधि के संदर्भ में विस्तार से विवेचन किया है।
महर्षि दयानन्द के अनुसार 'जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि की बढ़ती (वृद्धि) होवे और अविद्यादि दोष छूटें, उसको शिक्षा कहते हैं’(स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश)। महर्षि दयानन्द का शिक्षा दर्शन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक संस्कृतियों के समन्वय का प्रतीक है। शिक्षा का मुख्य ध्येय मानवमात्र में सुप्तरूप से विद्यमान क्षमताओं का विकास, परिष्करण और परिवर्धन है। साथ ही वह मूल्य बोध भी प्रदान करना है जिसके द्वारा उन क्षमताओं को मानव कल्याण के लिए सृजनात्मक रूप में प्रयुक्त किया जा सके।
शिक्षा शब्द 'शिक्ष्’धातु से निष्पन्न होता है। (संस्कृत धातुकोष पृ. १२०) जिसका अर्थ है- ज्ञान प्राप्त करना या विद्याग्रहण करना। शिक्षा के लिए विद्या शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। विद्या की उत्पत्ति 'विद्’ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। अत: विद्या का अर्थ हुआ- ज्ञान। ईशोपनिषद् के अनुसार विद्या से आशय उस ज्ञान से है जिसको प्राप्त करने के पश्चात् और कुछ जानना शेष न रह जाए। अत: विद्या का अर्थ हुआ- आत्मज्ञान।
महापुरुषों की दृष्टि में शिक्षा
महर्षि दयानन्द ने अपने अनेक ग्रन्थों में शिक्षा/विद्या की परिभाषा प्रस्तुत की है। व्यवहारभानु में वे लिखते हैं-'जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति और अविद्या आदि दोषों को छोड़कर सदैव आनन्दित हो सके, वह शिक्षा कहलाती है’।
'जिससे ईश्वर से लेकर पृथिवी पर्यन्त पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर उनसे यथायोग्य उपकार लेना होता है, उसका नाम विद्या है। जो विद्या के विपरीत है- भ्रम, अन्धकार और अज्ञानरूप है- इसलिए उसको अविद्या कहते हैं। (आर्योद्देश्यरत्नमाला)
'यथाविहित ज्ञान ही विद्या है। प्रज्ञा (यथार्थज्ञान) के विरुद्ध अनेक भ्रम हैं, किन्तु विद्या में भ्रम नहीं होता’। (उपदेशमंजरी)
जिससे पदार्थों को यथावत् जानकर न्याययुक्त कर्म किए जावें, वह विद्या और जिससे किसी पदार्थ का यथावत् ज्ञान न होकर अन्यायरूप कर्म किए जाएँ, वह अविद्या कहलाती है। (व्यवहारभानु)
उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि विद्या में दो मुख्य तत्त्व हैं। पहला है- ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान का वर्धन और दूसरा है- प्राप्त ज्ञान का मानव जीवन के लिए उपयोग करना। इस प्रकार महर्षि के मत में शिक्षा की परिभाषा में विद्या (ज्ञान) की प्राप्ति और उसके आधार पर मानवीय गुणों (सभ्यता, धर्म, शिष्टाचार, संयम) का होना आवश्यक है।
उनके इस विचार का समर्थन महर्षि अरविन्द के इस कथन में मिलता है कि 'ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म आर्ष-शिक्षा के मूल तत्त्व हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए- ऐसी उपयुक्त शिक्षा देना जिससे भावी सन्तान ज्ञानी, सत्यनिष्ठ और विनीत हो’। (योगी श्रीअरविन्द)
डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार भारत सहित समस्त संसार के कष्टों का कारण यह है कि- शिक्षा का संबंध नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति न रहकर केवल मस्तिष्क के विकास से रह गया है। जिस शिक्षा में हृदय और आत्मा की अवहेलना है, उसे पूर्ण नहीं माना जा सकता।
प्राचीन शास्त्रों व उपनिषदों के मनीषियों ने निरन्तर व निश्चयात्मक शब्दों में पुरजोर घोषित किया था कि अज्ञान पाप है। यह बात निरुद्देश्य नहीं है। बेरोजगारी नि:सन्देह दु:खद है पर उससे भी अधिक दु:खद है- अज्ञान। सांस्कृतिक या बौद्धिक जीवन की अवज्ञा करके कोई भी जीवन के उन्नत लक्ष्यों तक नहीं पहुँचा है। किसी भी प्रकार के विकास के लिए शिक्षा प्रथम आवश्यकता है। शिक्षा से ही व्यक्ति में आत्मविश्वास का भाव जागृत होता है। शिक्षा एक ऐसी उपलब्धि है जो कल्पवृक्ष व कामधेनु के समान सकल कार्य सिद्ध करने में समर्थ है।
'विद्याविहीना: पशुभि: समाना:’ बिना शिक्षा के मानव जीवन पशु के तुल्य है। वास्तव में बिना शिक्षा के मनुष्य को न अपने कत्र्तव्य का ज्ञान होता है और न उसकी आन्तरिक और बाह्य शक्तियों का विकास ही होता है। अत: मानव वृत्तियों के विकास तथा आत्मिक शान्ति के लिए शिक्षा परमावश्यक है। शिक्षा से मनुष्य की बुद्धि परिष्कृत और परिमाजत होती है। उसे सत् और असत् का विवेक होता है।
विद्या ददाति विनयं, विनयाद्याति पात्रताम्।
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति, धनाद्धर्मं तत: सुखम्।।
अर्थात् विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है। विनम्रता से योग्यता, योग्यता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। हमारे सुभाषितों में कहा गया है कि 'सा विद्या या विमुक्तये’ अर्थात् विद्या वही है, जो हमें बन्धनों से मुक्त करे।
एक समय था जब हमारी शिक्षा विश्वभर में सर्वोत्कृष्ट थी। मनु ने लिखा है-
एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन:।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा:।।
भारत विद्यागुरु कहलाता था। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने भारत की इसी प्राचीन शिक्षा के संबंध में लिखा था-
सब देश विद्या प्राप्ति को, सतत यहाँ आते रहे।
सुरलोक में भी गीत ऐसे, देवगण गाते रहे।।
हैं धन्य भारतवर्षवासी, धन्य भारतवर्ष है।
सुरलोक से भी सर्वदा, उसका अधिक उत्कर्ष है।।
प्राचीनकाल में हमारे यहाँ शिक्षा नगर के कोलाहल और कलरव से दूर सघन वनों में स्थित महर्षियों के गुरुकुलों और आश्रमों में दी जाती थी। छात्र पूरे पच्चीस वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ तथा गुरु के चरणों की सेवा करता हुआ विविध विद्याध्ययन करता था। इन पवित्र आश्रमों में विद्यार्थी की सर्वांगीण उन्नति पर ध्यान दिया जाता था। उसे अपनी बहुमुखी प्रतिभा के विकास का अवसर मिलता था। विज्ञान, चिकित्सा, नीति, युद्ध कला, वेद तथा शास्त्रों का सम्यक् अध्ययन करके विद्यार्थी पूर्णरूप से विद्वान् होकर तथा योग्य नागरिक बनकर अपने घर लौटता था। उस समय भारतवर्ष समस्त विश्व को ज्ञान का वितरण करता था। विश्व का यह सबसे बड़ा शिक्षा-केन्द्र था। राष्ट्रभाषा देववाणी संस्कृत थी। देश-देशान्तरों से बहुत से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तक्षशिला और नालन्दा विश्वविद्यालय उस समय देश के शिक्षा-केन्द्रों में प्रमुख थे। शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य ज्ञानार्जन करना था। इसलिए सिद्धान्त वाक्य बना कि 'ज्ञान मनुष्य का तृतीय नेत्र है’। उस समय शिक्षा धनोपार्जन का माध्यम नहीं थी। आज हमारी शिक्षण-पद्धति की सबसे बड़ी कमी उसका बदलते हुए परिवेश के साथ कदम से कदम नहीं मिला पाना है। जहाँ शिक्षा को समाज की पुनर्निर्माण में सहायक होना चाहिए, वहाँ वह विषमिले अमृत के समान सिद्ध हो रही है जिससे देश में आत्मविश्वास का अभाव, अन्धविश्वासों का साम्राज्य, जातीय श्रेष्ठता का अभिशाप और साम्प्रदायिकता एवं क्षेत्रीयता का नग्र नृत्य या यों कहें कि वीभत्स ताण्डव परिलक्षित हो रहा है। आजादी के लगभग ७५ वर्ष पश्चात् भी हमारी शिक्षा निरर्थक व त्रुटिपूर्ण है। तभी तो राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त ने इस शिक्षा के संबंध में कहा है-
यह आधुनिक शिक्षा किसी विधि प्राप्त हम कर भी सकें।
तो लाभ क्या बस क्लर्क बनकर पेट अपना भर सकें।।
लिखते रहें जो सिर झुका सुन अफसरों की गालियाँ।
तो दे सकेंगी रात को दो रोटियाँ घरवालियाँ।।
मैकाले ने ब्रिटिश संसद में कहा था कि 'मुझे विश्वास है कि इस शिक्षा-योजना से भारत में एक ऐसा शिक्षित वर्ग बन जाएगा जो रक्त और रंग से भारतीय होगा पर रूचि, विचार और वाणी से अंगेज’। मैकाले द्वारा भारत भूमि पर लगाए इस पौधे ने प्रतिकूल वातावरण में कृत्रिम सांस लेकर हमारी शिक्षा प्रणाली को नष्टप्राय कर दिया है। असंतोषवश छात्र धनार्जन हेतु देश से बाहर जा रहे हैं। हरगोविन्द खुराना व ऐसी ही कई प्रतिभाओं का विकास देश के भीतर न जाने क्योंकर नहीं हो पा रहा है। इस शिक्षा में न प्राचीनता का बोध है और न वर्तमान की क्रांति। न प्राचीनकाल का उच्चाधार तथा गौरव है और न ही वर्तमान की अनुसंधानवृत्ति। न रामकृष्ण, दयानन्द, श्रद्धानन्द व विवेकानन्द की भक्ति है और न ही न्यूटन, आइंस्टीन की सी शक्ति है। ऐसी शिक्षा व्यर्थ है जो असमर्थ को समर्थ, दु:खी को सुखी, बेरोजगार को रोजगार तथा अकर्मण्य को कर्मठ व कत्र्तव्यपरायण न बना सके। युगानुसार शिक्षा का लक्ष्य गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना होना चाहिए किन्तु दुर्भाग्य है कि यह शिक्षा बेराजगारी की जन्मदात्री बन बैठी है। यह सही है कि वर्ष २००२ में संविधान के ८६वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद-२१ ए के भाग-३ द्वारा, ६-१४ वर्ष आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। इसको प्रभावी बनाने के लिए ४ अगस्त, २००९ को लोकसभा में यह अधिनियम पारित कर दिया गया तथा १ अप्रैल, २०१० से इसे लागू कर दिया। अपने इस कदम के साथ ही भारत भी शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देने वाले विश्व के १३५ देशों में सम्मिलित हो गया। परन्तु मात्र अधिकार सृजित करना और इसके पूर्णत: क्रियान्वयन पर ध्यान न देना भी इसके औचित्य को सन्देह के घेरे में लाता है।
वर्तमान शिक्षा प्रणाली का दोष
वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का पहला दोष है कि यह निष्क्रिय तथा यान्त्रिक है। दूसरा दोष है कि यह केवल सैद्धान्तिक प्रणाली है। नैतिक तथा सांस्कृतिक शिक्षा का अभाव वर्तमान शिक्षा प्रणाली का तीसरा बड़ा दोष है। शारीरिक प्रशिक्षण का अभाव, वर्तमान शिक्षा प्रणाली का चौथा दोष है। पाँचवा- प्रदत्त शिक्षा व्यय साध्य है। छठा- यह छात्र के लिए मनोविनोद का साधनमात्र है। सातवाँ- जीविकोपार्जन वाली शिक्षा का अभाव। इन सभी दोषों के अतिरिक्त यह भी यथार्थ है कि इस शिक्षा-प्रणाली से सर्जनात्मकता को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है।
विश्वविद्यालय शिक्षा में निरंतर ह्रास का कारण है- अयोग्य व्यक्तियों को गलत प्रश्रय देना। आज विश्वविद्यालय गंदी राजनीति का क्रीडा-स्थल बन चुके हैं। यहाँ तक की प्राध्यापकों की नियुक्ति अथवा प्रोन्नति भी राजनीति के आधार पर की जाने लगी है। होमवर्क और परीक्षा की तैयारियों में जुटे बच्चे न सूर और कबीर के दोहे याद कर पाते हैं और न वडर््सवर्थ का रहस्यवाद उन्हें समझ आ पाता है।
आज हम जिस शिक्षा परिवेश में जी रहे हैं, वहाँ बचपन से ही बच्चों के कंधों पर उनके अभिभावक अपनी रुचियों के बस्ते का बोझ लाद देते हैं। एक छात्र क्या बनना चाहता है, उसकी क्या रुचियाँ हैं, इन बातों को अधिकांश अभिभावक वस्तुत: जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं और हम देखते हैं कि अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर आदि बना देने की उनकी चाह उन बच्चों को भविष्य में तोड़कर रख देती है और कई बार वे निराशा के गर्त में आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम भी उठा लेते हैं।
सरकार की शिक्षा नीति में भी एक कमजोर पक्ष यह भी दृष्टिगत होता है कि वह लोगों को शिक्षित न बनाकर साक्षर बनाने पर ही अधिक जोर दे रही है और अन्ततोगत्वा हमारी उच्च-शिक्षा प्रणाली का हाल यह है कि हम पढ़े-लिखे मजदूर तैयार कर रहे हैं। हम एक ऐसी शिक्षा-पद्धति में प्रवेश कर गए हैं, जहाँ मानवीय मूल्यों के दांव पर इंसान को मशीन बनाया जा रहा है। हमारे विज्ञान और तकनीकि ने हमें चांद पर भले ही पहुँचा दिया हो मगर हमारे अंदर के संवेदनशील इंसान को मार डाला है।
यह अवश्य प्रसन्नता की बात है कि भारतीय सॉफ्टवेयर पेशेवर को ग्लोबल ब्रांड के तौर पर स्थापित कर चुके हैं और उन्हें आई.टी. के क्षेत्र में उच्च स्तरीय तथा भरोसेमंद रियायती सेवा का प्रतीक माना जाता है। सुपर शक्ति बनने की भारत की आकांक्षा की राह में ये सर्वाधिक उपयुक्त वाहन साबित हो सकते हैं किन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के ७० वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी हमारी शिक्षा-प्रणाली पूर्ववत बनी हुई है। इतना अवश्य है कि पिछले ७० वर्षों में शिक्षा-पद्धति में सुधार एवं परिवर्तन हेतु आवश्यक सुझाव देने के लिए आयोग गठित किये गए, कई गोष्ठियां आयोजित की गईं और कई समितियां नियुक्त की गईं, उनकी रिपोर्ट और संस्तुतियां भी प्राप्त हो चुकी हैं, परन्तु नतीजा वही है, ढाक के तीन पात। हमारी शिक्षा-प्रणाली पूर्ववत क्लर्कों के उत्पादन की फैक्टरी बनी हुई है। शिक्षा की वर्तमान प्रणाली में एक कमी यह है कि जो मस्तिष्क विचार करना नहीं जानता है, उसे तथ्यों से भर दिया जाता है। सबसे पहले विद्यार्थी को अपने मस्तिष्क को नियन्त्रित करना सिखाया जाना चाहिए और उसके उपरान्त ही वह यथावश्यक तथ्यों को एकत्रित करें। सिखाने में ज्यादा समय इसी कारण लगता है क्योंकि विद्यार्थी अपने मस्तिष्क को एकाग्रचित्त नहीं कर पाता है।
शिक्षा का महत्त्व व्यक्ति की स्मरण शक्ति के विकास में निहित नहीं अपितु उसके समूचे व्यक्तित्व के उत्कर्ष में है। शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिकता का विकास करना ही नहीं बल्कि व्यक्ति की आध्यात्मिकता का विकास करने में है। शिक्षा मानव में सहयोग, श्रमप्रियता, रचनात्मक कार्यों में लगाव, बौद्धिक जागृति एवं अच्छे नागरिक बनने की क्षमता उत्पन्न करने में समर्थ होनी चाहिए।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें चाहिये, वह शिक्षा जो प्राचीन गौरवशाली परम्पराओं को स्मरण कराती हुई नैतिक मूल्यों को महत्त्व प्रदान करें। आगे आने वाले युग में असम्भव कल्पना का स्थान ठोस वास्तविकता लेगी जो विज्ञानसम्मत होगी। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर उन्हें समझाना होगा कि जीवन को वैज्ञानिक बना देने वाले देश हमसे कितने आगे हैं। हमारे पास वह सांस्कृतिक धरोहर है जो जापान, फ्रांस, अमेरिका आदि के पास नहीं है। उसे सुरक्षित रख वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर हमें 'सोने की सुगन्धÓ की कहावत चरितार्थ करनी होगी। देश के विकास एवं समृद्धि के लिए निष्ठावान्, कत्र्तव्यपरायण तथा सच्चरित्र विद्यार्थियों की आवश्यकता है जो विज्ञान, सदाचार एवं नैतिक मूल्यों से युक्त शिक्षा के संस्कारों से ही संभव है।
प्रासंगिक प्रश्न यह है कि जीवन में सफलता और सार्थकता में पारस्परिक संबंध क्या है? वे किस सीमा तक अन्योन्याश्रित हैं और सार्थकता के अभाव में सफलता का कोई औचित्य है भी अथवा नहीं? कामयाबी के पीछे नहीं, काबिलियत के पीछे भागो। थ्री इडियट्स फिल्म का यह संवाद इस फलसफे को बहुत हद तक स्पष्ट करता है। ऐसा ही कुछ फलसफा है मानव जीवन का। यूँ तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बेहतर कर उसे सार्थकता प्रदान करने की कोशिश करता है, पर ऐसे कुछ लोग ही होते हैं जो महज वक्त के साँचों में ढलने की बजाय अपने पुरुषार्थ, अध्यवसाय और प्रतिबद्धता के माध्यम से वक्त के साँचों तक बदल देेने की कूवत हासिल कर लेते हैं। निश्चय ही ऐसे विशिष्ट लोग महज सफलता के पीछे नहीं भागते। दरअसल सफलता एक वस्तुनिष्ठ या सपाट धारणा न होकर एक जटिल एवं सापेक्षित धारणा है। सफलता की धारणा का न तो कोई रटा-रटाया फार्मूला है और न ही कोई पूर्व निर्धारित मापदण्ड। किसी व्यक्ति को डॉक्टर या इंजीनियर बनकर १२-१५ लाख का वार्षिक पैकेज लेना सफलता प्रतीत होती है, तो कोई जरूरतमंद के काम आकर उसकी सहायता करने में ही सफलता का अहसास करता है। जिस तरह विद्या वही है, जो विमुक्त करें, उसी तरह सफलता वही है, जो आपको संतुष्ट करें और सुकून दे। यह निर्विवाद है कि महज भौतिक विकास ही नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी मनुष्यता के लक्ष्य हैं। ऐसे कई उदाहरण देखे जा सकते हैं, जहाँ व्यक्ति सफल तो है पर संतुष्ट नहीं। अत: शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए-भौतिक उन्नति के साथ-साथ संतुष्टि व सार्थकता। जिस प्रकार किसी वृक्ष की शाखाओं, पत्तों, फूलों और उसके फलों के विकास के लिए उस वृक्ष की मूल जड़ को स्वच्छ-स्वस्थ रखना अनिवार्य होता है, उसी प्रकार मानव जीवन के कार्यक्षेत्र के हरेक पहलुओं को नैतिक शिक्षा द्वारा स्वच्छ रखना अति आवश्यक है।
स्वभाषा का महत्त्व
आज तो विडम्बना यह है कि हम अपनी भाषा में बोलते हुए भी संकोच करते हैं और कई बार तो उसका अज्ञान प्रकट करके गर्व का अनुभव भी करने लगते हैं। जब तक हमारे विद्यार्थी यह न समझेंगे कि 'बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय को सूल’, तब तक वे अपने देश को कैसे पहचानेंगे? अपनी भाषा में बालक द्वारा ज्ञानार्जन की गति भी तीव्र होगी और वह अपने देश की मिट्टी पहचानने का अभ्यास होगा। यह सत्य है कि भारत के उभार का एक बड़ा उपकरण अंगे्रजी रही है, वह भाषा विवादों में तटस्थ निर्णायक की तरह मान्यता भी पाती रही है, भारत का हित सोचने वाले किसी भी नीति-निर्माता को अंग्रेजी की इस भूमिका से एतराज नहीं हो सकता। पर हमें सोचना ही होगा कि मातृभाषा के रूप में अंग्रेजी को अपनाकर कहीं हम बच्चों के पैर में एक भारी पत्थर तो नहीं बाँध दे रहे हैं और फिर उससे दौडऩे, उछलने और मुक्त होने की अपेक्षा भी कर रहे हैं। भारत की नवोन्मेषी प्रतिभा पर सबसे बड़ा भार अंग्रेजी है, यह बात भारत के नीति-निर्माताओं को कब समझ में आएगी? आयरलैंड, इजराइल, डेनमार्क, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देशों ने भारत के मुकाबले ज्यादा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, सिर्फ इसलिए कि इन दोनों ने अपनी मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया जबकि इन देशों की जनसंख्या भारत के एक बड़े जिले के बराबर ही है।
शिक्षा को सक्षम बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करनी होगी ताकि भीषण रूप से व्याप्त शैक्षिक विषमता समाप्त की जा सके। गाँव के सरकारी स्कूल और मिशनरी स्कूलों के बीच जो सारभूत अंतर है, वह एक ही राष्ट्र में दो देश पैदा कर रहा है। इसे 'इंडियाÓ एवं भारत का अंतर कहा जा सकता है। हमारे पाठ्यक्रम इस प्रकार के हों, जिनमें स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय ज्ञान को प्रमुख स्थान प्राप्त हो। हम ऐसे नागरिक तैयार करने पर शक्ति लगाएँ जो भारतीय पहले हों, अन्य कुछ बाद में। हम जितना ही अन्तर्राष्ट्रीय बनने की बातें करते हैं, उतने ही अराष्ट्रीय होते जा रहे हैं। हमें ऐसे पढ़े-लिखे नागरिक नहीं चाहिए जो भारत के अतीत को असभ्यों का इतिहास बताएँ और पश्चिम को समस्त ज्ञान का स्रोत मानें। हमें तो ऐसे विद्या-विनय सम्पन्न भारतीयों की आवश्यकता है जिन्हें यह तथ्य हृदयंगम एवं आत्मसात् हो कि ज्ञान का सूर्य पूर्व में ही उदय होता रहा है तथा उसने अपनी ज्ञान रश्मियाँ सर्वप्रथम भारत के प्रांगण में ही विकीर्ण की थीं।
यदि शिक्षा, रोजगार की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो, तो ऐसी शिक्षा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। महान् विचारक प्लेटो ने कहा था-'जिस दिशा में शिक्षा व्यक्ति की शुरूआत करती है, उसी दिशा में जीवन में उसके भविष्य का निर्धारण भी करती है।‘
आत्मनिर्भरता का सोपान 'शिक्षा’
रोजगारपरक शिक्षा का भारत के आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और प्रजातान्त्रिक विचारधारा को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान हो सकता है, बशर्ते इसके प्रति लोगों को जागरूक बनाया जाए। शिक्षा को आजीविका से जोडऩे के लिए सर्वप्रथम यह सर्वेक्षण होना चाहिए कि भारत में किस प्रकार की आजीविका की संभावना है। इन संभावनाओं को जानने के पश्चात् हमें अपने शिक्षण-प्रशिक्षण को उसी तरह ढालना चाहिए। यदि आगामी वर्षों में शिक्षकों व चिकित्सकों की आवश्यकता है तो तत्संबंधी पाठ्यक्रम खोले जाने चाहिए। यदि कम्प्यूटर-कर्मी, इंजीनियर, उद्योग-कर्मी या सैनिकों की आवश्यकता हो तो तत्सम्बंधी पाठ्यक्रम खोले जाने चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहले आजीविका के स्रोत खुलें, तभी तदनुसार प्रशिक्षण या साधनों का प्रश्न आता है। दुर्भाग्य से हो यह रहा है कि अवांछित प्रशिक्षकों की एक फौज सी तैयार हो रही है। परिणामस्वरूप बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर रही है। वर्तमान में बी.ए., बी.कॉम., बी.एस.सी., एम.ए., एम.कॉम., एम.एस.सी. के नाम पर जो तथ्यात्मक शिक्षा दी जा रही है, वह सारगर्भित न होकर एक छलावा सा है और छात्र में श्रम के प्रति अभिरूचि ही उत्पन्न नहीं होने देती है।
आज जब हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था पर दृष्टिपात करते हैं तो हस्तामलकवत् (हाथ में रखे आँवले की तरह स्पष्ट) प्रश्नचिन्ह उपस्थित होता है कि क्या यह शिक्षा व्यवस्था देश के नवयुवकों को सार्थक जीवन के लिए सक्षम बना रही है? क्या इससे अन्धकार का विनाश हुआ है और क्या शिक्षित वर्ग के लोग जीवन संग्राम में सफल भूमिका निभाने के लिए समर्थ बन पाए हैं? थियोडर रूजवेल्ट का कहना है कि 'एक व्यक्ति के मस्तिष्क को शिक्षित कर देना किन्तु उसके अंदर नैतिक शिक्षा का समावेश न करना समाज के लिए एक संकट को आमंत्रण देना है’।
शिक्षा में गुरुजनों की भूमिका
एक महत्त्वपूर्ण बात मेरे विचार में यह आ रही है जो अभिभावकों एवं गुरुजनों से सम्बन्धित है कि यह छात्र-छात्राओं की कोई बात आपको पसन्द न आएँ या उसके विचार आपके विचारों से मेल न खाएँ तो आपका दृष्टिकोण क्या रहता है? क्या हममें इतनी उदारता होती है कि छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व का सम्मान कर हम शान्ति के साथ उनके दृष्टिकोण पर विचार करें और यह गुंजाइश रखें कि उनका मत हमसे भिन्न होते हुए भी सही हो सकता है। क्या हम अपने व्यवहार पर बालक को टीका करने का अधिकार देते हैं और उसकी टिप्पणी पर, उसके सुझाव पर सम्मानपूर्वक विचार करने की उदारता रखते हैं? क्या हम अपने विचारों को उस पर न थोपकर, उनसे उसको न जकड़कर उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास में सहायक होने को तैयार हैं? २१वीं सदी हमारी इस अगली पीढ़ी की सदी है, हमारा वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी है।
शिक्षकों का विद्यार्थियों के जीवन में महत्त्वपूर्ण योगदान है। कहा गया है 'मातृमान् पितृमान् आचार्यवान् पुरुषो वेद:Ó आचार्य को समाज का निर्माणकत्र्ता एवं राष्ट्र के भावी कर्णधारों का उन्नायक कहा गया है। अध्यापक एक सभ्य समाज एवं राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला के स्थापनाकत्र्ता होते हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वाल्मीकि, शौनक, अगस्त्य, कपिल, परशुराम, द्रोणाचार्य, संदीपनि तथा पाणिनी जैसे अनेक महान् शिक्षकों ने ऐसे अनगिनत व्यक्तित्वों का निर्माण किया, जिन्होंने आगे चलकर विस्तृत साम्राज्य एवं शांतिपूर्ण समाजों को अस्तित्व प्रदान किया। शेष विश्व में भी सुकरात, प्लेटो, अरस्तू, रुसो, वाल्टेयर, दांते आदि जैसे अनेक अध्यापक हुए, जिन्होंने विभिन्न देशों में राष्ट्रीय एवं सामाजिक क्रांतियों का बीजारोपण किया। इन क्रांतियों के फलस्वरूप नवीन समाजों व राष्ट्रों का जन्म हुआ। अरस्तू के बिना सिंकदर, द्रोणाचार्य के बिना अर्जुन, रामकृष्ण परमहंस के बिना विवेकानन्द तथा गुरु विरजानन्द के बिना दयानन्द आदि की मूल प्रतिभा, संकल्प शक्ति एवं पूर्ण कार्यक्षमता का व्यावहारिक उपयोग असंभव था।
यह निर्विवाद है कि बालक स्कूल में जाने के साथ ही अपने शिक्षक की बात को माता-पिता की बात से अधिक मानता है। इस कारण गुरु का उत्तरदायित्व माता-पिता से भी अधिक हो जाता है। गुरु का बच्चे पर ऐसा प्रभाव होता है कि उसका प्रत्येक शब्द बालक के लिए उद्बोधक बन जाता है। उसे यह ज्ञान होता है कि किन-किन क्रियाकलापों से विद्यार्थी का शरीर स्वस्थ, उसका मानस संतुलित, उसकी भावना ऊध्र्वगामी हो, उसके ज्ञान का संवर्धन होता रहेगा। फ्राबेल ने कहा था कि बालक एक पौधा है, विद्यालय एक बगीचा है तथा शिक्षक एक माली है। बाग में माली अपने पौधों की जिस प्रकार देखभाल करता है, उसी प्रकार शिक्षक में नन्हें बालक रूपी पौधों को संवारकर आदर्श नागरिक के रूप में तैयार करता है। महर्षि अरविन्द की पुस्तक 'महर्षि अरविन्द के विचार’ में शिक्षक के संबंध में लिखा है-'अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति के माली होते है, वे संस्कार की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से उन्हें सींच-सींच कर महाप्राण शक्तियाँ बनाते हैं।’ इटली के एक उपन्यासकार ने शिक्षक के बारे में कहा है कि शिक्षक उस मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। वह ऐसा प्रकाशपुंज है जो अपने व्यक्तित्व की आभा से विद्यार्थी और तद्द्वारा समाज एवं राष्ट्र को प्रदीप्त करता है किन्तु इन सबके लिए यह भी वांछनीय है कि शिक्षक और शिष्य में निरन्तरता बनी रहे और यह संबंध व्यक्तिगत स्तर पर हो।
प्राचीनकाल में शिक्षकों को समाज द्वारा सर्वोपरि सम्मान दिया जाता था, जिसका आज अभाव परिलक्षित हो रहा है। सीमित सुविधाओं में अत्यधिक उत्तरदायित्व के निर्वहन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण शिक्षक ही है। एक कक्षा में अगिनत बच्चों की देखभाल और साधनों की उपलब्धि में कठिनाइयाँ। ऐसी स्थिति में हम सबका शिक्षकों के प्रति कुछ कत्र्तव्य है जिसका निर्वहन करते हुए यह शुभाशंषा की जा सकती है कि शिक्षकगण को समाज में सर्वोत्तम सम्मान प्राप्त हो और वे अपनी नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा से ज्ञान के दीपक सतत प्रज्ज्वलित करते रहें।
विद्यार्थी का लक्ष्य व स्वरूप
जहाँ तक विद्यार्थीगण का संबंध है, उनका लक्ष्य होना चाहिए-विद्याध्ययन के साथ-साथ विविध ज्ञान प्राप्त कर अनुशासन के साथ अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। विद्यार्थी जीवन ही समस्त मानव जीवन की आधारशिला है जिस पर ज्ञान का भवन भली प्रकार खड़ा हो सकता है। एक विद्वान् ने ठीक ही कहा है कि 'किसी भी देश का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता हैÓ। बाल्यकाल में पडऩे वाले संस्कार अमिट होते हैं। चारित्रिक गुण ही व्यक्ति को जीवन की उच्च अट्टालिकाओं पर पहुँचा सकते हैं। चारित्रिक गुणों का कायदा है कि वे पश्चातवर्ती जीवन में किसी पर लादे नहीं जा सकते वरन् छात्र जीवन में अन्तर् में अंकुरित होते हैं। किसी भी प्रकार का विषय ज्ञान समय के साथ भूला जा सकता है परन्तु चरित्र निर्माण के विद्यालयी जीवन में पडऩे वाले अनुभव चिर-स्थायी हो जाते हैं। विद्यालय वह पावन कर्मस्थली है जहाँ अर्जित किया हुआ ज्ञान आजीवन विद्यार्थी के साथ रहता है। गुरुजनों का आदर, समय का सदुपयोग, सत्य व ईश्वर में आस्था तथा समाज एवं राष्ट्र की सेवा में सर्वस्व अर्पित करने की भावना वे जीवन मूल्य हैं जिन्हें विद्यालयीय जीवन में ही आत्मसात् किया जाता है।
संस्कृत साहित्य में आदर्श विद्यार्थी के पाँच लक्षणों का वर्णन मिलता है-
'काकचेष्टा बकध्यानं, श्वाननिद्रा तथैव च।
अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थि-पंचलक्षणम्।।’
अर्थात् कौए की सी चेष्टा, बगुला का सा ध्यान, कुत्ते की सी निद्रा, थोड़ा खाने वाला (अल्पाहारी) और घर से मोह न रखने वाला आदर्श विद्यार्थी है।
विपदाएँ समक्ष आती हैं तो ये पंक्तियाँ ध्यातव्य हैं-
जितना कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला।
गौरवगंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला।।
वही समाज सुव्यवस्थित है और वही राष्ट्र सुरक्षित है जहाँ का विद्यार्थी संयमी, सतर्क और सुविचारी है। जिस प्रकार सेना को एक छोटा सा सैनिक पूर्णत: ऐसे अनुशासित होता है कि सारी सेना का उस पर गर्व तथा विश्वास होता है, उसी प्रकार नैतिक, धार्मिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा से युक्त विद्यार्थी अपना कत्र्तव्य सच्ची निष्ठा के साथ भली प्रकार सम्पादित कर अपने विद्यालय तथा देश का गौरव बढ़ा सकता है।
सभी छात्र-छात्राओं के लिए जितना अध्ययन एवं अन्य कार्य आवश्यक है, उतना ही व्यक्तित्व को विकसित करने वाली अन्य गतिविधियाँ भी। भाषा की उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने हेतु तथा किसी विषय पर विचार अभिव्यक्त करने की कला को विकसित करने हेतु वाद-विवाद प्रतियोगिता का अप्रतिम महत्त्व है जो इस पीढ़ी को भविष्य में नेतृत्व प्रदान करने के लिए तैयार करता है। एक विद्यार्थी अपने ज्ञान का अधिकाधिक संवर्धन करें और लेटेस्ट डवलपमेंट से भी वाकिफ रहे। इसके प्रकाश में क्विज कान्टेस्ट का अपना महत्त्व है। हस्तकला, ड्राइंग, पेंटिंग आदि इस भौतिकवादी युग में भी जीवित रहें, इस उद्देश्य से चित्रकला आदि भी अत्यन्त उपयोगी है। खेलों में अभिरुचि जागृत करना भी आवश्यक है। ईश्वर ने संसार को क्रीडांगन के रूप में रचा है। इन्हीं खेलों की भाँति जीवन भी एक खेल है, इसे सफलतापूर्वक खेलना, जय-पराजय में समान रहना, यह हमें खेल ही सिखाते हैं और शिक्षा देते हैं- साहस, धैर्य एवं सहनशक्ति की।
विद्यार्थियों को समझना होगा कि पड़े हुए १००/- रुपये के बजाए अपने द्वारा कमाया एक रुपया अधिक मूल्यवान् है। जीवन में अनुचित साधनों से पैसा कमाकर धनाढ्य व सफल होने के बजाए असफल होना बेहतर है। किसी दूसरे व्यक्ति की प्रगति में ईष्र्या नहीं कर उनकी उन्नति व उत्कर्ष में भागीदार बनना सकून एवं सन्तुष्टि देने वाला है किन्तु साथ ही यह भी कि अपने जीवन से संबंधित कोई भी महत्त्वपूर्ण निर्णय से पहले सुनें सबको किन्तु निर्णय स्वविवेक से लें और तदनुरूप कार्य करें। सत्य के कपड़े में छानकर शुभ को समक्ष लाना प्रत्येक विद्यार्थी का कत्र्तव्य है।
यह भी ध्यातव्य है कि जीवन में सुख और शान्ति पाने का एकमात्र उपाय पुरुषार्थ व परिश्रम है। परिश्रमरूपी पथ पर चलने वाले विद्यार्थी को जीवन मेें सफलता, संतुष्टि, उन्नति और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। आलसी विद्यार्थी जीवन भर कुण्ठित और दु:खी रहता है क्योंकि वह सब कुछ भाग्य के भरोसे पाना चाहता है। एक कवि के शब्दों में:-
लो भाग अपना शीघ्र ही, कत्र्तव्य के मैदान में,
हो बद्ध परिकर दो सहारा, देश के उत्थान में।
डूबे न देखो नाव अपनी, है पड़ी मझधार में,
होगा सहायक कर्म का पतवार ही उद्धार में।
जीवन को सुन्दर ढंग से जीने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी सलक्ष्य जीये। लक्ष्यहीन जीवन, समुद्र में पड़ी उस तरी के समान है, जिसे लहरों के थपेड़े, जहाँ चाहे, ले जाते हैं। अक्सर ऐसी नाव लहरों के थपेड़ों के मध्य घिरकर नष्ट हो जाती है। सच बात तो यह है कि जीवन में रस तभी आता है, जब विद्यार्थी के सामने कुछ उद्धेश्य होता है। उस उद्धेश्य को पा लेने की चुनौती ही उसके हृदय में उमंग और उत्साह को जन्म देती है। इसलिए कविवर हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि-पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर लें।
आज शिक्षा की सुई या तो रुढि़वादिता की तरफ झुकती है और नवीनता की विरोधी चेतना तैयार करती है या अंधी आधुनिकता की तरफ झुककर तथाकथित विकास की अंधेरी गली में ले जाने का प्रयत्न करती है। यह आवश्यक है कि सम्यक् शिक्षा का रश्मिपुंज उपयोग में आए जो सार्थक आधुनिकता का मार्ग प्रशस्त करें। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जहाँ हम अपने स्वार्थों के लिए नहीं बल्कि समाज कल्याण के लिए अध्ययन करें। भारत जो कि नई विश्व व्यवस्था में अपनी सम्मानजनक जगह बनाने के लिए प्रयासरत है, उसे अपनी जड़ औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली की पुन: संरचना करने की सबसे अधिक जरूरत है, क्योंकि भारी विषमता से ग्रस्त भारतीय समाज में नवोन्मेषी भारतीयों को तैयार करना भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।
इस परिप्रेक्ष्य में ज्ञान के आलोक से अज्ञानान्धकार को दूर करने की भावना मन से लेकर ऐसे ज्ञान दीपक को प्रज्ज्वलित रखने वाले व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र की अक्षयश्री कहे जा सकते है और यह सुविदित है कि प्राचीन एवं अर्वाचीन शिक्षा की उत्कृष्टता को गति देने हेतु श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज एवं उनके साथ सम्बद्ध विभूतियाँ आचार्यकुलम् आदि के माध्यम से अभूतपूर्व कार्य कर रही हैं। निश्चित ही ये आचार्यकुलम् पूज्य स्वामी जी के कर्म के ओज से ओजमय एवं उनके संरक्षण के दैदीप्त से प्रकाशित हो संस्कारों की नींव पर समर्पण के खम्भों के सहारे पल्लवित-पुष्पित हो नए आयामों को स्पर्श करेंगे एवं उपलब्धियों की अजस्र निर्झरणी बहा समाज को सुवासित करेंगे।
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Nov 2024 17:59:04
जीवन सूत्र (1) जीवन का निचोड़/निष्कर्ष- जब भी बड़ों के पास बैठते हैं तो जीवन के सार तत्त्व की बात...