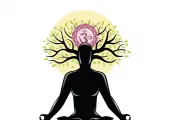योग क्या है?
On

डॉ. साध्वी देवप्रिया,
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्षा- दर्शन विभाग पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार
युग पुरुष, युग निर्माता, युगद्रष्टा, योगऋषि परम पूज्य श्रद्धेय, वन्दनीय स्वामी जी महाराज के अखण्ड-प्रचण्ड पुरुषार्थ से इस युग में एक अभिनव योगक्रान्ति का उदय हुआ तथा इसके साथ ही माननीय प्रधानमन्त्री जी के नेक संकल्प से आज भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनियाँ योग की शरण में आयी है व शेष आने को तैयार है या यूँ कहें कि आने को बाध्य है। २१ जून अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं, किन्तु यहाँ विचारणीय यह है कि क्या योग मात्र एक दिन अभ्यास करने के साथ ही समाप्त हो जाता है? क्या प्रतिदिन सुबह-सुबह एक या दो घण्टे व्यायाम-प्राणायाम करने का नाम ही योग है? क्या सुबह-शाम व्यायाम-प्राणायाम के साथ-साथ यज्ञ-हवन-ध्यान आदि करने का नाम ही योग है? अवश्य उपरोक्त सभी अभ्यास योग के अंश हैं, मगर योग की समाप्ति नहीं हैं, इससे आगे योग का बहुत विस्तार है। योग के विषय में जो अत्यन्त प्रचलित प्रसिद्ध शास्त्र के प्रमाण हैं वे 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:’, 'योग: समाधि:’, 'समत्वं योग उच्यते’, 'योग: कर्मसु कौशलम’ इत्यादि हैं इसके साथ-साथ षड्दर्शन, एकादशोपनिषद् व वेदों में योग का विशद् वर्णन है।
यह वर्णन आज से नहीं सदियों से है। लेकिन, योग के सैकड़ों-हजारों प्रमाणों का स्मरण करने से बेहतर है योग का यथाशक्ति क्रियात्मक अभ्यास करना। श्रद्धेय आचार्य जी कहते हैं कि सैकड़ों हजारों शब्दों की ध्वनि से एक कर्म की ध्वनि महान् होती है और पतञ्जलि योगपीठ इसका साक्षात् प्रमाण है। आज पतञ्जलि का जो विस्तार हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, वह सब योग के क्रियात्मक अभ्यास का ही प्रतिफल है। अत: आइये जानें कि योग के विषय में प्राचीन व वर्तमान ऋषियों का क्या कहना है?
वर्तमान युग में योग के प्रामाणिक ऋषि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि योग का प्रारम्भ सद्विचार से होता है और समाप्ति सदाचरण पर होती है। अर्थात् जो सिद्धान्त आचरण में नहीं उतरते वे जीवन में कोई परिवर्तन घटित नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक यही बात योग के प्रणेता परम-ऋषि पतञ्जलि भी कहते हैं। वे अपने शास्त्र का प्रारम्भ ही वृत्ति अर्थात् विचार के निरोध से करते हैं 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:’। क्योंकि जैसा हमारा विचार होता है, वैसी ही अन्दर भावना निर्मित हो जाती है, जैसी भावना होती है वैसा ही हमारा वाणी, व्यवहार व आचरण होता है, जैसा हमारा आचरण होता है वैसी ही हमारी आदतें बन जाती हैं, आदतें ही सुदृढ़ होकर हमारा स्वभाव, प्रकृति या रवैया बन जाता है और स्वभावानुसार हम जो कार्य करते हैं वह हमारा भाग्य (कर्माशय) बन जाता है और जैसा कर्माशय वैसा ही हमारा यह जन्म और अगला जन्म होता है।
अत: इस अनादि व अनन्त चक्र को यदि तोडऩा है अपने नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, आनन्द स्वभाव में यदि प्रतिष्ठित होना है तो योग की शरण में आना अनिवार्य है और उसकी शुरुआत हमें विचार से करनी है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है, यह स्वत:ज्ञात (Understood) ही है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन व स्वस्थ विचार हो सकता है।
इसलिए शरीर का स्वस्थ होना तो अनिवार्य है ही। उसके पश्चात् महर्षि कहते हैं कि पहले क्लिष्टवृत्ति को त्यागकर अक्लिष्ट वृत्ति में प्रवेश कर जाओ, वर्तमान की भाषा में कहें तो पहले नकारात्मक या दु:ख देने वाले तमाम विचारों से स्वयं को मुक्ति दिलाकर सकारात्मक अर्थात् स्वयं को व दूसरों को सुख देने वाले विचारों में प्रतिपल जीने का अभ्यास करें, न कि केवल सुबह-शाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की भाषा में कहें तो उच्च-चेतना, ऋषि चेतना, गुरु चेतना, दिव्य चेतना या भागवत चेतना में जीने का सतत अभ्यास करें न केवल सुबह-शाम।
क्योंकि यदि किसी पौधे को सुबह-सुबह तो गंगाजल से सींचें और दिन में उस पर तेजाब डाल दें तो बेचारा जल ही जायेगा। इसलिए पानी भले सुबह-सुबह ही डाल दें मगर दिन में उसे हानिकारक तत्त्वों से बचायें यह ध्यान अवश्य रखें। इसी प्रकार योग-प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास यदि सुबह-सुबह या सुबह-शाम करें तो पर्याप्त है मगर दिन भर में अपने अन्दर कोई बुरा विचार प्रवेश न करे इसका भी बराबर ध्यान रखें। इसी को महर्षि पतञ्जलि कहते हैं- 'अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोध:’ अभ्यास का अभिप्राय है प्रतिपल चित्त की प्रशान्तवाहिता बनाये रखने का यत्न। योगी के चित्त की स्थिति बाहर की तमाम परिस्थितियों पर हावी रहती है जबकि सामान्य व्यक्ति के चित्त की स्थिति पर बाहर की परिस्थितियाँ हावी हो जाती हैं। उसके लिए जैसी बाहर की परिस्थिति, वैसी उसके चित्त की स्थिति और योगी के लिए जैसी प्रशान्त उसके चित्त की स्थिति, वैसी ही प्रभावहीन बाहर की परिस्थितियाँ बन जाती हैं।
वैराग्य का अभिप्राय है तमाम वस्तुओं व व्यक्तियों को अनित्य व परिवर्तनशील जानकर आसक्ति का त्याग करके, सब कुछ ईश्वर का भगवद् स्वरूप जानकर प्रीतिपूर्वक व श्रद्धापूर्वक सदुपयोग करना। यह योग का अभ्यास कब तक व कितने दिन करना पड़ेगा? इसका उत्तर है जब तक जिन्दा रहें तब तक या फिर यूँ कहें कि अगले जन्मों में भी जब तक मोक्ष को प्राप्त न कर लें तब तक या फिर यूँ कहें कि जब तक आप अपने शान्त स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनन्द स्वरूप में प्रतिष्ठित रहना चाहें तब तक। जब आप दु:ख, अशान्ति, तनाव आदि में जीना पसन्द करें तब योग का परित्याग कर सकते हैं। इस सदी के महान् सन्त श्रद्धेय स्वामी सोमानन्द जी महाराज कहते थे 'भाई हमारा चरित्र कितना ऊँचा व महान् था यह तो उस दिन पता चलेगा, जिस दिन मैं इस संसार से विदा हो जाऊँगा।‘ इतने महान् सन्त की भी यह प्रतिबद्धता है कि एक दिन भी उस जगज्जननी से दूर हुए तो चकनाचूर हो सकते हैं। फिर सामान्य व्यक्ति की जागरूकता का तो क्या ही कहना।
मगर हाँ, इतनी बात अवश्य है कि कुछ दिन यदि योग का आन्तरिक व बाह्य अभ्यास कर लिया जाये तो वह हमारा स्वभाव बन जाता है और फिर जैसे स्थूल शरीर को मोडऩा-तोडऩा सहज व सरल हो जाता है उसी प्रकार योगी अपने चित्त को भी अनावश्यक या बाधक विषयों से हटाकर सहज ही ईश्वर की तरफ मोड़ देता है। इसके साथ ही महर्षि पतञ्जलि ने और भी कई उपाय बताये हैं, अपने गुण, कर्म, स्वभाव व चित्त की स्थिति के अनुसार हम उनका चयन कर सकते हैं, यथा-'ईश्वरप्रणिधानाद् वा’। 'तप:स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग:’ उसके पश्चात् अष्टांग योग का पालन। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। यह अष्टांग योग का अभ्यास साधक को आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वोच्च स्थिति तक पहुँचाने में पूर्ण सक्षम व अद्वितीय उपाय है। गुरु शरणागति भी अध्यात्म में अत्यन्त सहायक व अचूक उपाय है, मगर यदि मन में अहंकार प्रबल है तब यह बहुत कठिन भी हो जाता है क्योंकि गुरु का प्रथम रूप है यम अर्थात् मृत्यु। वह अहंकार को मार देता है। गुरु और अहंकार दोनों साथ नहीं रह सकते।
आइये! इन उपरोक्त उपायों में से जो भी हमें अनुकूल लगे उसी को सम्बल बनाकर इस विश्व योग दिवस पर हम योगमार्ग के पथिक बनकर अपने सच्चे लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लेकर यात्रा प्रारम्भ करें।
श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि योग का प्रारम्भ सद्विचार से होता है और समाप्ति सदाचरण पर होती है। अर्थात् जो सिद्धान्त आचरण में नहीं उतरते वे जीवन में कोई परिवर्तन घटित नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक यही बात योग के प्रणेता परम-ऋषि पतञ्जलि भी कहते हैं। वे अपने शास्त्र का प्रारम्भ ही वृत्ति अर्थात् विचार के निरोध से करते हैं 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:’। क्योंकि जैसा हमारा विचार होता है, वैसी ही अन्दर भावना निर्मित हो जाती है, जैसी भावना होती है वैसा ही हमारा वाणी, व्यवहार व आचरण होता है, जैसा हमारा आचरण होता है वैसी ही हमारी आदतें बन जाती हैं, आदतें ही सुदृढ़ होकर हमारा स्वभाव, प्रकृति या रवैया बन जाता है और स्वभावानुसार हम जो कार्य करते हैं वह हमारा भाग्य (कर्माशय) बन जाता है और जैसा कर्माशय वैसा ही हमारा यह जन्म और अगला जन्म होता है।
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Nov 2024 17:59:04
जीवन सूत्र (1) जीवन का निचोड़/निष्कर्ष- जब भी बड़ों के पास बैठते हैं तो जीवन के सार तत्त्व की बात...