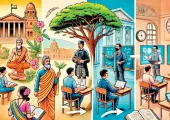आध्यात्मिक अनुसंधान: चिंतन, चुनौतियाँ एवं अवलोकन
On

डॉ. रीना अग्रवाल (हिंदी वैज्ञानिक-बी)
पतंजलि हर्बल अनुसंधान हरिद्वार, उत्तराखंड
आध्यात्मिकता को व्यक्ति के पवित्र अर्थ और जीवन में उद्देश्य की खोज के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका अर्थ व्यक्तिगत विकास, धार्मिक अनुभव, अलौकिक क्षेत्र या मृत्यु के पश्चात विश्वास की खोज करना अथवा अपने ‘आंतरिक आयाम’ को समझना हो सकता है। आध्यात्मिक का अर्थ ‘आत्मा के विषय’ से है जो पुरानी फ्रांसीसी स्पिरिचुअल (12वीं शताब्दी) व लैटिन स्पिरिचुअलिस से लिया गया है। आध्यात्मिक होने का अर्थ भौतिकता से परे होना, उस परमात्मा अनुभव कर पाना। यदि हम सृष्टि के सभी प्राणियों में उसी परमसत्ता के अंश को देखते हैं जो हममें है, तो वास्तव में हम आध्यात्मिक हैं।
अध्यात्म का अर्थ ‘स्वयं का अध्ययन’ या आत्मा का अध्ययन
‘अध्यात्म’ का शाब्दिक अर्थ आत्मा से संबंध, आत्मबोध, आत्मा-परमात्मा संबंधी विचारों से है। अध्यात्म का अर्थ ‘स्वयं का अध्ययन’ या आत्म अध्ययन से है अर्थात ईश्वरीय आनंद की अनुभूति प्राप्त करने का मार्ग ही अध्यात्म है। अध्यात्म मनुष्य को स्वयं के अस्तित्व से जोडऩे एवं उसकी सूक्ष्म विवेचन करने में समर्थ बनाता है। वास्तव में, आध्यात्मिक होने का अर्थ मनुष्य के अपने अनुभव के धरातल पर यह जानता है कि वह स्वयं ही अपने आनंद का स्रोत है, आनंद उसके अंतर में व्याप्त है।
मूल शब्द अध्यात्म में ‘इक’ प्रत्यय लगाने से ‘आध्यात्मिक’ शब्द बना है। मन की शांति ही धार्मिक भक्ति पूर्ण, पवित्र प्रेम एवं आध्यात्मिक सुख है। अध्यात्म और भक्ति में क्या अंतर है! धार्मिक भक्ति में भक्त के मन में शरणागत एवं समर्पण का भाव सर्वोपरि होता है वहीं अध्यात्म में जिज्ञासु के अंतर में ‘अहंब्रह्मस्मि’ का भाव व्याप्त होता है। भक्ति-भावना में भक्त के मन में अपने इष्ट के प्रति जिज्ञासा अथवा संदेह नहीं होता है, कदाचित पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण का भाव समाहित होता है।
व्यापक रूप से ‘पवित्र प्रेम’ का अर्थ व्यक्तिगत मान्यताओं, व्यक्तिगत दृष्टिकोण और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर भिन्न हो सकता है। आमतौर पर यह प्रेम के उस रूप को संदर्भित करता है जिसे पवित्र, दिव्य एवं आध्यात्मिक रूप से महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
आध्यात्मिक प्रेम एवं पारलौकिक साझेदारी
आध्यात्मिक प्रेम और पारलौकिक साझेदारी, दोनों में आत्माओं के मध्य ‘एकता की भावना’ है। यह संबंध भौतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है अपितु अध्यात्म और आध्यात्मिक आयामों तक फैला हुआ है जो समकालिक भावना हो सकती है जहाँ घटनाएँ एवं परिस्थितियाँ इस तरह से संरेखित होती हैं जो संयोग से परे हैं।
आध्यात्मिक पवित्रता से ही दया, सच्चाप्रेम, भक्ति, उदारता, परोपकार की भावना जागृत होती है और देवत्व का विकास होता है। प्राय:लोगों में तमोगुण-रजोगुण की प्रधानता होती है। आध्यात्मिक साधना सत गुण को विकसित करती है। सत गुण बुद्धि ही मनुष्य को जीवंत प्राण धन, ओजस्वी-तेजस्वी और वर्चस्व से पूर्ण बनाती है। भगवान श्रीकृष्ण के प्रेम पर उद्धरण, ‘प्रेम ऐसी भावना है जो भौतिकता से परे है आध्यात्मिक और शाश्वत है। बिना शर्त के प्रेम करना, बिना कारण के देना, बिना अपेक्षा के परवाह करना औरबिना विचार के बात करना, यही निस्वार्थ प्रेम भावना है।’
आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है कि वह सदैव प्रसन्न और दूसरों के प्रति दयालु रहते हैं। उन्हें किसी को भी कमतर समझना या उनकी आलोचना करना पसंद नहीं होता है। इसके साथ ही वे दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने की आशा में प्रेरणा देते हैं। यदि आप ऐसे ही मूल्यों में विश्वास रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप आध्यात्मिक हैं। अध्यात्म मनुष्य को स्वयं के अस्तित्व के साथ जोडऩे और सूक्ष्म विवेचन करने में समर्थ बनाता है। आध्यात्मिक होने का अर्थ यही है कि व्यक्ति अपने अनुभवों से जानता है कि वह अपने आनंद का स्रोत ‘स्वयं’ है। आध्यात्मिकता का संबंध हमारे आंतरिक जीवन से है जो व्यक्ति अपने घर-परिवार में शांति पाता है वहीं सबसे सुखी और प्रसन्न है।
गीता का सार ‘प्रेम करुणा, दया और शांति से भरपूर’
मनुष्य की अपनी आत्मा को अध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों के दैहिक व्यक्तित्व से संबंधित कर्मों और उनकी विकास प्रक्रिया को कर्म या सकाम कर्म कहा जाता है। अध्यात्म के तीन तत्व ब्रह्म, जीव और माया हैं। गीता का यह सार हमें बताता है, ‘सबसे अच्छा प्रेम दया, करुणा और शांति से भरा होता है। ‘इसमें कहा गया है कि इन गुणों वाला व्यक्ति भौतिक वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता, सम्पत्ति अथवा अभिमान से नहीं बंधा रहता और खुले अंत:करण से ईश्वर की प्रार्थना करता है। वास्तव में, ईश्वर ऐसे मनुष्यों को प्रेम करते हैं उनकी देखभाल करते हैं।
आध्यात्मिक शक्ति पाने के लिए हम जीवन में विशेष रूप से पाँच तथ्य; स्वीकार भाव, संयम, सहयोग, नैतिकता और ध्यान को आत्मसात कर प्राप्त कर सकते हैं, हम जीवन पर्यंत, प्रतिपल असंतुष्ट और शिकायती भाव में जीते हैं, यही तनाव का एक मुख्य कारण है। अत: हमें संतुष्टि भाव में जीने की आदत धीरे-धीरे डाल लेनी चाहिए।
आध्यात्मिक जीवन जीने का विवेकपूर्ण तरीका
आध्यात्मिक प्रक्रिया तक पहुँचने के तीन माध्यम हैं। प्रथम, आप कुछ जीवनकालों के दौरान सही चीजें करते हुए धीरे-धीरे वहाँ तक पहुँच सकते हैं, द्वितीय, आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों में बने रहें, अपनी ओर से सर्वोत्तम कार्य करें, स्वयं को खुला व केंद्रित रखें और उस प्रक्रिया के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएँ। यहाँ आध्यात्मिक होने का अर्थ औसत से ऊपर उठना है। यह जीने का एक विवेकपूर्ण तरीका है, इसके लिए जन्मों तक साधना करनी पड़ती है। ऐसा चिंतन अधिकतर लोगों में प्रतिबद्धता और एकाग्रता की कमी के कारण होता है। इसका तृतीय माध्यम साधना है, जो एक ऐसी विधि है जिससे पूर्ण जागरूकता से आध्यात्मिक विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है। आध्यात्मिकता न तो मनोवैज्ञानिक और न ही सामाजिक प्रक्रिया है। यह पूर्ण रूपेण अस्तित्व से जुड़ी है।
यदि हम किसी भी कार्य में पूरी तन्मयता से डूब जाते हैं तो आध्यात्मिक प्रक्रिया वहीं प्रारंभ हो जाती है भले ही वह कार्य झाड़ू लगाना ही क्यों न हो! किसी वस्तु को सतही रूप से जानना सांसारिकता और गहराई तक जानना आध्यात्मिकता है।
तंबाकू, धूम्रपान, मदिरापान और नशे की प्रवृत्ति का त्याग
मन की शक्ति वृद्धि के लिए प्रतिदिन ध्यान अभ्यास करने से मानसिक शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट का ध्यान किया जा सकता हैं। इससे तन-मन की अद्भुत शांति के साथ-साथ मस्तिष्क का विकास भी संभव है। प्रात: उठकर ध्यान और प्राणायाम किया जा सकता है। आयु बढऩे के साथ-साथ मस्तिष्क के स्वास्थ्य में भी गिरावट आती है फलस्वरूप स्मरण क्षमता का ह्रास होने लगता है। ऐसे में अकसर कुछ लोग दवाइयाँ लेने लगते हैं। नित-प्रतिदिन कसरत और ध्यान करके मस्तिष्क के स्वास्थ्य का विकास किया जा सकता है। सदैव तंबाकू, धूम्रपान, मदिरापान और अन्य नशे की प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। इनसे फेफड़ों को नुकसान पहुँचता है और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को भी हानि पहुँचती है। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन ग्रहण करना चाहिए जो सदैव से उत्तम स्वास्थ्य का कारक है। उत्तम मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए अपनी खुराक में सूखे मेवे, जैतून का तेल, स्वास्थ्यवर्धक नव-आविष्कृत तत्व, खनिज तत्व युक्त भोज्य पदार्थ, मछली और प्रोटीन को सम्मिलित करें और जब हम तनाव ग्रस्त या कुंठाग्रस्त होते हैं तब भी मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अत: तनाव मुक्त रहकर मस्तिष्क के स्वास्थ्य में वृद्धि की जा सकती है। आजकल लोगों, विशेषकर युवा वर्ग ने आध्यात्मिकता से एक तरह की दूरी बना ली है। इसका कारण आध्यात्मिकता को अनुचित तरह से प्रस्तुत करना है। कुछ लोग आध्यात्मिकता का मतलब स्वयं को कष्ट देना, अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करना, जीवन से पलायन एवं जीवन विरोधी मानते हैं। बहुधा यह भी माना जाता है कि आध्यात्मिक लोगों को जीवन-आनंद लेने की मना ही है उनके लिए हर प्रकार से कष्ट सहन करना आवश्यक है जबकि सच्चाई यह है कि आध्यात्मिक होने का वाह्य जीवन से कोई लेना-देना नहीं है।
अब प्रश्न आता है कि ‘एक आध्यात्मिक और संसारी मनुष्य’ में क्या अंतर है? इसका उत्तर ‘एक संसारी मनुष्य केवल अपना भोजन कमाता है’ बाकी सब कुछ जैसे; प्रेम, प्रसन्नता, आनंद और शांति के लिए उसे दूसरों की भीख पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके विपरीत ‘एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी शांति, प्रेम और प्रसन्नता सब कुछ स्वयं कमाता है’और केवल भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है किंतु यदि वह चाहे तो अपना भोजन भी कमा सकता है। इन लक्षणों से समझने में सरलता होगी कि आध्यात्मिकता आखिर है क्या और एक आध्यात्मिक मनुष्य कैसा होता है!
नियमित ध्यान और योग, दिव्य शक्ति को जाग्रत करने का मार्ग
नियमित ध्यान और योग करने से मानसिक शांति और आत्मबल बढ़ता है जिससे दिव्य शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। सत्संग, आध्यात्मिक गुरुओं और संतों के सत्संग में भाग लेने से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है जो दिव्य शक्ति को जाग्रत कर सकता है। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए अग्र लिखित उपाय किए जा सकते हैं-
-
अपने चित्त को शांत रखें, अशांत चित्तकभी शक्तिशाली नहीं हो सकता है।
-
सकारात्मक चिंतन करें, सकारात्मक विचार मन को शक्ति एवं शांति प्रदान करता है।
-
स्वयं पर विश्वास रखें, इससे अंतर्मन को सुदृढ़ता एवं शक्ति प्राप्त होती है।
-
अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को निर्धारित कर उन पर ध्यान केंद्रित करें।
प्रसन्नता मनुष्य का सबसे बड़ा सुख
प्रसन्नता, संसार का सबसे बड़ा सुख है जो प्रसन्न है वह सुखी है और जो सुखी है वह अवश्य ही प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न मन ही आत्मा के स्वरूप को देख सकता है, परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है और जीवन के समस्त सुखों को प्राप्त कर सकता है। जीवन को हर प्रकार से सफल बनाने के लिए प्रसन्न रहना आवश्यक है। आध्यात्मिकता का किसी धर्म, संप्रदाय या मत से कोई लेना-देना नहीं। हम स्वयं अंदर से कैसे हैं आध्यात्मिकता इसके विषय में है। आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप मंदिर, मस्जिद या गिरिजाघर में करते हैं। यह केवल आपके अंदर ही घटित हो सकती है। आध्यात्मिक प्रक्रिया ऊपर या नीचे देखने के बारे में नहीं है।
निष्कर्ष
निष्कर्षात्मक रूप से कहा जा सकता है कि एक आध्यात्मिक वह व्यक्ति होता है जो दुनिया के भौतिक पहलुओं से परे जीवन, अस्तित्व और उद्देश्य की गहन समझ चाहता है। आध्यात्मिक होने में अक्सर अपने आंतरिक मूल्यों और स्वयं से अधिक महान किसी चीज़ से संबंध की खोज करना सम्मिलित है जिसकी व्याख्या धार्मिक, दार्शनिक या पारलौकिक शब्दों में की जा सकती है। मनुष्य में अद्भुत शक्ति होती है जो विभिन्न कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है, इसमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियाँ सम्मिलित होती हैं। ये ध्यान, प्रार्थना एवं अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों से प्राप्त की जा सकती हैं।
अंत में, जिसमें आत्मा, ब्रह्म तथा स्वरूप का विचार या विवेचन हो, परमात्मा या आत्मा, अध्यात्म से संबंध रखने वाला हो और भौतिकता एवं लौकिकता से भिन्न हो, वही आध्यात्मिक समझ और ज्ञान से सुसंस्कृत है, मनुष्य के आंतरिक ‘स्व’ और ‘ईश्वर’ से गहन जुड़ाव से आता है। यह भौतिक जगत से परे देखने और सभी वस्तुओं से पारस्परिक संबंधों को समझने की क्षमता है। आध्यात्मिकता का संबंध हमारे अंत:करण से है।
अंतत: आध्यात्मिकता स्वयं को जानने एवं समझने में सहायक है बिना आत्मज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान के मनुष्य एक दिशा विहीन नाव की भाँति है।
लेखक
Related Posts
Latest News
01 Dec 2024 18:59:48
योग प्रज्ञा योग - योग जीवन का प्रयोजन, उपयोगिता, उपलब्धि, साधन-साधना-साध्य, सिद्धान्त, कत्र्तव्य, मंतव्य, गंतव्य, लक्ष्य, संकल्प, सिद्धि, कर्म धर्म,...








.jpg)